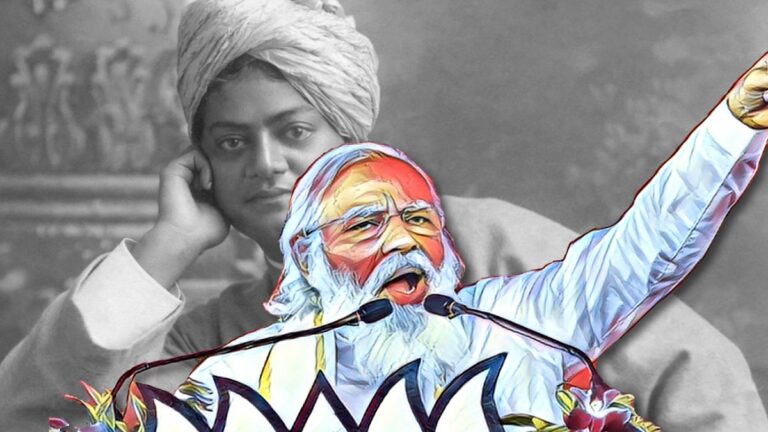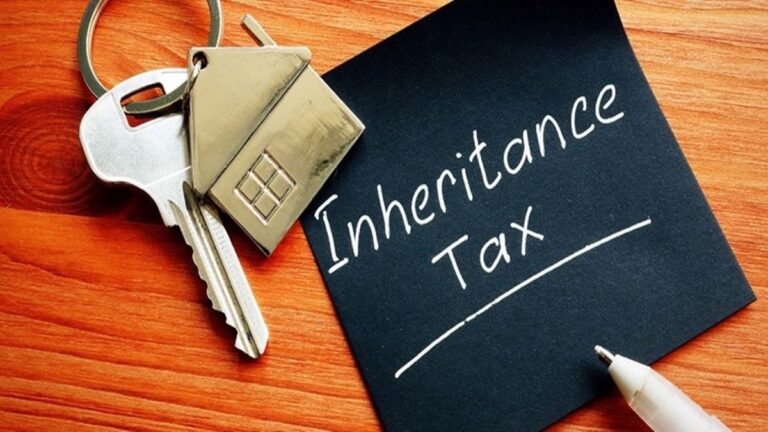चर्चित मार्क्सवादी दार्शनिक जॉर्ज लुकाच ने एक बार कहा था, “सबसे खराब समाजवाद भी सबसे अच्छे पूंजीवाद से बेहतर है।” 1969 में की गई और 1971 में दोहराई गई लुकाच की यह टिप्पणी, जो उस समय के सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के अनुभव पर आधारित थी, उस दौर में पश्चिमी वाम खेमे में भी संदेह की नजर से देखी जाती थी। लेकिन जिस तरह भारत और तीसरी दुनिया के अन्य आप्रवासियों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर सेना के जहाजों में भरकर डिपोर्ट किया गया, उसने लुकाच के इस बयान को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। तत्कालीन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के समाजवाद में कम से कम दो ऐसे स्पष्ट आकर्षक पहलू थे, जो इसे पूंजीवादी देशों से अलग करते थे।
हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर लाने की प्रक्रिया में एक ओर विश्व के नेतृत्वकारी पूंजीवादी देशों की नफरत, विशेषकर नस्लीय नफरत, स्पष्ट थी, जो समाजवादी देशों में आधिकारिक रूप से बिल्कुल नहीं थी। यह सर्वविदित है कि समाजवादी देशों में, सरकारी नीति के अभाव में भी, जनता के बीच कुछ नस्लीय पूर्वाग्रह मौजूद हो सकते थे। समाजवाद के खत्म होने के बाद वहां नस्लीय भावनाएं खुलकर सामने आईं।
दूसरी ओर, यह भी सच है कि विकसित पूंजीवादी देशों में प्रगतिशील ताकतें अधिक सहिष्णु और नस्लीय रूप से समावेशी समाज बनाने के लिए कठिन प्रयास कर रही हैं। बेशक, बहुत से लोग आप्रवासियों को जिस अमानवीय तरीके से डिपोर्ट किया गया, उसे पूंजीवाद से न जोड़कर ट्रंपवाद से जोड़ेंगे, यानी उस नव-फासीवादी गिरोह की चरम अमानवीयता से, जो इस समय वहां सत्ता में है।
हालांकि यह सच है कि ट्रंपवाद और पूंजीवाद एक नहीं हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह भिन्न और अलग परिघटनाएं मानना भी सही नहीं होगा। आज के दौर में नस्लवाद साम्राज्यवाद का ही उत्पाद है, और उत्पादन पद्धति के रूप में पूंजीवाद की कल्पना साम्राज्यवाद के बिना नहीं की जा सकती। यहां तक कि पूंजीवाद के भीतर की प्रगतिशील प्रवृत्तियां भी साम्राज्यवाद को अतीत की शोषणकारी और हानिकारक परिघटना के रूप में अस्वीकार नहीं करतीं।
बल्कि, वे इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखती हैं, जो सुदूर समाजों में प्रगति और आधुनिकता लेकर आई। इस विचार में यह अंतर्निहित है कि ऐसे समाज स्वयं प्रगति और आधुनिकता नहीं ला सकते। साम्राज्यवाद को एक सौम्य प्रक्रिया के रूप में देखना वास्तव में उस नस्ल को श्रेष्ठ मानने का परिणाम है, जो साम्राज्यवादी अभियानों में शामिल थी।
वर्तमान पूंजीवादी केंद्रों में मौजूद प्रगतिशील प्रवृत्तियों के इरादे चाहे जितने नेक हों, जब तक वे साम्राज्यवाद को स्पष्ट रूप से नकारती नहीं हैं, वे नस्लवाद के दाग से मुक्त नहीं हो सकतीं। यह तथ्य आज भी दो घटनाओं से स्पष्ट है, जिनमें प्रगतिशील तत्व भी उन दो युद्धों का समर्थन करते हैं, जिन्हें सभी प्रमुख पूंजीवादी केंद्र समर्थन दे रहे हैं। इनमें से एक युद्ध एक पूरे देश की जनता के नस्लीय सफाए के लिए है, तो दूसरा साम्राज्यवादी खेमे के विस्तार के लिए।
दूसरे शब्दों में, नस्लवाद बड़े पूंजीवादी केंद्रों में अंतर्निहित है-न केवल लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रहों के रूप में, बल्कि शासक वर्ग के उदारवादी खेमे के भीतर भी। पूंजीवादी संकट के दौर में यह नया आवेग ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इजारेदार पूंजी कुछ असहाय आप्रवासी समूहों को ‘पराया’ ठहराने के लिए इसका उपयोग करती है, ताकि अपने वर्चस्व को मिल रही चुनौतियों का मुकाबला कर सके और मजदूर वर्ग को विभाजित कर सके।
इसके विपरीत, संकट के समय तत्कालीन समाजवादी सरकारें और उनका शासक वर्ग पूरी तरह नस्लवाद के खिलाफ था, और समाज में ऐसी किसी भी अभिव्यक्ति को सख्ती से दबा देता था। बहुत से लोग इसे विचार थोपना कह सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि, चाहे इसे थोपना माना जाए या नहीं, इसने ट्रंपवाद जैसी किसी चीज के उभार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी।
अब दूसरे पहलू पर विचार करें, जिसमें अब तक का समाजवाद अपने को बेहतर साबित करता है-वह है पूर्ण रोजगार की उपलब्धि। इसने उस मुख्य भौतिक कारक, बेरोजगारी, का अंत कर दिया, जो विकसित पूंजीवादी देशों की जनता में आप्रवासियों के खिलाफ नाराजगी का प्रमुख कारण है। तीसरी दुनिया के देशों के आप्रवासी अमेरिका जैसे देशों में जाने की इच्छा इसलिए रखते हैं, क्योंकि उनके मूल देशों में भयावह बेरोजगारी की मार पड़ती है। यह सच है कि पलायन करने वाले लोग जरूरी नहीं कि एकदम दरिद्र हों।
यह तथ्य कि प्रत्येक प्रवासी को ‘डंकी रूट’ से अमेरिका में प्रवेश के लिए बिचौलियों को 45 लाख रुपये तक देने पड़ते हैं, दर्शाता है कि उनके पास कुछ संसाधन थे। लेकिन निश्चित रूप से, उनकी पलायन की इच्छा के पीछे दो प्रमुख कारण थे: पर्याप्त वेतन वाले सम्मानजनक रोजगार का अभाव, और उनके समाज में व्याप्त आय की भारी असमानता, जो तुलना करने पर उनकी भौतिक स्थिति के प्रति गहरा असंतोष पैदा करती है। ये दोनों स्थितियां पूंजीवादी निर्माण की परियोजना का परिणाम हैं।
चाहे देश की जीडीपी विकास दर कितनी भी अधिक हो, या जीडीपी का आकार कितने ही ट्रिलियन तक पहुंच जाए, ये कारक हमेशा मौजूद रहेंगे। इसलिए, आबादी के एक हिस्से में पलायन की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। यह अत्यंत शर्मनाक है कि आजादी के 75 साल बाद भी लोग इतनी हताशा के साथ विदेश भागना चाहते हैं, जिसमें इतने बड़े खतरे शामिल हैं कि उन्हें पिंजरे में बंद जानवरों की तरह बांधकर वापस भेजा जा सकता है। तीसरी दुनिया के देशों में पूंजीवाद के निर्माण का यह अपरिहार्य परिणाम है।
दूसरी ओर, ट्रंप जैसे व्यक्ति आप्रवासियों को इस तरह डिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि अमेरिका स्वयं आप्रवासियों द्वारा बसाया गया देश है। इंग्लैंड से आए लोगों ने वहां के मूल निवासियों की जमीन छीनकर इसे बनाया, और आज यह बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का गढ़ बना हुआ है। पूंजीवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत यह गलत दावा करता है कि दीर्घकाल में पूंजीवाद का विकास वहां की श्रमशक्ति की वृद्धि दर पर निर्भर करता है। यदि यह दावा सच होता, तो अमेरिका में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आप्रवासियों का स्वागत किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बेरोजगारी का कोड़ा ट्रंप के इस कठोर कदम को और लोकप्रिय बना रहा है।
वास्तव में, स्थिति की विडंबना यह है कि जर्मनी में वामपंथी धड़ा, जो मूल पार्टी से अलग होकर बना, उसे भी आप्रवासियों पर वही रुख अपनाना पड़ा, जो वहां का दक्षिणपंथी शासक वर्ग ले रहा है। बेरोजगारी का प्रभाव इतना व्यापक है कि यह आप्रवासियों के मूल देशों को भी प्रभावित करता है और जहां वे प्रवास के लिए जा रहे हैं, वहां भी। यह पूंजीवाद के साथ सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो संकट के समय भयावह रूप ले लेती है, जैसा कि वर्तमान में देखा जा रहा है।
यही उस अमानवीयता की जड़ है, जिसे हम आज देख रहे हैं, जहां इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें हथकड़ियों-बेड़ियों में बांधकर डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके विपरीत, समाजवादी देश इससे पूरी तरह मुक्त थे। उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उनके यहां श्रमशक्ति की कमी थी।
हंगरी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यानोश कोर्नाई, जो संयोगवश समाजवादी नहीं थे, ने माइकल कालेकी का अनुसरण करते हुए मांग की कमी और संसाधन की कमी वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर रेखांकित किया था। उन्होंने बताया कि जहां पूंजीवाद मांग की कमी वाली व्यवस्था है, वहीं समाजवाद संसाधन की कमी वाली व्यवस्था है।
इसका एक निहितार्थ यह था कि समाजवादी समाज अभाव, खरीद के लिए लंबी कतारों और राशनिंग वाले समाज थे। वे अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए जितना उत्पादन करते थे, वह उस समय की जनता की क्रयशक्ति से कम था। इसका अर्थ था कि श्रमशक्ति सहित सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा था।
आधुनिक युग में केवल समाजवादी समाज ही ऐसे थे, जहां पूर्ण रोजगार था। वहां श्रम की मांग इतनी अधिक थी कि उसकी पूर्ति महिलाओं के श्रम में भारी वृद्धि से होती थी, जिसके गहरे सामाजिक निहितार्थ थे। रोजगार उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ आत्मसम्मान भी बढ़ाता था, जबकि बेरोजगारी आत्महीनता का बोध पैदा करती है। उस समय के समाजवादी समाजों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसमें वाम खेमे के लेखक भी शामिल हैं। उस व्यवस्था के विध्वंस के साथ यह धारणा बनाई गई कि हमारे जैसे समाजों में पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है।
सच्चाई यह है कि जब तक हम पूंजीवाद में जी रहे हैं, हम अरबपति पैदा कर सकते हैं, लेकिन औपनिवेशिक दौर की तरह निम्न वर्गीय भारतीय होने का अपमान हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आम मेहनतकशों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता रहेगा। उनमें से कुछ बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे देशों में जाते रहेंगे और इसी तरह हथकड़ियों-बेड़ियों में बांधकर वापस भेजे जाते रहेंगे।
केवल एक समाजवादी समाज, जो अतीत की गलतियों से सीखते हुए हम आज अपने देश में बनाने की बेहतर स्थिति में हैं, बेरोजगारी की विपदा का मुकाबला कर सकता है और अपने लोगों को पिंजरे में बंद जानवरों की नियति से बचा सकता है।
(साभार: People’s Democracy, अनुवाद: लाल बहादुर सिंह)