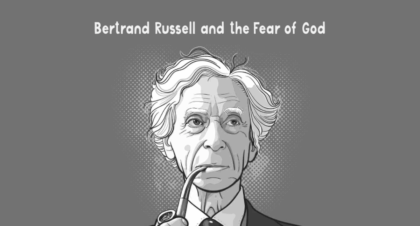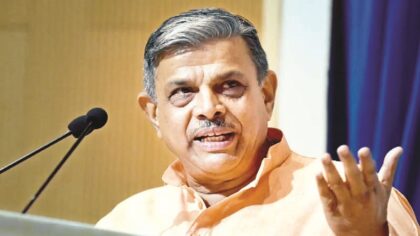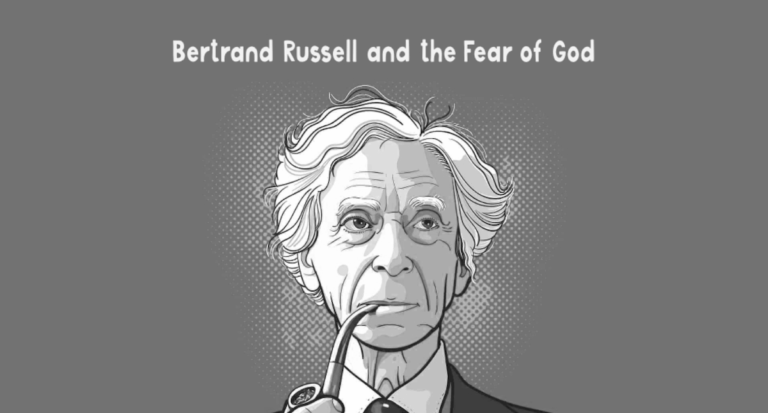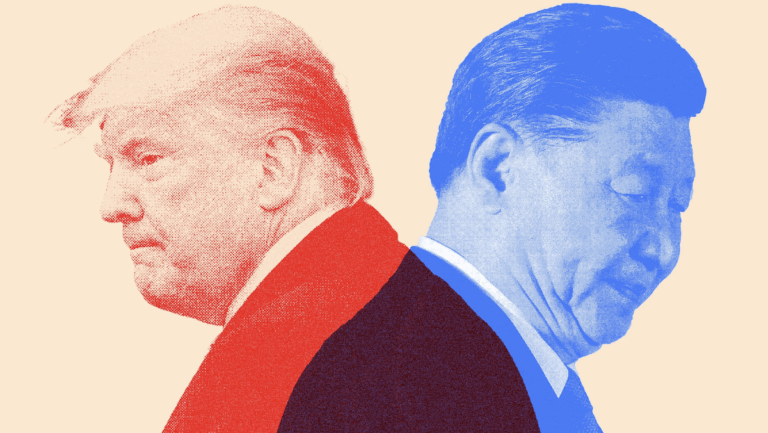बागेश्वर। एक दिन दोपहर के समय में हम दोनों भाई बहनों की खाना खाने के बाद आपस में बात हो रही थी तभी भाई साहब ने मुझे मंदिर में रखे तांबे के बर्तनों की सफाई करने को कहा, सफाई के दौरान मेरी नजर उन बर्तनों पर बनी कलाकारी पर पड़ी। उन कलाकारियों को देखकर मैं सचमुच में हैरान थी जिसके बाद मुझे यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर यह तांबे के बर्तन बनते कहां और कैसे हैं? फिर क्या था इसी सवाल को लेकर मैं अपने अन्य जानकार साथियों के पास पहुंची। उन्होंने मुझे बताया कि बागेश्वर में आज भी एक ऐसा गांव मौजूद है जहां कई प्रकार के तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं लेकिन निराश करने वाली बात यह थी कि वहां केवल दो-तीन लोग ही अब बचे हैं जो वर्तमान में तांबे के बर्तन बनाने का काम कर रहे थे लेकिन इतनी जानकारी से भला मैं कहां संतुष्ट होने वाली थी। मैंने अगले दिन योजना बनायी और फिर पहुंच गयी ताम्र शिल्पियों के इस गांव में।
गांव में पहुंचकर मैंने उस गांव के ग्राम प्रधान से बात की और कड़कती धूप में ग्राम प्रधान भी हांफते-हांफते आए और उन्होंने मुझे सुंदर जी के घर पहुंचा दिया। दरअसल सुंदर जी ही वह व्यक्ति हैं जो आज भी ताम्र कला की पुरानी विरासत को संजोए हुए हैं।

उनकी कला सचमुच में हैरान करने वाली थी क्योंकि इस प्रकार की कला बनाते हुए मैंने कभी नहीं देखा था लेकिन आज मैं इन कलाओं को अपने सामने एक व्यक्ति को बनाते हुए देख रही थी। दरअसल इस गांव का इतिहास काफी पुराना है। आज़ादी के पहले से ही खर्कटम्टा गांव को ताम्र शिल्पियों के नाम से जाना जाता था। आजादी से पहले खर्क टम्टा समेत देवलधार, जोशीगांव, टम्टयूड़ा, बिलौना आदि गांव में ताम्र शिल्प से तांबे के परंपरागत तरीके के बर्तन जैसे गागर, तौले, वाटर फिल्टर, पूजा सामग्री धार्मिक अनुष्ठान एवं वाद्ययंत्र, तुरही, रणसिंघी बनाते थे। साथ ही इन कामों में महिलाएं भी उनकी मदद किया करती थीं।
लेकिन जैसे-जैसे नवीनीकरण का दौर आया तो यह कला कुछ बुजुर्गों तक सिमट कर रह गई। निराशा का यह भाव सुंदर जी के चेहरे पर भी देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी इस काम को सीखने की इच्छुक नहीं है। उनका कहना था कि वो और उनके कुछ साथी गांव में हाथ से तांबे के बर्तन बनाने का काम करते हैं। लेकिन कोरोना उन लोगों के लिए कहर साबित हुआ। अच्छा-खासा कारोबार डूबने लगा और एक बार जो पीछे गया तो अभी तक उससे उबर नहीं पाया है।

वहीं पुराने दिनों को याद करते हुए सुंदर जी बताते हैं कि करीब तीन-चार सालों तक उन्होंने रामनगर के कई बनियों के साथ काम किया। उस दौरान तांबे के बर्तनों की काफी मांग थी। तब नेपाल समेत बड़े महानगरों में काफी सामान जाता था। बाद में हम अपने गांव चले आए और यहां हमने मिलकर काम शुरू किया था तब 50 से 60 रुपये तक की बिक्री प्रतिदिन हो जाया करती थी लेकिन अब काम कम हो गया है और इसी बीच नई युवा पीढ़ी का मशीनों की तरफ झुकाव बढ़ता गया लेकिन आज भी हाथ से बने तांबे के बर्तनों को काफी शुद्ध और मजबूत माना जाता है।
उनसे बात करने पर मालूम पड़ा कि पुराने जमाने में आम तौर पर तांबे एवं पीतल के बर्तनों का दैनिक कार्यों में भरपूर इस्तेमाल किया जाता था लेकिन तांबे के बर्तनों के संबंध में जानकारी ना होने की वजह से बहुत कम लोग हाथ से बने बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने यह भी साफ तौर पर बताया कि तांबे के बर्तनों को हाथ से बनाने में काफी मेहनत लगती है। बातों-बातों में वे हमें अपने कारखाने की तरफ ले गए जो उनके घर के ठीक बगल में था। कारखाने में उनकी जरूरत के बहुत सारे औजार रखे हुए थे उनमें से एक पंखे की तरह दिखने वाला चरखा था जिसे घुमाने पर उसकी हवा से भट्टी में आग जलती थी और उस भट्टी में तांबे की चादर को गरम किया जाता है और फिर उसे हथौड़े से पीट-पीटकर बर्तन के आकार में उसे साधा जाता है। जिसमें उनका कभी तो एक-दो घंटे या फिर कभी पूरा दिन का समय लग जाता था।

हालांकि ताम्र व्यवसाय को पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एससीएसटी हब योजना बनाई थी ताकि ताम्र शिल्पियों को इसका फायदा मिल सके। इस योजना के तहत हस्त निर्मित तांबे से बने पूजा पात्रों को चार धाम में बेचने की योजना बनाई गई थी। अब यह अलग बात है कि इस योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा या फिर ये काम भी मशीनों के हवाले कर दिया जाएगा। शिल्प कारीगर सुंदर लाल और उनके साथियों को उनकी शिल्प कला के लिए पूर्व में उत्तराखंड सरकार के साथ ही उद्योग विभाग से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद उनकी सुध किसी ने नहीं ली। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो आजीविका के लिए हाथ से तांबे के बर्तनों पर अपना हुनर निखार रहे हैं। उन्हें भी मलाल बस इस बात का है कि उनकी कला धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है जबकि वे अब तक कई विभागों से कह चुके हैं कि वे मुफ्त में अपनी जमीन युवाओं को ट्रेनिंग के लिए देने के लिए तैयार हैं।
वह इस सिलसिले में सरकार से निवेदन की मुद्रा में कहते हैं कि ताम्र व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और इसे पहचान दिलाने के लिए सरकार को शिल्प ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। और नयी पीढ़ी को ताम्र शिल्प की बारीकियां सिखा कर उसे भी क्षेत्रीय रोजगार से जोड़ा जा सकता है। और इस तरह से उत्तराखंड में विलुप्त हो रहे ताम्र शिल्प को प्रदेश के साथ ही देश-विदेश तक पहुंचाया जा सकता है। ताम्र शिल्प को एक पहचान मिल सके और पहचान के साथ ही यह युवाओं और कई ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार की सीढ़ी बन सके।
इन सब बातों के बाद हमने सुंदर जी और उनके गांव से अलविदा ली और वास्तव में सुंदर जी की मेहनत देखकर हमें महसूस हुआ कि वास्तविक मेहनत पुराने जमाने के लोगों द्वारा की जाती थी। हम तो बस मशीनों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। और मशीनों के इशारों पर काम करते हैं लेकिन आज भी दुनिया में सुंदर जी जैसे लोग हैं जो आज भी सालों पुरानी परंपराओं को अपनी मेहनत और हुनर के बल पर संजोए हुए हैं। उम्मीद है कि सरकार और आला अधिकारियों को निश्चित ही सुंदर जी जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जिससे कि ऐसे मेहनती लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और हमारी युवा पीढ़ी को भी अपनी पुरानी परंपराओं व कला के बारे में जानकारी मिल सके।
हालांकि तांबे के बर्तन आज भी बाजार में दिखते तो हैं लेकिन दुकानदारों से बात करने पर मालूम हुआ कि ये बर्तन महानगरों में बनी फैक्ट्रियों से मंगाए जाते हैं। वहां से लाकर इन्हें बाजारों में बेचा जाता है लेकिन सुंदर जी ने बताया कि बाजारों में मिलने वाले तांबे के बर्तनों और हाथ से बनाए हुए तांबे के बर्तन में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि हाथ से बनाए हुए तांबे के बर्तन काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं जो सालों साल चलते हैं जबकि मशीनों द्वारा बनाए गए तांबे के बर्तनों में मजबूती और शुद्धता की कमी होती है।
(बागेश्वर, उत्तराखंड से लता प्रसाद की रिपोर्ट।)