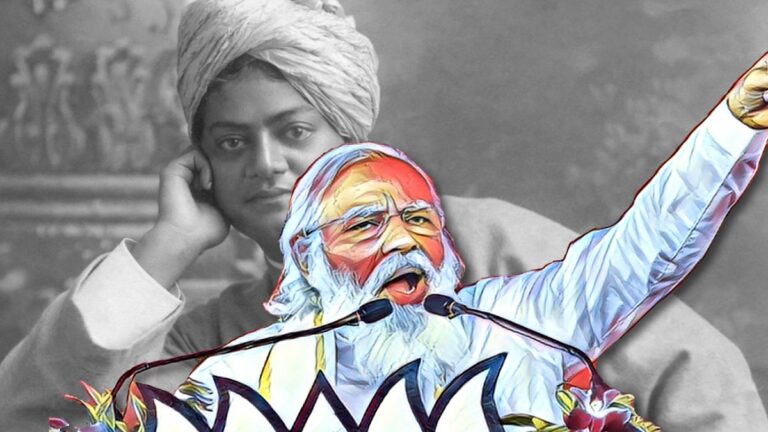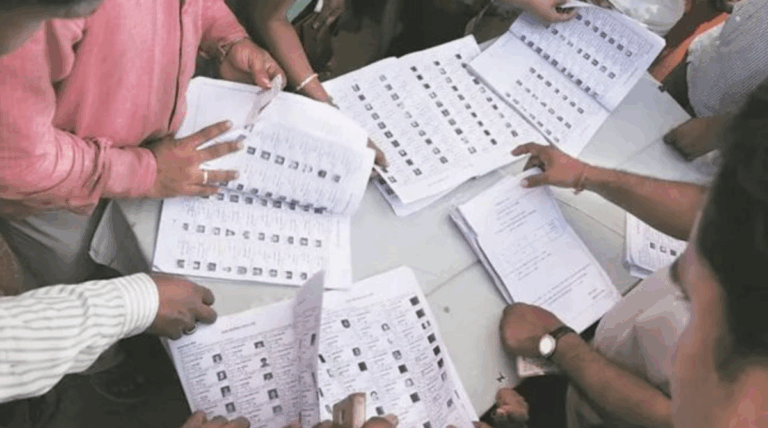फ्रेंच अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी के भारत आने का यह लाभ हुआ कि इससे बढ़ती आर्थिक गैर-बराबरी का मुद्दा (कम-से-कम मीडिया की) चर्चा में आया।
पिकेटी का स्टार वैल्यू है। 2013 में आई उनकी किताब Capital in 21st century ने तथ्यों और आंकड़ों से बताया था कि पिछले चार-साढ़े चार दशकों में दुनिया में किस तरह से आमदनी और धन की गैर-बराबरियां बढ़ती चली गई हैं और अब ये कितना विकराल रूप ले चुकी हैं।
पिकेटी ने चार दशक पहले अपनाई गई आर्थिक नीतियों को इस परिघटना के लिए जिम्मेदार बताया है। जाहिरा तौर पर ये परिघटना नव-उदारवाद पर अमल का परिणाम है।
पिकेटी ने इस बात को लगातार आगे बढ़ाया है। Capital in 21st century के प्रकाशन के साथ अपनी नई बनी हैसियत का लाभ उठाते हुए उन्होंने पेरिस में Inequality Lab नाम की बहुचर्चित संस्था की स्थापना की, जो विभिन्न देशों के बारे में विषमता की स्थिति पर लगातार रिपोर्ट जारी करती है। इस संस्था ने तथ्य संबंधी उन कमियों की भरपाई भी की, जो Capital in 21st century में रह गई थीं।
मसलन, उस किताब में भारत की बहुत कम चर्चा थी। लेकिन बाद (2015) में पिकेटी ने अर्थशास्त्री लुकस चांसेल के साथ मिल कर Inequality Lab की तरफ से भारत के बारे में एक अलग शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया कि 1947 के बाद से 1980 तक भारत में आर्थिक विषमता घटी, उसके बाद यह रुझान ठहर गया, और 1990 के बाद तो गैर-बराबरी इतनी तेजी से बढ़ी कि अब वह इतिहास के सर्वाधिक भयंकर रूप में है।
पिकेटी और चांसेल ने इस वर्ष भारत में हुए आम चुनाव से ठीक पहले अपनी उस रिपोर्ट को अपडेट करते हुए ‘ब्रिटिश राज से अरबपतियों के राज तक’ (https://wid.world/document/chancelpiketty2017widworld/) नाम से एक और रिपोर्ट जारी की थी।
उसमें उन्होंने बढ़ी विषमता के बारे में ताजा आंकड़े दिए। उन्होंने भारत सरकार को विषमता घटाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन सुझावों को नई दिल्ली में आयोजित चर्चा और कुछ अखबारों को दिए इंटरव्यू में पिकेटी ने दोहराया। उनके मुताबिक,
- गुजरे वक्त में जो देश धनी हुए, उन्होंने ऐसा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए किया। लेकिन हाल के दशकों में उन्होंने विषमता घटाते हुए ऐसा किया है।
- भारत के आंकड़ों- खासकर आर्थिक आंकड़ों- को अब दुनिया भर में संदेह की निगाह से देखा जाता है। पिकेटी ने भी भारत सरकार को सलाह दी कि वह अधिक आंकड़े जारी करे और सूचना देने के मामले में पारदर्शिता बरते। उन्होंने कहा- “आंकड़े चाहे जितने अपूर्ण हों, मगर (उनके अध्ययन से) आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तुलनात्मक कसौटियों पर भारत बेहद विषम देश है। भारत गैर-बराबरी को घटाए, तो वह गरीबी कम करने में भी सफल रहेगा।”
तो पिकेटी के सुझाव हैः
- भारत को जीडीपी-टैक्स अनुपात बेहतर करना चाहिए। वैसे तो आदर्श यह है कि यह अनुपात 50 से 55 प्रतिशत हो (यानी भारत की कुल जीडीपी जितनी है, उसके 50 से 55 फीसदी के बराबर कर वसूली हो), मगर इसे 25 से 30 प्रतिशत तक ले जाने की शुरुआत तुरंत करने की जरूरत है। अभी यह 13 से 14 प्रतिशत है।
- पिकेटी ने कहाः ‘मेरा सुझाव है कि भारत में कर न्याय (tax justice) की महत्त्वाकांक्षी योजना अपनानी चाहिए। पिछले 10 से 20 साल में सबसे धनी जिन भारतीयों ने खूब संपत्ति बटोरी है, उनसे कहा जाए कि वे अपने नए धन का एक हिस्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं में निवेश के लिए वापस करें। आप उत्पादकता खाई (productivity gap) को मजदूरों की बर्खास्तगी को आसान बना कर हासिल नहीं कर सकते- ऐसा आप ऐसे महत्त्वाकांक्षी योजना लागू कर ही कर सकते हैं।’
- व्यावहारिक उपाय के तौर पर उनका कहना है कि भारत सरकार अरबपतियों पर दो प्रतिशत का वेल्थ टैक्स लगाए, तो उससे सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो सकता है।
- भारत में हर वर्ष होने वाली कुल आमदनी का 55 से 60 फीसदी हिस्सा सबसे धनी 10 प्रतिशत आबादी की जेब में चला जाता है। उधर निचली 50 आबादी के हिस्से में लगभग 15 प्रतिशत जाता है। इससे हर साल गैर-बराबरी बढ़ रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि सबसे धनी आबादी पर अधिक टैक्स लगाया जाए। यानी कर व्यवस्था को अधिक प्रगतिशील बनाने की जरूरत है। इसका अर्थ है कि कर ढांचे में प्रत्यक्ष करों (आय कर, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, उत्तराधिकारी कर) आदि का योगदान अधिक होना चाहिए, जबकि जीएसटी जैसे परोक्ष करों का हिस्सा घटाया जाना चाहिए।
- पिकेटी का कहना है कि भारत में कर व्यवस्था में कई खामियां हैं, जिससे लोग आसानी से टैक्स की चोरी कर लेते हैं। इन खामियों को दूर कर टैक्स प्रशासन को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।
मगर इन सुझावों का तभी कोई महत्त्व होगा, अगर सरकार विषमता को कोई समस्या माने! पिकेटी इस बार एक संस्था की तरफ से आयोजित चर्चा में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आए। उस चर्चा में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन भी मौजूद थे। (मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक) नागेश्वरन पिकेटी के बाद बोले और उन्होंने पिकेटी के तर्कों का जवाब दिया। उनकी प्रमुख दलीलें रहीं-
- अधिक कर लगाया गया, तो देश से पूंजी का पलायन शुरू हो जाएगा। पूंजी को देश से भगा देना आसान है, लेकिन उससे वापस लाना बेहद मुश्किल है।
- अरबपतियों पर अतिरिक्त कर लगाने के सुझाव को ठुकराते हुए नागेश्वरन ने कहा कि ऐसे उपायों से हर समस्या हल नहीं हो सकती।
- वेल्थ टैक्स जैसे करों को लागू करना मुश्किल काम है। धन को मापना और उस पर टैक्स लगा उसे वसूलना कठिन चुनौती है।
- नियम-कानून के जरिए जबरन समानता थोपने से सूक्ष्म एवं लघु कारोबार को नुकसान होगा।
- धन या आमदनी को नियंत्रित करने की कोशिश को उन्होंने ‘सीमा लगाने का अत्याचार’ (tyranny of threshold) कहा।
- नागेश्वरन की एक अन्य दलील थी कि देश में ‘न्यायपूर्ण विकास’ हो रहा है या नहीं, इसे मापने की कसौटी गैर-बराबरी घटाना नहीं, बल्कि गरीबी घटाना है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शामिका रवि भी इस चर्चा में उपस्थित थीं। उन्होंने कहाः
- आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) एक ऐसा लक्ष्य है, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
- यूरोप में डी-ग्रोथ (आर्थिक ह्रास) हो रहा है। हमारी निगाह में डी-ग्रोथ अनैतिक है। ग्रोथ ही वह आधार है, जिससे आज हम यहां तक पहुंचे हैं।
तो स्पष्ट है कि भारत सरकार के सलाहकार यह मानते हैं कि भारत सही दिशा में है और इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। उनकी निगाह में ग्रोथ एक पवित्र लक्ष्य है, भले इसका लाभ कितने ही कम लोगों को मिल रहा हो।
वे वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के अब अमान्य हो रहे पैमाने तथा कुछ अपने गढ़े आंकड़ों के आधार पर दावा करते हैं कि भारत में गरीबी घटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरबपतियों को वेल्थ क्रियेटर (धन निर्माता) बता कर उनकी सार्वजनिक प्रशंसा करते रहे हैं। वे देश के सबसे धनी तबकों को “विकसित भारत” का माध्यम बता चुके हैं।
तो फिर सरकार पिकेटी जैसे अर्थशास्त्रियों की बात क्यों सुने!
इसके पहले कि हम इस प्रश्न आएं, इसे रेखांकित कर लेना उचित होगा कि थॉमस पिकेटी या उनके Inequality Lab से जुड़े अर्थशास्त्री कम्युनिस्ट या वामपंथी नहीं हैं।
उनकी निगाह में यूरोपीय सोशल डेमोक्रेसी आदर्श व्यवस्था थी, जो नव-उदारवाद के बोझ तले अब चरमरा रही है। इस रूप में उनकी सोच अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के करीब है, जिनका अर्थशास्त्र न्यू डील के दौर में अमेरिका और बाद में यूरोप का आर्थिक मार्गदर्शक रहा।
बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने पिछले हफ्ते पिकेटी का एक इंटरव्यू में प्रकाशित किया। इसमें एक सवाल यह था- ‘आपको आज के दौर का कार्ल मार्क्स कहा जाता है, क्या आप इससे खुश हैं?’ पिकेटी का जवाब था- ‘मैं मार्क्स को कैसे देखता हूं, इसको लेकर निश्चित नहीं हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कीन्स को, या मार्क्स को तरजीह दूंगा। मार्क्स में कई अच्छी बातें हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं, जो अच्छी नहीं हैं।’
तो इसके बाद यह चर्चा ठहर जानी चाहिए कि पिकेटी कम्युनिस्ट हैं या उनके सुझाव मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं। असल में मार्क्सवाद के तहत पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के अंदर विषमता का समाधान ढूंढना कभी लक्ष्य या व्यावहारिक कार्यक्रम नहीं रहा।
मार्क्सवादी इसे सुधारवादी कदम- जिसका मकसद नव-उदारवादी दौर में पूंजीवाद के अनिवार्य और चरम परिणाम के पीड़ितों पर मरहम लगाने की कोशिश के रूप में देखेंगे।
यह सवाल उठ सकता है कि नव-उदारवाद के इन चरम नतीजों पर नियंत्रण की आखिर जरूरत क्या है? दरअसल, यह खुद पूंजीवाद की जरूरत है।
कुछ दिन पहले खुद नागेश्वरन ने उद्योगपतियों की संस्था एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा था कि कॉरपोरेट मुनाफा गुजरे 15 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है, लेकिन कंपनियों ने कर्मचारियों की तनख्वाह उसी अनुपात में नहीं बढ़ाई है। बढ़े मुनाफे का इस्तेमाल उन्होंने कर्ज चुकाने में किया है।
तब उन्होंने कहा था- ‘बैलेंस सीट को बेहतर करना अच्छी बात है। लेकिन कॉरपोरेट मुनाफे और श्रमिकों की आय वृद्धि के बीच संतुलन बने रहना चाहिए। यह अनुपात कायम नहीं रहा, तो अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग नहीं बचेगी और कॉर्पोरेट उत्पादों की खरीद नहीं होगी।’
नागेश्वरन ने जो कहा, उसकी पुष्टि मार्केट एजेंसियों के जुटाए आंकड़ों से भी हुई है। दरअसल, उसका परिणाम श्रमिक वर्ग की वास्तविक आय में भारी गिरावट के रूप में सामने आया है, क्योंकि इस दौर में महंगाई वृद्धि दर भी काफी ऊंची रही है। उपभोग और मांग गिरने की यह भी एक बड़ी वजह है। इसका असर कॉरपोरेट बिक्री पर पड़ने लगा है। (https://janchowk.com/beech-bahas/indian-economy-why-did-the-race-backwards-accelerate/)
इस परिघटना से देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। वित्तीय कारोबार को हटा दें, तो आज संभवतः यह नजर आएगा कि वास्तविक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की असली सूरत क्या है। मगर भारत में इस तरह के आंकड़े अक्सर नहीं जारी किए जाते।
बहरहाल, यह दुनिया भर में देखने को मिला है कि आज के वित्तीय पूंजीवाद के दौर में धनी लोग उत्पादन एवं वितरण की अर्थव्यवस्था में निवेश से ज्यादा दिलचस्पी शेयर, बॉन्ड, ऋण, बीमा एवं रियल एस्टेट कारोबार में दिखाते हैं। सरकारों की नीतियां इसमें सहायक हुई हैं।
ऐसा इस तर्क पर किया गया है कि इससे क्रियेट हुए वेल्थ का एक हिस्सा रिस कर सबसे गरीब लोगों तक भी पहुंचेगा। यही ट्रिकल डाउन थ्योरी है। (https://www.cbsnews.com/news/tax-cuts-rich-50-years-no-trickle-down/)
इस तरह छोटी-सी धनी आबादी का धन और बढ़ता गया है। परिणामस्वरूप गैर-बराबरी बढ़ी है। अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि गैर-बराबरी बेलगाम होने पर वास्तविक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ बुरी तरह प्रभावित होता है।
(file:///C:/Users/satye/Downloads/How_does_income_inequality_affects_economic_growth.pdf)
और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। आर्थिक गैर-बराबरी सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बनती है। यह बात ऐतिहासिक अनुभव से सिद्ध है, लेकिन अब इस बारे में पर्याप्त अकादमिक अध्ययन भी मौजूद हैं। सामाजिक अस्थिरता कई रूपों में जाहिर हो सकती है।
मसलन, अपराध बढ़ना, हिंसा की घटनाओं में वृद्धि, आत्म-हत्या की वारदातों का बढ़ना, सामाजिक तनाव, और राजनीतिक उथल-पुथल- ये सभी सामाजिक अस्थिरता से जुड़े पहलू हैं। रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर फ्रांस की क्रांति और रूस की अक्टूबर (1917 की बोल्शेविक) क्रांति तक के जो कारण समझे गए हैं, उनमें आर्थिक विषमता भी एक मानी गई है। (https://x.com/MortenStostad/status/1867728718048928087)
अब रहा यह सरकारी दावा कि भारत में गैर-बराबरी भले बढ़ रही हो, लेकिन साथ ही गरीबी भी घटी है। यह दावा दो पैमानों को आधार बना कर किया जाता है। उनमें एक तो विश्व बैंक का पैमाना है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति दिन खर्च क्षमता को आधार बनाया गया है।
इसके मुताबिक क्रय शक्ति समतुल्यता (परचेजिंग पॉवर पैरिटी-पीपीपी) पर 2017 की कीमत पर 2.15 डॉलर प्रति दिन खर्च क्षमता वर्तमान पैमाना है। यह रकम आज सवा 47 रुपये के करीब होगी। यानी जो व्यक्ति इतना खर्च करने में सक्षम हो, वह गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा।
दूसरा पैमाना भारत सरकार की संस्था नीति आयोग ने गढ़ा है। मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स की इस गणना से उपरोक्त रकम और कम हो जाती है।
मगर खुद वर्ल्ड बैंक के पैमाने को आज ठोस चुनौतियां मिल चुकी हैं। अध्ययनकर्ताओं ने यह साबित किया है कि नव-उदारवाद को स्वीकार्य बनाने के मकसद से तैयार ये पैमाने सिरे से नाकाफी है। यह गणना अत्यंत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी रकम के आधार की गई है।
फिर महंगाई बढ़ने के साथ इसकी अपर्याप्ता बढ़ती जाती है। पीपीपी की गणना सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत को ध्यान में रख कर की जाती है- मसलन इसमें हवाई यात्रा की औसत कीमत भी शामिल होती है। जबकि गरीब लोग ऐसे उपभोग से दूर रहते हैं। उनकी प्रमुख जरूरत भोजन है, जबकि इस दौर में खाद्य मुद्रास्फीति आम महंगाई दर से बेहद ऊंची रही है।
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2023.2217087)
इसलिए यह अस्वाभाविक नहीं है कि भारत में प्रति व्यक्ति कैलोरी उपलब्धता घटती गई है। नव-उदारवाद से पहले के दौर में कैलोरी उपलब्धता गरीबी मापने का मुख्य पैमाना था। आज इस पैमाने पर देखें, तो भारत की दो तिहाई से तीन चौथाई तक की आबादी गरीबी रेखा के नीचे आएगी।
कहने का तात्पर्य यह कि गैर-बराबरी बढ़ने के बावजूद गरीबी घटी है, एक फर्जी दावा है। गरीबी घटाने के लिए जिस सामाजिक एवं मानव विकास संबंधी निवेश की आवश्यकता है, भारत में जीडीपी के अनुपात में वह खर्च लगातार घटता चला गया है।
इस परिस्थिति में पिकेटी जैसे अर्थशास्त्रियों के सुझाव, हालांकि अपर्याप्त हैं, फिर वे बेहद अहम हो गए हैं। तो कहा जा सकता है कि मौजूदा सरकार उनकी उपेक्षा कर भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था, सामाजिक शांति एवं देश के भविष्य के लिए जोखिम लगातार बढ़ा रही है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं।)