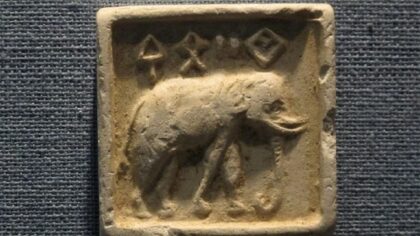चारधाम परियोजना हिमालय के नीचे चल रही है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना चारधाम रेलवे परियोजना का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। ऋषिकेश से प्रयाग को जोड़ने के लिए योजना बनाई गई इस रेलवे लाइन में 13 स्टेशन, 16 सुरंगें और 35 पुल शामिल होंगे।
परियोजना के लिए अधिग्रहित कुल भूमि में से 71.56% वन क्षेत्र है, और बाकी अधिकांशतः कृषि योग्य भूमि या आबादी वाले गांव हैं। परियोजना के डिजाइन और पर्यवेक्षण का अनुबंध इटली और स्विट्जरलैंड की कंपनियों को सौंपा गया है।
जिन जिलों से होकर यह रेलवे लाइन गुजरने वाली है, वे मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं और वहां की बड़ी आबादी भूमिहीन किसानों की है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और चीन सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति को मजबूत करना है।
इस विशाल परियोजना की मूल समस्या खराब योजना, वैज्ञानिक निर्माण प्रक्रियाओं की कमी और पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों की सरकारी उपेक्षा है। बुनियादी ढांचे के इस दबाव में सरकार ने हिमालय के पर्यावरणीय सीमाओं को नजरअंदाज कर दिया है।
उदाहरण के लिए, ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का चौड़ीकरण भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि का कारण बन गया है।
मेरे अध्ययन में 247 किलोमीटर के खंड में 309 सड़क-बाधित भूस्खलन दस्तावेजित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की बढ़ती भूगर्भीय अस्थिरता की पुष्टि करते हैं। इस गलियारे में भूस्खलन का घनत्व 1.25 प्रति किलोमीटर मापा गया है। परियोजना का विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव चिंताजनक है क्योंकि ये भूस्खलन अक्सर सड़क अवरोध, मौतों और जीवन को खतरे में डालने का कारण बनते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के नाम पर सरकार इस परियोजना को एक रणनीतिक कदम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है।
इस क्षेत्र की कई गांवों के ताजे जल स्रोत या तो सूख गए हैं या सुरंगों के निर्माण के कारण भारी प्रदूषित हो गए हैं। चमोली जिले के पनाया पोखरी गांव उन गांवों में से एक है जिसने अपने ताजे पेयजल स्रोत को खो दिया है। उत्तराखंड की पहाड़ियां क्षेत्रीय जल चक्र को बनाए रखने में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं।
जब इन पहाड़ियों में ड्रिलिंग की जाती है, तो अक्सर वहां ताजा पानी निकलता है, जो मानसून के महीनों में पहाड़ियों के भीतर संग्रहीत होता है और सूखे के महीनों में स्थानीय लोगों के लिए जल के भंडार के रूप में कार्य करता है।
इन पहाड़ियों के माध्यम से कंक्रीट की नहरें बनाने से जल निकासी प्रणाली बाधित हो जाती है और अंततः तालाब सूख जाते हैं, जो भूजल पर निर्भर होते हैं। इन गांवों के लोग पहली बार जल संकट का सामना कर रहे हैं और उन्हें दूषित पानी उबालकर पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
हालांकि कृषि और संबद्ध गतिविधियां उत्तराखंड के अधिकांश लोगों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत बनी हुई हैं, लेकिन 1947 से खेती के अंतर्गत आने वाली भूमि में भारी कमी आई है। इस स्थिति में भी पश्चिमी हिमालयी राज्य खाद्य-सुरक्षित बने हुए हैं और अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी मंडियों पर निर्भर हैं।
उत्तराखंड की अधिकांश आबादी का जीवन कृषि के इर्द-गिर्द घूमता है। इस क्षेत्र में सरकारी निवेश और समर्थन रोजगार सुनिश्चित करेगा, स्थानीय लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाएगा और स्थानीय बाजार बलों को प्रोत्साहन देगा।
टिहरी गढ़वाल के मालथा जैसे गांवों में किसानों को सिंचाई के लिए किसी भी सहायता से पहले भूमि खाली करने का नोटिस मिला है।
परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरणीय क्षरण से परे स्थानीय समुदायों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में नौकरी बाजार पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है, और अन्य संभावित रोजगार के अवसर मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
हिमाचल जैसे राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, और यह इसके मुख्य कारणों में से एक है। बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती हैं, विशेष रूप से नवउदारवादी आर्थिक नीति के आगमन के बाद। यह मौन आपदा स्थानीय समुदायों को भारी रूप से प्रभावित कर रही है।
कई हिमालयी कस्बों में देखी गई जीवन-यापन की कठिनाइयां अनियंत्रित निर्माण, खराब जल निकासी प्रणाली और बढ़ते बुनियादी ढांचे के दबाव का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। जोशीमठ, जो इन प्रभावों से प्रभावित कस्बों में से एक है, ने भूमि में महत्वपूर्ण विकृति दिखाई है, जिसे वैज्ञानिक क्षेत्र पर डाले गए अत्यधिक बोझ का परिणाम मानते हैं।
भौगोलिक भू-आकृतियों की संरचनात्मक असमर्थता राज्य-जनित दुष्प्रभावों से सीधे संबंधित है। ये दुष्प्रभाव न तो आकस्मिक हैं और न ही अनियोजित; बल्कि ये वैश्विक वित्त, अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी या साम्राज्यवादी पूंजी के प्रवेश के लिए स्थान देने की एक सुविचारित रणनीति है।
1990 के दशक में पर्यावरण प्रभाव आकलन के पहले प्रस्ताव के बाद इसमें मापदंडों में धीरे-धीरे बदलाव देखा गया। पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ने के बजाय, हमारे वैश्विक वित्तीय नेताओं ने सतत विकास के प्रश्न को प्राथमिकता दी, जो बड़े कॉर्पोरेट्स के लाभ बाजार का समर्थन करता है।
प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से लाभ कमाने की इस प्रक्रिया के कारण, पर्यावरण संरक्षण और कमजोर जलवायु एवं पर्यावरणीय स्थलों को मजबूत करने के सवाल को अकेला छोड़ दिया गया है और इसका कोई व्यावहारिक समाधान नहीं दिखता।
हिमालय के केंद्र में बड़े पूंजीपतियों की स्थापना और पलायन की इस पूरी प्रक्रिया ने एक लंबी और अपरिवर्तनीय आपदा की यात्रा शुरू कर दी है। व्यापारियों, कारीगरों, कृषि उत्पादन और पशुपालन को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया है।
पहाड़ी क्षेत्रों में सामूहिक श्रम की धारणा को राज्य द्वारा एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से खत्म कर दिया गया है, ताकि बाहरी लोगों, तथाकथित आर्थिक प्रदाताओं, का एक आत्मनिर्भर क्षेत्र में सहज प्रवेश हो सके।
2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड के एक हजार से अधिक गांव निर्जन हो चुके हैं, और सैकड़ों गांवों में 10 से कम लोग निवास करते हैं।
यह जनसंख्या कमी, जिसे तथाकथित विकास उछाल ने और बढ़ा दिया है, क्षेत्र की पारंपरिक आजीविका और सांस्कृतिक ताने-बाने को खतरे में डाल रहा है।
पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक हर्बल चिकित्सा, दवा, खाद्य, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों द्वारा तेजी से शोषित किया जा रहा है। स्वदेशी और स्थानीय लोग इस शोषण का शिकार बनते जा रहे हैं। व्यापारिक व्यक्ति, प्रशासन, राजनीतिक व्यक्ति और स्थानीय प्रभावशाली सभी संसाधनों के शोषण में शामिल हैं।
कई आकर्षक रिपोर्टों में, शोधकर्ताओं ने जैविक विविधता सम्मेलन का समर्थन किया, जहां संयुक्त राष्ट्र ने सामुदायिक निवासियों से लाभ साझा करने का आश्वासन दिया था। क्या यह स्थानीय समुदाय की मदद कर पाया?
परिणाम की तस्वीर बहुत अलग और निराशाजनक है। डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ जैसे संस्थान खुलेआम संसाधनों और सामुदायिक अधिकारों की लूट का समर्थन कर रहे हैं।
बड़ी दवा कंपनियों ने सभी उद्योगों पर एकाधिकार कर लिया है और अनुसंधान प्रयोगशालाएं बनाना और प्रबंधन करना शुरू कर दिया है, बिना उस विशाल लाभ का हिस्सा साझा किए जो वे हर दिन कमा रही हैं।
ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा अधिकारों की मदद से और बड़े वित्तीय संस्थानों, निगमों और राजनेताओं के पूर्ण समर्थन से, वे कानूनों को अपने लाभ के लिए बदल रहे हैं।
यह समय है कि लोग इस साजिश को समझें, जो कॉर्पोरेट और राजनेताओं के गठजोड़ ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। पहली नजर में, इसे एक पर्यावरणीय चिंता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन असल में यह संसाधनों को प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण है, जिसे संरक्षण के नाम पर अंजाम दिया जा रहा है।
(निशांत आनंद स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)