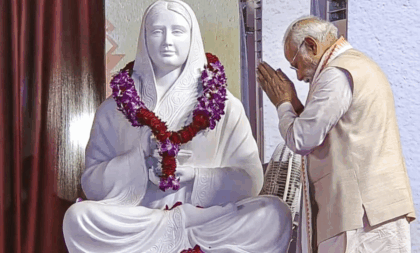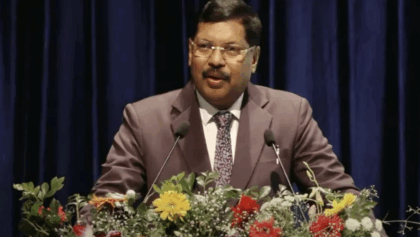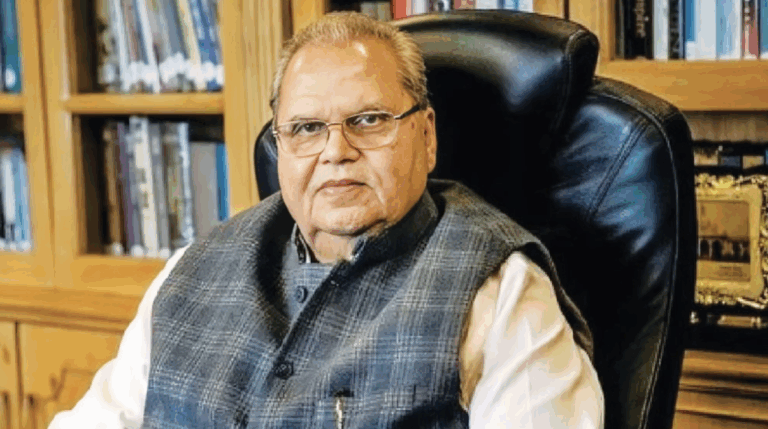भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो गए, उनका कार्यकाल साहसिक हस्तक्षेप, प्रक्रियागत स्पष्टता और संस्थागत सुधार से चिह्नित था। 14 मई 1960 को जन्मे खन्ना एक समृद्ध कानूनी विरासत वाले परिवार से आते हैं। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना को न्यायपालिका में पारदर्शिता की ठोस पहल करने के लिए जाना जायेगा। उनके पिता देव राज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और उनकी मां सरोज खन्ना लेडी श्री राम कॉलेज में लेक्चरर थीं।18 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए न्यायमूर्ति खन्ना अपने साथ तीन दशकों से अधिक का न्यायिक और वकालत का अनुभव लेकर आए।
वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एच.आर. खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने केशवानंद भारती (1973 ) में मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले (1976) में एकमात्र असहमति व्यक्त की थी-यह न्यायिक स्वतंत्रता का एक ऐसा कार्य था, जिसके कारण उन्हें जनवरी 1977 में मुख्य न्यायाधीश का पद खोना पड़ा था। सीजेआई खन्ना के दादा, सरव दयाल, एक प्रमुख वकील थे, जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति में कार्यरत थे।
18 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए न्यायमूर्ति खन्ना अपने साथ तीन दशकों से अधिक का न्यायिक और वकालत का अनुभव लेकर आए हैं, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण भूमिकाएं और आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में कार्य शामिल हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जो कल अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, को उनके सम्मान में आयोजित औपचारिक बेंच कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्यों द्वारा गर्मजोशी और शानदार विदाई दी गई। खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार के युवा सदस्यों तक कानूनी बिरादरी के एक व्यापक वर्ग ने मुख्य न्यायाधीश खन्ना के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीजेआई खन्ना ने न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की विरासत को आगे बढ़ाया। “कानून की कोई भी शाखा ऐसी नहीं है जिसमें बेंच के इस तरफ से आपके विचारों की स्पष्टता स्पष्ट न हुई हो। युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें मंच पर आकर बहस करने के लिए प्रेरित करना, एक न्यायाधीश के सर्वोत्तम गुणों को दर्शाता है। आप न्यायपालिका में जो वास्तव में मायने रखता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं,” सिब्बल ने कहा।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचन्द्रन, संजय हेगड़े, विभा दत्ता मखीजा, शादान फरासत, पीसी सेन, मेनका गुरुस्वामी, दुष्यन्त दवे, अधीश अग्रवाल, एएम सिंघवी, एएसजी ऐश्वर्या भाटी और एन वेंकटरमन, एससीएओआरए के अध्यक्ष विपिन नायर आदि ने भी निवर्तमान सीजेआई की प्रशंसा की। उनकी “स्टील की रीढ़” और कोर्ट को संभालने के शानदार तरीके के लिए उनकी सराहना की गई।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने सभी को उनकी सराहना के लिए धन्यवाद दिया। “मैं पूरी तरह से अभिभूत हूं, मैं अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर आया हूं। और यादें जो बहुत अच्छी हैं, जो हमेशा रहेंगी। एक बार जब आप वकील बन जाते हैं, तो आप वकील ही बने रहते हैं। न्यायपालिका पर जो सार्वजनिक विश्वास है, उसे हासिल नहीं किया जा सकता। इसे अर्जित करना होता है। और हम इसे बार और बेंच के सदस्यों के माध्यम से अर्जित करते हैं। न्यायपालिका एक सामान्य शब्द है जो न्यायाधीशों और बार दोनों को संदर्भित करता है। आप (बार) सिस्टम पर अन्य जांचों के अलावा एक अंतर्निहित जांच हैं। आप (बार) विवेक के रक्षक हैं।”
जहां तक उनके उत्तराधिकारी का सवाल है, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि न्यायमूर्ति गवई एक उत्कृष्ट मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो “संस्था, मौलिक अधिकारों और कानून के बुनियादी सिद्धांतों को कायम रखेंगे।”
बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सीजेआई संजीव खन्ना के 20 महत्वपूर्ण निर्णय और आदेश-
सीजेई खन्ना का सबसे ताज़ा आदेश वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 पर चिंता को लेकर रहा..
केस का शीर्षक: असदुद्दीन ओवैसी बनाम भारत संघ
शीर्ष अदालत ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में बड़ा हस्तक्षेप किया।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कुछ संशोधनों, विशेषकर ‘वक्फ-बाय-यूजर’ अवधारणा को हटाने, सरकारी अधिकारियों को दी गई शक्तियों तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर चिंता जताई। केंद्र सरकार अंततः वक्फ अधिनियम में कुछ संशोधनों पर आगे न बढ़ने पर सहमत हो गई। अब इसपर आगे विस्तृत सुनवाई 14 मई को नये चीफ जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष होगी।
संविधान पीठ के निर्णय
1. मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने की शक्ति
केस का शीर्षक: गायत्री बालासामी बनाम आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से माना कि अपीलीय न्यायालयों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 या 37 के तहत मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने की सीमित शक्तियां हैं। बहुमत के लिए लिखते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने समक्ष किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए पुरस्कारों को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि इसका प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने कुछ पहलुओं पर असहमति जताई।
2. बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौते अस्वीकार्य हैं लेकिन शून्य नहीं हैं।
केस का शीर्षक: भारतीय स्टाम्प अधिनियम और भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया
सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यद्यपि बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौते अग्राह्य हैं, लेकिन बिना मुहर लगे होने के कारण वे प्रारम्भ से ही शून्य नहीं हो जाते।
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (तत्कालीन न्यायमूर्ति) ने बहुमत की राय लिखी, जबकि न्यायमूर्ति खन्ना ने अलग लेकिन सहमति वाली राय लिखी।
अपने मत में न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि बिना स्टाम्प वाले समझौते शून्य या प्रारम्भ से ही शून्य नहीं होते हैं तथा स्टाम्प की कमी से समझौता शून्य या अप्रवर्तनीय नहीं हो जाता है, अपितु यह उसे साक्ष्य में अग्राह्य बना देता है।
3. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन
केस का शीर्षक: संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया था।
न्यायालय ने माना कि यह एक अस्थायी प्रावधान है। साथ ही, इसने जम्मू-कश्मीर (J&K) को दो केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में विभाजित करने के 2019 के कानून की वैधता पर निर्णय लेने से भी इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति खन्ना, जिन्होंने सहमति व्यक्त करते हुए अपनी राय लिखी, ने पाया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 असममित संघवाद की विशेषता थी, न कि संप्रभुता का संकेत, तथा इसका निरस्तीकरण संघीय ढांचे को नकारता नहीं है।
4. अनुच्छेद 142 के तहत विवाह विच्छेद करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति
केस का शीर्षक: शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर विवाह के पूरी तरह से टूट जाने के आधार पर तलाक दे सकती है, जिसे अभी तक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं बनाया गया है।
न्यायालय ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को कुछ आवश्यकताओं और शर्तों के अधीन समाप्त किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति खन्ना, जिन्होंने निर्णय लिखा था, ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवाह के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर तलाक देना अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह एक विवेकाधिकार है जिसका प्रयोग बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए।
5. चुनावी बांड योजना को रद्द करना
केस का शीर्षक: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी गई थी।
इसने माना कि यह योजना, अपनी गुमनाम प्रकृति के कारण, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति पर प्रहार करती है।
न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 12 अप्रैल, 2019 से राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांडों का ब्योरा देने के लिए दबाव डाला, जबकि बैंक ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इसका खुलासा करने में देरी की।
न्यायमूर्ति खन्ना ने सहमति जताते हुए लिखा कि यदि दान बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जाता है तो दानकर्ताओं की निजता का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने लिखा कि उनकी पहचान “उस व्यक्ति और बैंक के अधिकारियों को असमान रूप से ज्ञात है, जहां से बांड खरीदा गया है। “उन्होंने यह भी कहा कि दानकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध, उत्पीड़न और प्रतिशोध की आशंका इस योजना के लिए औचित्य के रूप में काम नहीं कर सकती है।
6. आरटीआई मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर भी लागू
केस का शीर्षक: सीपीआईओ, सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। हालांकि, न्यायालय ने न्यायिक प्रशासन के कुछ पहलुओं में गोपनीयता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया और सार्वजनिक हित के आधार पर सूचना के अधिकार को योग्य ठहराया।
न्यायमूर्ति खन्ना ने बहुमत के लिए लिखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि आरटीआई अधिनियम मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर भी लागू होता है। उन्होंने लिखा कि न्यायिक स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से सूचना के अधिकार का विरोध नहीं करती है।
अन्य निर्णय
7. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत मकान मालिक-किरायेदार विवादों का निपटारा मध्यस्थता योग्य है
केस का शीर्षक: विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि किरायेदारी संबंधी विवादों का मध्यस्थता से निपटारा किया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के तहत मध्यस्थता पर रोक नहीं लगाई गई है, सिवाय उन किरायेदारी विवादों के जो किराया नियंत्रण कानून के तहत आते हैं।
बहुमत की ओर से लिखते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 8 और 11 के चरणों में, न्यायालयों को मध्यस्थता समझौते की वैधता की प्रथम दृष्टया जांच करनी चाहिए।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि इस प्रकार की जांच से लागत बचेगी तथा आपत्ति करने वाले पक्षों को परेशान होने से रोका जा सकेगा, जब मध्यस्थता न होने की दलील को स्वीकार न करने का कोई स्पष्ट औचित्य न हो।
8. घृणास्पद भाषण समानता के अधिकार का खंडन करता है
केस का शीर्षक: अमीश देवगन बनाम भारत संघ
2020 में, शीर्ष अदालत ने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ टिप्पणी के लिए पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने ‘घृणास्पद भाषण’ की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने घृणास्पद भाषण और मुक्त भाषण के बीच अंतर, घृणास्पद भाषण को अपराध घोषित करने की आवश्यकता और इसकी पहचान करने के लिए परीक्षणों पर प्रकाश डाला।
हालांकि, न्यायमूर्ति खन्ना के फैसले में स्पष्ट किया गया कि घृणास्पद भाषण के संदर्भ में गरिमा का तात्पर्य “किसी व्यक्ति के रूप में सम्मान या प्रतिष्ठा के किसी विशेष स्तर से नहीं है, जैसा कि मानहानि के मामले में होता है, जो व्यक्तिवादी है।”
न्यायालय ने कहा कि शब्दों के प्रभाव का मूल्यांकन विवेकशील, दृढ़-चित्त, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानदंड से किया जाना चाहिए, न कि उन लोगों के आधार पर जो कमजोर और अस्थिर मन वाले हैं, न ही उन लोगों के आधार पर जो हर प्रतिकूल दृष्टिकोण में खतरे की गंध सूंघते हैं।
9. पश्चिम बंगाल में 25,000 कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द करना
केस का शीर्षक: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य
अप्रैल में शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसने 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (एसएससी) द्वारा की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य कर दिया था।
न्यायमूर्ति खन्ना, जिन्होंने निर्णय लिखा था, ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।
10. जीएसटी और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की शक्तियां
केस का शीर्षक: राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 69 और 70 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो जीएसटी अधिकारियों को व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और समन करने की शक्ति प्रदान करती है।
ऐसा करते हुए, न्यायालय ने माना कि अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर दंड प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम और जीएसटी अधिनियम दोनों के तहत की गई गिरफ्तारियों पर समान रूप से लागू होते हैं।
निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी कहा कि जीएसटी अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने योग्य हैं।
11. ईडी मामलों में चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालना
केस का शीर्षक: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय
दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले फैसले में न्यायमूर्ति खन्ना (तत्कालीन न्यायमूर्ति खन्ना) की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक समान नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल जांच के उद्देश्य से नहीं की जा सकती। बल्कि, इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब संबंधित अधिकारी अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर और लिखित में कारण दर्ज करके यह राय बनाने में सक्षम हो कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है, उन्होंने रेखांकित किया।
12. प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ की संवैधानिक वैधता
केस का शीर्षक: बलराम सिंह बनाम भारत संघ
मुख्य न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने कहा कि लगभग 44 वर्षों के बाद इस संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने का कोई “वैध कारण या औचित्य नहीं है।”
13. 100% ईवीएम-वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका खारिज
केस का शीर्षक: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग
न्यायमूर्ति खन्ना (तत्कालीन न्यायमूर्ति खन्ना) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के आंकड़ों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) रिकॉर्ड के साथ 100% क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह देखे कि क्या वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो सकती है और क्या चुनाव चिन्ह के साथ-साथ प्रत्येक पार्टी के लिए बार कोड भी हो सकता है।
14. सीआरपीसी के तहत आरोपपत्र कब पूरा होता है?
केस का शीर्षक: शरीफ अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
न्यायालय ने कहा कि आरोपपत्र में सभी कॉलमों की स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए ताकि न्यायालय को यह समझने में मदद मिल सके कि किस आरोपी ने कौन सा अपराध किया है और फाइल पर कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं।
तथ्यों का पर्याप्त विवरण दिए बिना आरोपपत्र दाखिल करने की प्रथा की निंदा करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा,
“कुछ राज्यों में आरोप-पत्र में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित विवरणों की प्रतिलिपि होती है, और फिर साक्ष्यों और सामग्री पर कोई स्पष्टीकरण दिए बिना यह बता दिया जाता है कि अपराध हुआ है या नहीं।”
15. हैदराबाद में सांसदों, विधायकों और न्यायाधीशों के लिए भूमि आवंटन रद्द करना
केस का शीर्षक: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम डॉ. राव वीबीजे चेलिकानी
मुख्य न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हैदराबाद नगर निगम सीमा के भीतर सांसदों, विधायकों, सिविल सेवकों, न्यायाधीशों, रक्षा कर्मियों, पत्रकारों आदि की आवासीय सोसायटियों को भूमि के अधिमान्य आवंटन को रद्द कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना, जिन्होंने यह निर्णय लिखा था, ने 2005 के आंध्र प्रदेश सरकार के ज्ञापन (जीओएम) को रद्द कर दिया, जिसके तहत ऐसा किया गया था।
16. धारा 102 सीआरपीसी के तहत पुलिस अधिकारी की शक्ति
केस का शीर्षक: नेवादा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य
2019 में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 102 में प्रदर्शित ‘किसी भी संपत्ति’ में ‘अचल संपत्ति’ शामिल नहीं होगी।
न्यायमूर्ति खन्ना (तब वे न्यायमूर्ति थे) ने कहा कि धारा 102 के तहत किसी पुलिस अधिकारी को चोरी की गई या किसी अपराध से संबंधित किसी संपत्ति को जब्त करने की शक्ति में अचल संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने और सील करने की शक्ति शामिल नहीं होगी।
महत्वपूर्ण असहमतियां
17. सेंट्रल विस्टा परियोजना
केस का शीर्षक: राजीव सूरी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 बहुमत से सेंट्रल विस्टा परियोजना और दिल्ली में एक नई संसद के निर्माण की केंद्र सरकार की योजना को बरकरार रखा।
परियोजना के पुरस्कार से सहमत होते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि मामले को सार्वजनिक सुनवाई के लिए वापस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि हेरिटेज संरक्षण समिति की कोई पूर्व स्वीकृति नहीं थी। इसके अलावा, पर्यावरण मंजूरी के पहलू पर, उन्होंने कहा कि एक नॉन-स्पीकिंग आदेश पारित किया गया था।
18. मध्यस्थों का संशोधित शुल्क पैमाना
केस का शीर्षक: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन बनाम एफकॉन्स गुनानुसा जेवी
तीन जजों की बेंच ने माना कि मध्यस्थों के पास पक्षों की सहमति के बिना एकतरफा अपनी फीस तय करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची के तहत निर्धारित शुल्क पैमाना अनिवार्य नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थों की फीस शुरू में ही तय कर दी जानी चाहिए ताकि बाद में अनावश्यक मुकदमेबाजी और पक्षों तथा मध्यस्थों के बीच टकराव से बचा जा सके।
न्यायमूर्ति खन्ना ने इस सीमित बिन्दु पर असहमति व्यक्त करते हुए लिखा कि मध्यस्थता समझौते के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक उचित शुल्क तय करने का हकदार है।
उल्लेखनीय हस्तक्षेप
19. सर्वेक्षण पर रोक, मौजूदा पूजा स्थलों के खिलाफ नए मुकदमे
केस का शीर्षक: अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ
मुख्य न्यायाधीश खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने देश भर की ट्रायल अदालतों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा धार्मिक ढांचों के धार्मिक चरित्र को लेकर दायर मुकदमों में उनके खिलाफ कोई प्रभावी आदेश या सर्वेक्षण पारित न करें।
न्यायालय ने कहा कि उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 ऐसे मुकदमों पर रोक लगाता है तथा जब तक 1991 के कानून की वैधता पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इस तरह के मुकदमों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
(जे पी सिंह कानूनी मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं।)