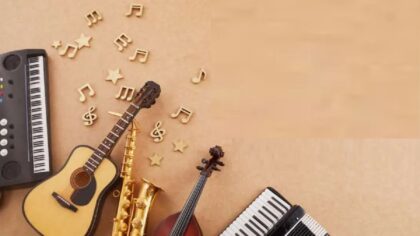यूं तो पूरा हिमालयी क्षेत्र ही संवेदनशील है। हिमालय भू गर्भिक तौर पर सबसे नए बने पर्वत हैं और अब भी निरन्तर बनने की प्रक्रिया में हैं। जिससे हिमालय की नाजुकता दुनिया के अन्य पर्वतों की अपेक्षा ज्यादा है। उत्तराखण्ड का पर्वतीय क्षेत्र भी हिमालय की इसी नाजुकता के चलते व हिमालयी ध्वंसों की वजह से लगातार आपदाओं का ग्रास बनता रहता है ।
तिब्बती व भारतीय प्लेटों की गतिशीलता जहां भूकम्पों का कारण बनती है वहीं यह नाजुकता विपरीत मौसम में भू स्खलनों व भू धंसाव का कारण बनती है।
पिछले दस-बीस वर्षों में इन आपदाओं की श्रृंखला में लगातार वृद्धि हुई है। बड़े भूकम्पों के चलते व अतिवृष्टि, बादल फटने के चलते पिछले तीन दशकों में उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र ने भीषण आपदाओं के सामना किया है। 1991 व 1998 के भूकम्प हों अथवा 2013 व 2021 की बड़ी आपदाएं। इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी आपदाओं की लंबी श्रृंखला है।
जोशी मठ का उत्तराखण्ड के पर्यटन व तीर्थाटन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह अपनी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के लिये व प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी महत्व रखता है। इतिहासकारों ने जोशी मठ को 7 वीं से 10वीं सदी तक कत्यूरी राजवंश की राजधानी के बतौर स्वीकार किया है। आठवीं सदी में शंकराचार्य के यहां आगमन ने इसे सांस्कृतिक-धार्मिक तौर पर विशिष्टता प्रदान की। हिंदुओं की चार पीठों में एक प्रमुख पीठ ज्योतिषपीठ व चार प्रमुख धामों में प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ के निकट होने से इस नगर के महत्व को अखिल भारतीय कलेवर दिया। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड इसके निकट है और उसी के निकट प्रसिद्ध फूलों की घाटी ने इस नगर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र के तौर पर स्थापित किया। औली, गोरसों, नन्दा देवी क्वारीपास व बहुत से अन्य बेहतरीन ट्रैक रूट हिमालयी बुग्याल व पर्वतारोहण, स्की, जैसे साहसिक अवसरों की उपलब्धता ने जोशीमठ को पर्यटन तीर्थाटन के अनुपम केंद्र के बतौर पहचान दी स्थापित किया है ।
इसके साथ ही इस क्षेत्र में धौली गंगा, अलकनन्दा, ऋषिगंगा, कल्पगंगा के रूप में प्रचुर जल संसाधन भी है। जिससे सरकार ने सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की श्रृंखला को यहां मंजूरी दी।
इस सबके चलते जनसंख्या का संकेंद्रण भी यहां बढ़ा। पिछले 20-30 सालों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जहां सन 90 से 2000 तक जोशीमठ की जनसंख्या 10 से 15 हजार के बीच ही थी आज यह 26 से 32 हजार के बीच है।
यह क्षेत्र पूर्व से ही भू स्खलनों के लिए संवेदनशील रहा है ।
7 फरवरी को ऋषिगंगा से शुरू हुई आपदा ने तपोवन में एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णु गाड जल विद्युत परियोजना के बैराज को ध्वस्त करते हुए वहां कार्य कर रहे 140 लोगों के प्राण भी ले लिए। इसके बाद यह बाढ़ व मलवा जोशीमठ के नीचे अलकनन्दा में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ गयी। क्योंकि यह बाढ़ इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरे क्षेत्र को हिलाया होगा। इसके ठीक आठ माह बाद अक्टूबर माह में अतिवृष्टि ने क्षेत्र के भूस्खलन को सक्रिय किया। नवम्बर अंतिम सप्ताह में लोगों ने अपने घर मकानों पर दरारें देखीं जो धीरे-धीरे बढ़ने लगीं। यह पूरे जोशीमठ में ही हो रहा था। कुछ जगहों पर यह बहुत अधिक हुआ। लोगों को मजबूरन जान बचाने के लिए घर खाली करने पड़े। जोशी मठ की सड़कें टेढ़ी होने लगीं। जगह-जगह भूमि धंसने लगी। जिससे लोगों में दहशत हुई।
इसके बाद ही लोगों ने सरकार से क्षेत्र के व्यापक अध्ययन की मांग की। जिसके लिए पत्र व्यवहार ज्ञापन दिए। प्रदर्शन भी किये। न ही सरकार ने घर मकानों पर दरारों से प्रभावितों की सुध ली और न ही अध्ययन करवाने को गम्भीरता से लिया।
1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जोशीमठ को ग्लेशियर की लाए हुए मलवे पर,अर्थात मोरेन पर, बसा हुआ बताया गया। हेम (Heim ) और गेन्सर (Gansser) के 1939 के अध्ययन के अनुसार मुख्य केंद्रीय भ्रंश (M C T main central thrust) के ठीक ऊपर स्थित यह क्षेत्र भूकम्पीय व भू गर्भिक हलचलों का केंद्र है।
1960 के दशक में इन्हीं हलचलों की वजह से भू स्खलन व भू धंसाव सक्रिय हुए। तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने गढ़वाल के कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करवाया। कमेटी ने इस क्षेत्र की स्थिरता व दीर्घकालिकता के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिनका कभी पालन नहीं हुआ । जिसमें इस क्षेत्र में भारी निर्माण पर प्रतिबंध व इस क्षेत्र में स्थित बोल्डरों से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किये जाने, ढलानों पर वृक्षारोपण करने व व्यवस्थित जल निकासी किये जाने की बातें थीं। हुआ इसके ठीक विपरीत। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि तब एक बहुत बड़े राज्य का हिस्सा होते हुए, सुदूर सीमांत क्षेत्र में हो रही हलचलों पर सरकार की न सिर्फ नजर थी बल्कि गम्भीरता पूर्वक उसका संज्ञान लेते हुए बाकायदा अध्ययन करवाया गया।
आज जब हम एक बहुत छोटा राज्य हैं, जोशीमठ से देहरादून की दूरी मात्र 300 किलोमीटर है, जनता लगातार उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर व्यापक अध्ययन करवाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही है तब भी सरकार की प्रतिक्रिया शून्य है। इसके बावजूद कि ऐसे अध्ययन हेतु देश के सर्वोच्च संस्थान ,ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक, पर्यावरणविद सामाजिक कार्यकर्ता व विशेषज्ञ इसी राज्य में उपलब्ध हैं।
सरकार द्वारा व्यापक अध्ययन की लगातार उपेक्षा किये जाने पर स्थानीय संघर्ष समिति जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की गुजारिश पर स्वतंत्र तौर वैज्ञानिकों की एक टीम ने वर्तमान परिघटना को समझने के लिए जोशीमठ का सर्वेक्षण किया व अपनी रिपोर्ट संघर्ष समिति को दी। डॉ एस पी सती, डॉ नवीन जुयाल व डॉ शुभ्रा शर्मा की यह रिपोर्ट 1976 की मिश्रा कमेटी के सुझावों का पालन नहीं करने को विशेष रूप से चिन्हित करती है। जिसमें भारी निर्माण पर प्रतिबंध व बोल्डरों से छेड़छाड़ न किये जाने के सुझाव शामिल थे । इसके विपरीत न सिर्फ यह किया गया बल्कि बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी । जिसमें नगर के नीचे से ही सुरंग बनाई गई । भारी विस्फोटों के जरिये न सिर्फ जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगे खुदी भारी निर्माण भी हुए ।
डॉ एस पी सती डॉ नवीन जुयाल व डॉ शुभ्रा शर्मा की रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ में हो रही वर्तमान परिघटना के लिए 1976 में गठित मिश्रा कमेटी की सिफारिशों सुझावों को अनदेखा करना एक प्रमुख कारण है।
7 फरवरी को आई बाढ़ जिसमें हजारों टन मलवा बह कर आया व बहाव की गति भी सामान्य की अपेक्षा कई गुना बढ़ गयी थी, इसके चलते यह स्वाभाविक ही है कि इसने अपर्दन को बढ़ाया हो और पुराने भूस्खलन को सक्रिय कर दिया हो। जिसने मलवे से ढंकी ढलानों को अस्थिर कर दिया। इस बाढ़ ने ही जोशीमठ के तलहटी में बह रही धौली गंगा व अलकनन्दा जोशीमठ के निचले हिस्से में तल में कटाव को और तीव्र कर दिया। इनका कहना है कि यह सक्रियता आगे भविष्य में स्थिर न होने तक जारी रह सकती है।
जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी एक कारण है। इसके लिए 1890 के एक फोटो के द्वारा देखा गया कि तब कितने कम घर थे उसके मुकाबले आज वह पूरी हरी भरी ढलान जो तब 1890 में खाली थी आज मकानों से पट गयी है।
जोशीमठ की पहले से कमजोर नाजुक ढलान को अनियंत्रित जल निकास प्रणाली और चट्टानों, पत्थरों, बोल्डरों को निर्माण सामग्री के लिए निकाल लिए जाने से भूस्खलन को गति मिली है।
जोशीमठ के नीचे से गुजर रही तपोवन विष्णुगाड परियोजना की सुरंग जिसमें कि 24 दिसम्बर, 2009 को एक बोल्डर के गिरने से सुराख हो गया और 600 लीटर प्रति सेकंड की दर से जल रिसाव होने लगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि इससे उनके स्रोतों पर असर हुआ है पर इसने कितना इसको नुकसान किया इसका अध्ययन होना बाकी है।
जोशीमठ के आस-पास चारधाम के लिए व सीमा के लिए बन रहे सड़क चौड़ीकरण की परियोजनाएं भी निश्चित ही भूस्खलन भू धंसाव को बढ़ाने का कारक होंगे और हैं।
डॉ सती, डॉ जुयाल और डॉ शुभ्रा की रिपोर्ट सुझाव देती है कि जोशीमठ क्षेत्र पर वर्तमान में उपलब्ध भूगर्भिक एवं पारिस्थितिक अध्ययन विरल एवं बिखरे हुए हैं, एकीकृत अध्ययन की जरूरत है, जिसमें इस इलाके की स्थिरता, प्राकृतिक स्रोतों संसाधनों का प्रबंधन व व्यापक उच्च स्तरीय हिम जलीय हिम नदी व वानस्पतिक अध्ययन की जरूरत है। जिसके आधार पर भविष्य में इस क्षेत्र के स्थिरीकरण के विकास की योजना पर कार्य हो सके।
तत्काल किये जाने वाले कार्य में रिपोर्ट कहती है कि खनन पर सख्ती से तुरन्त रोक लगानी चाहिए खासतौर पर स्थिर चट्टानों के खनन पर। क्योंकि भूमि के नीचे कैविटी (खाली या पोली जगह) बन गयी हैं। जो कि क्षेत्र के लिए गम्भीर खतरा बन रही हैं । इसलिए यह बढ़े नहीं इस पर रोक लगनी चाहिए ।
सड़क चौड़ीकरण के कार्य के दौरान जहां जहां पुराने भूस्खलन क्षेत्र हैं वहां हमारे इंजीनियर को भूमि के स्थिरीकरण स्थायित्व की नई तकनीक का व सुधारीकरण में अभिनव प्रयोग करते हुए निर्माण करना चाहिए।
जहां-जहां भूमि धंसाव है उसे रोकने के लिए चट्टानों में पिलर डाल कर या एंकर से मजबूत किया जाना चाहिए ।
7 फरवरी की आपदा ने क्योंकि नदी तट को बहुत नुकसान किया है और यह जोशी मठ के तल से कटाव को बढ़ाएगा इसलिए धौली और अलकनन्दा के तटबंधों का बंधना जरूरी है जिससे भविष्य में होने वाले अपर्दन को रोका जा सके।
उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश नगरों गांवों के हालात इस समय इसी तरह के हैं, मौसम के बदलाव ने भूस्खलन भूधंसाव की घटनाओं में बढ़ोत्तरी ही की है जिससे पहले ही पलायन से खाली हुए नगर गांव आपदा की मार से और वीरान हो रहे हैं। इनके बचाने के लिए बहुत व्यापक तौर पर एकीकृत वैज्ञानिक अध्ययनों की व चिंतन की जरूरत है। इसके अभाव में हम हिमालय की आबादी के साथ ही हिमालय को भी खो देंगे।
(जोशीमठ से पर्यावरण एक्टिविस्ट अतुल सती की रिपोर्ट।)