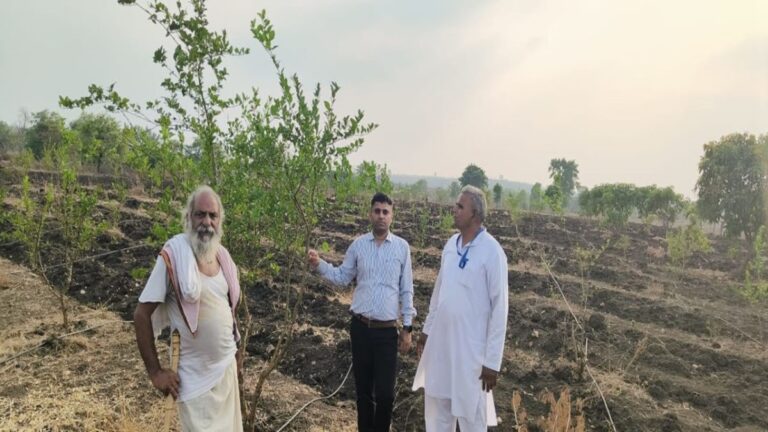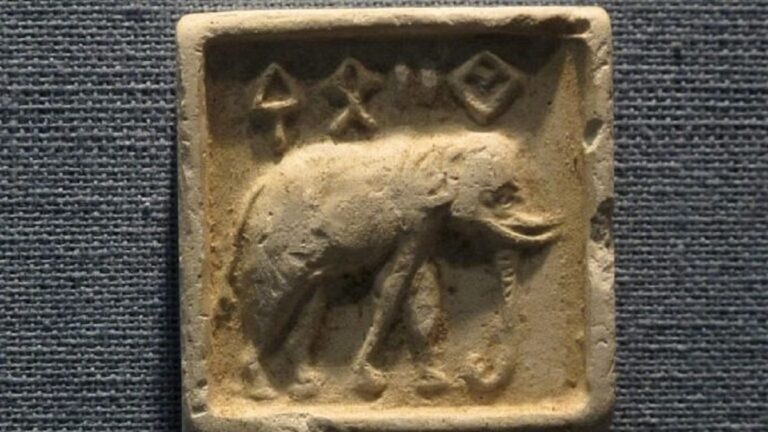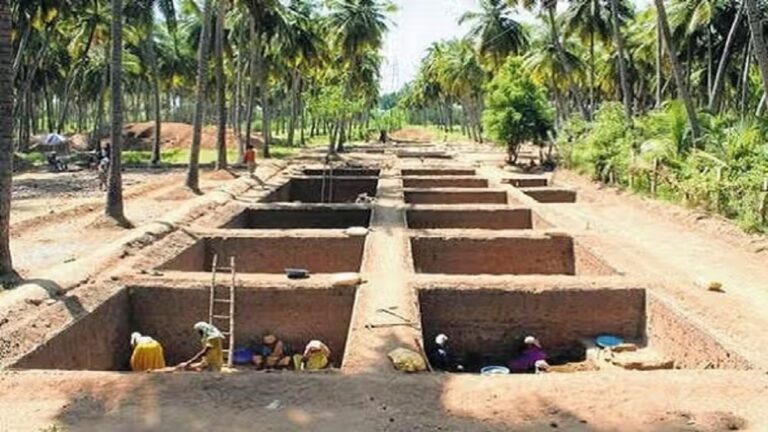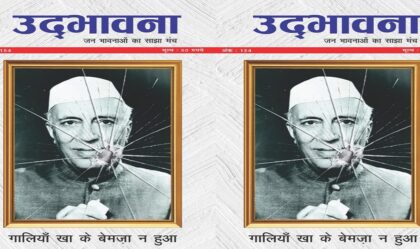पिछले कुछ दिनों से चंद अखबारों और मीडिया पोर्टल पर एक छोटी से खबर चल रही थीः वेनेजुएला में आखिरी ग्लेशियर भी नहीं बचा। पर्यावरण के खाने में छपी यह छोटी सी खबर दुनिया के पर्यावरण में हो रहे बदलाव की उस भयावहता को दिखाता है जिससे अनजान बने रहना संभव नहीं रहेगा। पिछले दो महीनों में दुनिया के स्तर पर गर्मी और तापमान का बढ़ता स्तर और अचानक हुई असामान्य बारिश का नजारा हम अफ्रीका से लेकर भारत और ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात से लेकर अफगानिस्तान में देख सकते हैं। लेकिन, वेनेजुएला की घटना एक नये तरह की है।
जब पर्यावरण पर नजर रखने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बताया कि लातिन अमेरिका का एकमात्र बचा रहने वाला हम्बोल्ट का ग्लेशियर पिघलकर इतना छोटा हो चुका है कि इसे ग्लेशियर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसका आकार 2 हेक्टेयर से भी कम हो चुका है। आमतौर पर ग्लेशियर का आकार 10 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले बर्फ से भरे इलाके को माना जाता है। 2011 में यहां ग्लेशियर की संख्या 6 से घटकर 1 रह गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तेजी से धरती का तापमान बढ़ रहा है उससे यही लगता है कि इंडोनेशिया, मेक्सिको और स्लोवानिया में भी ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे।
लातिन अमेरीका में एंडील की विशाल पर्वत श्रंखला है जो लगभग 8900 किमी की लंबाई में फैला हुआ है जिसमें कुछ की ऊंचाई लगभग 7000 मीटर तक है। यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम पठार हैं। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार इसका दक्षिणी भाग टूटकर अलग हुआ और यह टूटी हुई प्लेटें भारतीय उपमाद्वीप से आकर जुड़ीं। यही गोंडवाना क्षेत्र का निर्माण करता है। इस टूट, बिखराव और निर्माण में लाखों बरस गुजरे, और इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और आज के स्वरूप में आने से जो प्राकृतिक अवस्थितियां बनीं वे एक दूसरे के साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। लातिन अमेरीका के इन पहाड़ों में दुनिया के सबसे प्रचीनतम सभ्याताओं और संस्कृतियों का निर्माण हुआ, जिसे यूरोपीय पूंजीवाद और वहां पर बसने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया।
लातिन अमेरीका के इन देशों में तेजी से लुप्त हो रहे ग्लेशियरों, और अब वेनेजुएला में पूरी तरह से ही नष्ट हो गया है, का एक बड़ा कारण धरती के तापमान में हो रही वृद्धि है। लेकिन, इसके साथ-साथ अल नीनो का वह प्रभाव भी है जिससे समुद्र की गर्म हवा में न सिर्फ तेजी आती जाती है, उसका बहाव दक्षिण अमेरीका की ओर होने से वहां सूखे की स्थिति को पैदा कर देता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तरी प्रशांत महासागर से दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर चलने वाली गर्म हवा से लातिन अमेरीका और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में भी तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में, हवा का दबाव न सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करता है, साथ ही भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों पर मानसून के दबाव को कमजोर बना देता है। वहीं दक्षिणी एशियाई देशों में समुद्री हलचल में तेजी से अस्थिरता, सतह के गर्म होने और चक्रवातों में तेजी आने को भी देखा जा सकता है।
यहां हमें यह जरूर समझना होगा कि प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की हवाओं का बहाव ही अलनीना और अलनीनो का निर्माण करता है और यह एक सामान्य प्राकृतिक अवस्था ही है। इसकी वजह से, दक्षिणी अमेरीका, अफ्रीका से लेकर भारत और दक्षिण एशियाई देशों में बारिश की एक पूरी संरचना बनती है। पिछले 30 सालों में अलनीनो का प्रभाव असामान्य तौर पर बढ़ता गया है। इसका धरती के कुल तापमान में वृद्धि से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका स्पष्ट विश्लेषण अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन, अलनीनो के दौरान समुद्र की सतह के गर्म होने और गर्म हवा चलने और इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर उठ जाने की बात मानी जाती है। निश्चित ही, यदि औसतन धरती का तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि मानी जाय और साथ ही स्थानीय पर्यावरण के कारकों को जोड़ा जाय, तब स्थिति काफी बदलती हुई दिखती है।
इस संदर्भ में भारत में बदलते पर्यावरण को देखना बेहद जरूरी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते न सिर्फ भारत का पश्चिमोत्तर और केंद्रीय हिस्सा मई के पहले हफ्ते तक खुशनुमा मौसम से लबरेज था, बल्कि कश्मीर, हिमांचल और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिला। इसी साल के शुरूआती दिनों में इसी प्रभाव के चलते सूखी हवाओं की वजह से हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बेबर्फ गुजर रहा था। हालांकि बाद के दिनों में बर्फबारी हुई जो काफी देर तक होती रही। वहीं पिछली गर्मियों के शुरूआती दिनों में ही बारिश में तेजी आई और पिघलते ग्लेशियरों का पानी के साथ मिलकर पहाड़ों में हुई तबाही को देखा जा सकता है।
पिछले महीने सिक्किम में आये अचानक बाढ़, बिजली परियोजना का नुकसान और बड़े पैमाने में रिहाईशों की तबाही और लोगों की मौत पर एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अचानक बारिश और झील के जलस्तर के अचानक उठान की वजह से उपरोक्त तबाही आई थी। इस रिपोर्ट में सैटेलाईट से हासिल ग्लेशियरों की गतिविधि का जिक्र यह कहते हुए नहीं किया गया था कि इसकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं है। जबकि भारत के पर्यावरणविद हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों के बारे में न सिर्फ चेता रहे हैं बल्कि समय-समय पर अपनी रिपोर्ट भी जारी कर रहे हैं।
वेनेजुएला में ग्लेशियर के खत्म होने की कहानी, अपने सामने तबाही के एक ऐसे मंजर का दर्ज करने जैसा है जिसका स्पर्श हमारे शरीर तक आता है। हम पिछले दिनों अचानक तामपान में वृद्धि देखते हैं, अचानक ही अफगानिस्तान में आई बाढ़ का नजारा देखते हैं, दुबई में बाढ़ की तबाही पर भौचक्का हो रहे हैं और लंबे समय से सूखे की मार में तबाह ब्राजील में बाढ़ की विभिषिका की खबर पढ़ते हैं। यह सबकुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
हम अपने देश में जरूर रहते हैं, लेकिन जिस हवा, बारिश और ताप के बीच रहते हैं उसका कोई वतन नहीं है, जिस धरती पर रहते हैं उसे हमने देश में जरूर बदला है लेकिन उसका निर्माण प्रकृति ने बड़ी उथल-पुथल के साथ किया है और इसे अब भी वह बना रहा है। इस बनने की प्रक्रिया में इंसान इसका एक सक्रिय हिस्सा बन चुका है। निश्चित ही इसे बचाने में भी इंसान सक्रिय हिस्सेदार हो सकता है। इसकी शुरूआत वह लोगों के साथ मिलकर कर सकता है। जीने लायक पर्यावरण के लिए जरूरी है कि इंसान पर्यावरण को बचाने के लिए पहलकदमी ले और काम सामूहिक प्रयास से ही संभव है। हमें जरूर ही अपने पेड़, खेत, जंगल, नदी और ग्लेशियर बचाने लिए आगे आना चाहिए। वेनेजुएला अब और नहीं होना चाहिए।
(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)