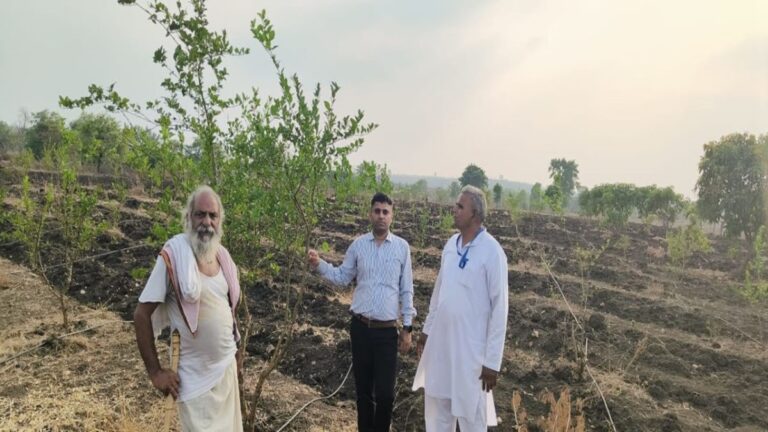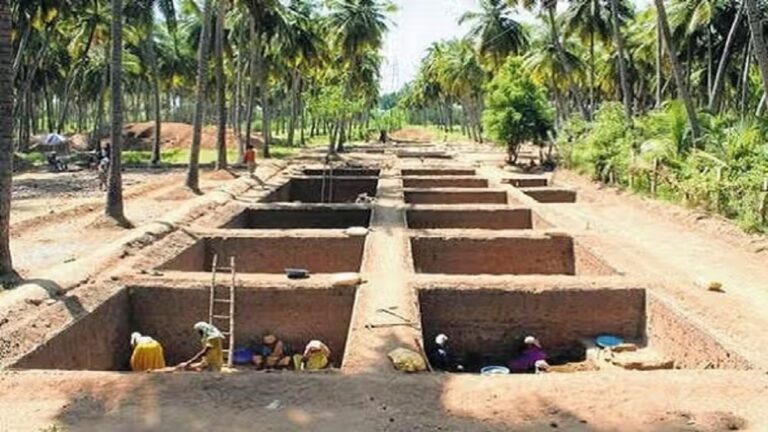जब पिछले हफ्ते दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (EV Policy 2.0) का ड्राफ्ट सामने आया, तो चर्चाओं का बाजार अचानक गर्म हो गया। इस नीति का घोषित उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना है। इसके तहत 15 अगस्त, 2025 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, और नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। यही शर्त मालवाहक वाहनों पर भी लागू होगी। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम, MCD आदि के वाहनों को 31 दिसंबर, 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना होगा। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों को भी इसी तरह के बदलाव से गुजरना होगा।
ड्राफ्ट में दो प्रावधान विशेष रूप से चर्चा का केंद्र बने। पहला, 15 अगस्त, 2026 तक पेट्रोल, डीजल, और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव। दूसरा, जिन परिवारों के पास पहले से दो पेट्रोल, डीजल, या सीएनजी वाहन हैं, उन्हें तीसरा वाहन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक खरीदना होगा। कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। ज्यादातर खबरें ‘सूत्रों के हवाले’ से छपीं, हालांकि इस तरह की खबरें मार्च के मध्य से ही सामने आने लगी थीं।
इस नीति की तीखी आलोचना हुई है। बहरहाल, यह ड्राफ्ट नीति भविष्य में किस रूप में सामने आएगी, यह देखना बाकी है। सरकार ने इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया है।
प्रदूषण कम करने का बोझ आम लोगों पर
इस नीति का आधार यह दावा है कि पारंपरिक वाहनों से निकलने वाला धुआँ प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन इससे मुक्त हैं। यदि इस दावे को सही मान भी लिया जाए, तो सवाल उठता है कि प्रदूषण कम करने का सारा बोझ आम लोगों, खासकर कामकाजी वर्ग, पर ही क्यों डाला जा रहा है? दोपहिया वाहन और ऑटो-रिक्शा आम लोगों की आजीविका और आवागमन का प्रमुख साधन हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक प्रणाली में बदलने का खर्च उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन बनेगा। दूसरी ओर, कार मालिकों पर ऐसा कोई दबाव नहीं डाला गया है।
नीति में सार्वजनिक वाहनों का उल्लेख तो है, लेकिन नौकरशाहों और अन्य प्रभावशाली समूहों द्वारा सरकारी या निजी वाहनों के उपयोग पर कोई चर्चा नहीं है। इस नीति के अंतर्विरोध स्पष्ट हैं, और इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ के दावे भी ठोस नहीं दिखते।
सीएनजी का असफल प्रयोग और प्रदूषण की हकीकत
इस सदी की शुरुआत में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल वाहनों से होने वाले धुएँ को लेकर खूब हंगामा हुआ। न्यायालय ने सक्रियता दिखाते हुए डीजल वाहनों पर तत्काल प्रतिबंध, धुआँ उत्सर्जन करने वाली मशीनों पर कड़े मानक, और उद्योगों के लिए नीतियाँ लागू कीं। उस समय सीएनजी को प्रदूषण का रामबाण उपाय बताया गया, मानो यह दिल्ली की हवा को पूरी तरह स्वच्छ कर देगा। लेकिन पिछले 20 वर्षों का अनुभव और अध्ययन बताते हैं कि ये दावे गलत साबित हुए।
उस समय दावा किया गया था कि सीएनजी से हवा में मौजूद सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10) न्यूनतम स्तर पर आ जाएँगे। लेकिन आज दिल्ली में इन कणों की मात्रा न केवल कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है। हर साल सर्दियों की शुरुआत में धुएँ का धुंध (स्मॉग) दिल्ली को महीनों तक ढँके रहता है।
निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और कमजोर सार्वजनिक परिवहन
पिछले दस वर्षों के आँकड़े बताते हैं कि दिल्ली में कारों की संख्या ने भारत के अन्य शहरों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सरकारी उपयोग में आने वाले वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। DTC ने कुछ हद तक इलेक्ट्रिक बसों को अपनाया है, लेकिन अन्य सार्वजनिक वाहन अभी भी सीएनजी पर निर्भर हैं।
कई पर्यावरणविदों और संस्थानों की रिपोर्ट्स बार-बार इस बात पर जोर देती हैं कि दिल्ली में कमजोर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के कारण लोग निजी वाहनों पर निर्भर हो गए हैं। पिछले दस वर्षों में AAP सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन व्यवहार में इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई। उससे पहले, शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार के समय सार्वजनिक वाहनों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का प्रयोग भी असफल रहा।
आज दिल्ली की अधिकांश आबादी महँगी मेट्रो और सीमित संख्या में चलने वाली DTC बसों पर निर्भर है। एक बड़ी आबादी ओला, उबर जैसी निजी कैब सेवाओं या दोपहिया/चारपहिया वाहनों का उपयोग करने को मजबूर है। आवागमन का बढ़ता खर्च और सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता लोगों को निजी वाहनों की ओर धकेल रही है। दिल्ली-NCR में रहने वाले मेहनतकश लोगों के लिए दोपहिया वाहन न केवल सुविधा, बल्कि अनिवार्यता बन गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों का पर्यावरणीय प्रभाव
इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताना भी भ्रामक है। ये वाहन हवा में सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन करते हैं, और इनकी बैटरी उत्पादन और निपटान से होने वाला प्रदूषण पेट्रोल वाहनों से कम नहीं है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, इलेक्ट्रिक कचरा (E-waste) वैश्विक पर्यावरण के लिए एक नई चुनौती बन रहा है। भारत में 2015 में E-waste की मात्रा 1.47 लाख मीट्रिक टन थी, जो 2021 तक 21.50 लाख टन प्रतिवर्ष तक पहुँच गई। पिछले पाँच वर्षों में इसमें और वृद्धि होने का अनुमान है।
हाल ही में सरकार ने E-waste प्रबंधन के लिए एक नीति बनाई, जिसके तहत कचरे के निपटान का खर्च इलेक्ट्रिक कंपनियों पर डाला गया। इस नीति के खिलाफ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
प्रदूषण की समस्या: दोषारोपण का खेल
यह विडंबना है कि दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या को कभी पंजाब के किसानों पर, कभी अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर, कभी पेट्रोल-डीजल वाहनों पर, तो कभी वाहनों के अत्यधिक उपयोग पर डाल दिया जाता है। प्रदूषण को एक ऐसी पहेली बना दिया गया है, जिसका हल निकालने की बजाय दोषारोपण किया जाता है।
दिल्ली की मेट्रो और अन्य केंद्रीकृत वातानुकूलित परिवहन व्यवस्थाएँ भारी मात्रा में बिजली की खपत करती हैं। इस बिजली उत्पादन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। धुआँ न दिखना पर्यावरण की स्वच्छता की गारंटी नहीं है। यह ड्राफ्ट नीति एक शिक्षित समाज के साथ मजाक नहीं तो और क्या है?
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं)