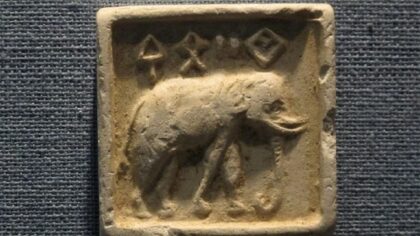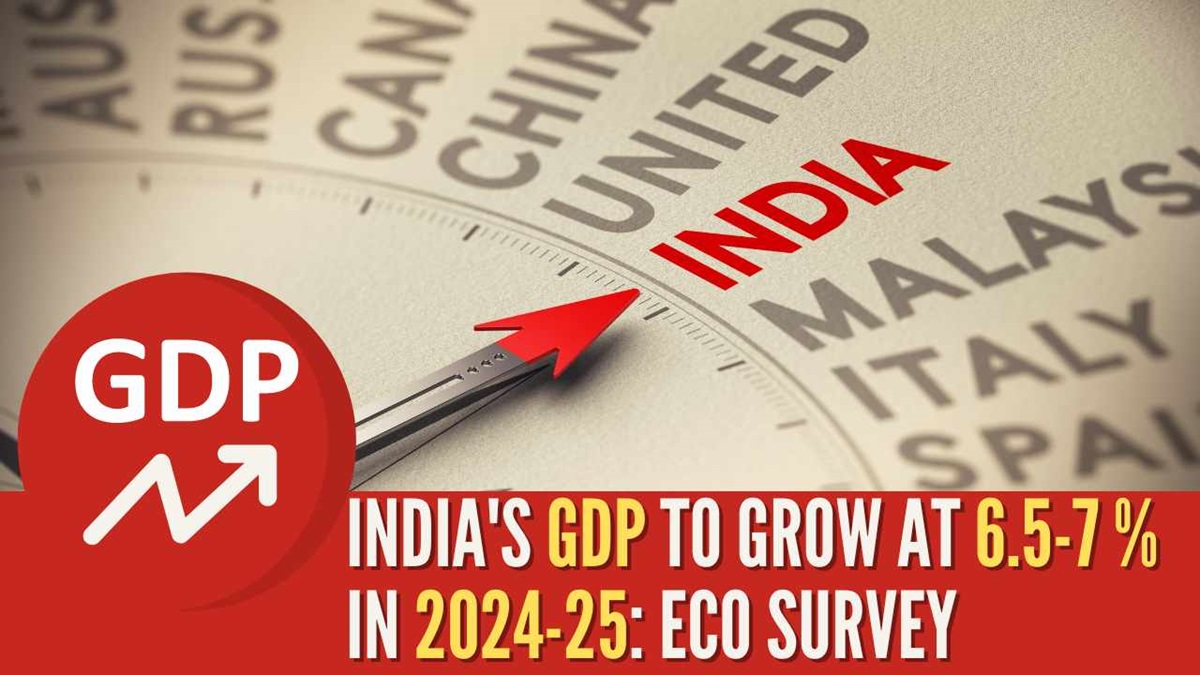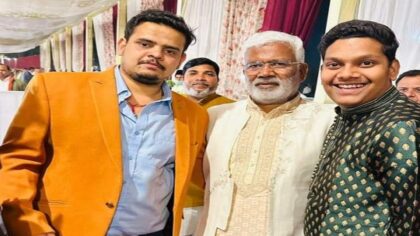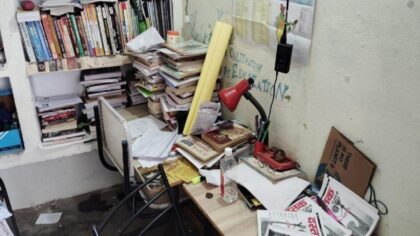जी हां! इस वर्ष की जीडीपी शुरुआत उतनी धमाकेदार नहीं हो सकी, जिसकी उम्मीद लगा रखी थी। खबर है कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल-जून की जीडीपी विकास दर 6.7% पाई गई है। यह पिछले 5 तिमाही का सबसे निचला स्तर है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जीडीपी विकास दर का अनुमान 7.1% लगा रखा था, जबकि रायटर्स अख़बार के द्वारा 52 अर्थशास्त्रियों के बीच किये गये सर्वेक्षण का औसत भी भारत की जीडीपी को 6.9% की दर पर प्रोजेक्ट कर रहा था।
देश के वित्तीय समाचारपत्रों की आज की यह सबसे बड़ी खबर है। जल्द ही सरकार, वित्त मंत्री, आरबीआई और तमाम अर्थशास्त्री इस बारे में लंबे-लंबे लेख लिखेंगे और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा।
लेकिन घबराएं नहीं, देश अभी भी सुरक्षित हाथों में है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता और अगले दो वर्षों के भीतर भारत, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने ही वाला है।
लेकिन इन चोंचलेबाजी से आपको क्या मिलेगा, या 90% भारतीय की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में न ही जीडीपी निकालने वालों को कोई फर्क पड़ता है और न ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को और न ही देश की सरकार को। फिर आप और हम इस जीडीपी के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? इसलिए, क्योंकि जो दिखता है, वही बिकता है।
इसलिए हम भी जीडीपी विकास दर पर चल रही बकवास के बारे में थोड़ा-बहुत जान लेते हैं। वर्ना हम विकास की दौड़ में पीछे छूट गये तो? देखिये नम्बर क्या कहते हैं? पिछली तिमाही में भारत की जीडीपी की विकास दर 8.2% थी, जबकि उससे पहले वाली तिमाही में तो विकास दर 12.8% के रिकॉर्ड स्तर पर थी, जिसकी तुलना में 6.7% तुलनात्मक रूप से काफी कम है।
इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में विकास दर 2% और सर्विस सेक्टर में 5.7% है, जो अपेक्षाकृत काफी कमजोर है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र और पॉवर सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है। अच्छी खबर ये है कि निजी खपत क्षेत्र में 58.6% से बढ़कर इस तिमाही में यह 60.4% हो गई है, हालांकि सरकारी खर्च की तेजी में कमी देखने को मिली है।
लेकिन अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य पहली तिमाही में 6.7% को अच्छी ग्रोथ मान रहे हैं। उनका कहना है कि देश में लोकसभा चुनावों की वजह से मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लगा हुआ था, और सरकार पूंजीगत व्यय को अमल में नहीं ला सकती थी, इसकी वजह से विकास दर नीची रही। जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा किया है, और खनन एवं बिजली उत्पादन में भी प्रगति हुई है।
अगली तिमाही में अच्छे मानसून और सरकारी खर्च में बढ़ोत्तरी के चलते ग्रोथ रेट में बेहतरी आने की संभावना है।बिजली, कोयला, स्टील और रिफाइनरी जैसे कोर सेक्टर में उत्पादन बढ़ने की खबर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरी का सूचक है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वी अनंत नागेश्वरण की मानें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार पर निरंतर गति से बढ़ने वाली है।
वैसे बता दें कि गोल्डमन साच्स ने एक सप्ताह पूर्व ही घोषित कर दिया था कि भारत की जीडीपी विकास दर 2024 और 2025 में अनुमान से 0.2% कम रहने वाली है। बैंक ने 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7% और 2025 के लिए 6.4% का अनुमान जारी किया है। इसके पीछे सरकार के द्वारा पहली तिमाही में खर्चों में कटौती को मुख्य कारक बताया गया है।
ये सब बातें हमारे देश के नीति-नियंता कर रहे हैं, और रेटिंग एजेंसियों तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा और स्टॉक मार्किट के गुरुओं की भाषा है। आम लोगों के लिए इन सारी बातों का कुल-जमा यही है कि आपकी पॉकेट में कुछ आये न आये देश की अर्थव्यवस्था की सींग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े हुए लोगों के हाथ से अभी नियंत्रण खत्म नहीं हुआ है।
आपको भारी आर्थिक झटका अभी भी नहीं लगने वाला है, और आप अगली एक-दो तिमाही आराम से सांस ले सकते हैं। इससे अधिक इन आंकड़ों का आम लोगों की जिंदगी में कोई महत्व नहीं है।
जीडीपी की बहस का फायदा क्या है?
स्वंय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मत है कि जीडीपी की गणना के द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था की हालत का ठीक-ठीक अंदाजा लगाना संभव नहीं है। वित्तीय सूचना साइट इन्वेस्टोपेडिया के अनुसार, जीडीपी को पहली बार 1937 में अमेरिका में महामंदी के दौरान एक अवधारणा के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
अर्थशास्त्री साइमन कुज़नेट्स ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट में इसका प्रस्ताव रखा था। बाद में इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मापने के मानक तरीके के रूप में व्यापक रूप से अपनाया गया। लेकिन अब कई विशेषज्ञों का कहना है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अब आउटडेटेड तरीका हो गया है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक प्रगति के एक प्रमुख ट्रैकर के रूप में, यह मानव, सामाजिक या प्राकृतिक पूंजी को मापने और उसका हिसाब रख पाने में असमर्थ है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के मुताबिक जीडीपी, राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के स्वास्थ्य को मापता है। GDP डेटा किसी देश में किसी विशेष अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य पर आधारित होता है। GDP को मापने से अर्थव्यवस्था का आकार और विकास दर के बारे में पता लगाया जा सकता है।
बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के अनुसार, GDP की गणना करने के तीन तरीके हैं। आप किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ सकते हैं या आप सभी की आय को जोड़ सकते हैं। GDP की गणना करने का तीसरा तरीका यह मापना है कि देश में सभी ने क्या खर्च किया है।
इसमें घरेलू खर्च, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात शामिल हैं – आपके देश के अन्य देशों को निर्यात के मूल्य में से आपके देश में आयात के मूल्य को घटाया जाता है।
जीडीपी क्यों मायने रखती है?
इन्वेस्टोपेडिया का कहना है कि जीडीपी नीति निर्माताओं, निवेशकों और व्यवसायों को अर्थव्यवस्था की सेहत को समझकर निर्णय लेने में मदद करती है। इसका उपयोग विभिन्न देशों और क्षेत्रों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। जब जीडीपी बढ़ रही होती है, तो श्रमिक और व्यवसाय आम तौर पर तब की तुलना में बेहतर स्थिति में होते हैं, जब यह नहीं बढ़ रही होती है।
आईएमएफ के मुताबिक, “जब जीडीपी घट रही होती है, तो अक्सर रोजगार में गिरावट आती है।” बीबीसी के मुताबिक, जीडीपी सरकारों को यह तय करने में मदद करती है कि “वे सार्वजनिक सेवाओं पर कितना खर्च कर सकती हैं और उन्हें करों में कितना इजाफा करना चाहिए।”
लेकिन किसी देश में जीडीपी ग्रोथ का मतलब यह नहीं है कि उस देश की जनसंख्या में सभी लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा होगा। उदाहरण के लिए, भारत में कोविड-19 महामारी के बाद से देखने को मिल रहा है कि कम मूल्य वाली उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे कि कुकर, बाइक, सस्ती कारें या एलआईजी और एमआईजी मकानों की बिक्री में भारी कमी आई है।
और अब रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी सस्ते मकानों के निर्माण का काम छोड़, लक्ज़री भवन निर्माण पर फोकस किया हुआ है। इसी प्रकार फ्रिज, एसी, एसयूवी कारों में भी विलासितापूर्ण वस्तुओं की डिमांड में बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि सस्ते फ्रिज, टीवी और बाइक की बिक्री में भारी गिरावट आई है।
देश की 90% आबादी के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, या उनकी कमाई घटी है। उधर दूसरी तरफ, चंद लोगों की कमाई या मुनाफे में उछाल आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में जीडीपी वृद्धि का फायदा, चंद लोगों को हो रहा है, जबकि आबादी के बड़े हिस्से की ग्रोथ बढ़ने के बजाय रुक गई है या उनकी माली हालत बिगड़ रही है।
लेकिन तेज जीडीपी वृद्धि के आंकड़े दिखाकर सरकार और अर्थशास्त्री इस कड़वी हकीकत को छिपाने में लगे हुए हैं, और उस छोटे से हिस्से के लिए विदेशी पूंजी निवेश और गहन पूंजी निवेश की अपनी गरीब विरोधी आर्थिक नीति को जारी रखने जा रहे हैं।
दूसरा, किसी देश में जीडीपी विकास दर है, लेकिन देश में जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो वास्तव में यह विकास दर क्या है? आबादी के जिस हिस्से में इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है? इसी प्रकार मुद्रा स्फीति और जीडीपी विकास दर का भी संबंध आपस में विरोधाभाषी है।
पिछले दो वर्षों से भारत में खाद्य पदार्थों के दाम में भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। धनी वर्ग के लिए खाद्यान्न में मूल्य वृद्धि का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिन परिवारों की आय ही 8-10,000 रूपये मासिक है, उनके लिए सालाना 6-8% मुद्रा-स्फीति का मतलब वास्तविक आय में भारी कमी है।
इसी प्रकार, यदि पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.7% के स्थान पर 2% ही होती, लेकिन देश की 90% आबादी की आय में 5% की वृद्धि और खाद्य पदार्थों के मूल्य में कमी आ गई होती, तो यह 80% आबादी की आय में वृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता।
इसलिए कहा जा सकता है कि जीडीपी वृद्धि की चोंचलेबाजी से बड़ी पूंजी और स्टॉक मार्केट में निवेशकों एवं विदेशी संस्थागत निवेशकों का भले ही लाभ होता हो, देश की वास्तविक दशा-दिशा में इससे कोई लाभ नहीं होता।
कई बार तो इसके आंकड़ों को दिखाकर व्यापक आबादी के वास्तविक मुद्दों की अनदेखी कर देश और देशवासियों को दीर्घकालिक संकट के हवाले कर दिया जाता है।
(रविंद्र पटवाल जनचौक की संपादकीय टीम के सदस्य हैं।)