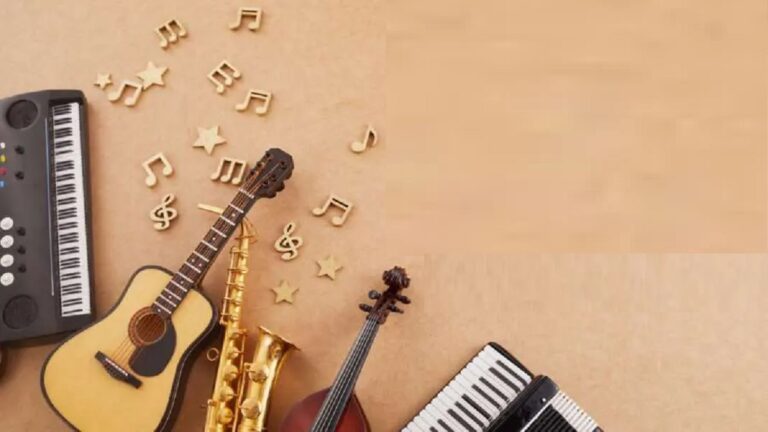यह पहला हिंदी दिवस था जब हिंदी भाषा के विषय में लिखने में संशय, दुविधा और संकोच का अनुभव हुआ। भय इस बात का था कि हिंदी के प्रति प्रेम और कृतज्ञता की किसी भी अभिव्यक्ति का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए न कर लिया जाए जो हिंदी की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल और उसकी आत्मा पर आघात करने वाला हो, जो हिन्दी के तेवर और मिजाज के एकदम ख़िलाफ़ हो। निजी चर्चाओं में- जो शायद सोशल मीडिया पर चल रही बहसों से प्रेरित थीं- कई मित्र कहते पाए गए कि हम हिंदी भाषी कायर हैं, हममें हमारी अघोषित राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रति गौरव की भावना का सर्वथा अभाव है, हम तो उसे यह दर्जा भी नहीं दिला पाए हैं। हिंदी तो हमारी मातृ भाषा है बावजूद इसके हम उसका तिरस्कार देख रहे हैं और फिर भी चुप हैं। आप दक्षिण में चले जाइए, बंगाल या उड़ीसा में चले जाइए, आप हिंदी भाषी होने के कारण वहां पराए ही बने रहेंगे। इन इतर भाषा भाषी प्रदेशों के निवासियों को समझाना पड़ेगा कि अगर नए भारत में रहना है तो हिंदी के सम्मुख नतमस्तक होना ही होगा। और यह सीख सबसे पहले उन्हें हिंदी भाषी प्रदेशों द्वारा दी जानी चाहिए। हमारी हिंदी पट्टी से जब इन इतर भाषा भाषियों का दाना पानी बन्द होगा तब इनके होश ठिकाने आएंगे। ऐसा लगा कि नए भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे एनआरसी के लिए हिंदी के रूप में एक नया आधार युद्ध स्तर पर तैयार हो रहा है। समय समय पर हिंदी भाषा के भीतर भी एक एनआरसी लागू करने के असफल प्रयास होते रहे हैं। यह प्रयास हिंदी को पराए शब्दों से मुक्त करने की अपीलों के रूप में होते हैं और संस्कृतनिष्ठ हिंदी को शुद्ध और पवित्र मानने के विचित्र विचार पर आधारित होते हैं जो शायद भाषा वैज्ञानिक रूप से जितना असंगत है उससे भी ज्यादा व्यवहारिक रूप से अस्वीकार्य है।
हिंदी का इतिहास यह बताता है कि हिंदी शासकों और शोषकों की भाषा कभी नहीं रही। चाहे वह भद्रजनों और विद्वानों द्वारा धार्मिक कर्मकांडों में अपनाई जाने वाली भाषा संस्कृत हो या मुग़ल शासकों की राज भाषा फ़ारसी – ये हिंदी को भाषा वैज्ञानिक और शब्द भंडार की दृष्टि से निर्मित या प्रभावित अवश्य करती हैं किंतु इन भाषाओं में व्याप्त कुलीनता का अहंकार हिंदी को छू तक नहीं पाया है। हिंदी ने अपना शर्मीला स्वभाव बरकरार रखा है और राजभाषा का दर्जा हासिल करने के बावजूद जब भी अंग्रेजी ने अकड़ दिखाई है या क्षेत्रीय भाषाओं ने अपने स्वर उच्च किए हैं- हिंदी ने पलटवार करने के बजाए झुकना ही पसंद किया है। हिंदी की प्रकृति विस्तारवादी कभी नहीं रही। विश्व के अनेक देशों में हिंदी भाषी लोगों की उपस्थिति है, ये वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में अपनी सशक्त पकड़ भी रखते हैं, सत्ता में या उसके आस पास इनकी निर्णायक मौजूदगी भी होती है किंतु इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ कर इन्हें कभी जन प्रतिरोध, गुस्से एवं घृणा का सामना करना नहीं पड़ा है। हिंदी और हिंदी भाषी ज़मीन के बजाए दिलों को जीतने पर भरोसा करते रहे हैं और तोड़ने के बजाए जोड़ने पर विश्वास करना उनका स्वभाव है।
हिंदी और उर्दू के बीच विभाजनकारी रेखा सर्वप्रथम ‘फूट डालो और राज करो’ के सिद्धांत के हिमायती अंग्रेजों ने खींची थी। इससे पहले तो मीर और गालिब जैसे नामचीन शायर खुद को हिंदवी या हिंदी के साहित्य सेवी का दर्जा देते थे। बारहवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी के अंत तक हिंदी और उर्दू का विभाजन तो दूर ब्रज और अवधी का भेद भी उपस्थित नहीं था। फ़ारसी भाषा और साहित्य परंपरा से प्रभावित साहित्यकार नस्तालिक लिपि में अपनी रचनाएं करते थे और अपनी भाषाओं को हिंदवी या हिंदी और देहलवी की संज्ञा देते थे। अमीर खुसरो द्वारा मसनवी नुह्सेपहर में भारत की बारह महत्त्वपूर्ण भाषाओं के साथ ‘देहलवी’ की भी गणना की गई है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा और साहित्य परंपरा का अनुसरण करने वाले साहित्यकार जो अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए नागरी या कैथी लिपि का उपयोग करते थे वे अपनी भाषा को भाखा कहा करते थे। इन भाषाओं की कोई विशेष धार्मिक पहचान रही हो ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता।
प्रोफेसर शैलेष ज़ैदी ने हिंदवी के चर्चित अचर्चित कवियों को बहुत परिश्रम पूर्वक सूचीबद्ध किया है। बारहवीं से सोलहवीं शताब्दी के बीच अपनी विलक्षण प्रतिभा से साहित्य जगत को चमत्कृत करने वाले अब्दुर्रहमान, बाबा फ़रीद, हमीदुद्दीन नागौरी, बू अली क़लन्दर, अमीर खुसरो, यह्या मनयरी, शम्स बलखी, मुल्ला दाऊद,शेख मंझन, मलिक मुहम्मद जायसी आदि सभी हिन्दवी के ही कवि थे। हिंदवी आम जनता की भाषा थी। मुग़ल शासकों द्वारा सेना में स्थानीय लोगों की भर्ती, हाट बाजारों में होने वाली अंतर्क्रिया तथा मुगल शासकों एवं स्थानीय निवासियों के मध्य संबंधों की स्थापना ने हिंदवी को जन्म दिया जिसमें मध्य एशिया की भाषाओं के शब्द बड़ी तादाद में उपस्थित थे। न केवल भाषा के गठन की दृष्टि से हिंदवी आम लोगों की जरूरतों से उपजी थी बल्कि काव्य विषयों की दृष्टि से भी वह प्रगतिशील तत्वों से भरपूर थी और शरीअत के संकीर्ण बंधनों पर प्रहार करते हुए धार्मिक कर्मकांडों की जकड़न से दूर प्रेम और विश्वास के एक उदार लोक की झलक स्वयं में समेटे थी। सूफी कवियों और सिद्ध योगियों के मध्य वैचारिक अंतर्क्रिया निरन्तर होती रहती थी।
देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले भाखा के कवियों की विशेषताएं भी लगभग ऐसी ही हैं, संस्कृत के आधिपत्य को चुनौती देते ये कवि प्रेम और पारस्परिक सौहार्द के माध्यम से उस ईश्वर की प्राप्ति को सुलभ बनाने में लगे थे जिसे अन्यथा जटिल कर्मकांडों का चक्रव्यूह रचकर आम जनता की पहुंच से दूर कर अभिजात्य वर्ग तक सीमित कर दिया गया था। चाहे वे कबीर हों या तुलसी आम लोगों को उनके जीवन की पीड़ा और दुविधा से मुक्ति दिलाना इनकी रचनाओं का लक्ष्य था।
इतिहास यह दर्शाता है कि हिंदी अपनी उत्पत्ति से ही उस सामासिक संस्कृति की सशक्त अभिव्यक्ति रही है जो हमारे बहुजातीय एवं बहुधर्मी देश में सहज स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। किंतु इतिहास के अध्ययन के अपने खतरे हैं। हिंदी नवजागरण की प्रकृति असंदिग्ध रूप से उपनिवेशवाद विरोधी थी किंतु स्वातंत्र्य पूर्व काल में जिस प्रकार अत्यंत उदार और विचारशील हिन्दू एवं मुस्लिम नेता भी संकीर्ण धार्मिक पहचान और व्यापक समावेशी संस्कृति के मध्य चयन की दुविधा से जूझते रहे उसी प्रकार हिंदी और उर्दू के विद्वान भी निज भाषा एवं निज संस्कृति की व्याख्या में धर्म को आधार बनाने की प्रवृत्ति से ग्रस्त होते रहे।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अनेक विद्वान हिन्दू-मुस्लिम एकता के पोषक और ऐसी भाषा के प्रयोगकर्ता एवं समर्थक के रूप में देखते हैं जो भारतेंदु युगीन भाषा परंपरा के अधिक निकट थी और उर्दू फ़ारसी के शब्दों से परहेज़ नहीं करती थी। किन्तु हिंदी प्रदीप के अंक 15 में अक्तूबर 1884 में महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं– कचहरियों में उर्दू अपना दबदबा जमाये हुए है। अपने सहोदर पुत्र मुसलमानों के सिवा हिन्दू जो उसके सौतेले पुत्र हैं उन्हें भी ऐसा फंसाय रखा है कि उसीके असंगत प्रेम में बंध ऐसे महानीच निठुर स्वभाव हो गये हैं कि अपनी निजी जननी सकल गुण आगरी नागरी की ओर नजर उठाय भी अब नहीं देखते। एक अन्य स्थान पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं- कुछ समय से विचारशील जनों के मन में यह बात आने लगी है कि देश में एक भाषा और एक लिपि होने की बड़ी जरूरत है, और हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि ही इस योग्य है। हमारे मुसलमान भाई इसकी प्रतिकूलता करते हैं। वे विदेशी फारसी लिपि और विदेशी भाषा के शब्दों से लबालब भरी हुई उर्दू को ही इस योग्य बतलाते हैं। परन्तु वे हमसे प्रतिकूलता करते किस बात में नहीं ? सामाजिक, धार्मिक, यहां तक कि राजनैतिक विषयों में भी उनका हिन्दुओं से 36 का संबंध है। भाषा और लिपि के विषय में उनकी दलीलें ऐसी कुतर्कपूर्ण, ऐसी निर्बल, ऐसी सदोष, ऐसी हानिकारिणी हैं कि कोई भी न्यायनिष्ठ और स्वदेशप्रेमी मनुष्य इनसे सहमत नहीं हो सकता। बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्री, और मदरासी तक जिस देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा को देशव्यापी होने योग्य समझते हैं वह अकेले मुट्ठी भर मुसल्मानों के कहने से अयोग्य नहीं हो सकती। आबादी के हिसाब से मुसल्मान इस देश में हैं ही कितने ? फिर थोड़े होकर भी जब वे निर्जीव दलीलों से फारसी लिपि और उर्दू भाषा की उत्तमता की घोषणा देंगे तब कौन उनकी बात सुनेगा? (महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली, प्रथम खण्ड, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, पृष्ठ 21) बावजूद इन उद्धरणों के द्विवेदी जी के लिए कोई सस्ता फतवा जारी करना उनके साथ ज्यादती होगी क्योंकि उनका दोष शायद इतना ही था कि उनकी दृष्टि अपने समय से पार नहींं देख पाई थी।
पाश्चात्य दर्शन एवं आलोचना का गहन अध्ययन, उर्दू पर अच्छी पकड़ व रसखान, जायसी, कुतुबन, अमीर खुसरो आदि पर सविस्तार सकारात्मक लेखन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनूठी विशेषताएं हैं। किंतु त्रिवेणी में जायसी का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी अनायास ही लिख जाते हैं- कुतुबन ने मुसलमान होते हुए भी अपनी मनुष्यता का परिचय दिया। इस एक कथन को आधार बना कर शुक्ल जी की आलोचना के उदार पक्षों को खारिज करना ठीक नहीं है। शुक्ल जी मध्यकाल को हिन्दू मुस्लिम संघर्ष के लिए स्मरण करने की प्रवृत्ति का ही परिचय दे रहे हैं और हममें से बहुत से लोगों की सोच कुछ ऐसी ही है चाहे हम हिन्दू हों या मुसलमान। शुक्ल जी का यह कथन दर्शाता है कि अध्ययनशील और सजग बुद्धिजीवी भी अंग्रेजों द्वारा गढ़े गए उस नैरेटिव के जाने अनजाने शिकार बन जाते थे जो हिंदुओं और मुसलमानों को शत्रु के रूप में प्रस्तुत करता था- दो ऐसी कौमें जो धार्मिक सांस्कृतिक रूप से इतनी भिन्न थीं कि आपसी संघर्ष ही इनकी नियति था।
वर्तमान समय में किसी भी विद्वान के कथनों को उनके व्यापक संदर्भों से काटकर अपने संकीर्ण हितों की सिद्धि के लिए प्रस्तुत करने का चलन बना हुआ है। चाहे वे बहुसंख्यक की तानाशाही एवं संकीर्ण राष्ट्रवाद की वकालत करने वाली शक्तियां हों या इनका प्रतिकार करने वाली वाम रुझान वाली ताकतें- दोनों का विश्वास सतही सामान्यीकरणों के आधार पर देशभक्त, राष्ट्रवादी या ब्राह्मणवादी जैसे फतवे जारी करने पर है और सोशल मीडिया के पाठकों को ये खूब रुचिकर और प्रेरक भी लगते हैं। उदार और वैज्ञानिक सोच एवं परंपरा तथा धर्म के विमर्श के बीच झूलते दुविधाग्रस्त मनीषियों के मूल्यांकन के लिए इतिहास को समग्रता से समझना आवश्यक है। किन्तु ऐसा हो नहीं रहा। इतिहास से मनचाहा और मनमाना खिलवाड़ करने की यह प्रवृत्ति बड़ी घातक है।
यह कटु सत्य है कि किसी बच्चे को भी यदि सही संबंध स्थापित करने जैसा प्रश्न दिया जाए तो वह उर्दू का संबंध मुसलमान और हिंदी का संबंध हिंदुओं से जोड़ेगा। यह विभाजनकारी सोच देश के बंटवारे के लिए उत्तरदायी रही और पाकिस्तान का उर्दू प्रेम पुनः उसके विभाजन का कारण बना। अब पुनः भाषा का भाषेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा दिए गए नारे “जपौ निरंतर एक ज़बान/ हिंदी हिन्दू हिन्दुस्तान” की गूंज फिर सुनाई दे रही है। अब क्षेत्रीय भाषाएं निशाने पर हैं। इन्हें राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुलवादी सामासिक संस्कृति और सोच के आधार पर बहुत खूबसूरती से चल रहे देश के लोग अचानक पता नहीं क्यों सशंकित हो रहे हैं कि उनकी भाषा का निरादर हो रहा है या उनसे उनकी भाषा छीनी जा सकती है। पता नहीं किस राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने की बात हो रही है जिसके अभाव में मानो आज देश खण्ड खण्ड होकर गहरे संकट में है।
अब जब तकनीकी क्रांति सारे बंधनों को तोड़ने के बहुत निकट पहुंच रही है तब भाषा का सवाल अर्थहीन सा लगता है। हिंदी को जन जन की भाषा बनाने में मठाधीशों की जितनी भूमिका रही है उससे कहीं अधिक भूमिका शायद हिंदी सिनेमा और लुगदी साहित्य की रही है। मनोरंजन के साधनों के रूप में सिनेमाघरों की स्थापना, टेलीविजन, सीडी-डीवीडी-पेन ड्राइव का जमाना, और अब मोबाइल टीवी – तकनीकी विकास के बदलते रूप हैं। यह हमारे जीवन के अविभाज्य अंग हैं। लगभग अस्सी के दशक तक हिंदी सिनेमा की भाषा को कोई अल्पज्ञ बड़ी आसानी से उर्दू कह सकता था लेकिन यह आम हिंदुस्तानी के दिल में उतरने वाली बोलचाल की भाषा ही थी। हिंदी सिनेमा ने हिंदी को देश और दुनिया में खूब फैलाया। इक्कीसवीं सदी के इन प्रारंभिक वर्षों में सिनेमा और टीवी सीरियलों की भाषा हिंगलिश कही जा सकती है। दृश्य श्रव्य माध्यमों में अभिनय, संगीत, साज सज्जा आदि ऐसे कितने ही साधन उपलब्ध होते हैं कि भाषा सशक्त न होने पर भी न भावाभिव्यक्ति प्रभावित होती है, न भावों की संप्रेषणीयता में कमी आती है। हल्के, तनाव रहित ऐंद्रिक मनोरंजन की अपेक्षा रखने वाले पाठकों को हिंदी के लुगदी साहित्य ने खूब लुभाया। बाद में इस तरह का मनोरंजन सीरियलों के जरिए मिलने लगा। आज भी आम लोगों की वेशभूषा, व्यवहार और भाषा पर फिल्मों और सीरियलों का प्रभाव देखा जा सकता है।
तकनीक ने अनुवाद को सरल और सर्व सुलभ कर दिया है। फिल्में रिलीज़ के समय ही अनेक भाषाओं में डब होकर हर तरह के दर्शकों तक पहुंचती हैं। क्षेत्रीय सिनेमा और हिंदी सिनेमा तथा भारतीय सिनेमा और विश्व सिनेमा के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं। अंग्रेजी भाषा की बेस्ट सेलर किताबें लगभग तत्काल ही हिंदी में उपलब्ध हो जाती हैं। कई हिंदी के अखबार अंग्रेजी से अनुवाद की बुनियाद पर निकल रहे हैं। गूगल तत्काल ही एक भाषा से दूसरी भाषा में कामचलाऊ अनुवाद कर देता है। अनुवाद में जो गलतियां दिखती हैं, वे भी बेहतर सॉफ्टवेयर आने के साथ कम हो जाएंगी। लिपियों का महत्व भी कम हो रहा है। रोमन लिपि में टाइप कर किसी भी भारतीय भाषा की लिपि में अपने कंटेंट को पाया जा सकता है। फोनेटिक टूल्स दिनों दिन परिमार्जित होते जा रहे हैं। स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही बोलकर लिखना संभव हुआ है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने हर आयु वर्ग और हर शैक्षिक स्तर के लोगों को अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की सुविधा दी है। यह अभिव्यक्ति अनगढ़ है, अपरिमार्जित और अपरिष्कृत है किंतु सोशल मीडिया पर मिलने वाली डांट फटकार और ऑनलाइन व्याकरण एवं वर्तनी की जांच करने वाले टूल्स के जरिए लोग स्वयं को सुधार भी रहे हैं। पुराने मापदंडों पर यह भाषा भले ही कमजोर है किंतु इसे ग्रहण करने वाले पाठक और श्रोता को स्पंदित करने में यह सर्वथा सक्षम है। न तो इसकी सुग्राह्यता में कोई कमी आई है न लोगों की संवेदनशीलता में। विश्व व्यापार की जरूरतें ऐसी हैं कि जो भी नए उपकरण बन रहे हैं वह भाषा के बंधनों को गौण बना रहे हैं।
व्यावसायिक सफलता अर्जित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने अधिकारी कर्मचारियों को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने का प्रशिक्षण दे रही हैं। एक विशाल बाजार के रूप में भारत की संभावनाओं ने हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं में पूरी दुनिया की रुचि जगा दी है। हिंदी अगर विश्व भाषा का रूप ले रही है तो इसके पीछे बाजार की ताकतें बड़ी हद तक जिम्मेदार हैं। हिंदी की शक्ति का उद्घोष करते करते हमें यह स्मरण रखना होगा कि आत्म गौरव का भाव यदि यथार्थ की बुनियाद पर नहीं टिका है तो वह आत्मप्रवंचना में बदल सकता है। आज भाषा को महज सूचनाओं और आवश्यकताओं के संप्रेषण के माध्यम के रूप में रिड्यूस कर दिया गया है। ऐसी दशा में भाषा के जरिए हिंसक सर्वोच्चता स्थापित करने की रणनीति सफल होगी ऐसा नहीं लगता। भाषाई आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन की प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान भड़की हिंसा के समय हिंदी भाषी लोगों ने असाधारण संयम का परिचय दिया था। यदि पारस्परिक सद्भाव, सामाजिक समरसता तथा अपनी भाषा की हिंसक विजय में से किसी एक को चुनना होगा तो हिंदी भाषी निश्चित ही पहले विकल्प का चयन करेंगे।
(डॉ. राजू पाण्डेय स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रहते हैं।)