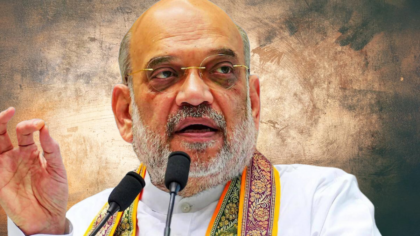लोकतंत्र में चुनाव के महत्व से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी लोकतंत्र को कमजोर करता है। चुनाव संपन्न कराने के काम में गंभीर गड़बड़ी की आशंकाएं आम है। जीवन का और इसलिए लोकतंत्र का भी आधार विश्वास है।
कहना न होगा कि संस्थाओं की विश्वसनीयता में काफी छीजन आई है। इस छीजन से जीवन भी परेशान है और लोकतंत्र भी हलकान है। परेशान जीवन और हलकान लोकतंत्र भारत का हकलाता हुआ सच है, जो दहाड़ते हुए झूठ के डर से दुबका हुआ है।
ऐसे में क्या तो जनमत सर्वेक्षण और क्या चुनाव परिणाम! चुनाव परिणाम के दायरे में कयासों के कबूतर उड़ाने का ही क्या फायदा! जीवन का हर कार्य चुनाव परिणाम पर पड़नेवाले असर को रखकर करना न तो उचित है और न उसकी व्याख्याएं ही उस ‘नजरिये’ से की जानी चाहिए।
चुनावी माहौल में बात सिर्फ जीत-हार की होती है, जीवन के जरूरी प्रसंग आच्छादित हो जाते हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण और सबसे बड़े घटक दल, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर सबकी खास नजर रहती है। सब की यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), इंडिया अलायंस, विभिन्न रंग-ढंग के राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषकों, पत्रकारों और आम लोगों की खास नजर।
वे क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या कहते हैं, वगैरह-वगैरह। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे राजनीति में हैं और विपक्ष में हैं। वे इस ‘खास नजर’ के होने से बिल्कुल अनजान भी नहीं रहते होंगे। समझा जा सकता है कि वे ‘खास नजर’ में डालने के लिए भी ‘कुछ-कुछ’ करते हैं, कहते हैं।
जीवन के हर क्षेत्र में ‘सर्व-बुझक्कड़’ होते ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग चुप-चाप देख लेते हैं, जो बोलना होता है वह लगभग मन-ही-मन बोल लेते हैं। आम लोगों में समझने की सहज बुद्धिमत्ता (Common Sense) होती है, वे भी अपने ढंग से अपने लिए समझा करते हैं।
राहुल गांधी की गतिविधियों के वीडियो मीडिया में घूमते रहते हैं। लोग-बाग उनकी गतिविधियों का मजा भी लेते हैं और समझते भी रहते हैं। पिछले दिनों वे दीया बनानेवाले परिवार से मिले। परिवार में बच्चियां और महिला उन्हें अपना काम समझा रही थी। वे काम को करते हुए समझने की कोशिश करते हुए दिखे।
वे जिस किसी भी कामगार के पास जाते हैं, उस कामगार के काम को करते हुए समझना चाहते हैं। कामचलाऊ ही सही लेकिन राहुल गांधी की समझ के इस कायदा और कवायद महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है।
वे उस काम के महत्व को समझते हुए उसे बढ़ावा देने, जीवनयापन के साधन के रूप में उसे समानांतर आर्थिकी से जुड़ने-जोड़ने की संभावनाओं का भी इशारा करते हैं।
कहना जरूरी है को काम करने को आर्थिकी से जोड़ने के साथ-ही-साथ काम करने को कामगार के सम्मान और आनंद से भी जोड़ने का प्रयास करते दिखते हैं। जीवनयापन में स्वावलंबन और पर्यावरण-पोषी आर्थिक गतिविधि और विकास का भी संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं।
शायद यही वह पेच है जिस के चलते उग्रता-प्रधान राजनीति और आक्रामक विकास के गठजोड़ को राहुल गांधी की राजनीतिक उपस्थिति और कार्यशैली की बहुआयामी कल्पनाशीलता से परेशानी और बेचैनी होती है।
सिर्फ चुनावी जीत और सत्ता की आकांक्षा राहुल गांधी में होती तो राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पूंजी-पार्टी ही क्यों न हो, राहुल गांधी को ‘मैनेज’ करना उनके लिए बहुत कठिन नहीं होता।
इस बार काम करते हुए राज-मिस्त्री से मिलने गये तो साथ में उन का भांजा भी था। सर्व-बुझक्कड़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि वे अपने भांजे को राजनीति में ‘लॉन्च’ कर रहे हैं! अगर वे अपने भांजे को कामगारों की दुनिया से परिचित करवा रहे हैं, तो इस में गलत क्या है?
रही ‘लॉन्च’ करने की बात तो कहनेवाले तो यह भी कहते रहे हैं कि ‘परिवारवादी कांग्रेस’ राहुल गांधी को ‘लॉन्च’ करने में लगी रहती है। यह कहने कोई संकोच नहीं है कि जिन्हें लोकतंत्र में यकीन नहीं है वे ही ‘लॉन्च की राजनीति’ पर सब से ज्यादा बात करते हैं। कहनेवाले तो खुद राहुल गांधी को ही राजनीति में अनिच्छुक नेता भी कहा करते थे।
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के आभा-मंडल से जुड़ी पूरी व्यवस्था राहुल गांधी को ‘बेवकूफ’ साबित करने में लगी हुई थी। हां, यह समझना भूल होगी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के आभा-मंडल से जुड़ी व्यवस्था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही काम नहीं करती है।
वह व्यवस्था कहीं भी हो सकती है और कांग्रेस के अंदर तो खैर रही है! राहुल गांधी को ‘बेवकूफ साबित’ करने की परियोजना अब यकीनन फेल हो चुकी है। अब तो राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के ‘जिम्मेवार लोग’ ने ही कह दिया है कि ‘राहुल गांधी उनसे मिलते ही नहीं हैं।’
यहां कम-से-कम दो बातें स्पष्ट हो गई, पहली यह कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के साथ उनका टकराव वास्तविक है। और दूसरी यह कि इस टकराव और मनमुटाव को ‘लाभप्रद मेल-मिलाप’ में बदलने के लिए सार्वजनिक रूप से ‘मास्टर-स्ट्रोक’ लगाने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने कर दी है।
हालांकि इस ‘मिलते ही नहीं में’ उनकी अपनी चालाकी भी छिपी हुई है। वैसे, देखा जाये तो राहुल गांधी तो उन से रोज मिलते हैं। हां, उस तरह नहीं मिलते हैं जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के लोग मिलना चाहते हैं; ढाल और तलवार की तरह से मिलते हैं।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से किसी का मिलना असल में उसके मिटने की पूर्व क्रिया है। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के घुलने-मिलने में मिलने के इरादा में मिलने की चाहत उतनी नहीं होती है, जितनी कि मिलनेवाले को अपने में घुला लेने की धूर्तता होती है।
अपने ‘बचपन’ में ही राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने मुसलमान, कम्युनिस्ट आदि को दुश्मन के रूप में चिह्नित कर लिया था। आज भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कांग्रेस में उन्हें मुसलमान और कम्युनिस्ट दोनों की प्रेत-छाया डोलती नजर आती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर कांग्रेस मुक्त भारत करने में फेल होने के बाद अब ‘प्लान-बी’ के तहत बार-बार कांग्रेस को ‘अर्बन नक्सल’ के द्वारा संचालित पार्टी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने तो कांग्रेस मुक्त भारत की गर्जना और ‘अर्बन नक्सल’ की घोषणा पर तो कभी अपना ‘श्रीमुख’ नहीं खोला! अब क्यों राहुल गांधी की संगत करना चाहते हैं?
अद्भुत है पहले बेवकूफ साबित करने की लीला खुले आम करते रहे, अभी भी ‘अर्बन नक्सल’ बताते अघाते नहीं हैं!
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के परम-प्रिय बुलडोजर पराक्रमी योगी आदित्यनाथ अयोध्या में प्रकाश-पर्व मनाते हुए काशी, मथुरा को याद करते हैं। किस इरादे से? उसी मथुरा में बैठक के बाद राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मुहब्बत की दुकान चलानेवाले राहुल गांधी से मिलने-जुलने की बात कहते हैं।
महाभारत में प्रसंग है कि ऐसी ही परिस्थिति में ‘अंकल धृतराष्ट्र’ भीम से मिलने और गले लगाने की पवित्र भावना से पीड़ित हो गये थे। वहां कृष्ण थे तो धृतराष्ट्र के गले लगते ही भीम की लौह-मूर्ति चूर-चूर हो गई और भीम मुसकुराते हुए बच निकले। कुल मिलाकर यह कि इस मिलने में कहीं कोई भलाई नहीं है, इतना तो राहुल गांधी भी जानते ही होंगे! क्या पता! मिल ही लेंगे!
समय के साथ उत्थान-पतन होता रहता है। यह जीवन की और जगत के विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहां यह भी दिखता है कि किसी भी ‘उत्थान’ में ‘सब के कुछ-कुछ’ के उत्थान का कोई-न-कोई प्रसंग होता है, तभी उसे उत्थान माना जाता है। ‘पतन’ में अधिकतर का पतन होता है और ‘कुछ या एक’ का ही उत्थान होता है और अधिकतर का ‘पतन’ होता है।
कहना न होगा कि उथल-पुथल का दौर उत्थान-पतन के रूप में सामने आता है। भारत इस समय उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है तो जाहिर है कि इस में उत्थान-पतन भी शामिल है। गौर करना चाहिए कि इस उथल-पुथल में किस के उत्थान की और किसके पतन की प्रक्रिया शामिल है।
आम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। सच पूछा जाये तो भारत में आम लोगों की संख्या बहुत नहीं है। पूरे ‘मतदाता समाज’ को आम आदमी माना जा सकता है क्या? माना जा सकता है, लेकिन कौन मानता है! कोई नहीं। वह क्या बात होती है जो आदमी को आम आदमी बनाती है?
शायद ही इस मामले में कोई सर्वमान्य मत या परिभाषा हो। क्या आम लोग मध्य वर्ग का होता है? क्या मध्य वर्ग के सभी लोग आम आदमी ही होते हैं? धनाढ्य, जीवन के विभिन्न क्षेत्र के प्रसिद्ध, प्रशंसित और पदानुसार शक्तिशाली लोग आम आदमी में गिने जा सकते हैं! नहीं गिने जा सकते हैं।
आम आदमी वे होते हैं जिन के पास सपने होते हैं। जिंदगी भर सपनों का पीछा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज-कल में ही, या आज नहीं तो कल उन का सपना जरूर सच होकर रहेगा। सपने पूरे होते हैं कभी आधा तो कभी अधूरा।
आम आदमी शहर का हो तो वह होता है जिसकी जिंदगी का बहुमूल्य समय लाइन लगाते हुए बीतती है, कभी सवारी पाने के लिए तो कभी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। आम आदमी, जिस के सिर पर छटनी की प्रेत-छाया मंडराती रहती है।
गांव का है तो आम आदमी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क के किनारे या पंचायत भवन के सामने चुकूमुकू बैठक में संवैधानिक लोकतंत्र का समय काटता रहता है। जिनके पास न सपने बचे हैं न कोई उम्मीद बची है, आम आदमी के गोल से बाहर हो जाते हैं।
जिनके सामने सभ्य, बेहतर सामाजिक और नागरिक जीवन की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, उन्हें आम आदमी कहा जा सकता है क्या! इस सवाल के जवाब पर ही यह तय किया जा सकता है कि आम आदमी की तादाद में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है या कमी आ रही है!
चुनाव में आम आदमी की नहीं मतदाता समाज की भूमिका होती है। यह तब-जब चुनाव सही-सही हो। सही-सही चुनाव हो इस के लिए आदर्श आचार संहिता बनी हुई है! कैसी आदर्श आचार संहिता! चुनाव आयोग पर ही कोई आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है।
राजनीतिक दलों पर चुनावी आदर्श आचार संहिता कैसे लागू हो सकता है? चुनाव आयोग के पास शिकायतें की जा रही है। मगर शिकायत करने से क्या फायदा? क्या फायदा, जब शिकायतों पर गैर की तरह से गौर किया जाना स्वीकृत रिवाज बन गया हो।
पुरखों का कितना विश्वास रहा होगा लोकसेवकों पर! उन्हें सामान्य अर्थों में नौकरशाह नहीं माना होगा, उन्हें। ‘शाह’ नहीं सेवक माना होगा। लोकतंत्र की परिकल्पना में लोक अपनी शक्ति तो राजनीतिक दलों और उनके नुमाइंदों को देता है लेकिन शक्ति देने की प्रक्रिया में पवित्रता की कामना करता है।
इस पवित्रता की रक्षा के लिए शिक्षित, समझदार, न्याय-निष्ठ लोकसेवक पर पुरखों ने भरोसा किया! संविधान में ‘शक्ति के पृथक्करण’ की व्यवस्था की ताकि लोकतंत्र का ढांचा ही नहीं उसकी भावना और संभावना भी सदा समृद्ध रहे! ऐसी दुर्दशा!
दुर्दशा, उन सपनों की जिन्हें खुली आंख से देखते हुए देश के एक नहीं, अनेक नहीं, असंख्य स्त्री-पुरुषों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अपने बलिदान की शक्ति और संभावनाएं हमवतनों के सुपुर्द कर दिया।
भारत की संस्कृति का संकेत है कि नीयत सही हो तो उलटा करते हुए भी अंततः कार्य-सिद्धि हो ही जाती है और राजनीति के साफ-साफ संकेत है कि नीयत गलत हो तो सीधा, सरल और सुनिश्चित रास्ता भी विनाशकारी प्रक्रिया में फंसा देता है। कोई किससे करे शिकायत जब दिल में तीर की तरह से चुभा हो कि मगर शिकायत करने से क्या फायदा?
चुनाव परिणाम की नहीं लोकतंत्र के परिणाम की चिंता करने का वक्त है यह। स्मरण रहे अभी भी ‘बहुत कुछ’ है। बस सर्वमान्य माननीयों के ‘मत्स्य-न्याय’ के मोह से बाहर निकलकर सोचने की ‘खास’ जरूरत है। हां, जरूरतें और भी हैं।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)