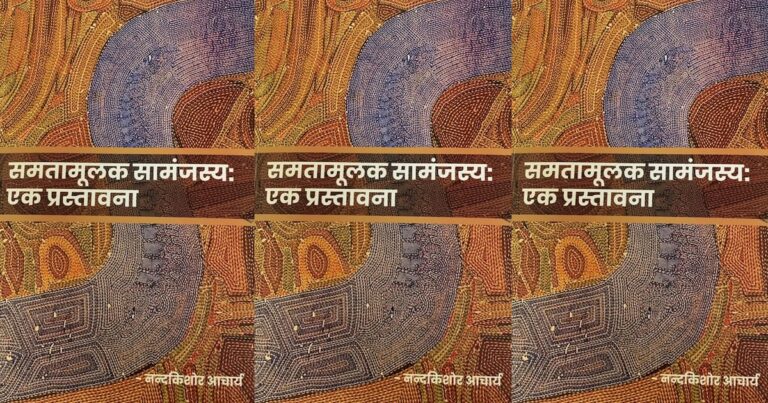दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की पराजय के बाद जितनी खुशी भारतीय जनता पार्टी के भीतर है उससे कहीं ज्यादा खुशी इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस) की घटक दल कांग्रेस पार्टी के भीतर है। उसके बड़े नेताओं ने भले ही प्रकट रूप से कोई बयान न दिया हो लेकिन थिंक टैंक के रूप में काम करने वाले तमाम लोगों ने इस बात पर खुशी जताई है कि उसने अपने उस शत्रु से बदला ले लिया है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए एक रणनीति के रूप में खड़ा किया था।
भले ही कांग्रेस को महज छह प्रतिशत वोट हासिल हुआ हो लेकिन उसने भाजपा की बी टीम को हरा दिया है और अब उसके लोग दावा कर रहे हैं कि अगला नंबर भाजपा को हराने का है। दूसरी ओर भीतर से आने वाली अपुष्ट खबरें में यह दावा किया जा रहा है कि एकदम लेन देन और धन और पद की लोलुपता पर आधारित इस चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हर प्रकार से पटाया और उन्होंने आम आदमी पार्टी को हराया। बताते हैं कि ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र चुनाव में हुआ था जहां पर भाजपा ने कांग्रेस के लोगों की लालच का फायदा उठाकर उन्हें लड़ते हुए भी न लड़ने के लिए राजी कर लिया था।
साजिशों की यह थ्योरी विचारों से बहुत दूर निकल चुकी है और उसमें नैतिकता और चरित्र के पतन की इंतहा झलकती है। अगर आप कांग्रेस को जिताने का स्वप्न देख रहे युवा बौद्धिकों से बात करें तो उनके भीतर यही विचार और योजना समाजवादियों और बहुजन आंदोलन के लिए भी भरी हुई है। इसीलिए कांग्रेस का समर्थन करने वाले तमाम ऐसे बौद्धिक हैं जो इस देश की राजनीति में समाजवादियों के आंदोलन को सिरे से नकार कर देश में संघ और भाजपा की राजनीतिक शक्ति बढ़ने के लिए डॉ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को ज्यादा दोषी ठहराते हैं।
भले ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जाति जनगणना कराने और उसके अनुरूप आरक्षण का विस्तार करते हुए पचास प्रतिशत की सीमा बढ़ाने और संवैधानिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने का एजेंडा चला रहा हो लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर जाति जनगणना का विचार स्वीकार्य नहीं हुआ है।
सवर्ण बिरादरी से आने वाले उसके समर्थकों में यह एक फर्जी और बीते समय का एजेंडा लगता है और एक किस्म से दलितों-पिछड़ों के तुष्टीकरण करने वाला काम लगता है। यानी कांग्रेस के समर्थकों के एक तबके के भीतर जितना आम आदमी पार्टी के प्रति द्वेष है उससे कम समाजवादी तबके के लिए नहीं है। वह उसे दूसरे नंबर का शत्रु तो मानता ही है और मौका मिलने पर उसे भी खत्म करने के लिए तैयारी करता दिखता है।
कांग्रेस के तमाम समर्थकों से यह पूछने पर कि आखिर हिंदुत्व की राजनीति को पराजित करने या कमजोर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वे राष्ट्रवाद को ही रामवाण औषधि के रूप में बताते हैं। उनके पास इस बात का कोई खाका नहीं है कि यह राष्ट्रवाद भाजपा के राष्ट्रवाद से कितना भिन्न होगा या कितना समावेशी होगा। या वह उतना ही उग्र होगा?
इन बातों का निष्कर्ष है कि इंडिया नाम के समूह के भीतर जो दल हैं उनमें कोई वैचारिक साम्य नहीं है। और न ही लोकतंत्र के मूल्यों और संविधान को बचाने की प्रतिब्धता। अगर वैसा होता तो वे एकजुट होकर विचारमंथन करते और आम आदमी की जीत के लिए योजना बनाते। वे वास्तव में जितनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि वे कहते रहते हैं कि एक बार भाजपा को केंद्रीय सत्ता से हटा दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाजपा के समर्थकों की सारी आक्रामकता तभी तक है जब तक वे सत्ता में हैं। जैसे ही वे सत्ता से बाहर हुए वे ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन वे यह नहीं बताते कि इस तरह आपस में लड़ते हुए वे कैसे भाजपा को सत्ता से हटा सकते हैं?
अपने मित्र डॉ प्रेम सिंह, जो निरंतर नवउदारवाद को ही मौजूदा राजनीतिक समस्याओं की जननी मानते हैं, कहते हैं कि यह लड़ाई भाजपा(एनडीए) बनाम कांग्रेस(एनडीए) की है ही नहीं। वास्तव में यह लड़ाई दक्षिणपंथ बनाम दक्षिणपंथ की है। इसके भीतर से कोई मूलगामी बहस निकल ही नहीं रही है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने रायपुर अधिवेशन में समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया, वह कहीं भी एआई जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के खतरों और अपनी नवउदारवादी नीतियों के प्रति आलोचनात्मक नहीं हुई।
उसके नेता राहुल गांधी के हाल में संसद में दिए गए जिस भाषण की सारे सेक्यूलर लोगों में बड़ी वाहवाही हो रही है उसमें कहीं भी नवउदारवाद और वैश्वीकरण की आलोचना नहीं थी। बल्कि उसे नए सिरे से और तेजी से अपनाने का आह्वान था। निश्चित तौर पर वह भाषण भाजपा नेताओं के छिछले भाषणों के मुकाबले ज्यादा तैयारी और समझदारी से दिया गया था लेकिन वह समझदारी युवाओं को भाजपा के ही पाले में ले जाता है। ऐसा भाषण दरअसल उदारीकरण की गोद में लोकतंत्र को एक बच्चे की तरह से बिठाने और उसके लालन पालन जैसा ही है।
ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर रास्ता क्या है? क्या हम केजरीवाल के अन्ना आंदोलन को महज इसलिए खारिज कर सकते हैं कि उसके पीछे विवेकानंद फाउंडेशन का निर्देशन था। वैसे जैसे तमाम लोग जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आंदोलन बताकर खारिज करते हैं। फिर तो हम इन आंदोलनों में उमड़े युवाओं और उनके भीतर से उभर रही वैकल्पिक विचारधारा का अपमान करते हैं। तब तो सामाजिक मंथन की हर प्रक्रिया अपने में एक साजिश है।
ध्यान रखिए कि आजाद भारत में अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसका राजनीतिक संगठन विपक्ष में रहा हो तो ऐसा कोई व्यापक जनआंदोलन नहीं था जिसमें उसने घुसपैठ न की हो। चाहे लोहिया का गैर-कांग्रेसवाद का आंदोलन रहा हो, जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, वीपी सिंह का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन हो। यहां तक कि उदारीकण के गांधीवादी और समाजवादी आंदोलन को भी हड़पने के लिए उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच खड़ा कर दिया। लेकिन इन आंदोलनों में युवा, किसान, मजदूर और समाज के दूसरे आंदोलन के नेताओं की भागीदारी को अगर एकदम खारिज कर दिया जाएगा तो वह लोकतंत्र का अपमान ही होगा।
सवाल यह है कि हमारे देश के विपक्षी दल वास्तव में भाजपा को सत्ता के हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या विपक्ष की बाकी बची जमीन में एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं? इसमें दूसरी बात ज्यादा सही लगती है लेकिन चलो मान लेते हैं कि दोनों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात जो दावे के साथ कही जा सकती है कि उनके भीतर इस लड़ाई को जीतने का न तो विश्वास है और न ही वे इस लड़ाई को आम आदमी को जितने के लिए लड़ रहे हैं।
उन्होंने निरंतर चुनाव को जितना महंगा किया है उससे साफ है कि आम आदमी इन चुनावों में भागादारी का हकदार नहीं रहा वह तो महज रेवड़ी और लोकलुभावन नारे का हकदार रहा। उसे कोई मुफ्त बिजली और पानी देने के नाम पर लुभाता है और झटका देता है तो तो कोई कुंभ में डुबकी लगवाने के नाम पर बुलाता है और भगदड़ में कुचलवा देता है। लेकिन आर्थिक ढांचे में बढ़ती बेरोजगारी के कारण वह लगातार छला तो जा ही रहा है, उसके वोट पैसे और शराब से खरीदे भी जा रहे हैं।
आज समय आ गया है कि आम आदमी अपना एजेंडा स्वयं तक करे और इस लोकतंत्र को चुनावबाज नेताओं और पार्टियों के चंगुल से निकालने की तैयारी करे। जाहिर है उसका तरीका सत्ता और धन के बढ़ते केंद्रीकरण में नहीं उसके विकेंद्रीकरण में है।
सत्ता के विकेंद्रीकरण का व्यापक आंदोलन राजनीतिक दलों के एजेंडे पर कभी नहीं होगा। उन्हें तो अपने लिए सत्ता चाहिए, अपने परिवार के लिए सत्ता चाहिए और अपने गिरोह के लिए सत्ता चाहिए। इस आंदोलन के विचार के केंद्र में होगा उदारीकरण की नीतियों का नकार और सत्ता को राज्य और बाजार के हाथ से छीनकर जनता के हाथ में देने का कार्यक्रम। जब तक ऐसे कार्यक्रम नहीं चलेंगे तब तक भले कभी आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए लेकिन आम आदमी तो हारता ही रहेगा।
(अरुण कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)