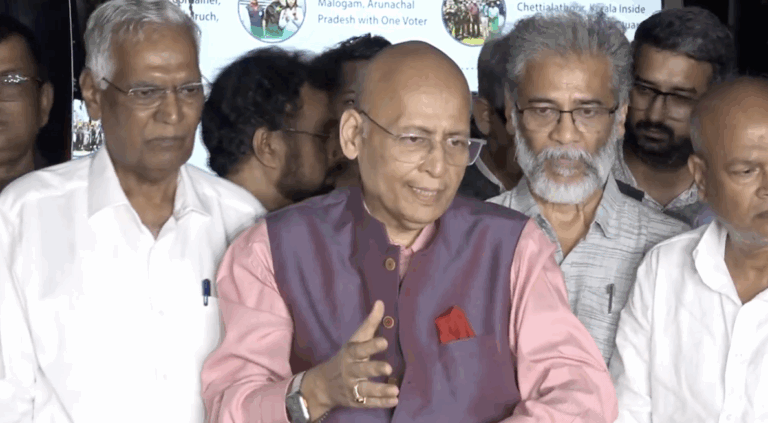लोकसभा चुनाव का नतीजा चार जून को ही जाहिर हो पाएगा। लेकिन इस बीच चुनाव परिणाम को लेकर अनुमान तेजी से बदले हैं। अब इस संभावना को गंभीरता से लिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह जा सकती है। बल्कि अब यह कयास भी लगाया जाने लगा है कि इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा (यानी 272 सीटें) पार करते हुए सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकता है। ये अनुमान किस हद तक सही साबित होंगे, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। मगर यह साफ है कि अब ऐसी संभावनाओं को वित्तीय बाजार और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी गंभीरता से लिया जा रहा है।
बल्कि ऐसी संभावना को देखते हुए वित्तीय बाजार की एजेंसियों और संचालक संस्थाओं ने पूर्वानुमान आधारित हमले शुरू कर दिए हैं। यह धारणा बनाने की गंभीर कोशिश हो रही है कि अगर इंडिया एलायंस की सरकार बनी और उसने विभिन्न पार्टियों के चुनाव घोषणापत्रों में शामिल जन-कल्याण की योजनाओं पर सचमुच अमल किया, तो “भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद” हो जाएगी।
पूर्वानुमान आधारित हमले की सबसे बेहतरीन मिसाल अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) की धमकी है। रेटिंग एजेंसियों का काम मूल रूप से निवेशकों को किसी देश या कंपनी में निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहायक बनना है। इसके लिए वे अपना आकलन बताती हैं कि संबंधित स्थान पर निवेश में क्या जोखिम हो सकते हैं। इस कार्य के सिलसिले में ये एजेंसियां किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अपना “आउटलुक”- यानी नजरिया बताती हैं और उस देश की निवेश संबंधी “रेटिंग” तय करती हैं। आम समझ यह है कि आउटलुक और रेटिंग में समानता रहनी चाहिए।
बहरहाल, किसी एजेंसी का यह काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि संबंधित देश को चेतावनी के लहजे में अपनी सलाह दे। मगर वित्तीय पूंजीवाद के दौर में ये एजेंसियां अपनी ऐसी ही चालों से सरकारों की नीतियों को प्रभावित करती हैं। चूंकि शासन में कोई पार्टी या नेता आए, अंततः उसकी डोर कॉरपोरेट एवं वित्तीय बाजार के हाथ में होती है, इसलिए ऐसी एजेंसियों की रेटिंग को इस नव-उदारवादी दौर में अत्यधिक महत्त्व मिला हुआ है। इसके बावजूद कि कंपनियों या देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाजा लगाने का इन एजेंसियों का रिकॉर्ड बेहद खराब है। 2007-08 में आई वैश्विक मंदी के पहले दुनिया की किसी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने उन बैंकों या वित्तीय कंपनियों की कमजोर सेहत के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी थी, जो एक के बाद एक ढहती चली गईं।
इसके बावजूद अमेरिका स्थित तीन रेटिंग एजेंसियां- मूडी’ज, एसएंडपी ग्लोबल, और फिच- विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों की नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में बनी हुई हैं। अब अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपना नजरिया ‘स्थायी’ से बेहतर करते हुए ‘सकारात्मक’ कर दिया है। आम तौर पर अपेक्षा यह होती है कि जब कोई देश के चुनाव परिणाम को लेकर अनिश्चय की स्थिति में हो, तो रेटिंग एजेंसियां स्थिति स्पष्ट होने तक इंतजार करें। लेकिन एसएंडपी ग्लोबल ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की है।
दिलचस्प यह है कि एसएंडपी ने भारत की दीर्घकालिक या अल्पकालिक निवेश रेटिंग में कोई सुधार नहीं किया है। उसने दीर्घकालिक रेटिंग ‘बीबीबी माइनस’ और अल्पकालिक रेटिंग ‘ए-3’ बनाए रखा है। यानी अभी ये एजेंसी मानती है कि भारत के ऋण या सामान्य बाजार में निवेश की स्थितियां जस-की-तस हैं। फिर भी उसने आउललुक बदला है, तो लाजिमी है कि इस पर सवाल उठेंगे।
सवाल यह उठा है कि क्या आउटलुक परिवर्तन एसएंडपी ग्लोबल के किसी ठोस आकलन पर आधारित है, या एक किस्म का सियासी बयान है। एजेंसी की दो टिप्पणियों ने ऐसे प्रश्न उठाने का आधार उपलब्ध कराया है।
- एजेंसी ने कहा है कि उसकी राय में चुनाव परिणाम चाहे जो हो, भारत में नीतिगत स्थिरता बनी रहेगी।
- मगर साथ ही उसने चेताया है कि जारी नीतियों को लेकर प्रतिबद्धता में कोई कमी आई, तो वह फिर से अपना नजरिया “सकारात्मक” से “स्थायी” कर देगी।
मतलब यह कि अगली सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार की तरह बहुराष्ट्रीय और मोनोपॉली पूंजी को सर्वोच्च प्राथमिकता जारी रखने के बजाय जन-कल्याणकारी योजनाओं पर धन खर्च करने की नीति अपनाई, तो एजेंसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी बाजार को भारत के बारे में नकारात्मक संदेश देगी। वैसे ही यह अनुमान धड़ल्ले से लगाया जा रहा है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला, तो शेयर बाजारों में भारी गिरावट आएगी। कयास तो यहां तक लगाए गए हैं कि यह गिरावट 15 से 20 प्रतिशत तक हो सकती है।
इसी माहौल के बीच एसएंडपी ने चेतावनी दी है कि अगर अगली सरकार ने मौजूदा नीतियों को बदला, तो ये एजेंसी अपना नजरिया बदलकर उस प्रक्रिया को और गति देगी। जाहिर है, उससे अगली सरकार पर दबाव बढ़ेगा। वित्तीय पूंजीवाद के इस नव-उदारववादी दौर में निवेशक भावनाओं को चोट पहुंचने का जुमला और पूंजी के पलायन की आशंका- दो ऐसे औजार हैं, जिनसे किसी देश में सरकार चाहे जो बने, उसे “पटरी” पर रखने की कोशिश की जाती है। इस कार्य में रेटिंग एजेंसियां एक बड़ा हथियार हैं।
संभावित राजनीतिक स्थितियों के मद्देनजर नीतियों को पहले से प्रभावित करने की रेटिंग एजेंसियों की कोशिश बेशक देश के आंतरिक मामले में एक अनावश्यक हस्तक्षेप माना जाएगा। लेकिन ऐसे हस्तक्षेप आज सामान्य बात हैं।
बहरहाल, बात यहीं तक नहीं है। वित्तीय और मोनोपॉली कॉरपोरेट सेक्टर ने अपने नियंत्रण वाले मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए भी पूर्वानुमान आधारित हमले (pre-emptive) शुरू कर दिए हैं। इंडिया एलायंस के घटक दलों- खासकर कांग्रेस के चुनावी वादों की अब मीडिया में जैसी चीर-फाड़ की जा रही है, वैसा उस समय नहीं हुआ था, जो कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया था। तब शायद यह मानकर मीडिया ने इसे नजरअंदाज किया था कि ये चुनावी संभावना-विहीन एक पार्टी के वादे हैं। लेकिन अब मीडिया कांग्रेस के वायदों को पूरा करने पर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकने वाले कथित दुष्प्रभावों का चित्रण करने में अपनी काफी ऊर्जा लगा रहा है।
ऐसा करते हुए बुनियादी पत्रकारीय ईमानदारी को भी किस तरह तिलांजलि दे दी गई है, इसकी एक नायाब मिसाल एक बिजनेस पत्रिका की वेबसाइट पर छपा एक “विश्लेषण” है। इसे इस शीर्षक के साथ छापा गया हैः ‘अर्थशास्त्रियों की चेतावनी- राहुल गांधी के चुनावी वादे भारत की राजकोषीय सेहत को नष्ट कर सकते हैं’. (Economists warn Rahul Gandhi’s poll promises can ruin India’s fiscal health – BusinessToday)
ध्यान दीजिएः हेडलाइन में कहा गया है- अर्थशास्त्रियों की चेतावनी। लेकिन इस लंबी रिपोर्ट में एक भी अर्थशास्त्री का नाम नहीं है। उद्धरण कई हैं, लेकिन हर जगह कहा गया है एक अर्थशास्त्री ने बताया– या अर्थशास्त्री ने कहा। अब देखिए कि उस अर्थशास्त्री ने क्या बताया। उसने राहुल गांधी के वादों से राजकोष पर कितना बोझ पड़ेगा, यह बताया। कुल बोझ को 17 से 22 लाख करोड़ रुपये सालाना तक बताया गया। कांग्रेस गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में एक लाख रुपये देने का वादा किया है। मगर उन अर्थशास्त्री महोदय ने एक लाख के आधार पर तो अनुमान बताया ही, यह भी बताया कि अगर ये रकम दो लाख रुपये कर दी गई, तो कुल कितना बोझ पड़ेगा!
यह बेहिचक कहा जा सकता है कि कांग्रेस के तमाम आकर्षक वादे कैजुअल नेचर के हैं। कांग्रेस उनकी फंडिंग कहां से करेगी, यह उसने नहीं बताया है। जब उसने उत्तराधिकार कर और वेल्थ टैक्स लगाने से मुंह चुरा लिया, तब उसके वादे और भी रहस्यमय- या कहें अविश्वसनीय हो गए। लेकिन वित्तीय बाजार इस समझ के साथ पूर्वानुमान आधारित हमले नहीं कर रहा है। उसका हमला इस पूर्व-चिंता के कारण है कि कहीं अगली सरकार ने ऐसे वादों पर आंशिक अमल भी किया, तो अभी जिस तरह देश के सारे संसाधन उसकी जेब में जा रहे हैं, उसमें कटौती हो जाएगी।
राजनीतिक-अर्थशास्त्र का यह गतिशास्त्र दुनिया के तमाम “लोकतांत्रिक” देशों में देखने को मिल रहा है। इसीलिए धुर-दक्षिणपंथी पार्टियां शासक वर्ग और वित्तीय पूंजी की प्राथमिकता बनती जा रही हैं। (Quarter of political donations in EU go to extremist and populist parties, data reveals | Europe | The Guardian) इन तबकों को चिंता तब होती है, अगर जन-कल्याण के वास्तविक और विश्वसनीय एजेंडे वाली कोई ताकत राजनीति में उभरने लगती है। बल्कि एक समझ तो यह है कि धुर-दक्षिणपंथी और नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले दलों को राजनीति में सफलता इसीलिए मिलने लगी, क्योंकि शासक वर्गों ने ऐसी ताकतों पर अपना दांव लगाया।
मगर इसका परिणाम विभिन्न समाजों में तीखे ध्रुवीकरण, तनाव और हिंसा की परिस्थितियों के रूप में सामने आया है। इन सबका सीधा निशाना लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बनी हैं। इसलिए आज अधिक से अधिक विशेषज्ञ यह महसूस करने लगे हैं कि राजनीति में यथाशीघ्र अगर जन हित को केंद्रीय स्थान नहीं मिला, तो इस दौर में लोकतंत्र की बलि चढ़ सकती है।
दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्रियों और राजनीति-शास्त्रियों ने इसी महीने जर्मनी के बर्लिन में अपने सम्मेलन के बाद वर्तमान संकट से निकलने का एक ठोस एजेंडा पेश किया। (Berlin Summit Declaration May 2024 – Forum for a New Economy (newforum.org)). इसमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आर्थिक उपाय सुझाए गए हैं, वे कांग्रेस के घोषणापत्र से बहुत आगे जाते हैं। असल में कांग्रेस का वादा तो नव-उदारवादी दायरे में पूरी तरह सिमटा हुआ है। उसमें उस वेलफेयरिज्म (जन कल्याण की योजनाओं) की तरफ लौटने का संकेत भर है, जिसका सुझाव “आर्थिक सुधारों को मानवीय चेहरा” प्रदान के लिए कभी खुद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दिया करते थे।
मगर वित्त बाजार और कॉरपोरेट मोनोपॉली को अब उतना “मानवीय चेहरा” भी बर्दाश्त नहीं है। वे कैश ट्रांसफर की उन योजनाओं का भी विरोध कर रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप खुद उनके कारखाना उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। बहरहाल, वित्तीय पूंजीवाद के दौर में निवेश, उत्पादन, और वितरण की परंपरागत पूंजीवादी व्यवस्था की श्रमसाध्य प्रक्रिया में जाना भी पूंजीपतियों को मंजूर नहीं है। शेयर, बॉन्ड, ऋण बाजार में निवेश के जरिए पैसे से पैसा बनाना उन्हें अपने माफिक ज्यादा लगता है। और इसमें तनिक भी खलल की संभावना दिखने पर वे अपनी पुरजोर ताकत उसे नाकाम करने में लगा देते हैं। यही हम इस समय भारत में होते देख रहे हैं।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)