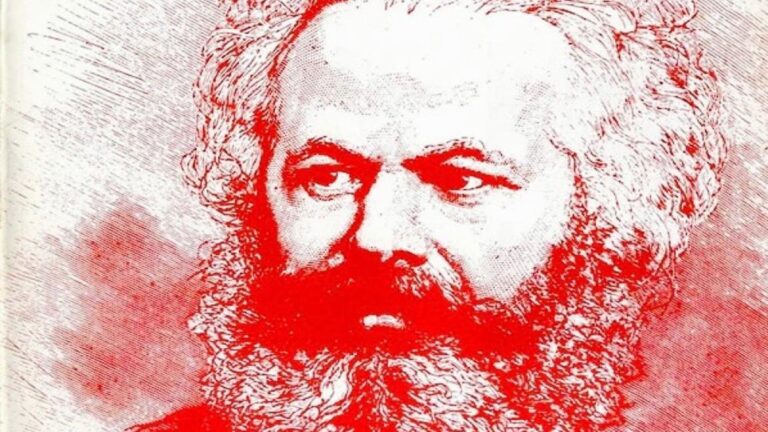जब दिल्ली के मुंगेशपुर में मौसम विभाग का यंत्र ने 52.9 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया, तब मौसम विज्ञानियों को लगा कि मशीन में ही कुछ गड़बड़ी आ गई है। उन्होंने मशीन के सेंसर की पड़ताल की, इसके बाद मौसम विभाग से जुड़े केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस तापमान पर सवाल उठा दिया। मौसम विभाग ने इसे जांच करने का निर्णय लिया। फिलहाल अभी तक इस पर अंतिम बयान नहीं आया है। लेकिन, यह सवाल तो उठ ही गया कि दिल्ली का तापमान इतना ऊपर जा सकता है!
अमूमन बारिश, ताप, ठंड जैसी शब्दावलियां मौसम विभाग के खाते में चली जाती हैं और इसे प्रकृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। लेकिन, पिछले दो दशक से इस शब्दावलियों की परिभाषा में मनुष्य का हिस्सा भी गिना जाने लगा है। खासकर, जब तेजी से ग्लेशियर पिघलने लगे, धरती के ताप में वृद्धि और असामान्य बारिश और सुखाड़ की परिघटनाओं से आम लोगों को यह बात साफ होने लगी कि यह सब इंसानों की प्रकृति के साथ मनमाना छेड़छाड़ का नतीजा है।
हालांकि, वैज्ञानिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा इस संदर्भ में सक्रिय था और वह चेतावनी दे रहा था। खुद सरकारें और पूंजीपति भी इससे अवगत थे और प्रकृति के दोहन को लेकर वे सालाना बैठकें कर रहे थे। धरती के ताप बढ़ने के कारण और इसके नतीजों को लेकर काफी कुछ सामने आ रहा था। खासकर, जब दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन सूखने की ओर बढ़ चली और अंटार्टिका के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे, तब इस दिशा में और भी गंभीर अध्ययन सामने आये।
धरती के तापमान में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक विकास को माना गया जिसमें कार्बन का उत्सर्जन मुख्य है। इसी के साथ बायोगैस भी एक कारण है। शहरीकरण और कोयला, पेट्रोलियम का प्रयोग इसमें बड़ा योगदान देते हैं। जंगलों की कटाई और वन्यजीवों का नाश आदि इसी का बड़ा हिस्सा है। इस तरह के कारकों का सीधा प्रभाव एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र, समुद्री विक्षोभों से कई महाद्वीपों और कुछ देशों व शहरों पर सीधा पड़ता है। मसलन, बारिश, ठंड और ताप तीनों ही किसी क्षेत्र, शहर में संघनित प्रभाव डाल सकते हैं यदि उसकी परिस्थितियों इसके अनुकूल हो।
आइए, दिल्ली में इसके लिए बनती स्थितियों को देखते हैं: 1-दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 13.2 प्रतिशत हिस्सा जंगल है। भारत का औसत जंगल क्षेत्र 21.7 प्रतिशत है। यदि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में इसका प्रतिशत देखें तब दिल्ली का दक्षिणी हिस्सा जितना हरा भरा है, उस मुकाबले अन्य हिस्से बेहद उजाड़ दिखते हैं।
2- दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का 75 प्रतिशत हिस्सा शहरी है। 2019 में यूनाइटेड नेशन ने दिल्ली की बढ़ती आबादी के आधार पर इसे दुनिया के शहरों में दूसरे स्थान पर रखा था। 2011 के आंकड़ों में यहां की आबादी 1 करोड़ 67 लाख पार कर चुकी थी। एनसीआर में ढाई करोड़ की सीमा पार हो चुकी थी। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में प्रति वर्ग मील 30 हजार से अधिक लोग रहते हैं। निश्चित ही इस बड़ी आबादी के रहने के लिए मकानों की जरूरत है। पिछले तीन दशक से दिल्ली में आवास एक भयावह समस्या की तरह उभर कर सामने आया। दिल्ली के अंदर कई उद्योगिक क्षेत्रों को बंद किया गया। इसी तरह जमीनों का अधिग्रहण और नियमितिकरण के नाम पर झुग्गी बस्तियों को उजाड़ना और नई कालोनियों का निर्माण जारी रहा है। दिल्ली आवासीय, संस्थानिक, मेट्रो, सड़क परियोजनाओं आदि के निर्माण कार्य से भरा हुआ शहर है। यदि हम बिजली प्रयोग के आधार पर पिछले एक दशक में हुई बढ़ोत्तरी को देखें, तो यह पिछले साल तक 37 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया था।
3- दिल्ली में कुल पंजीकृत गाड़ियों की संख्या 1.2 करोड़ है जिसमें से 33.8 लाख निजी कार हैं। गाड़ियों के पुराने हो जाने का वर्गीकरण बहुत सारी गाड़ियों को चलन से बाहर करती हैं, लेकिन गाड़ियों की खरीद पर इसका असर नहीं पड़ता है। दिल्ली प्रति 100 वर्ग किमी में 1749 किमी सड़क घनत्व रखता है। फ्लाईओवर का निर्माण और चौड़ीकरण निश्चित ही इस घनत्व को बढ़ा देता है।
4- दिल्ली में कई सारे उद्योगिक क्षेत्रों को बंद करने के बावजूद अभी भी 29 उद्योगिक क्षेत्र हैं। बवाना, नरेला जैसे सुदूर गांव, जहां अभी हाल तक खेती हो रही थी, वह आवासीय परियोजनाएं और उद्योगिक गतिविधियां बढ़ती गई हैं। यही स्थिति नजफगढ़ इलाकों में भी है। पूरे एनसीआर में उद्योगों का जाल बिछा हुआ है। जो दिल्ली का एक बड़ा घेरा बनाता है।
5- दिल्ली दो पहाड़ी सरंचनाओं के बीच में है। एक ओर अरावली की अंतिम सीमा है और दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र की शुरूआत है। यमुना का बहाव पहले अरावली की पहाड़ियों से होता हुआ नीचे आता था। यह जैसे-जैसे नीचे की ओर खिसकते गई इसने अपने पीछे हौज, झील और पानी के स्रोतों का निर्माण करती गई। इस सदंर्भ में दिल्ली में आज भी पानी के विशाल स्रोत मौजूद हैं। इसके साथ ही, अरावली में लंबी यात्रा करते हुए साहिबी नदी नजफगढ़ से होते हुए वजीराबाद में यह यमुना में जाकर मिलती है। पिछले चार दशकों में गुड़गांव ने साहिबी नदी को खत्म कर देने वाला विकास हुआ। इसके बाद जब वह दिल्ली में उतरती है तब वह ‘बड़का नाला’ में बदल जाती है। इसी तरह दिल्ली में यमुना को विकास की परियोजनाओं ने न सिर्फ उसके हिस्से की जमीन को खा लिया, साथ ही उसके बहाव और जल को नष्ट कर दिया है। इसी तरह दिल्ली की कई झीलों को विकास ने खत्म कर दिया। आज भी बहुत सारी झीलें अपने अस्तित्व के जूझ रही हैं। निश्चित ही पिछले कुछ वर्षों से झीलों को बचाने में सक्रियता देखी जा रही हैं, लेकिन यह अब नुकसान की तुलना में बेहद थोड़ा ही है।
6- दिल्ली की भौगोलिक स्थिति में पश्चिमी विक्षोभ से उठने वाले बादल और हवाएं राजस्थान और हिमालय के नीचे पंजाब और हरियाणा से होते हुए नीचे दिल्ली की ओर उतरती हैं। इससे गर्मी, सर्दी और बारिश के साथ-साथ यहां के प्रदूषण की गंभीरता को भी प्रभावित करती हैं। जहां जाड़ों में हवा का संघनन मैदानी क्षेत्रों में बढ़ता है, वहीं गर्मी में लू का प्रकोप बढ़ जाता है। दिल्ली क्वार्टजाइट से बने पठारों पर बसा है, जिसके उतरान पर यमुना है। ऐतिहासिक तौर पर यह सूखा क्षेत्र है। यहां की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बसावटों के पैटर्न को देखें तब इसमें झीलों, फिर नदी और अंत में भूगर्भ जलों के प्रयोगों को क्रमशः देखा जा सकता है।
यदि हम इसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आ रहे बदलाव के संदर्भ में देखें, तो इस ऐतिहासिकता में आज के विकास का दौर भयावह शक्ल दिखा रहा है। राजस्थान से लेकर गुरूग्राम तक अरावली का उजाड़ और विकास में चमकती सड़कें, मकानों की श्रृंखला और उद्योगों के जाल को देखा जा सकता है। वहीं पंजाब से लेकर हरियाणा तक हरित क्रांति का प्रभाव खेती में पानी और खाद का प्रयोग और नई फसल के लिए पीछे के फसलों के शेष को खत्म करने के लिए आग लगाने की घटना एक बड़ी समस्या में बदल चुकी है। इसी तरह उत्तराखंड और हिमांचल में पर्यटन के विकास ने चौड़ी सड़कों और गाड़ियों की सुविधाओं ने कार्बन उत्सर्जन को ग्लेशियर तक पहुंचा दिया है।
यहां हमने उन कारणों का हवाला दिया है जिसमें सिर्फ शहरीकरण ही नहीं, जो तापमान वृद्धि में 60 प्रतिशत की भूमिका निभाता है; विकास की जो एक पूरी भौगोलिक संरचना भी एक कारण है जिससे तापमान में वृद्धि एक असामान्य घटना की तरह नहीं, एक अनिवार्य परिणाम की तरह सामने आता है। ऐसे में प्रशांत सागर में बहने वाली हवा जिसमें तापमान में बढ़त और घटत दोनों ही परिघटनाएं सामने आती हैं, का असर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है।
प्रशांत महासागर की गर्म हवाएं भूमध्यसागर की हवाओं को प्रभावित करती है। अमूमन अप्रैल महीने के मध्य से भूमध्य सागर की हवाओं की आर्द्रता कम होने लगती हैं। लेकिन, इस बार यह आर्द्रता महीने के अंत तक चली और फिर अचानक सूखी और गर्म हवा में बदल गई। यह ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए पश्चिमोत्तर से होते हुए दिल्ली की ओर उतरी तब यह अन्य कारकों के साथ मिलकर तापमान को अचानक ही ऊंचा उठा दिया। इसने राजस्थान में रिकार्ड स्तर का तापमान बढ़ाया और दिल्ली में यह ऐतिहासिक तौर पर ऊंचा हो गया। इसने गर्म जगहों के कई सारे द्वीप बनाए। इसने दिल्ली के उन गांवों को अपनी गिरफ्त में लिया, जहां गांव के नाम पर सिर्फ उनके नाम भर रह गये हैं, गांव की प्राकृतिक स्थितियों को शहरों ने निगल लिया है। हालांकि यह शहर अब भी उन्हें गांव की तरह ही देखता है और उनकी बिजली की सप्लाई तक उसी स्तर की दी जाती है।
तापमान वृद्धि और इंसान की जिंदगी, दोनों के प्रति इतनी बेपरवाही क्यों?
चुनाव आयोग ने जब ऐतिहासिक तौर पर सबसे लंबे दूसरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किया तब क्या उसने मौसम विभाग से जानकारी हासिल किया कि इस गर्मी मौसम का हाल क्या रहेगा? जो हालात हैं उससे यही लगता है कि इस संदर्भ में शायद ही कोई सलाह लिया गया। चुनाव के शुरूआती दौर में ही झारखंड, बिहार, बंगाल से लेकर दक्षिण के सभी राज्यों में एंटी साइक्लोकिन हवाओं के चलते इन इलाकों का तापमान अप्रैल के महीने में 40 डिग्री से ऊपर चला गया था।
समुद्री हवाओं के दबाव की वजह से आर्द्रता भी बढ़ गई थी, खासकर समुद्र तटीय क्षेत्रों में यह काफी था। इसकी वजह से इंसान के शरीर की इस तरह की नमी वाला ताप जानलेवा होता है। चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में क्या तैयारियां की थीं, फिलहाल खबरों में इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन, जब चुनाव का अंतिम चरण आया तब इतना तो साफ हो गया कि इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने कोई खास तैयारी की ही नहीं थी। 31 मई, 2024 को डिजीटल मीडिया और बाद में प्रिंट मीडिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 18 मतदान कर्मियों की लू लगने से मौत हो गई। इसमें मिर्जापुर में सबसे अधिक मौतें हुईं।
राजस्थान से लेकर बिहार तक में लू और गर्मी से मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इसका एक बड़ा कारण हीटवेव की कुल समयावधि का बढ़ना है। पहले यह 20 से 40 दिन के बीच रहता था, अब यह तीन महीने की अवधि को पार कर गया है। इस बढ़ती अवधि और तापमान में हो रही वृद्धि की सूचना मौसम विभाग जारी करता है। जब चुनाव आयोग चुनाव के फेज तय कर रहा था, तब उसने इस अवधि को ध्यान में क्यों नहीं रखा? इस साल भी अलनीनो का असर रहेगा और पश्चिमी विक्षोभ कहर ढा सकता है, इसका अनुमान दुनिया के कई मौसम विज्ञानियों और संस्थाओं ने जारी किया था, क्या चुनाव आयोग को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? इस लू और गर्मी से मौत हुई मौत का आंकड़ा देने से अधिक इस बात को जानना जरूरी है जिसमें मानव शरीर की ताप सहने की क्षमता कितनी है!
यह माना जाता है मानव शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सामान्य तौर पर काम करता है। जब भी तामपान इससे ऊपर जाता है, शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। यदि तापमान अधिक हो और आर्द्र्ता बढ़ती जाय तब शरीर को दोहरा काम करना होता है। उसे शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक पसीना बहाना होता है और शरीर के अंगों का दुरूस्त रखने के लिए अधिक उर्जा पैदा करता है। इसका सीधा प्रभाव खून की धमनियों, लीवर, कीडनी और मांशपेशियों पर पड़ता है। इन सभी का असर मस्तिष्क की गतिविधि और हृदय के धड़कनों पर पड़ता है। तेज बुखार, अचेत होना, हृदय गति का रुक जाना वे कारण होते हैं जिसमें मनुष्य की मौत हो जाती है।
यदि अधिक तापमान में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लगातार 5 से 6 घंटे तक 40 डिग्री तामपान में बना रहता है या तापमान के अनुरूप शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, …तब उसकी गंभीर तौर पर बीमार होने और यहां तक की मौत हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि चुनाव की गतिविधियां इसी तापमान पर जारी रहीं और चुनाव कर्मियों को इसी तापमान में लगातार काम पर झोंका जाता रहा है। निश्चित ही यह बेहद गंभीर मसला है और इसी संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा इस तरह से चुनाव आयोजित करने की जबाबदेही की मांग करनी चाहिए।
मौन व्रत, किसके लिए?
इस समय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान के बाद मौन व्रत धारण कर लिया है। वह जब मौन व्रत धारण कर रहे थे, तब भी अभी प्रधानमंत्री के पद पर ही हैं। यह हम सभी को जानने का हक है कि यह मौन व्रत किसके लिए है? इस लू के थपेड़ों में मर जाने वाले लोगों के लिए है? इस दौरान जो उन्होंने नफरत से भरे भाषण दिये, यह उसके पश्चाताप में है? या आने वाले समय के लिए चिंतन-मनन के लिए यह है? एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति सार्वजनिक जीवन का हिस्सा होता है। और, यदि वह नीति निर्माताओं में से एक है तब तो उसकी जिम्मेवारी सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वह देश के शीर्ष निर्णायक व्यक्ति हैं और उसकी जिम्मेवारी किसी भी नागरिक से कई गुना अधिक है। यह संसदीय राजनीति का सबसे अजूबा दौर है जिसमें जिम्मेवारी का कोई अर्थ नहीं रह गया है और धूर्तता और झूठ राजनीति की मुख्य ताकत बन गई है।
अमी सीजायर के एक लेख के छोटे से हिस्से को उद्धृत करना उपयुक्त होगाः ‘जो सभ्यता अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं होती वह एक पतनशील सभ्यता का निर्माण करती है। जो सभ्यता आ खड़ी हुई समस्याओं को हल करने की बजाय आंख चुराने का रास्ता चुनती है तब वह एक बीमार सभ्यता का निर्माण करती है। लेकिन, जो सभ्यता धूर्तता और झूठ के सिद्धांत पर चल निकलती है वह एक मरी हुई सभ्यता होती है।’
यह बात सिर्फ पिछले 10 साल के संदर्भ में ही उपयुक्त नहीं है। यह वर्तमान में चल रहे चुनाव के संदर्भ में भी उपयुक्त है। यह उस अपनाई गई प्रक्रिया के साथ भी सच है जिसमें इतनी लंबी गर्मी में लोगों को लोकतंत्र के उत्सव में आने के लिए मजबूर किया गया और इसके आयोजन में लगे लोगों में से कई लोगों की मौत हुई। यह इस समय के वर्तमान के लिए भी सच् है जिसमें पूरा देश ताप से तप रहा है और उस असहनीय ताप में मजदूर काम पर जा रहे हैं। वह प्रवासी मजदूर बनकर काम के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। वे रीयल स्टेट की बनती बिल्डिंग से लेकर सड़क परियोजनाओं में तपती धूप में काम कर रहे हैं। ताप से तपती धरती एक जानलेवा लू के साथ इंसान के शरीर को निचोड़ लेने के लिए तैयार है और यह पिछले डेढ़ महीने से चल रहा है और यह जून के मध्य तक बना रहेगा। ऐसे में, इस जानलेवा गर्मी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की क्या योजना है?
वह इस देश की 40 करोड़ की अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की जिंदगी के बारे में क्या सोच रही है जो 45 डिग्री ताप पर काम करने के लिए मजबूर हैं? क्या यह प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता है? क्या बाढ़ ही आपदा है? ठंड और ताप क्या इस श्रेणी से बाहर हैं?
शहरों के लिए सब्जियां उगाने वाला किसान इस गर्मी में जब खेत में जूझ रहा है और पानी और बिजली की किल्लतों के बावजूद वह शहर की आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहा है, तब क्या प्रधानमंत्री उनकी जिंदगी की सुरक्षा की कोई चिंता करते हुए दिख रहे हैं?
इस देश में लू से मरने वालों की संख्या गिनी जा रही है, तब क्या प्रधानमंत्री उन्हें एक नागरिक की मौत की तरह देखते हुए उससे बचाने के उपायों के बारे में सोच रहे हैं?
बहुत सारे सवालों के बीच जब हम विकास के बढ़े प्रतिशत को देखते हैं तब यह जरूर ही ख्याल आता है कि इसकी नींव में मुनाफे के तौर पर जो अतिरिक्त श्रम है उसे देने के बाद उन मजदूरों की जिंदगी कितनी बची रह गई थी! जब हम शेयर बाजार की उछाल में दलालों को पैसा गिनते हुए देखते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि इन बढ़े हुए पैसे किन हाथों से छिनकर उन तक पहुंचे, और उन खाली हाथ मजदूरों के पेट में भोजन के कितने अन्न पेट में गये होंगे!
प्रधानमंत्री जब मौन व्रत पर है और इसके ठीक पहले वे खुद को परमात्मा के दूत बता रहे थे, संभव है आने वाले दिनों में वह संसदीय लोकतंत्र की जरूरत से ऊपर उठा लें और नागरिकों को भेड़ बनाकर उनका चरवाहा बन जाने का दावा कर लें। संसदीय लोकतंत्र में मसीहा होने का दावा इससे कम अर्थ में अभिव्यक्त नहीं होता। यह अलग बात है कि तंत्र कोई भी हो, निर्णायक जनता ही होती है।
इतिहास के युगों पर भले ही राजाओं के नाम लिखे हों, इतिहास के निर्णयों पर भले ही चारणों ने किसी चक्रवर्ती के गीत गाये हों, वह सब खंडहरों में विलीन होता गया। जन न तो जंगलों से विदा हुए, न समुद्रों को नापना छोड़ा, न गांवों को उजाड़ किया और न शहरों में बसने से गुरेज किया, उसने कभी भी सार्वजनिक जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। उसने खेती किया, सड़क बनाया, शहर बनाया, कर दिया, राजा बनाया और जब यह सब उनके ऊपर से गुजरना शुरू कर दिया तब उसने उन्हें नष्ट कर दिया और फिर एक नये रास्ते का चुनाव किया। इतिहास की इस गति से कौन इंकार कर सकता है। मसीहा बनने की चाह मौन व्रत के नाटक का अंतिम पटाक्षेप की तरह सामने आना है। यदि यह होता है, तब देश के इतिहास का सबसे बुरा दौर शुरू होगा। उम्मीद है, ऐसी उम्मीद खारिज होगी।
(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)