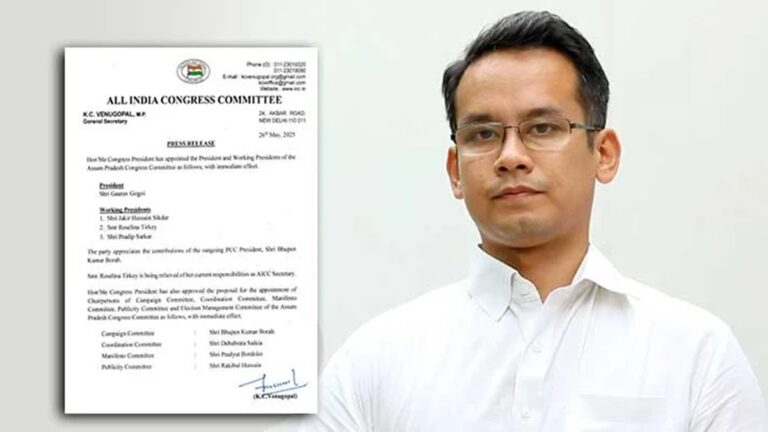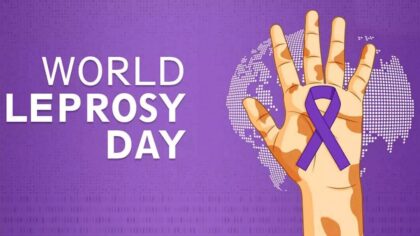दक्षिण अफ्रीका की धूल भरी सड़कों, विस्तृत खेतों और दूर तक फैली पहाड़ियों को देखिए-यह वही धरती है, जिसने सदियों तक अपने असली मालिकों को खून और आंसुओं की कीमत पर गुलामी झेलते देखा है। यह वो मिट्टी है, जिसे काले अफ्रीकी किसानों ने अपने श्रम से सींचा, मगर जिसका स्वामित्व हमेशा श्वेत उत्पीड़कों के हाथ में रहा।
यह केवल जमीन नहीं, बल्कि इतिहास है-ऐसा इतिहास जिसमें शोषण, दमन और अन्याय के असंख्य अध्याय लिखे गए हैं। और अब, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है-बिना मुआवजे के भूमि अधिग्रहण कानून पर हस्ताक्षर करके।
लेकिन यह कानून सिर्फ सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि ज्वलंत विद्रोह की घोषणा है। यह उन जंजीरों को तोड़ने का आह्वान है, जो सदियों से अफ्रीकी जनता को उसकी खुद की जमीन से बेदखल करती आई हैं। 1913 के कुख्यात ‘नैटिव लैंड एक्ट’ ने इस अन्याय की नींव रखी थी, जब काले नागरिकों को उनकी ही भूमि से बेदखल कर दिया गया और उन्हें सिर्फ 7% भूमि पर सिमटने के लिए मजबूर कर दिया गया। यह वही कानून था, जिसने अफ्रीका की आत्मा पर गहरे घाव किए, जिसे आज भी इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में गिना जाता है।
फिर आया 1948, जब रंगभेदी सरकार ने सत्ता संभाली और काले अफ्रीकियों को और भी गहरे अंधकार में धकेल दिया। ‘ग्रुप एरियाज़ एक्ट’ और ‘बैंटू होमलैंड्स पॉलिसी’ जैसे कानूनों ने श्वेत अल्पसंख्यकों को 80% से अधिक भूमि पर कब्ज़ा करने की खुली छूट दी। उस दौरान श्वेत ज़मींदारों ने कृषि योग्य भूमि पर एकाधिकार कर लिया और काले किसानों को बंजर, अन- उपजाऊ इलाकों में धकेल दिया गया, जहां जीवन बिताना किसी संघर्ष से कम नहीं था।
1994 में जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने, तो उम्मीद की किरणें जगी थीं। सबको लगा था कि अब न्याय होगा, अब वह ज़मीन लौटेगी, जिसे लूट लिया गया था। लेकिन क्या हुआ? क्या सच में वह न्याय मिला? नहीं! सच्चाई यह है कि 1994 में भी काले अफ्रीकियों के पास सिर्फ 4% कृषि भूमि थी, और आज 30 साल बाद भी यह आंकड़ा मात्र 24% तक ही पहुंच पाया है, जबकि श्वेत किसानों के पास अब भी 70% से अधिक भूमि है। क्या यह लोकतंत्र की जीत है? क्या यह समानता का युग है? नहीं, यह अब भी उपनिवेशवाद की छाया में जीता हुआ ढोंग मात्र है!
अब, जबकि राष्ट्रपति रामफोसा ने इस नए कानून पर हस्ताक्षर किए, तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। श्वेत प्रभुत्ववादी, पूंजीपति वर्ग और भूमिपतियों के लिए यह भयावह सपना बन चुका है। डेमोक्रेटिक एलायंस (डीए) और फ्रीडम फ्रंट प्लस जैसे दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
वे इसे निजी संपत्ति पर हमला बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है-किसकी निजी संपत्ति? क्या वह संपत्ति वैध रूप से अर्जित की गई थी? या फिर वह वही ज़मीन है, जिसे श्वेत रंगभेदी सरकार ने चोरी किया था? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, तब तक इस विरोध के पास कोई नैतिकता नहीं है।
इतिहास हमें बताता है कि जब भी भूमि का असमान वितरण हुआ है, तब-तब विद्रोह की ज्वालाएं भड़की हैं। फ्रांसीसी क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब किसानों और मजदूरों ने सामंतों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने भी यही साबित किया कि उत्पादन के साधनों पर जनता का अधिकार ही असली न्याय है। जब भी मेहनतकश जनता ने अपनी भूमि छीनी है, तब सत्ता के गलियारों में भूकंप आया है।
दक्षिण अफ्रीका की यह लड़ाई भी उसी इतिहास का अगला अध्याय है। आज यह सवाल सिर्फ ज़मीन के टुकड़े का नहीं है, बल्कि यह पूरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने की लड़ाई है। केवल भूमि का पुनर्वितरण पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन किसानों को ज़मीन दी जाएगी, उन्हें आधुनिक कृषि उपकरण, तकनीकी सहायता और बाजार तक सीधी पहुंच मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह कानून भी महज दिखावटी सुधार बनकर रह जाएगा, जैसा कि दुनिया के कई अन्य देशों में देखा गया है।
हमारे पास ज़िम्बाब्वे का उदाहरण है, जहां भूमि पुनर्वितरण योजना के बाद आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। सरकार ने ज़मीन तो बांटी, लेकिन उत्पादन के साधनों पर ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप, कृषि व्यवस्था चरमरा गई और देश गहरे आर्थिक संकट में चला गया। दक्षिण अफ्रीका को इस गलती से सीखना होगा। सिर्फ ज़मीन देना काफी नहीं होगा, बल्कि उत्पादन और वितरण की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ना होगा।
इस कानून का विरोध करने वाले पूंजीवादी और श्वेत प्रभुत्ववादी यह तर्क दे रहे हैं कि इससे देश में आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। लेकिन यह तर्क खोखला है। सच्चाई यह है कि असली आर्थिक अस्थिरता तो तब से चली आ रही है, जब काले अफ्रीकियों को उनकी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। आज जब न्याय की बात हो रही है, तो इसे आर्थिक संकट कहकर बदनाम किया जा रहा है। यह वही मानसिकता है, जिसने सदियों तक गुलामी को जायज़ ठहराया था।
अब यह लड़ाई सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं है। यह पूरी दुनिया के शोषितों की लड़ाई है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, हर जगह मेहनतकशों की ज़मीन पर कुछ गिने-चुने पूंजीपतियों और सामंतों का कब्जा है। यह लड़ाई सिर्फ अफ्रीकी किसानों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उत्पीड़ितों की है। जब तक यह संघर्ष अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता, तब तक सामाजिक न्याय अधूरी कल्पना मात्र बना रहेगा।
अब समय आ गया है कि इस कानून को प्रतीकात्मकता से बाहर निकालकर एक वास्तविक क्रांति में बदला जाए। राष्ट्रपति रामफोसा को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कानून केवल कागजों तक सीमित न रह जाए। हर किसान, हर मजदूर को उसकी ज़मीन का अधिकार मिले और उसे उत्पादन के साधन भी दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह कानून भी अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा।
क्या हम इस क्रांति के साक्षी बनेंगे? क्या हम उस संघर्ष का हिस्सा बनेंगे, जो सदियों के अन्याय को पलटने के लिए लड़ा जा रहा है? या फिर हम चुपचाप देखते रहेंगे, जैसे सदियों तक अन्याय को देखते आए हैं?
अब यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। यह केवल भूमि सुधार नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। यह न्याय की अंतिम लड़ाई है। यह शोषण के अंत की शुरुआत है। यह उस क्रांति का शंखनाद है, जो केवल दक्षिण अफ्रीका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उत्पीड़ितों को जगाने के लिए आई है।
अब कोई समझौता नहीं होगा। अब कोई झूठे वादे नहीं होंगे। अब यह संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचेगा। यह अंतिम विद्रोह है। यह शोषण की आख़िरी दीवार को तोड़ने की आख़िरी कोशिश है।
(मनोज अभिज्ञान स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)