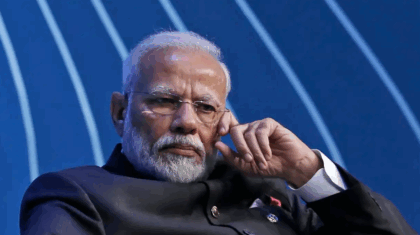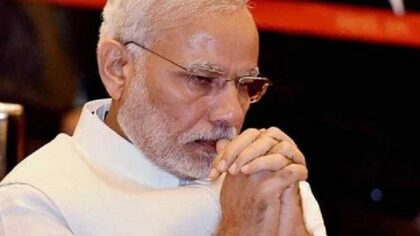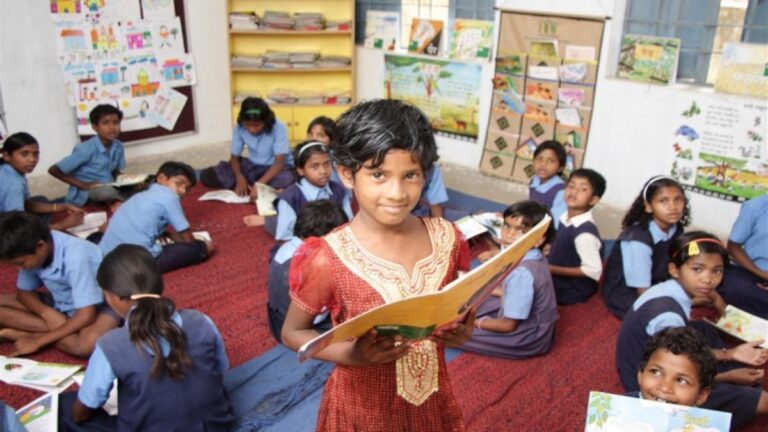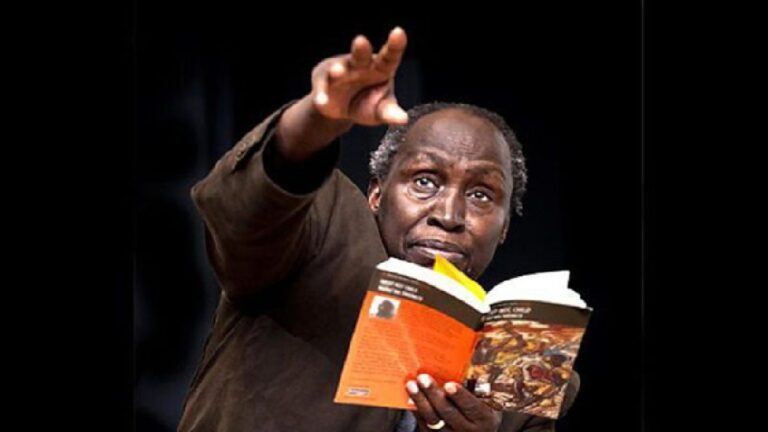एक लंबे समय बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खबर में आई। इसने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को हरियाणा के मानेसर में अमेजन कंपनी के गोदाम में अमानवीय श्रम हालात की छपी खबर के आधार पर नोटिस जारी किया था। एनएचआरसी ने मजूदरों के काम के हालात की न्यूनतम मानकों के उल्लघंन की खबर को संज्ञान में लेते हुए मंत्रालय को एक हफ्ते के भीतर विस्तार से रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
यह एक अच्छी खबर थी। एक लंबे समय बाद, खासकर पिछले दस सालों में उत्पीड़न की हजारों खबरों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चुप्पी बहस का हिस्सा भी नहीं रह गई थी। बड़े पैमाने पर बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, अल्पसंख्यक समुदायों, मजदूरों, किसानों और यहां तक कि राजनीतिक दलों पर दमन की खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लगातार चुप्पी के चलते यह मान लिया गया था कि यह संस्था सरकार की ही एक संस्था की तरह काम करने को अभिशप्त हो गई है। हालांकि, तब भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लोगों ने ज्ञापन देना बंद नहीं किया था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना बकायदा मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। इस अधिनियम के तहत मानवाधिकार का अर्थ इस तरह से बताया गया हैः ‘‘एक व्यक्ति की जिंदगी, आजादी, समानता और सम्मान का वह अधिकार हासिल है, जो संविधान या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित है और भारत की न्याय व्यवस्था से लागू किया है।(सेक्शन 2डी)।’’
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्रसंघ से जुड़ा मानवाधिकार संगठन ‘अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। इसी की एक कमेटी इससे जुड़े मानवाधिकार संगठनों की गतिविधियों पर नजर भी रखती है। 1999 में इस कमेटी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ‘ए’ श्रेणी प्रदान किया था। सन् 2000 के बाद इस संस्था की स्थिति बिगड़ती गई लेकिन उसकी श्रेणी में बदलाव नहीं आया। 2016 तक आते आते स्थिति बिगड़ चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इसकी संरचना और कार्यपद्धति पर सवाल उठाये। 2017 में एक फिर इसे ‘ए’ श्रेणी वापस मिल गया।
2023 में एक बार फिर इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर सवाल उठाया। खासकर, पदाधिकारियों को मनोनीत करना और महिला और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व न होना, मनोनयन की पारदर्शिता में कमी का मसला उनके लिए मुख्य था। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि 2021 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को सर्वोच्च न्यायलय से सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया था।
मानवाधिकार के मामलों में भारत की स्थिति बद से बदतर हो रही थी। मानवाधिकार आयोग कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और ऐसे संगठनों का दमन एक रोजमर्रा की खबर में बदलती चली गई। वकीलों की गिरफ्तारी इसी का अगले कदम की तरह दिखता है। चुनाव के पहले जिस तरह से राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को जिस तरह से दमन का निशाना बनाया गया, भारत के इतिहास में आपातकाल के दौर में हुए दमन से भी आगे निकल जाने की तैयारी जैसा दिख रहा था। इस चुनाव में संविधान बचाना एक नारा बन गया। इस पूरे दौर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चुप्पी निश्चित ही इसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर रही थी।
मोदी 2.0 की आजादी का अमृतकाल का असर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर भी पड़ा। इसने सितम्बर, 2023 के ब्रोशर में विरासत का गुणगान करते हुए वेद, उपनिषद और विविध धर्मशास्त्रों का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति के ‘न्याय के सिद्धांतों’ का उल्लेख किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के ब्रोशर के अनुसार, ‘‘मनुस्मृति जब अपने समय की सामाजिक मान्यताओं को प्रदर्शित करता है, तब वह न्याय के सिद्धांतों, जिसमें अपराध के अनुपात में दंड निहित है, की रूपरेखा भी प्रदर्शित करता है।’’
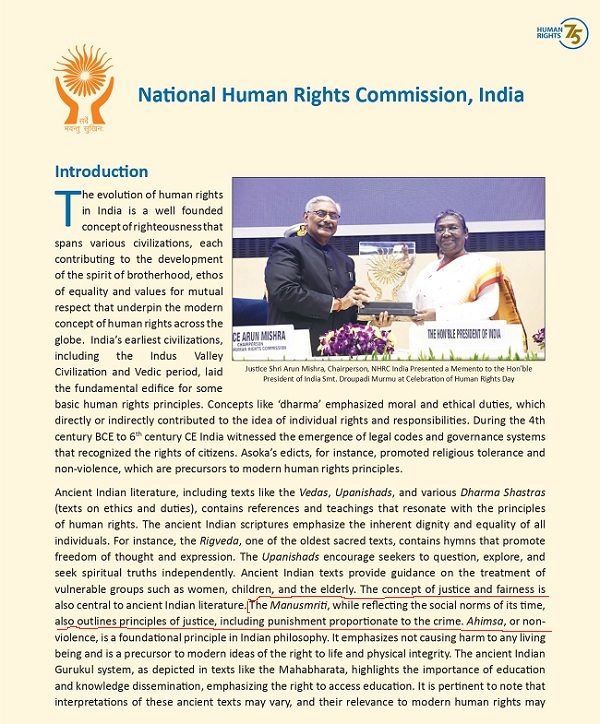
ब्रोशर जिन बातों को सूत्रबद्ध कर मनुस्मृति के हवाले से उद्धृत करता है, क्या वह सही है? क्या मनुस्मृति अपराध के अनुपात में दंड की व्यवस्था निर्धारित करता है? जो भी मनुस्मृति को सरसरी तौर पर भी पढ़ा है उसमें अपराध का अनुपात उसकी जाति और लिंग से निर्धारित किया जाता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जब मनुस्मृति के दहन का आयोजन किया तब वह सिर्फ एक किताब नहीं जला रहे थे। वह समाज के भीतर बनी हुई मनुस्मृति की ‘न्याय प्रणाली’ को चुनौती दे रहे थे। वह भारत में संविधान का राज चाहते थे। वह आधुनिक समाज में स्वतंत्रता, समानता, जीवन और उसके सम्मान के मूल्य पर आधारित न्याय व्यवस्था चाहते थे।
उन्होंने जो ‘मनुस्मृति दहन’ का सिलसिला शुरू किया उसका उद्देश्य उस ‘विरासत’ को ध्वस्त करना था जो भारत के गांवों और शहरों तक फैला हुआ है। आज भी सनातन के नाम पर जाति और वर्ण के भेदभाव, ब्राम्हण को सर्वोच्च इंसान मानने वाले पंडों, पुरोहितों, यहां तक कि बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। आज भी ऐसे लोगों की विशाल संख्या है जो कथित ‘विरासत’ वाला ही समाज बनाकर रखना चाहते हैं। भारत का संविधान और कानून व्यवस्था, न्यायप्रणाली अपने विभिन्न प्रावधानों के तहत जाति और वर्ण के आधार पर होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण पर दंड की व्यवस्था कायम करता है। यह मनुस्मृति की विरासत को सिरे से खारिज करता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विरासत के नाम पर जिस तरह से मनुस्मृति का उल्लेख किया गया है, वह बेहद चिंताजनक और मानवाधिकार की स्थिति के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। खासकर, उस दौर में जब हिंदुत्व की लहर विरासत के नाम इतिहास को खंडहर बनाने पर तुली हुई हो और प्राचीनता के गर्त में डूब जाने के लिए उतावला हो गई हो। गांव से लेकर शहर, मोहल्लों से लेकर काम के स्थलों, शिक्षा संस्थानों से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर जाति आधारित उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं रोजमर्रा का हिस्सा बनी हुई हों, तब मनुस्मृति को न्याय की विरासत की तरह देखना मानवाधिकार के लिए गंभीर चुनौती है। इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को जरूर ही दुरूस्त कर लेना चाहिए।
विरासत में प्राचीन धर्मग्रंथों, दार्शनिकों में न तो बौद्ध ग्रंथों, उसके चिंतन और बुद्ध की चर्चा है और न ही आजीवक और जनधर्म के मुनियों, उनके ग्रंथों और उनके सिद्धांतों की चर्चा है। एक व्यक्ति की अच्क्षुण सत्ता की व्याख्या करने वाले सांख्य दर्शन का उल्लेख है और न ही नागार्जुन के असीम करूणासिक्त शून्यवाद को याद किया गया है, जिसकी भूमि पर करुणा और तप का सिद्धांत विकसित हुआ और भक्ति काल में इसने जीवन हासिल किया। इस विरासत की गाथा में विशाल मध्यकाल गायब है। इस दौर में मानव जीवन को गहरे प्रभावित करने और उसे मूल्यों के आधार पर जीने की ओर ले जाने वाली भक्ति और सूफी धारा का जिक्र नहीं आता है। मध्यकाल की न्यायव्यवस्था की बातें नदारद हैं।
हम इस ब्रोशर में सीधे उपनिवेशिक काल में उतरते हैं और फिर संयुक्त राष्ट्रसंघ का हिस्सा होने के साथ मानवाधिकार के नये रास्ते पर चल निकलते हैं। कोई भी समाज, राष्ट्र, देश अपनी विरासत को याद करता है। वह उसी परम्परा को याद करता है जो उसे वर्तमान तक और भविष्य की प्रगतिशील धारा तक ले जाता है। इतिहास हमेशा दो परम्पराओं को लेकर चलता है। इन परम्पराओं का चुनाव ही हमारी विरासत होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा चुनी गई विरासत किसी भी तरह हमारी विरासत का हिस्सा नहीं हो सकती। यह निश्चित ही भारतीय राज्य की संविधान, कानून और सरकार की जो आधारभूमि है, उसमें भी मनुस्मृति का ‘न्याय का सिद्धांत’ विरासत का हिस्सा नहीं हो सकता। यह उसकी आधारभूमि का उल्लंघन है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)