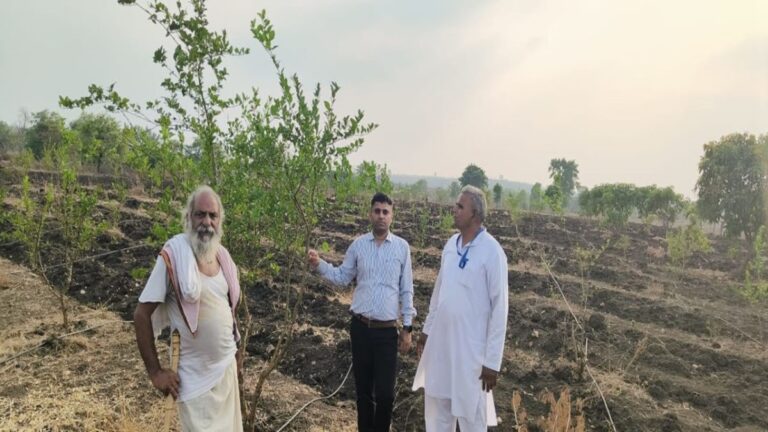हिमालयी क्षेत्र में चरम मौसमी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद ग्लेशियरों की अवस्था के बारे में सरकारी स्तर पर कोई व्यापक अध्ययन नहीं हुआ जबकि ग्लेशियर हिमालय की जलवायु के मुख्य नियामक हैं। वे देश के महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। इसे देखते हुए संसदीय स्थाई समिति ने ग्लेशियरों के मामलों का अध्ययन व प्रबंधन के लिए एक अधिकार संपन्न शीर्ष संस्था बनाने की सिफारिश की है।
जल-संसाधन विभाग से जुड़ी संसदीय स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट “भारत के ग्लेशियरों का प्रबंधन” में यह सिफारिश की है। रिपोर्ट को पिछले सप्ताह संसद के पटल पर रखा गया। संसदीय समिति ने यह अध्ययन हिमालय क्षेत्र में अक्सर आ रही आपदाओं के मद्देनजर किया था। खासकर उत्तराखंड के चमोली में 2021 फरवरी में आई भयानक बाढ़ जो ग्लेशियर टूटने के कारण आई थी। पूर्वानुमान के लिए अपेक्षित आंकड़ों के अभाव को देखते हुए समिति ने तत्काल माउंटेन हजार्डस एंड रीसर्च इस्टीच्यूट की स्थापना की जरूरत बताई है।
समिति ने कहा है कि ग्लेशियरों के मामले कई मंत्रालयों और विभागों व संस्थानों के कामकाज के दायरे में आते हैं। इनमें भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, खनन मंत्रालय, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान व तकनीक मंत्रालय के अलावा जल-संसाधन मंत्रालय आदि शामिल हैं। इनके अध्ययन व शोध के आंकड़े बिखरे हुए हैं। उनके आधार पर कोई व्यवस्थित कार्ययोजना नहीं बनाई जा पाती।
समिति की सिफारिश जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस प्रस्तुति पर आधारित है कि उसने 1950 से 2020 के बीच ग्लेशियरों के आयतन घटने के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। साथ ही वर्ष 2100 की स्थिति के बारे में कोई आकलन या पूर्वानुमान नहीं किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी ग्लेशियर के आयतन में कमी के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। मंत्रालय ने हिमालय पर वैश्विक तापमान में बढोतरी के प्रभाव का अध्ययन भी नहीं कराया है, इसके लिए कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है।
हिमालय क्षेत्र में हिम-स्खलन या बादल फटने से आई बाढ़ के बारे में केंद्रीय जल आयोग स्थानीय अधिकारियों के चेतावनी नहीं देता। हिमालय में उन इलाकों को चिन्हित भी नहीं किया गया है जिनमें ग्लेशियर के पिघलने और इससे बनी ग्लेशियर झीलों के फटने की आशंका है। ग्लेशियर झीलों की संख्या और विस्तार में सामयिक परिवर्तनों के बारे में इसरो और जीएसआई ने भी कोई अध्ययन नहीं किया है।
समिति ने कहा है कि इन कमियों को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिकार संपन्न संस्था बनाने की सिफारिश की जाती है जो विभिन्न हाइड्रो-जियोलाजिकल और हाइड्रो-मेटेयोरोलॉजिकल संकटों को बारे में विभिन्न सूचनाओं के बीच समन्वय कर सके। जिससे ग्लेशियरों से जुड़े संकटों के बारे में सारी जानकारी एक जगह एकत्र हो और समय पर उपलब्ध कराने में सुविधा हो।
ग्लेशियर हिमालयी क्षेत्र के जलचक्र के महत्वपूर्ण अवयव हैं। तीन विशाल नदी प्रणालियों का उदगम इनसे होता है- सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनसे हिमालय की तराई के करोड़ों निवासियों को जल उपलब्ध होता है। इस पूरे इलाके में बरसात के बाद भी पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इन नदी प्रणालियों से हो पाती है।
समिति ने उल्लेख किया है कि हिमालय क्षेत्र में अभी 9,775 ग्लेशियर हैं और लगभग 1306.1 घन किलोमीटर बर्फ की परत है जिसका मतलब 1110 घन किलोमीटर जल होता है। सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र घाटियों में अलग अलग इकट्ठा बर्फ व जल के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है। संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा सदस्य पर्बतभाई सावाभाई पटेल हैं।
हिमालय में बर्फ की परत की मोटाई घटने की गति हाल के वर्षों में काफी बढ़ गई है। इसलिए समिति ने सलाह दी है कि ग्लेशियरों की निगरानी नजदीक से की जाए और ग्लेशियरों से जल-निस्सरण, ग्लेशियर झीलों का निर्माण और उन झीलों का टूटना और अचानक विनाशकारी बाढ़ आने की निगरानी बहुत जरूरी हो गया है। इन हादसों से संभावित नुकसान को कम करने के उपाय भी किया जाना जरूरी है।
इस लिहाज से ग्येशियरों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए जरूरी अध्ययन करने, निगरानी व पूर्वानुमान के लिए उपयुक्त उपाय करने में वैज्ञानिकों, योजनाकारों व अकादमिक लोगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। बिखरे हुए शोध व अध्ययन से कोई खास लाभ नहीं होने वाला। इनके आधार पर कोई कार्ययोजना नहीं बनाई जा सकती। इसलिए एक शीर्ष संस्थान बनाने की जरूरत है जो ग्लेशियरों से जुड़े सभी संस्थानों के बीच तालमेल बिठाए और जरूरी कार्ययोजना तैयार करे।
(अमरनाथ झा वरिष्ठ पत्रकार हैं)