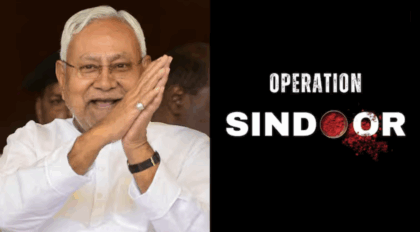बर्फ़ से ढकी वादियां, झीलों की तह में छुपे नर्म जज़्बात, और हवा में घुली सुकून की सरगोशियां- कश्मीर की वो तस्वीर थी, जो सदियों से इस मुल्क की मोहब्बत की मिसाल बनती आई है। मगर अब, उस तस्वीर में बारूद की बदबू घुल चुकी है, और फूलों की घाटी में लहू का रंग उतर आया है।
पहलगाम की नर्म सरज़मीन पर हुई ये दरिंदगी, कोई हमला नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत पर लिखा गया एक खूनी पैग़ाम है।
एक ख़ूबसूरत सुबह जब सैलानी अपने बच्चों की हथेलियों में उम्मीदों की मेंहदी लगाए पहलगाम की वादियों में उतरते हैं, तो कौन जानता था कि वही वादियां, एक लम्हे में क़ब्रगाह में तब्दील हो जाएंगी?
दरिंदों ने टोका, रोका, पूछा- “क्या मज़हब है तुम्हारा?”
और फिर वो किया जो किसी मज़हब में जायज़ नहीं, किसी तहज़ीब में माफ़ नहीं, किसी इंसानियत में बर्दाश्त नहीं।
मगर सोचिए- यह सवाल दरअसल ‘मज़हब’ से ज़्यादा एक ज़हर था।
एक ऐसा ज़हर जो हमारे दिलों में दरार पैदा करे, जो हमें बांटे, जो हमारे बीच मोहब्बत के पुलों को गिरा दे।
क्योंकि अगर हमला महज़ किसी धर्म पर होता- तो ज़ख़्म पूरे मुल्क में महसूस न होते।
मगर ये तो हमला वतन पर था।
हम सब पर था।
हमारी रूह पर था।
कितनी अजीब बात है-
जो मारे गए, वो गिनती में दर्ज हैं,
मगर जो ज़िंदा रह गए, उनके दिलों में जो मरा – उसका हिसाब कौन रखेगा?
आतंकवाद का मक़सद गोलियां चलाना नहीं होता, उसका असली मक़सद दिलों में दीवारें बनाना होता है।
वो पूछते हैं “तुम कौन हो?”, ताकि हम एक-दूसरे को शक की निगाह से देखें।
वो बांटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एकजुट भारत- उनके लिए सबसे बड़ा ख़ौफ़ है।
लेकिन क्या हमें अब भी ये समझ नहीं आता?
क्या हर हादसे के बाद हम वही पुराना खेल दोहराएंगे- एक मज़हब को गुनहगार बना, दूसरे को पीड़ित?
क्या हर लहू की बूंद पर हम राजनीति की सियाही मल देंगे?
हम कब समझेंगे कि आतंकवादी के पास न मज़हब होता है, न मातम।
उसके पास बस एक एजेंडा होता है- भारत को तोड़ने का, और हम सब उस एजेंडे में मोहरे बनते जा रहे हैं।
पठानकोट, ऊरी, पुलवामा और अब पहलगाम-
क्या ये सिलसिला थमने वाला नहीं?
क्या हर बार हम सिर झुकाकर, आंसू बहाकर, दो पल का शोक मनाकर फिर वही भूलने वाला समाज बन जाएंगे?
और क्या हमारी सरकारें सिर्फ़ श्रद्धांजलियों की तस्वीरों में मुस्तैद हैं?
क्या खुफ़िया तंत्र सिर्फ़ तब जागेगा जब बारूद की गूंज वादियों से उठकर दिल्ली की दीवारों तक पहुंचेगी?
आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि आतंकियों ने गोली क्यों चलाई-
बल्कि यह है कि हम हर बार क्यों चुप हो जाते हैं?
हम क्यों नहीं पूछते कि ये हमले रुक क्यों नहीं रहे?
क्यों नहीं मांगते जवाब- उस सत्ता से जिसने हर चुनाव में सुरक्षा का वादा किया था?
मगर अफ़सोस, आज सबसे ऊंची आवाज़ वही है जो सबसे ज़हरीली है-
जो इस खून को भी मज़हब के तराज़ू में तौल रही है।
जो इस मातम को भी हिंदू बनाम मुसलमान बनाने में जुटी है।
मगर सुनो-
पहलगाम के उन दरख़्तों ने जो चीख़ें सुनीं, उनमें ना कोई भगवा था, ना हरा।
उनमें सिर्फ़ एक रंग था- इंसानियत का सुर्ख़ रंग।
और यही रंग हमें एकजुट कर सकता है।
हमें मज़हब के नाम पर बंटने नहीं देना।
हमें मोहब्बत के नाम पर इकट्ठा होना है।
अब वक़्त है कि हम ये साबित करें –
कि हम पहलगाम नहीं भूलेंगे,
मगर उसकी याद को नफ़रत की आग नहीं,
इत्तिहाद की लौ से रोशन करेंगे।
बोलिए- मगर ज़मीर से।
लिखिए- मगर मोहब्बत से।
लड़िए- मगर दरिंदों से, एक-दूसरे से नहीं।
क्योंकि जब आख़िरी गोली चल चुकी होगी और आख़िरी चीख़ खामोश हो जाएगी, तब इतिहास हमसे सिर्फ़ एक सवाल पूछेगा-
“जब इंसानियत मारी जा रही थी, तुम किसके साथ खड़े थे?”
(जौवाद हसन स्वतंत्र पत्रकार हैं।)