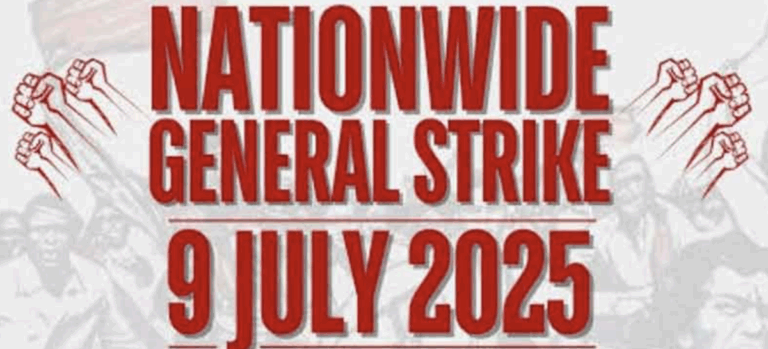असल जातिवादी राजनीति कुछ लोगों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है, न कि बहुलांश के साथ होने वाले अन्यायों पर बात करना
मैं यह लेख केंद्र सरकार द्वारा 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे के संदर्भ में लिख रहा हूं जिसमें कहा गया है कि 2021 में जाति जनगणना “व्यवहारिक तौर पर संभव” नहीं होगी। यह बहाना समकालीन वास्तविकताओं पर आधारित समावेशी विकास के लिए नए मानक गढ़ने के लिए उन जरूरी आंकड़ों को जुटाने के मार्ग में बाधा पैदा करेगा, जिसकी सामूहिक मांग पूरे भारत से की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में यह कहा कि उसका यह रुख 1951 के बाद से लिए गए “सचेत” निर्णय पर आधारित है। सरकार का यह कथन तर्क और इरादे दोनों स्तरों पर अनुपयुक्त है। यह तर्क के स्तर पर इसलिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इससे सरकार को ठोस एवं विशिष्ट आंकड़े प्राप्त होंगे, जिससे उसे लक्षित-नीति निर्माण का अवसर मिलेगा। वह ऐसा अवसर क्यों गवां रही है? यह इरादे के तौर पर इसलिए अनुपयुक्त है क्योंकि सरकार को 1951 तक पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले इसके कई मौजूदा मंत्रियों ने साफ शब्दों में जाति जनगणना का वादा किया था। जाति जनगणना सरकार के लिए “व्यवहारिक कदम”नहीं है क्योंकि कई अन्य वादों की तरह, जाति जनगणना कराने का वादा भी एक जुमला था, सिर्फ खोखली बयानबाजी।
तीन दशकों से अधिक समय से सामाजिक न्याय के दर्शन और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कई नेताओं और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा जाति जनगणना या जातियों की अद्यतन संख्यात्मक स्थिति की जानकारी की मांग को दृढ़ता से उठाया जा रहा है। मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने अन्य राजनीतिक दलों के सहयोगियों के साथ मिलकर संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगहों पर इस तरह के आंकड़ों की आवश्यकता के मुद्दे को उठाया। इस मांग के पीछे का उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों के अनदेखे पहलुओं और संसाधनों में उनके हिस्सेदारी को सामने लाना था। इस तरह के आंकड़े हमें न केवल विभिन्न जाति समूहों की सटीक आबादी बताएंगे बल्कि आजादी के बाद से तथाकथित समावेशी विकास का आकलन करने में भी मदद करेंगे। इन महत्वपूर्ण चिंताओं के आलोक में, और कुछ मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद, 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सबाल्टर्न आवाजों के दबाव में जाति जनगणना कराने का फैसला किया।
70 से अधिक वर्षों से, हम सभी सरकारों के मुंह से गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी समाप्त करने और संसाधनों के समान वितरण के बारे में सुन रहे हैं। जबकि निरपेक्ष गरीबी कई गुना बढ़ गई है, जातियों और वर्गों के बीच असमानता दिन-ब-दिन चौड़ी होती जा रही है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मानकों पर दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समूहों की बदतर जीवन स्थितियों के बारे में कड़वी सच्चाईयों का खुलासा किया है, और उनका और हाशिए पर जाना हमारे समय की त्रासदी है। कई अध्ययनों से पता चला है कि प्रभुत्वशाली अभिजात्य वर्ग ने संसाधनों के 90 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि आबादी में इनकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम है। अभिजात्य वर्ग के इस समूह का एक बड़ा हिस्सा राज्य को जन-समर्थक नीतियां बनने से रोक रहा है। इस प्रभुत्वशाली आभिजात्य समूह के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को इस या उस बहाने से एक के बाद दूसरी आने वाली सरकारों ने दबा दिया।
यदि समावेशी विकास हमारे देश की संवैधानिक प्राथमिकता है, तो हमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की मांग जरूर करनी चाहिए और इसे सार्वजनिक तौर पर सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि हमारी विकास नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ निर्धारित किया जा सके और उसे आकार दिया जा सके और इन नीतियों एवं कार्यक्रमों से हाशिए पर रहने वाले लोगों और समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। विकास वास्तव में सशक्तिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इसकी प्राथमिकता तय करने का निर्णय उन लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता है जिनके पास 90 प्रतिशत संसाधन हैं। यह सही या उचित नहीं लगता है कि विकास का अर्थ केवल सेंसेक्स के उतार-चढ़ाव से निर्धारित किया जाना चाहिए, जो समकालीन समय में चर्चा का मुख्य विषय होता है, जिसमें अक्सर मानवीय पहलू और सरोकारों की कमी होती है।
सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग के साथ-साथ मुख्यधारा की मीडिया के कुछ लोग यह कहते रहते हैं कि जाति जनगणना को सार्वजनिक करने की मांग हर क्षेत्र में जातिवाद को जन्म दे सकती है। इस तरह के भय और भ्रम पैदा करने वाली बातों से वस्तुगत तौर से निपटने की जरूरत है। हम इस मुद्दे के इर्द-गिर्द किए जा रहे भ्रामक प्रचार का मुकाबला तथ्यों और ठोस तर्कों से करेंगे। आइए हम समकालीन विकास के मानदंडों के संबंध में कुछ जरूरी प्रश्न पूछें, जिसका संबंध सबका साथ, सबका विश्वास की बयानबाजी से है। कौन वे लोग हैं, जो ऐसे पेशे करते हैं, जो उन्हें न तो गरिमा प्रदान करते हैं और न ही पर्याप्त आजीविका? वे कौन से मेहनतकश लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है और जो हमेशा किसी न किसी गहरे आर्थिक संकट में रहते हैं? शहरों में अनिश्चित भविष्य के बावजूद हमारे गांवों से पलायन करने वाले लोग कौन हैं? कल्याणकारी राज्य या कम से कम सरकार यह जानने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती कि ये लोग कौन हैं? जबकि सरकारें अक्सर इनके बारे में बहुत जिज्ञासा दिखाती हैं। क्या उनकी जाति उनकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण करती है या उनकी एजेंसी बताएंगी कि सच्चाई क्या है?
हमें इस तथ्य का भी पता है कि ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों का बड़ा हिस्सा खतरनाक रूप से भूमिहीन है। आज जाति और भूमि के स्वामित्व के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है ताकि हम संवेदनशील और समावेशी हस्तक्षेपकारी योजनाएं तैयार करके इस विकट स्थिति से निपट सकें। क्या यह जातिवाद फैला रहा है अगर हम पूछें कि शहरी क्षेत्रों में कौन बेघर है या दिहाड़ी मजदूरों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? सिर्फ गरीबी, पिछड़ेपन और हाशिए पर जाने के जातिगत वास्तविकता पर सवाल उठाना जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं कहा जा सकता है और न ही इसे जातिवाद को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। वास्तव में, संविधान की प्रस्तावना की भावना के अनुसार चलते हुए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सार्वजनिक नीति हमारे समय की महत्वपूर्ण वास्तविकताओं के अनुरूप हो।
कई मित्र दावा करते हैं कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन असमानता के इर्द-गिर्द किए गए सभी अध्ययनों और शोधों से पता चलता है कि अधीनस्थ जातियों में गरीबी व्याप्त है। हमारी विकास की महागाथा में इन समूहों की भागीदारी और जुड़ाव की कमी पर सवाल उठाना जातिवादी राजनीति के लिए बोलना कैसे बन जाता है? कड़वी सच्चाई यह है कि असली जातिवादी राजनीति वह है जो मुट्ठी भर लोगों के विशेषाधिकारों को ढंकने के लिए “सचेत” निर्णय लेती है और अपने करोड़ों नागरिकों की बदतर स्थिति को खत्म करने के लिए इसे ( जाति जनगणना को) “व्यवहारिक तौर पर संभव” नहीं पाती है।
(यह लेख ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के सितंबर 27, 2021 के संस्करण में ‘कॉउंट द लैडर्स रंग्स’शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। लेखक बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता हैं। लेख का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद डॉ. सिद्धार्थ ने किया है।)