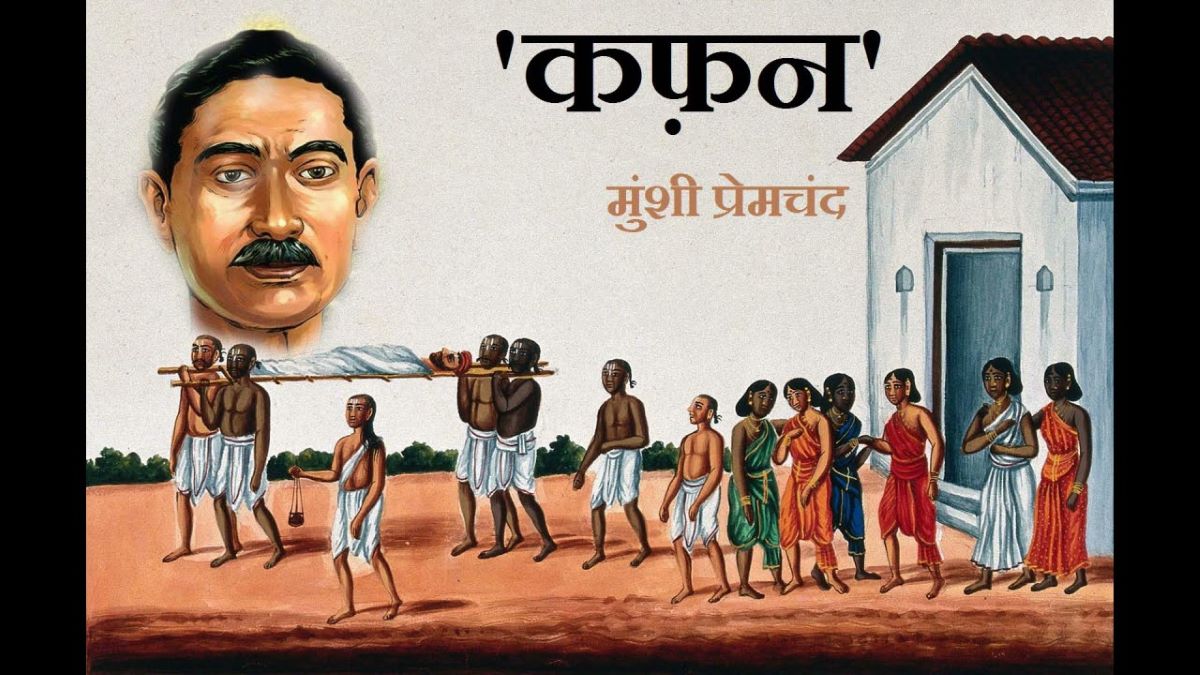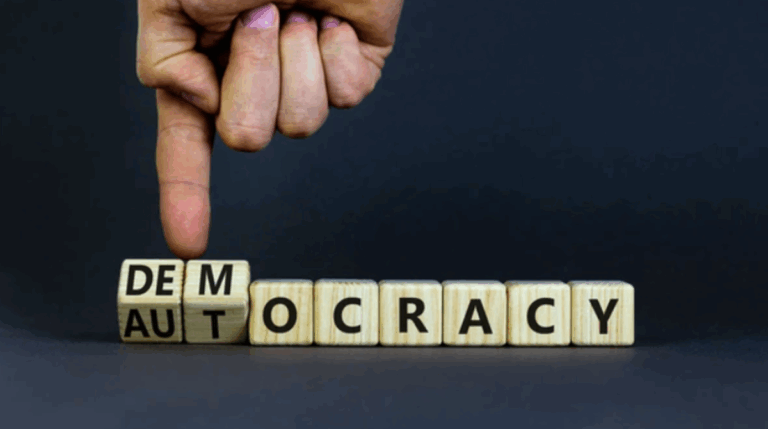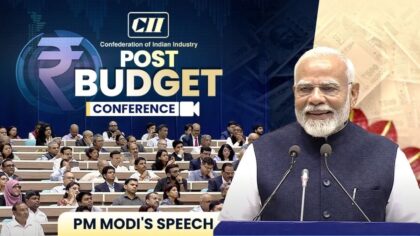सृजनात्मक साहित्य के महान से महान लेखक सफल और असफल होते रहे हैं। दुनिया के महान उपन्यासकारों और कहानीकारों की कहानियां देखिए। कोई एक कहानी बहुत सफल होती है, दूसरी में वे पूरी तरह गच्चा खा जाते हैं। यहां सफलता-असफलता का सिर्फ एक मतलब है, जीवन-यथार्थ की अभिव्यक्ति में सफलता और असफलता है। यह बात महान कहानीकार चेखव, मोपासा, जैक लंडन, आदि पर भी लागू होती है।
कहां, क्यों और कैसे? कफन मे प्रेमचंद गच्चा खाते हैं
प्रेमचंद की इस कहानी की रीढ़ ही मानव मनोविज्ञान की गलत समझ पर आधारित है। घूसी-माधव सिर्फ भुना आलू खाने की लालच में अपनी पत्नी और बहू को भयानक मानवीय यातना में अपने सामने ही मर जाने देते हैं। उसकी दर्दनाक पुकार और असहनीय पीड़ा से निकली आह का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि वह गर्भवती है। उसके पेट में माधव का बच्चा और घीसू का पोता-पोती है। एक तो वह औरत नहीं मर रही है, उसके साथ बच्चा भी मर रहा है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे भावनात्मक लगाव पत्नी, विशेषकर बच्चे से होता है। बच्चे की तुलना में पोते-पोती से कुछ ज्यादा ही होता है। पति-पत्नी का शारीरिक रिश्ता भावनात्मक रिश्ते को और मजबूती प्रदान करता है।
माधव और घीसू उस औरत और पेट में पल रहे बच्चे को सिर्फ इसलिए मर जाने देते हैं कि उनको ठीक से मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें नियमित काम नहीं मिलता। वे कामचोर हैं और जब वह मर रही है, तो दोनों आलू को दूसरा न खा जाए, इस चिंता और प्रतियोगिता में हैं।
अपनी पत्नी, उसके पेट में पल रहे बच्चे को माधव सिर्फ इसलिए मर जाने देता है, क्योंकि वह अपने बाप से आलू खाने की प्रतियोगिता में है। घीसू अपनी बहू और पोते-पोती को इसलिए मर जाने देता है कि वह अपने बेटे से भुना आलू खाने की प्रतियोगिता में है।
दुनिया के मनोवैज्ञानिकों और रचनकारों ने इस तरह के अमानवीकरण की कल्पना सिर्फ एक स्थिति में की है, जब आदमी का अस्तित्व दांव पर लगा हो, उसके सर्वाइवल का प्रश्न हो। उसकी जान जानी तय हो। उसे यह तय करना हो कि वह अपनी जान बचाएगा या अपने प्रिय या करीबी या साथी की। यह मनोविज्ञान मनुष्यों की तुलना में जानवरों के बारे में ज्यादा लागू होती है। लेकिन किन्ही हालातों में अपनी जान बचाने के लिए मनुष्य भी अपने प्रिय की, नजदीकी से नजदीकी की जान की बलि दे देता है, उसे मर जाने देता है। लेकिन इंसान के बारे में इसका उलटा भी अक्सर होता है, वह अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरे की जान बचाता है।
सर्वाइवल या जीवित रहने के लिए मनुष्य क्या-क्या कर सकता है, इस विषय पर जैक लंडन ने इस बहुत एक महत्वपूर्ण कहानी लिखी है। जो हिंदी में प्रकाशित उनके कहानी संग्रह ( जिंदगी से प्यार- ‘ताकि आग जले’) में है। वहां एक व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए या जीवित रहने के लिए क्या-क्या कर सकता है। इसका बहुत ही यथार्थ परक वर्णन है।
कफन कहानी में घीसू-माधव अपने सर्वाइवल के लिए अपनी बहू और पत्नी-बच्चे को तड़प-तड़प कर मर जाने देते हैं, ऐसा कहीं नहीं दिखता। उन्हें भूख लगी है, यह तो सच है। लेकिन भूख से वह मरने वाले हैं और मौत से बचने के लिए आलू के लिए प्रतियोगिता करते हैं, ऐसा नहीं दिखता। आलू खाना उनके सर्वाइवल का प्रश्न नहीं है। इतना ही नहीं, भूख और लालच से ज्यादा कोई दूसरा न खा जाए, इस प्रतियोगिता में अपनी पत्नी और बहु को बचाने तो छोड़ दीजिए, सहारा भी देने नहीं जाते।
कथा का यह मूल केंद्र ही मानव मनोविज्ञान की पूरी तरह गलत समझ पर आधारित है। कोई कह सकता है कि किसी एक मामले में यह हो सकता है, वह एक मामला भी जो सामने है, उसमें ऐसा होने की कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती है। सब कुछ आर्टिफिशियल और तयशुदा घटित होता दिखाई देता है।
दलित-मेहनतकशों का जीवन श्रम की गरिमा न होने और वाजिब मजदूरी न मिलने के चलते इस कदर अमानवीकृत हो चुका है कि या हो रहा है कि वे आलू खाने और भूख मिटाने की प्रतियोगिता में पत्नी-बहू और बच्चे की मौत की भी परवाह नहीं करते। यह यदि दलित मेहनतकशों के जीवन का यथार्थ था, यह यथार्थ पनप रहा था, तो दलित जीवन-यथार्थ की अभिव्यक्ति वाली महत्वपूर्ण रचनाओं में इसके कुछ रूप तो जरूर दिखते हैं।
ऐसा कुछ न दया पवार की आत्मकथा, ‘अछूत’ में दिखता है, न ‘जूठन’ में, न ही ‘मुर्दहिया’ में, न ही ‘मेरा बचपन मेरे कंधों पर’, न ही ‘अक्करमाशी’ में, न ही किसी और में। इन रचनाओं में दलित जीवन के अमानवीकरण के बहुत सारे रूप दिखते हैं, क्रूरताएं भी दिखती हैं, लेकिन कोई एक संकेत भी नहीं दिखता, जिसमें कोई दलित मेहनतकश इस कदर अमानवीकृत हो जाए कि वह आलू खाने की प्रतियोगिता में अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को सामने ही मर जाने दे। कुछ भी न करे। बहुत सारे शराबियों की लापरवाही से बच्चे भूखे रहते हैं, पत्नी बीमार रहती है। बूढे़ पिता खटते हैं, शराबी बेटा शराब पीने में मस्त रहता है। यह सब भी किसी की मौत का कारण बन सकता है। लेकिन इन मामलों में एक पर्दा होता है, चाहे जितना झीना हो।
लेकिन आप बैठकर आलू खा रहे हैं, आपके पास ही कोई आपका प्रिय मर रहा है। यह संवेदनहीनता की चरम सीमा होती है, जहां इंसान, इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह जाता है।
एक और बात यह कहानी ग्रामीण समाज की कहानी है, मूलत: सामंती समाज की कहानी है। स्वयं प्रेमचंद अपने चर्चित लेख ‘महाजनी सभ्यता’ में पूंजीवाद की तुलना में सामंती समाज के कुछ उदात्त मूल्यों की चर्चा करते हैं, कुछ मानवीय संबंधों की बातें करते हैं। जिसके बारे में, जिन्हें मार्क्स के शब्दों में, पूंजीवाद ने बर्फ के ठंडे पानी में डुबो दिया है। घीसू-माधव के अमानवीकरण की तस्वीर प्रेमचंद ने खींची है, वह पूंजीवादी अमानवीकरण नहीं है। घीसू-माधव किसी शहर की श्रम बस्ती में रहने वाले फैक्टरी के मजदूर नहीं हैं। जहां एक श्रमिक कई बार इतना अलग-थलग पड़ जाता है कि संबंधों और संवेदना तक को भूल जाता है। वह टूल्स के तौर इस कदर इस्तेमाल हो जाता है कि वह खुद एक अमानवीकृत टूल बन जाता है।
सच तो यह है कि प्रेमचंद की इस पूरी कहानी का प्लाट आर्टिफिशियल है। श्रमिकों के अमानवीकरण का सिद्धांत सामने रखकर लगता है कि कहानी बुनी गई है। इस तरह के चरित्र उन्हें भारत के ग्रामीण समाज में दिख रहे थे और उन्होंने उन्हें कहानी का विषय बनाया ऐसा नहीं लगता। कहानी पढ़कर साफ लगता है कि उन्होंने श्रमिकों के अमानवीकरण पर कहानी लिखने का निर्णय पहले लिया। कहानी के चरित्र और कथा-विन्यास को उस अपनी चाहत के इर्द-गिर्द बुना।
आम तौर पर प्रेमचंद अपने उपन्यासों-कहानियों में सामाजिक जीवन में मौजूद वास्तविक चरित्रों को उठाते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके उस पात्र को विकसित करते हैं, अन्य वास्तविक पात्रों को साथ मिलाकर कथा-विन्यास रचते हैं। जैसा कि हर सृजनशील रचनाकार करता है, एक पात्र में दो-तीन या इसके अधिक पात्रों का मेल कराते हैं। प्रेमचंद चूंकि प्रतिनिधिक पात्र रचते हैं, उनके लिए ऐसा करना और भी जरूरी था।
इस कहानी को पढ़कर लगता है कि प्रेमचंद श्रम और श्रमिक विरोधी हालातों में डिह्यूमनाइज होते मेहनतकशों का चरित्र रचने का निर्णय पहले लेते हैं। उसके आधार पर एक कहानी का ताना-बाना बुनते हैं। ऐसी कहानियां उस समय दुनिया में बहुत सारी लिखी जा रही थीं। जिसमें पूंजीवाद श्रमिकों को इस कदर लूट रहा है कि वे अमानवीकृत हो जाते हैं।
श्रम और श्रमिक विरोधी हालातों के चलते एक श्रमिक के अमानवीकरण की कहानी लिखने के पीछे, प्रेमचंद की चाहत चाहे कितनी महान रही हो। वे श्रम और श्रमिक विरोधी पूंजीवादी या सामंतवादी व्यवस्था को कटघरे मे खड़ा करने की कोशिश चाहे जितनी भलमनसाहत रखकर किए हों और यह कहानी लिखे हों। लेकिन ग्रामीण समाज के किसी दलित मेहनतकश के जीवन-यथार्थ को अभिव्यक्त नहीं करती है। यह ग्रामीण समाज के दलित मेहनतकशों के जीवन पर एक आरोपित कहानी है। जिसका उनके जीवन-यथार्थ से कोई रिश्ता नहीं।
मूल कथ्य से पहले और बाद में वे क्या और कितनी सूत्रवत और महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। यह कोई मायने नहीं रखता।
(डॉ. सिद्धार्थ लेखक व स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)