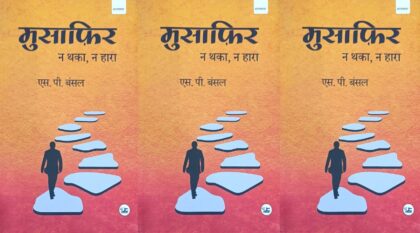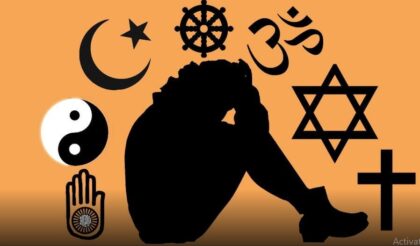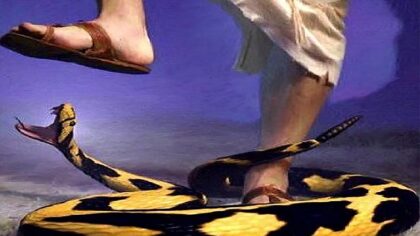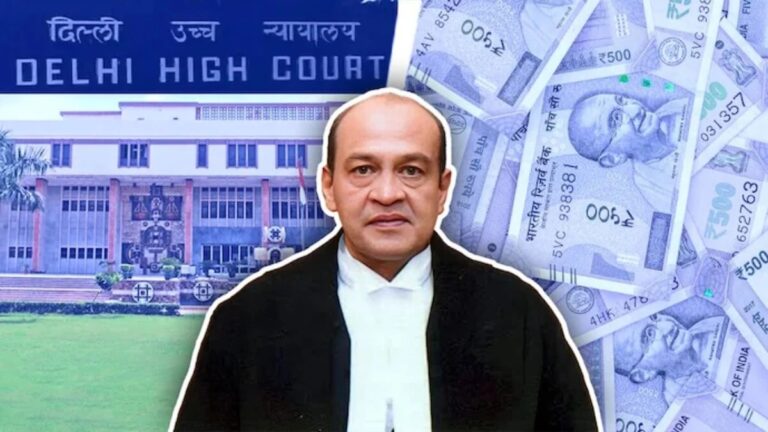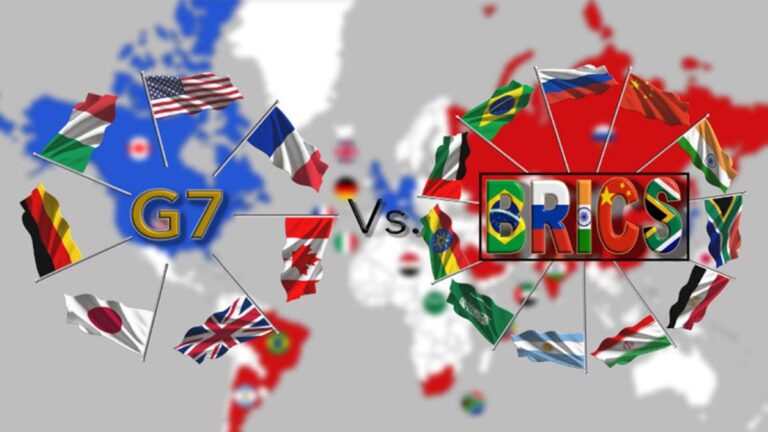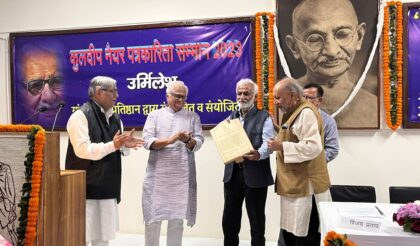श्रीलंका के संसदीय चुनाव में मार्क्सवादी राष्ट्रपति अनूरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाले मोर्चे- नेशनल पीपुल्स पॉवर (एनपीपी) को ऐतिहासिक और अनपेक्षित जीत मिली है। इस मोर्चे में दिसानायके की पार्टी- जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) प्रमुख घटक है। सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जब दिसानायके इसी मोर्चे के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे, तब एनपीपी को लगभग 56 प्रतिशत वोट मिले थे। पौने दो महीने बाद हुए संसदीय चुनाव में एनपीपी को 61.56 फीसदी वोट मिले। 225 सदस्यों के सदन में एनपीपी ने 159 सीटें जीत कर दो तिहाई से ज्यादा बहुमत हासिल किया है।
यह नतीजा अनपेक्षित इसलिए था, क्योंकि संसदीय चुनाव की बिसात बिल्कुल अलग होती है। इसमें मतदाताओं के सामने गिने-चुने विकल्प ही नहीं होते, बल्कि अलग-अलग इलाकों में अनेक पार्टियां होड़ में शामिल रहती हैं। पिछली संसद में एनपीपी के पास सिर्फ तीन सीटें थीं। इसे देखते हुए पहले चर्चा तो यही थी कि क्या एनपीपी को स्पष्ट बहुमत भी मिल पाएगा। ऐसा नहीं होता, तो दिसानायके एक लेम-डक (शक्तिहीन) राष्ट्रपति बन कर रह जाते। दिसानायके ने मतदाताओं से दो तिहाई बहुमत देने की अपील की थी।
दिसानायके का एक प्रमुख वादा देश में संसदीय व्यवस्था वापस लाना है। जेआर जयवर्धने जब राष्ट्रपति थे, तब 1978 में संसदीय व्यवस्था खत्म कर राष्ट्रपति ढंग की शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। इससे संसदीय व्यवस्था में विभिन्नताओं को मिलने वाली नुमाइंदगी की संभावना सीमित हो गई। देश के पूर्वोत्तर इलाकों में तमिल अलगाववाद के उग्र रूप लेने के पीछे जयवर्धने सरकार के इस निर्णय को भी एक कारण माना जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली अपनाए जाने के बाद 1982 में हुए चुनाव से लेकर पिछले चुनाव तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जब तमिल बहुल इलाकों ने उसी पार्टी को चुना हो, जो दक्षिणी एवं अन्य इलाकों में कामयाब हुई। लेकिन 2024 आकर यह ट्रेंड पलट गया है।
एनपीपी को देश के सभी इलाकों में बड़ा समर्थन मिला है। यहां तक कि राजधानी कोलंबो में भी, जो जयवर्धने के दौर से पिछले चुनाव तक यूनाइडेट नेशनल पार्टी (यूएनपी) का गढ़ बना रहा था। एनपीपी को बौद्ध बहुल उन इलाकों में जबरदस्त सफलता मिली है, जहां लंबे समय तक राजपक्षे परिवार के उग्र-राष्ट्रवादी नारे हावी रहे और उनकी पार्टी- श्रीलंका पोडुजुना पेरामुना (एसएलपीपी) विजयी होती रही। एसएलपीपी इस बार सिर्फ तीन सीटें ही हासिल कर पाई है। उसे महज 3.14 प्रतिशत वोट मिले हैं। यही कहानी मुस्लिम बहुल इलाकों की है। उन इलाकों में लंबे समय बाद ऐसा हुआ है, जब मजहबी पहचान वाले दलों के ऊपर मतदाताओं ने एनपीपी को तरजीह दी। श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस तो महज 0.78 फीसदी वोट पा सकी। उसे तीन सीटें मिली हैं।
नस्लीय और मजहबी पहचान की राजनीति से बंटे रहे श्रीलंका में रोजी-रोजी के सवाल के केंद्र में रख कर सामने आए मोर्चे को इस तरह का समर्थन मिलेगा, यह सोचना सचमुच कठिन था। लेकिन ऐसा हुआ है। तो यह समझना जरूरी होता है कि आखिर इन करिश्माई नतीजों के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं?
- अनूरा कुमारा दिसानायके 2022 की विशेष परिस्थिति से तैयार पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति चुने गए। देश में पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के कारण हुए जन विद्रोह के कारण- जिसे अरागलया नाम से जाना गया- तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे को सत्ता छोड़ देश से भागना पड़ा था। उसके बाद शासक वर्गों ने एस्टैबलिशमेंट के विश्वासपात्र रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बना दिया। विक्रमसिंघे ने आर्थिक संकट के प्रभाव से प्रभु वर्ग को अछूता रखते हुए सारा बोझ आम जन पर डालने की नीतियां अपनाईं। उससे उत्पन्न असंतोष का परिणाम क्रांतिकारी इतिहास वाली मार्क्सवादी-लेनिनवादी जेवीपी के नेता का निर्वाचन रहा। जेवीपी बाद में मुख्यधारा राजनीति में आ गई थी।
- दिसानायके ने राष्ट्रपति बनने के बाद लोगों को राहत देने के लिए कई खास कदम उठाए (इस लिंक पर ध्यान दें- खासकर 14 और 15 अक्टूबर को लिए गए निर्णयों परः https://muragala.lk/articles/npp-government-policy-timeline/)।
- श्रीलंका में आम जन की मुसीबत की वजह विक्रमसिंघे सरकार के समय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए मानी गई शर्तें थीं। इनके तहत सरकारी खर्च घटाने के लिए आम जन को मिलने वाली सब्सिडी और जन कल्याण की योजनाओं में कटौती कर दी गई। साथ ही बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण एजेंडे पर था। दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव के समय कहा था कि वे श्रीलंका की आईएमएफ के प्रति सहित तमाम अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं का पालन करेंगे, मगर आम जनता को उसका सारा बोझ उठाने से मुक्ति दिलवाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद आईएमएफ से वार्ता एवं अपने निर्णयों, दोनों से उन्होंने यह ठोस संकेत दिया कि इस वादे को पूरा करने के प्रति वे गंभीर हैं। इससे उनकी साख बढ़ी और यह पहलू संसदीय चुनाव के नतीजों में प्रतिबिंबित हुआ है।
- राष्ट्रपति और संसदीय- दोनों तरह की मिली-जुली व्यवस्था में अनेक फैसलों के लिए संसदीय मंजूरी की जरूरत पड़ती है। एनपीपी श्रीलंका के मतदाताओं को यह संदेश देने में कामयाब रही कि संसद में उसकी मजबूत उपस्थिति नहीं हुई, तो दिसानायके की जीत से जगी उम्मीदें धूल में मिल जाएंगी। इसका लाभ उसे मिला है।
जेवीपी के महासचिव तिल्विन सिल्वा ने संसदीय चुनाव का परिणाम आने के बाद कहा- ‘पहले जिन लोगों के मन में हमारे प्रति संदेह था, (पिछले पौने दो महीनों के अनुभव से) वे भी मानने लगे कि हम देश, इसकी राजनीति संस्कृति, और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध हैं।’
सियासत में साख सबसे बड़ी पूंजी होती है। कहा जा सकता है कि सितंबर में मतदाताओं ने परंपरागत दलों के प्रति विद्रोह की भावना को जताने के लिए दिसानायके को वोट दिया था। मगर इस बार कारण राष्ट्रपति के आरंभिक निर्णयों से एनपीपी की बनी साख है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिसानायके ये साख बरकरार रख पाएंगे। अक्सर देखा गया है कि ऊंची उम्मीदें जगा देने वाले नेता या दल से लोगों का मोहभंग भी उतनी ही जल्दी होता है। क्या दिसानायके सरकार सचमुच यह जन-विश्वास बनाए रख पाएगी कि वह देश, राजनीतिक संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था का पुननिर्माण के प्रति समर्पित है?
इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भविष्य में मिलेगा। बहरहाल, श्रीलंका के जनादेश के जो व्यापक निहितार्थ हैं, वे अभी ही स्पष्ट हैं। लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जिस समय धारणा दुनिया भर के चुनावी लोकतंत्र वाले देशों में धुर-दक्षिणपंथ के उभार की है, उस समय श्रीलंका ने वामपंथ का रास्ता कैसे चुन लिया है? इसे उलटी गंगा के रूप में देखना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
लेकिन विभिन्न ऐसे देशों में दिख रहे राजनीतिक रुझानों पर ध्यान दें, तो इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका और यूरोप तक के अनेक देशों में रुझान यह है कि राजनीति धुर-दक्षिणपंथ एवं विश्वसनीय वामपंथ (credible Left) के बीच बंट रही है। यह मध्यमार्गी राजनीति के प्रति मतदाताओं के विद्रोह का संकेत है। गुजरे चार दशकों में सेंटर लेफ्ट और सेंटर-राइट में बंटी मध्यमार्गी राजनीति विभिन्न प्रकार की अस्मिताओं के मुद्दों में सिमट गई। जबकि रोजी-रोजी के बुनियादी सवालों पर दोनों प्रकार की शक्तियों में आम सहमति बढ़ती चली गई। नतीजा हुआ कि ऐसी पार्टियों से रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान की आशाएं टूट चुकी हैँ। उधर पहचान की राजनीति को पुनर्संगठित कर तथा इसे अधिक उग्र एवं हिंसक रूप में उठा कर धुर दक्षिणपंथ अपने लिए जन समर्थन बढ़ाता चला गया है।
नए सिरे उभरी वामपंथी ताकतों को दबाने के लिए शासक वर्गों ने धुर दक्षिणपंथ को औजार बनाया है। अलग-अलग देशों में जिस अनुपात में विश्वसनीय वामपंथ को दबाने में कामयाबी मिली है, धुर दक्षिणपंथ आज उतनी ही अधिक बड़ी ताकत के रूप में मौजूद दिखता है। लेकिन जहां वामपंथ वैकल्पिक नीति एवं कार्यक्रम पेश कर अपनी विश्वसनीयता बना पाया है, वहां अलग कहानी सामने आई है।
श्रीलंका इस दूसरी परिघटना की मिसाल है। श्रीलंका इस बात की मिसाल है कि लोग धुर दक्षिणपंथ को नहीं अपना रहे, बल्कि वे मध्यमार्ग को ठुकरा रहे हैं। इसके लिए जो उपयुक्त माध्यम उन्हें मिलता है, उसे वे अपना रहे हैं। श्रीलंका में वामपंथ अपने को उपयुक्त माध्यम बना पाया, तो लोगों ने उसे गले लगाया है। वह अपनी विश्वसनीयता कायम रख पाया, तो वह बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा। इस मामले में वह कम-से-कम दक्षिण एशिया को वैचारिक नेतृत्व देने की हैसियत में होगा।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)