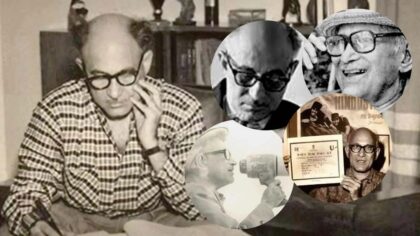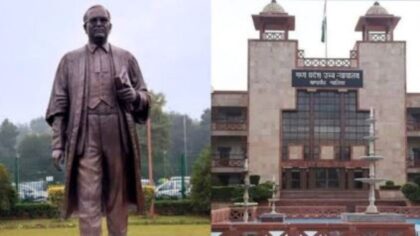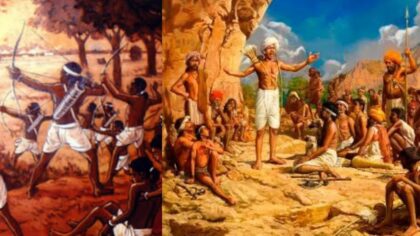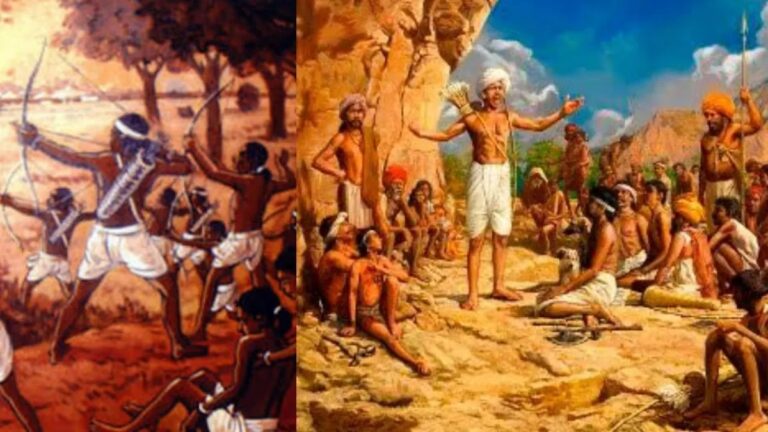अब दुनिया में यह अहसास गहराने लगा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने आर्थिक क्षेत्र में जो अभियान छेड़ा है, उसे टैरिफ वॉर कहना उनके मकसद और उनकी योजना को पूरी तरह व्यक्त नहीं करता। अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर आयात शुल्क शून्य करने की यूरोपियन यूनियन एवं अन्य कई देशों की पेशकश को जिस तरह ट्रंप प्रशासन ने ठुकरा दिया, उससे यह साफ हुआ कि जो शिकंजा अमेरिका ने उछाला है, उसका दायरा बड़ा है।
जिन देशों ने टैरिफ की मार से बचने के लिए अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते की राह पकड़ी, उन्हें भी इसका दो टूक अहसास हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने बातचीत की कार्यसूची में टैरिफ के साथ-साथ अमेरिकी कंपनियों के आगे कथित गैर-टैरिफ रुकावटों, करेंसी मैनुपुलेशन (मुद्रा की कीमत को कृत्रिम रूप से गिराना या बढ़ाना) और अपनी अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए संरक्षण आदि जैसे मुद्दे भी शामिल कर दिए हैं।
मगर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। यहां तक होती तो कहा जाता कि टैरिफ वॉर की आड़ में अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था की अपने माफिक समग्र पुनर्रचना (total restructuring) करना चाहता है। मगर बात इससे भी आगे गई है। वियतनाम भी उन देशों में है, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर मसले को हल करना चाहा। इसके लिए वॉशिंगटन पहुंचे वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल से अमेरिका ने कहा कि उसे अमेरिका या चीन में से किसी एक चुनना होगा।
और अब ऐसी खबरें आम हैं कि जिन लगभग 70 देशों ने अमेरिका से बातचीत की पहल की है, उन सबके सामने ट्रंप प्रशासन चीन से नाता तोड़ने की शर्त लगा रहा है।
तो साफ है, ट्रंप प्रशासन की मंशा सिर्फ विश्व अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना नहीं है। बल्कि वह लगे हाथ भू-राजनीति (geo-politics) को नए सिरे से ढालने में जुटा है। यानी गुजरे दो दशकों में दुनिया पर अमेरिकी प्रभाव घटने, अमेरिका केंद्रित एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंत और अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिम के खिलाफ ग्लोबल साउथ की नई धुरी उभरने की जो हकीकत सामने आई है, ट्रंप एक झटके से उस पूरी परिघटना को पलट देना चाहते हैँ।
मगर यह तभी संभव है, जब ग्लोबल साउथ के देशों को अमेरिका फिर से पर-निर्भर बनाने और उनके भौतिक एवं मानव संसाधनों पर अपना निर्बाध नियंत्रण कायम करने में सफल हो। इसलिए अमेरिकी बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऐसी शर्तें थोपी जा रही हैं, जिनसे ग्लोबल साउथ के देशों की अर्थव्यवस्था में आत्म-निर्भरता के जो भी पहलू निर्मित हुए हैं, वे नष्ट हो जाएं। हमेशा की तरह आंतरिक खाद्य सुरक्षा को समाप्त करना इसमें एक प्रमुख रणनीति है। इसीलिए भारत के सामने बीटीए में ऐसी मांगें अमेरिका ने रखी हैं, जिनसे भारत के कृषि क्षेत्र पर अमेरिकी कंपनियों का पूरा वर्चस्व बन सके।
टैरिफ वॉर से पेश आई चुनौतियों की चर्चा करते समय उपरोक्त पूरे संदर्भ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस भ्रम से निकल जाना चाहिए कि टैरिफ घटाने की पेशकश कर ट्रंप प्रशासन को तुष्ट किया जा सकता है। ट्रंप सभी देशों से पूरा सरेंडर चाहते हैं।
क्या भारत इसके लिए तैयार होगा?
भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मूलभूत कमजोरियां हैं, जिनकी वजह से फिलहाल भारत इस नई चुनौती के आगे एक हद तक लाचार दिखता है। ये कमियां आरंभ से रही हैं, लेकिन 1991 में अमेरिका निर्देशित भूमंडलीकरण को uncritically (बिना गुण-दोष में फर्क किए) गले लगाने के बाद से जड़ें और कमजोर होती गई हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उन्हीं कमियों को गुण बताऩे, कमजोरियों को ताकत बताने और उनके आधार पर बनी गैर-बराबरी की व्यवस्था को उपलब्धि मानने के बने चलन ने असहायता और बढ़ा दी है।
इसके बीच जैसे-तैसे अमेरिका से बात संभाल लेने की कोशिश के अलावा कोई और रास्ता हमारे राजनीतिक नेतृत्व को फिलहाल नजर नहीं आया है। यहां राजनीतिक नेतृत्व से मतलब पूरे political class (यानी सत्ता पक्ष एवं विपक्ष) से है, जिसके कंधों पर भारतीय हितों को परिभाषित करने और उसके अनुरूप रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। यह समूह मोटे तौर पर नव-उदारवादी भूमंडलीकरण की विचारधारा को इतना आत्मसात कर चुका है कि उससे भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी कमजोरियों के मूल्यांकन और उनके समाधान पर सोचने की आशा करना भी कठिन हो गया है।
जबकि आज चर्चा का अपेक्षित मुद्दा बहुत साफ है। महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर क्यों अमेरिका के व्यापार युद्ध की चुनौती को चीन ने स्वीकार किया, जबकि भारत उससे जैसे-तैसे बच निकलने का उपाय ढूंढने में जुट गया? क्यों चीन अमेरिकी दंभ के खोखलेपन को बेनकाब करने की दिशा में बढ़ा है, जबकि अपने यहां इस दंभ का साया सघन मालूम पड़ा है?
चीन से भारत की तुलना का स्वाभाविक आधार रहा है। इसलिए कि दोनों एक जैसी पृष्ठभूमि के देश हैं। दोनों में विशाल आबादी है और दोनों देशों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ कर लगभग एक साथ (भारत ने 1947 और चीन ने 1949) में अपनी विकास यात्रा शुरू की।
इस सिलसिले में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के एक कथन का अक्सर हवाला दिया जाता है। बताया जाता है कि एक निजी चर्चा के दौरान पंडित नेहरू ने कहा था-
“बेशक हमारे (भारत और चीन के) राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचे में अंतर है। लेकिन हमारे सामने जो समस्याएं हैं, वे एक जैसी हैं। यह भविष्य बताएगा कि किस और किसकी शासन-व्यवस्था ने हर क्षेत्र में बेहतर नतीजे हासिल किए।”
इसके पहले- 1950 के दशक के मध्य में दोनों देशों में उच्चस्तरीय संवाद हुए थे। बताया जाता है कि खास कर चीन गए भारतीय दल वहां कृषि ढांचे में लाए गए बदलाव और उससे हासिल परिणामों से खासे प्रभावित हुए। बाद में अमर्त्य सेन जैसे मशहूर अर्थशास्त्री ने भारत और चीन के विकास मॉडल्स के तुलनात्मक अध्ययन में खास दिलचस्पी ली।
अब वे बातें पुरानी हो चुकी हैं। जो पंडित नेहरू के लिए भविष्य था, वह हमारा वर्तमान है। नतीजे अब हमारे सामने हैं। अब यह स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए कि चीन का विकास मॉडल कामयाब रहा, जबकि भारत के मॉडल के बारे में ऐसा कहा जाए, उसके पहले कई अप्रिय तथ्य सामने आ खड़े होते हैं।
भारत आज जहां है, उससे संबंधित एक महत्त्वपूर्ण पहलू वैचारिक रहा है, जो पश्चिम की श्रेष्ठता की कहानी को uncritically आत्मसात कर लेने से उपजा। मगर इस पहलू को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। फिलहाल टैरिफ वॉर के संदर्भ में जरूरत भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरियों पर गौर करने की है। इन कमजोरियों की वजह से ही आज भारत अमेरिकी दंभ के आगे खड़ा होने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहा है। तो आखिर ये कमजोरियां हैं क्या?
- इस सदी में अक्सर भारत के जनसंख्या संबंधी लाभ (demographic dividend) की चर्चा होती रही है। संख्या के लिहाज से भारत की बड़ी आबादी को इसका आधार बताया जाता है। मगर हकीकत क्या है?
- बड़ी आबादी अपने-आप में कोई dividend नहीं होती। मुद्दा यह है कि क्या वह आज के तकनीकी एवं अर्थव्यवस्था संबंधी तकाजों के अनुरूप प्रशिक्षित एवं कुशल है? यहां हकीकत चिंताजनक होती चली गई है। अब तो आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से निकले छात्रों के लिए भी नौकरी का टोटा पड़ने लगा है। इसका कारण वहां पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण का पुराना पड़ता गया ढांचा है।
- स्कूली शिक्षा की अवस्था भी बहुत बेहतर नहीं है। शिक्षा के इस क्षेत्र पर तो आजादी के बाद से उचित ध्यान नहीं दिया गया। अक्षर ज्ञान करा देना शिक्षा नहीं है। आवश्यकता ऐसी बुनियाद डालने की होती है, जिससे आगे चल कर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं गणित शिक्षित नौजवानों का बड़ा नेटवर्क तैयार होता रहे। इस बिंदु पर समग्र स्थिति कभी बेहतर नहीं रही है।
- रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अब पहले भी ज्यादा उपेक्षित होता जा रहा है। ऐसे में जनसंख्या का लाभ मिलने की बातें बहकावा के अलावा कुछ और नहीं रह जातीं।
- उत्पादन के सर्व प्रमुख साधन- भूमि के स्वामित्व संबंधी व्यवस्था में आज तक आमूल परिवर्तन नहीं लाया गया। नतीजतन, भूमि उत्पादन के नियोजन से संभावित लाभ से देश वंचित बना हुआ है।
- उद्योग क्षेत्र में आजादी के बाद के आरंभिक दशकों में अच्छी पहल हुई। इस दिशा में कामयाबियां भी मिलीं। देश का जितना भी उद्योग केंद्रित शहरीकरण हुआ, वह उन्हीं दिनों अपनाई गई नीतियों का परिणाम है। स्टील, मशीन-टूल्स, संचार एवं वैज्ञानिक शोध में सहायक उद्योग तब लगाए गए। मगर 1991 के बाद यह सब ठहर गया। सारा ध्यान निजी क्षेत्र में उपभोक्ता सामग्रियों और सेवाओं के उत्पादन पर केंद्रित हो गया। उससे जैसी अर्थव्यवस्था बन सकती थी, वही आज हमारे सामने है।
- अब यह साबित हो गया है कि बिना नियोजन और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका के कोई अर्थव्यवस्था सशक्त एवं मानव विकास केंद्रित नहीं हो सकती। भारत ने इस दिशा में प्रयोग किए, मगर बीच रास्ते उसे छोड़ दिया गया। जब अर्थव्यवस्था का कोई तय लक्ष्य नहीं हो और उसे धनी लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद की जो कहानी हो सकती है, वह हमारे सामने है।
- किसी अर्थव्यवस्था की सफलता का पैमाना यह है कि उससे मानव विकास की कसौटियों पर कैसे नतीजे हासिल हुए हैं। किसी अर्थव्यवस्था के निर्धारक तत्व हैः स्वास्थ्य देखभाल एवं (quality) शिक्षा की सहज उपलब्धता और रोजगार केंद्रित आर्थिक नियोजन। कम-से-कम पिछले चार दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था इन लक्ष्यों से उलटी दिशा में गई है।
- इसका स्वाभाविक परिणाम है कि घरेलू बाजार का दायरा सीमित बना रहा है। हाल के वर्षों में यह और सिकुड़ता चला गया है। ऐसे में भारत की जितनी भी उत्पादक अर्थव्यवस्था है, उसके लिए निर्यात जीवन-मरण का प्रश्न बना हुआ है। इसीलिए अमेरिकी बाजार भारत के लिए इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसमें बनी जगह को बचाए रखना आज पूरे राजनीतिक वर्ग और अर्थ जगत की सर्वोच्च प्राथमिकता नजर आती है। इस मकसद से विभिन्न क्षेत्रों के बुनियादी हितों और देश के आत्म-सम्मान पर समझौते के लिए भी ये तबके तैयार नजर आए हैं।
मगर ट्रंप प्रशासन से द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना आसान नहीं है। इन दिनों अक्सर मीडिया ऐसी सुर्खियां बनती (या बनवाई) जाती हैं कि इस वर्ष के अंत तक यह समझौता हो जाएगा। मगर यूरोपियन यूनियन से मिल रहे संकेतों पर गौर किया जाए, तो यह एक कठिन लक्ष्य मालूम पड़ता है। प्रश्न यह है कि क्या भारत भू-आर्थिकी और भू-राजनीति को अपने माफिक ढालने की अमेरिकी परियोजना में सहायक बनेगा? और क्या इसके लिए रूस जैसे देश से पारस्परिक लाभ के अपने पारंपरिक संबंधों तथा ब्रिक्स या ग्लोबल साउथ के साथी देशों से अपने पुराने संबंधों की बलि चढ़ाने को तैयार होगा?
यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि ऐसा करने की कोई मजबूरी भारत के सामने नहीं है। तमाम कमजोरियों के बावजूद भारत के पास बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। टैरिफ वॉर के दौरान दिखे संकेतों से ही यह साफ है कि दुनिया में अपनी शर्तों पर और आत्म- सम्मान के साथ सिर्फ वे देश खड़े हो सकते हैं, जिनके पास अपनी राष्ट्रीय शक्ति हो। राष्ट्रीय शक्ति फूल-फल रही अर्थव्यवस्था, माकूल सैनिक तैयारी और वैचारिक सॉफ्ट पॉवर के मेल से बनती है। आज भारत इन बिंदुओं पर मध्यम दर्जे की शक्ति नज़र आता है। मगर ये कमजोरी स्थायी नहीं है, बशर्ते इसे स्वीकार कर नए सिरे से राष्ट्र निर्माण की परियोजना शुरू की जाए।
घरेलू अर्थव्यवस्था का मानव विकास केंद्रित निर्माण इस परियोजना का पहला पहलू होगा। अनुभव यह है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ उपलब्ध होने वाले संसाधन खुद ही सशक्त सैनिक तैयारी की जमीन निर्मित कर देते हैं। सॉफ्ट पॉवर किन्हीं उच्चतर मूल्यों के लिए विश्व मंच पर खड़े होने से बनता है। हाल के वर्षों में अमेरिका या पश्चिम ने अपना सबसे बड़ा नुकसान ऐसे उसूलों का नुमाइंदा होने की अपनी छवि को नष्ट करते हुए किया है। इससे विश्व स्तर पर एक शून्यता पैदा हुई है, चीन जिसे एक दूसरे कोण से भरने की कोशिश कर रहा है।
इस बीच भारत में ‘आपदा में अवसर’ का सरकार प्रायोजित नैरेटिव फिर सुर्खियों में दिखने लगा है। मगर जो कहानी जो बताई जा रही है, वह अन्य देशों पर अधिक टैरिफ लगने से भारत के लिए कथित अवसर पैदा होने से संबंधित है। कहा जा सकता है कि यह एक फर्जी कहानी है। जबकि भारत के सामने टैरिफ वॉर की ‘आपदा’ सचमुच एक अवसर लेकर आई है। लेकिन उस अवसर को यथार्थ में बदलने के लिए अर्थव्यवस्था को नए सिरे से ढालने का श्रमसाध्य रास्ता अपनाना होगा। दुर्भाग्य यह है कि आज ऐसा होने की संभावना नजर नहीं आती। इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा यह सोच है कि जो विचार या उपाय पश्चिम से नहीं आए हों, उन्हें साकार किया ही नहीं जा सकता!
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)