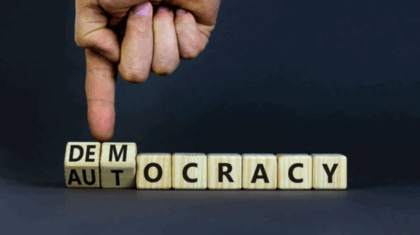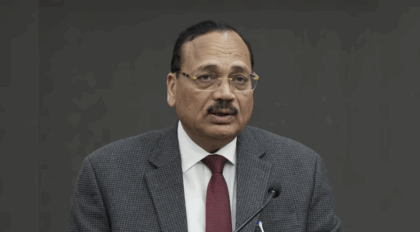लूणकरणसर, राजस्थान। तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, पर गांव की रसोई में महिला अब भी उसी जगह ठहरी हुई हैं, जहां हर सुबह धुंए से भरा चूल्हा उनका इंतज़ार कर रहा होता है। लकड़ी, गोबर और सूखे पत्तों से जलता यह चूल्हा सिर्फ उनका वक़्त ही नहीं बल्कि उसकी सांसें, आंख और शरीर के हिस्सों को भी धीरे-धीरे बीमार करता रहता है।
यह केवल एक रसोई की तस्वीर नहीं है, बल्कि पितृसत्ता के उस ढांचे की झलक होती है, जो महिलाओं को सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकारी मानता ही नहीं है। यह स्थिति देश के किसी एक गांव की नहीं होती है, बल्कि बिहार से लेकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और बर्फीले क्षेत्र जम्मू कश्मीर से लेकर रेगिस्तानी इलाका राजस्थान तक एक समान तस्वीर देखने को मिल जाएगी।
राजस्थान के बीकानेर स्थित लूणकरणसर ब्लॉक से 19 किमी दूर राजपुरा हुड्डान गांव भी यही तस्वीर पेश करता है। करीब 3200 की आबादी वाले इस गांव की कई महिलाएं अब भी खाना बनाने के लिए मीलों चलकर लकड़ियां बटोरती हैं। अक्सर उनके साथ घर की किशोरियां भी होती हैं। जो स्कूल जाकर अपना समय पढ़ाई या किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकती थीं, उसे वह सिर्फ इसलिए गंवा रही हैं क्योंकि समाज मान बैठा है कि “खाना बनाना तो घर की औरतों और लड़कियों का काम है।
हालांकि 2016 में केंद्र सरकार की शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने इस गांव के बहुत से घरों की महिलाओं के खाना बनाने के काम को आसान ज़रूर किया है, लेकिन फिर भी उनके कदम रसोई घर से बाहर नहीं निकल सके हैं। यह महिलाएं अब इसी बात पर संतोष कर लेती हैं कि उन्हें आज धुंए वाले चूल्हे से आज़ादी मिली है, एक दिन चारदीवारी से भी मिल जाएगी।
चालीस वर्षीय जमना देवी कहती हैं कि जब से घर में गैस सिलेंडर आया है, जीवन बहुत हद तक आसान हो गई है। पहले मिट्टी के चूल्हे पर 7 लोगों का खाना बनाना पड़ता था। दोपहर की तपती धूप में धुंए के बीच खाना बनाने से तबीयत ख़राब हो जाती थी। लेकिन उसी हालत में हमें चूल्हा फूंकना पड़ता था। अब सिलेंडर आ जाने से कम से कम उस नरक से छुटकारा तो मिला।
कुछ ऐसी ही ख़ुशी 11वीं में पढ़ने वाली गुड्डी को भी है। जिसे पिछले तीन सालों से अब लकड़ियां चुनने के लिए मां बाहर नहीं भेजती है। वह कहती है कि अब इस बचे हुए समय का उपयोग वह घर के अन्य कामों को निपटाने के लिए करती है ताकि उसे पढ़ने का पूरा समय मिल सके। यानी पढ़ने से पहले उसे भी रसोई और अन्य कामों को करना पड़ता है। लेकिन इस काम से उसके भाइयों को आज़ादी मिली हुई है।
लेकिन गांव के कुछ घर ऐसे भी हैं जहां की महिलाओं के हिस्से में अभी भी धुंए वाले चूल्हे लिखे हुए हैं। किसी के पास आज तक सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका है तो कोई उसे आपातकाल के लिए संभालकर रखती हैं, और रोज़ की ज़रूरत के लिए फिर उसी धुंए भरे चूल्हे पर लौट जाती हैं।
32 वर्षीय संतोष देवी कहती हैं कि हमारा परिवार बड़ा है। एक सिलेंडर मुश्किल से 15 दिन चल पाता है। जिसे दोबारा भरवाने में पैसे लगते हैं। इसीलिए हम इसे बहुत ज़रूरी होने पर ही खर्च करते हैं। अधिकतर समय इन्हीं चूल्हे के धुंए के बीच समय गुज़रता है।
कालो देवी कहती हैं कि हमें आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। चूल्हा जलाने के लिए हमें तपते रेगिस्तान में लकड़ियां चुनने के लिए दूर-दूर तक चलना पड़ता है। कालो देवी की पड़ोसन विमला कहती हैं कि हमने उज्ज्वला का नाम सुना है, लेकिन हमें आज तक यह नहीं पता है कि इसके लिए कहां आवेदन देना होगा? कई बार हमने प्रयास किया कि हमारे परिवार को भी इसका लाभ मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हमारी ज़िंदगी तो धुंए के बीच बीत गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को यह सुविधा मिल जाए।
एक अध्ययन के अनुसार 2016 में राजस्थान में COPD (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) से मृत्यु दर देश में सबसे अधिक थी, और श्वसन रोगों से होने वाली मौतें दूसरे स्थान पर थीं। 1990 में, राजस्थान में श्वसन रोगों से कुल मौतों में से 3.4% COPD के कारण थीं, जो 2016 में बढ़कर 7% हो गईं। वहीं जोधपुर, राजस्थान में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 43.1% महिलाएं मुख्य रूप से बायोमास ईंधन का उपयोग करती हैं, जबकि केवल 19.7% महिलाएं ही पूरी तरह से एलपीजी पर निर्भर हैं।
बायोमास उपयोगकर्ताओं के घरों में PM-2.5 स्तर एलपीजी उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक पाया गया। एक अन्य अध्ययन में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास ईंधन का उपयोग करने वाली महिलाओं में श्वसन लक्षणों की व्यापकता अधिक पाई गई है। ऐसे ईंधन के उपयोग से जुड़े घरों में महिलाओं को आंखों में जलन, सिरदर्द, और फेफड़ों की कार्यक्षमता में गिरावट जैसी समस्याएं अधिक होती हैं।
यह सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, यह एक ऐसी सामाजिक चुप्पी की बात है, जो सदियों से रूढ़िवादी सोच को ढ़ोते हुए यह मान चुकी है कि औरत की तकलीफ़ उसके कर्तव्यों का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कैसा कर्तव्य है जो किसी के स्वास्थ्य को निगल जाए? दरअसल, रसोई महज़ एक खाना पकाने की जगह नहीं है, यह एक ऐसी जगह है, जहां रोज़ एक स्त्री खुद को धुएं में जलाती है। गर्मी हो या बारिश, बीमारी हो या थकान, उसे रुकने की इजाज़त नहीं है।
यह एक ऐसी गलत परंपरा है, जो पितृसत्तात्मक समाज द्वारा पीढ़ियों से महिलाओं को ज़बरदस्ती ढोने पर मजबूर किया जाता है। यह वह चक्र है, जो उसके जन्म होने से शुरू होता है और बुढ़ापे तक चलता है। जिसे अक्सर समाज अनदेखा कर देता है। वह कभी इन बातों को महसूस ही नहीं कर पाता है कि एक महिला को भी वह सभी सुविधाएं और अधिकार पाने का हक़ है, जिसे समाज केवल पुरुष का अधिकार समझता है।
इसके लिए पहले उसे अपने नज़रिये को बदलना होगा। उस सोच से बाहर निकलना होगा जो महिलाओं को किचन और चारदीवारी तक सीमित रखने की तर्कहीन वकालत करता है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक और सुविधा पर सबसे पहला अधिकार उसी का है जो सबसे ज्यादा श्रम करते हैं। अगर सोलर चूल्हों या बायोगैस संयंत्रों को सही मायनों में घर-घर तक पहुंचाया जाए, तो हर घर को धुंए वाले चूल्हों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इसके साथ-साथ समाज को भी उस सोच से मुक्त होने की ज़रूरत है जो महिलाओं के अधिकारों को रसोई घर तक बांध कर रखना चाहता है।

(लूणकरणसर से प्रमिला की रिपोर्ट)