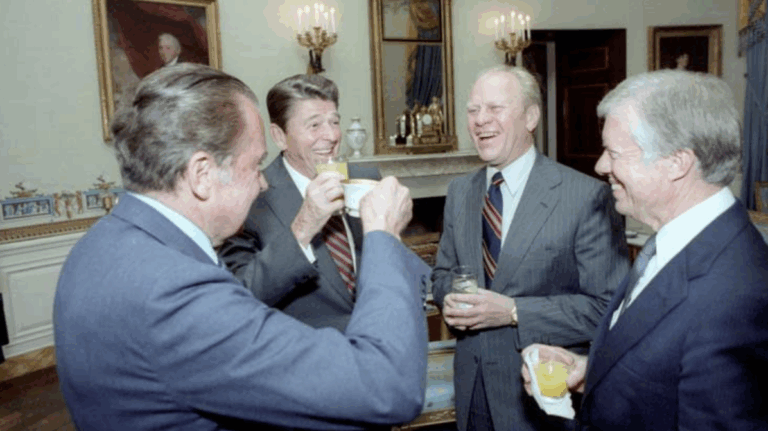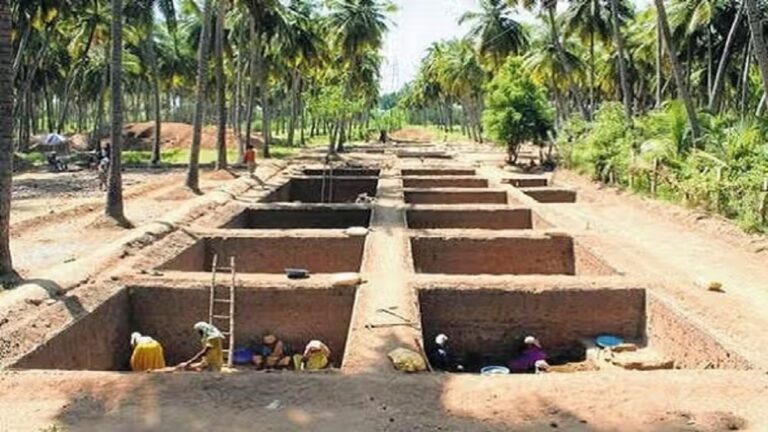अमेरिका के राष्ट्रपति आजकल यहूदी समुदाय के संरक्षक और अमेरिकी हितों के राष्ट्रीय हीरो बनने वाले भाषण दे रहे हैं। वे खुद को एक कठोर शासक के रूप में पेश कर रहे हैं, जो असहमतियों को राष्ट्रीय हित से आगे नहीं जाने देने की कसम खा रहे हैं। दरअसल, वे कुछ और नहीं, इतिहास के उन पन्नों में खुद को उतारना चाहते हैं, जो 1950 के पहले दशकों में खुले थे। उनकी समानता इतिहास के उन क्रूर शासकों से की जा सकती है, जिनका अब वर्तमान दौर चल रहा है।
भाजपा के चिंतक समूहों में गिने जाने वाले राम माधव इसे उदारवाद की राष्ट्रीय धारा की पुनर्स्थापना मानते हैं। इनकी चिंता सिर्फ इतनी है कि इस धारा के शासक उचित तरीके से सामंजस्य बनाकर नहीं चल रहे हैं। इस संदर्भ में इतना जरूर कहा जा सकता है कि विश्व की हिंसक आकांक्षाएं जन्म ले चुकी हैं, संभवतः ट्रंप इसे दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें दुनिया की चिंता है, वे इसे जरूर पागलपन बता रहे हैं।
ट्रंप ने टैरिफ युद्ध की शुरुआत कथित तौर पर अमेरिका में रह रहे ‘अवैध प्रवासियों’ को उनके देश वापस भेजने से की। उन्होंने भारत पर सबसे घिनौना प्रयोग किया और भारतीय प्रवासियों को हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजना शुरू किया। इतिहास का यह अपमानजनक क्षण भारत के राष्ट्रवादियों के लिए कोई सबक नहीं बना। वे औरंगजेब की कब्र पर भिड़े हुए थे और राणा सांगा के अपमान पर हाथ में तलवार लिए सड़कों पर क्रुद्ध होकर नाच रहे थे।
ऐसा लगता है कि भारत का राष्ट्रवाद इतिहास में सबसे पीछे चलने के लिए अभिशप्त है। लेकिन, यह अभिशाप उन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जो भारत को इतिहास निर्माण में सबसे अग्रिम मोर्चे पर रखने और भारतीय जनता को हर तरह की प्रताड़नाओं से मुक्त कराने के आग्रहों से लबरेज हैं। इनके हिस्से मौत की इबारत लिखना आज भी जारी है।
उदारवादी राष्ट्रवादियों को उभार जिस सांस्कृतिक चेतना की मांग करता है, उसकी जमीन हमेशा हाशिए पर फेंक दिए गए लोगों की आकांक्षाओं को लगातार भड़काए रखने और मुख्यधारा में बने रहने वाले लोगों को अनुशासित जीवन जीने के प्रवचनों और व्यवस्थाओं से बनती है। इसमें शासक वर्ग हमेशा खुद को संरक्षक और शासक को देवत्व से भरे इतिहास को खंगालने और भविष्य को देखने की दृष्टि का अक्सर प्रदर्शन करता रहता है।
इस प्रक्रिया में वह समाज के एक बड़े हिस्से का इतिहासबोध और जीवन की चाह को दीमक की तरह चाटकर खोखला बना देता है और उन्हें दृष्टिबोध के लिए अपने ऊपर निर्भर बना देता है। हालांकि यह सब कुछ बहुत छोटे दायरे में होता है, लेकिन प्रचारतंत्र इसे डरावने स्तर तक बड़ा बना देता है। ऐसे में, समाज का पूरा उत्पादक वर्ग, खासकर मजदूर और निम्न-मध्यवर्ग, हताशा का शिकार हो जाता है और छात्र-युवा वर्ग निराशा में डूबने लगता है।
लेकिन, आधुनिक राज्यों की अवधारणाओं में मजदूर वर्ग एक निर्णायक तत्व है। इसके बिना कोई भी राज्य न तो आधुनिक होने का दावा कर सकता है और न ही अस्तित्व में बना रह सकता है। पूंजी का निर्माण, आयात और निर्यात, चाहे जितना भी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, शेयर बाजारों से चले, वह अंततः उत्पादन के उन मानदंडों पर ही नापा जाता है, जिनके केंद्र में श्रम और उसकी उत्पादकता निर्धारित की जाती है। मुद्राएं भी इससे बाहर नहीं हैं। और, यह कोई मार्क्सवादी अवधारणा भी नहीं है। यह घोर उदारवादी आर्थिक चिंतन है। मार्क्स की आर्थिक चिंतनधारा इससे आगे की बात है। उदारवादी इन आर्थिक व्यवस्थाओं को बार-बार खींचकर राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं।
पिछले दस से बारह सालों से देश की केंद्रीय अर्थव्यवस्था को कथित गुजरात मॉडल पर विकसित करने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें कई प्रयोग किए गए। सड़कों की विशाल परियोजनाएं, नदियों को विकसित करना, आधुनिक शहरों का निर्माण और मेक इन इंडिया अर्थात स्टार्टअप को आगे ले जाना। इसके लिए पर्यावरण के नियमों को दरकिनार किया गया, जमीनों के अधिग्रहण की बेलगाम छूट दी गई, विरोध की आवाजों का दमन किया गया और मजदूरों के अधिकारों की भयावह कटौती की गई। समानांतर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिशें जारी रहीं, जिसमें विपक्ष की भूमिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल भी न रह जाए। लेकिन, बात नहीं बनी।
भारतीय उद्योगपतियों की इस बीच दो मांगें स्पष्ट रूप से सामने आईं-पहली, कुशल मजदूरों की कमी और दूसरी, काम के घंटों को बढ़ाया जाए। जहां तक दूसरी मांग की बात है, भारत के मजदूरों को लेकर आई अधिकांश रिपोर्टों में उनकी मांग के बराबर काम मजदूर कर रहे थे। पहली मांग ने एक पेचीदा स्थिति पैदा कर दी।
भाजपा की वर्तमान सरकार से पहले मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के समय में भी कुशल मजदूरों की मांग थी, लेकिन उस समय भारत न सिर्फ तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि रोजगार की स्थिति भी आज से बेहतर थी।
ऐसे में यह सवाल बनता है कि उस सरकार के जाने और इस नई सरकार के आने के बाद भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था के बीच कौन से वे कारण आ गए, जिनमें भारत के कुशल मजदूरों की संख्या इतनी तेजी से घट गई। भाजपा सरकार के समय दो ही वे क्षण आए, जिनमें अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। पहला, नोटबंदी और दूसरा, कोविड महामारी। नोटबंदी ने पूंजी की उपलब्धता को बाजार से बाहर कर दिया और सरकार के उस कठोर नियंत्रण में ले गई, जहां नीतिगत फैसले अराजकता से भरे हुए लगते हैं।
दूसरा, कोविड महामारी में भारत के मजदूरों का शहरों से पलायन और खेती पर दबाव और संकट। इसमें यदि हम तीसरा पक्ष जोड़ना चाहें, तो उसमें पेट्रोल की कीमत को जोड़ सकते हैं, जिसने सरकार की आय को स्थिर बनाए रखने और भारत के छोटे पूंजीपति वर्ग को पूंजी निर्माण में बने रहने का अवसर दिया।
फरवरी, 2025 में जारी किए गए आर्थिक सर्वे 2024-25 के आंकड़े दिखाते हैं कि महामारी के ठीक पहले मजदूरों की जो आय थी, महामारी के समय गिरी, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं दिख रही है। इसमें भी जो नियमित आय वाले मजदूर समूह हैं, उनकी आय लगभग स्थिर दिखती है, जबकि स्वरोजगार करने वालों की आय में थोड़ी वृद्धि देखी जा सकती है। यह वास्तविक आय के संदर्भ में आंकड़े हैं।
नियमित आय 2017-18 में 12,665 रुपये थी, जो 2023-24 में 11,858 रुपये रह गई। स्वरोजगार जैसी शब्दावली किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा सूचकांक नहीं है, और यह तब और भी नहीं है, जब नियमित रोजगार समूहों की आय घट रही हो। उपरोक्त सर्वे में अन्य देशों की तुलना में भारत के मजदूरों के काम के घंटों की तुलना करते हुए इसे दुरुस्त करने की सलाह दी गई है। इस दौरान कुशल मजदूरों को लेकर काफी बात हुई।
मार्च, 2025 के मध्य में बहुप्रचारित पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ आंकड़े और बयान दिए। एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने वाली इस योजना को 500 कंपनियों तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया था। इसके पहले दौर में कुल 1.27 लाख अवसर सृजित किए गए थे, जिनमें से 82,000 को लिया गया। इस योजना में, इंटर्नशिप का खर्च का मुख्य हिस्सा सरकार वहन करने का वादा किया है।
दूसरे दौर में 1.18 लाख पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में सरकार एक साल के लिए एकमुश्त 6,000 रुपये, प्रतिमाह 4,500 रुपये और कंपनी के सीएसआर से 500 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में वास्तविक आंकड़ों के आने में समय लगेगा, लेकिन 2025-26 के लिए कुल खर्च का जो अनुमान था, उसमें काफी बड़ी कटौती कर दी गई है।
यही हाल एआई से प्रशिक्षण का है। जब चीन से लेकर अमेरिका एआई की दुनिया में अपनी पकड़ बनाने की लड़ाई में एक-दूसरे से भिड़ गए, उस समय भारत के अर्थशास्त्री और नीति-निर्माता इस बात को लेकर रो रहे थे कि भारत का मजदूर वर्ग एआई के सामने बेहद कमजोर है। भारत के मध्यवर्ग की चिंता इससे कहीं अलग है। वह भारत की राजनीतिक व्यवस्था में फैली अराजकता और बढ़ती तानाशाही के बीच इतिहास और भूगोल की तलाश में लगा है और अमेरिकी व चीनी एआई ऐप से अपने संकट का जवाब ढूंढ रहा है।
जबकि भारत की सरकारी प्राथमिक शिक्षा संस्थानों के बंद होने/करने की संख्या लाख का आंकड़ा छू रही है। मेडिकल संस्थानों से लेकर विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों के अभाव ने पूरी शिक्षण प्रणाली को ही ध्वस्त कर दिया है। आईआईटी जैसे संस्थान युवाओं की आत्महत्याओं के केंद्र बन रहे हैं, जबकि कोचिंग संस्थान एक समानांतर शिक्षण संस्थानों में बदल गए हैं। यहां तक कि यूट्यूबर्स आधुनिक तकनीकी शिक्षा के उभरते संस्थानों में तब्दील हो रहे हैं।
भारत में रोजगार के परिदृश्य पर ‘पकौड़े छानने’ की अवधारणा देने वाले प्रधानमंत्री आज जब गरीब मुस्लिम युवाओं को ‘पंचर बनाने’ के रोजगार का कारण वक्फ की जमीनों पर डाल देते हैं, तब आप भारत की अर्थव्यवस्था में किसी दिशा की क्या ही उम्मीद करेंगे? जिस देश का पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवादियों के उत्पादों की दुकानदारी करना ही अपना मुख्य काम करता हो, वहां के राजनीतिक नेतृत्व से इससे अधिक क्या ही उम्मीद हो सकती है। लेकिन, निश्चित ही भारत का मजदूर वर्ग एक भयावह दौर से गुजर रहा है। मध्यवर्ग का एक हिस्सा बदलाव की उम्मीद कर रहा है, वह वर्तमान की सच्चाइयों से छटपटा रहा है। वह हताश होकर एआई के विभिन्न ऐप से पूछ रहा है: फासीवाद क्या है?
ऐप अपने हिसाब से उसे व्याख्या दे रहा है। पूछने वाला अपने सिद्धांत से मेल कराकर संतुष्ट है कि उसका विश्लेषण ठीक है, यह देश उसी तरफ जा रहा है। हालांकि, पिछले दस सालों में विधायिकाओं से पास किए गए बिल, कानून, आदेश और निर्णय आदि के आंकड़े उपलब्ध हैं और उनकी समीक्षाएं भी सामने हैं। उनके आंकड़ों का विश्लेषण बेहद आसानी से बता सकता है कि इस समय भारत में कौन-सी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है।
इसे एआई से पूछने से अधिक जरूरी है, विश्लेषण से सच्चाई तक पहुंचने की पद्धति को स्वीकारना। यह विडंबना ही है कि चीन और अमेरिका जैसे देशों में एआई का प्रयोग इंजीनियरिंग, मेडिकल और वित्तीय संस्थानों की संरचना में बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है, जबकि भारत में यह खेल-खिलौने की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा फेक वीडियो निर्माण और चित्रकला की दुनिया में कुछ नए प्रयोग करने में दिख रहा है।
यहां मार्क्सवाद की उन मूलभूत बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पूंजीवाद उत्पादन के क्षेत्र में जितनी अनुशासित व्यवस्था दिखती है, बाजार की दुनिया में वह उतनी ही अराजक होती है। जब बाजार के हालात बिगड़ जाएं, तब राजनीति अपने लोकतंत्र का लबादा उतारकर फेंकने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोकतंत्र का यह लबादा सभी फेंकने लगते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्ग करता है। वह चाहता है कि बाजार के युद्ध में और भी लोग उसके साथ आएं। इसके लिए वह सबसे पहले मजदूर और किसान वर्ग को राज्य का अभिन्न हिस्सा होने का अहसास कराता है। इसमें सबसे अग्रिम मोर्चे पर किसान होता है और दूसरे नंबर पर निम्न पूंजीपति वर्ग।
अंत में आता है मजदूर वर्ग। मध्यवर्ग के पास इतना अवसर रहता है कि वह इस पूरे परिदृश्य को घटित होते हुए देख सके और समय आने पर अपना रुख तय कर सके। वह सबसे लंबे समय तक चुप रहता है। भारत का किसान और मजदूर वर्ग विभाजन की विभीषिका से लेकर अब तक लगातार पलायन का शिकार रहा है। उसकी जातीय पहचान हमेशा ही खंडित होती रही है। उसके लिए जीने की जद्दोजहद ही मुख्य चुनौती रही है।
भारत के मजदूर वर्ग की वह मूल प्रकृति है, जिस पर राष्ट्रवाद की बेहद कम छाया है। संभवतः इन्हीं कारणों से भारत की वर्तमान राजनीतिक अर्थशास्त्र में इसे सबसे निम्न स्तर पर रखा गया है। नेतृत्व के अभाव में इसकी भूमिका आने वाले समय में और भी बदतर होने का अभिशाप झेलती हुई दिख रही है। आज सबसे जरूरी है, मजदूर वर्ग को रेखांकित करने वाली नीतियों और नियमों पर बात करना और उनके हालात को बयान करना।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं)