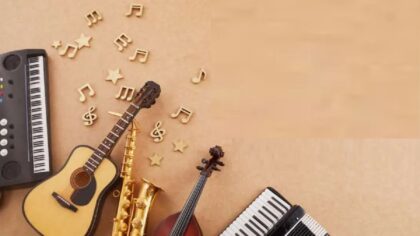सामने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के चुनाव हैं। चुनाव में विकास भी मुद्दों की सूची में शामिल रहता है। विकास जरूरी है। जरूरी है विकास में भागीदारी। जरूरी है बढ़ती हुई विषमताओं पर लगाम कसना। विकास के आंकड़ों के मोहक वन में रमनेवालों से अधिक खतरनाक भटकानेवाले होते हैं। आर्थिक विकास के साथ आर्थिक विषमता के संबंध के विश्लेषण से निष्पत्तिमूलक निष्कर्ष यह निकले कि विकास और विषमता में किसी तरह का ‘कारण-कार्य’ संबंध है, तो फिर नये सिरे से विकास की अवधारणा पर विचार किया जाना जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि विकास और विषमता का ‘कारण-कार्य’ संबंध आर्थिक कारोबार की स्व-चालित प्रक्रियाओं का स्वाभाविक परिणाम है या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप से यह संबंध बनता है।
उदार लोकतंत्र की पैरवी करनेवालों की दृढ़ मान्यता थी कि आर्थिक कारोबार के मामले में सरकार को कम-से-कम हस्तक्षेप करना चाहिए। (Minimum Government – Maximum Governance) ‘न्यूनतम सरकार – अधिकतम सेवा’ के आकर्षक पदबंध अंतर्गत लोकतंत्र को नये सिरे से परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव का मूल आशय क्या था और प्रभाव किस रूप में सामने आया! किस की सरकार, किस की सेवा! जनता की सरकार, बाजार की सेवा!
न्यूनतम सरकार का सीधा मतलब था, आर्थिक कारोबार में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। आर्थिक कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कानूनी रुकावटों को ज्यादा-से-ज्यादा समाप्त करना, यानी अधिकतम सेवा! यह सब लोकतंत्र की मूल प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह से बाजारवाद का अधीनस्थ बनाने के लिए किया गया। जाहिर है कि आर्थिक कारोबार में पिछड़े हुए या आर्थिक कारोबार से बाहर खड़े लोगों को या तो तेजी से अपनी हर गतिविधि को ‘आर्थिक कारोबार’ में बदलना जरूरी था या फिर पिछड़ते हुए चले जाने की नियति को स्वीकार करना था।
यह आश्वासन दिया गया कि बाजार में प्रतियोगिता का लाभ आम लोगों को मिलेगा। प्रतियोगिता स्वस्थ और सही हो इस के लिए जरूरी होता है किसी भी कीमत पर कारोबार में एकाधिकार बनने नहीं दिया जाये। भारत में इस की देखभाल के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का गठन किया गया। लाभ! लाभ सब के सामने है।
राजनीति और लोकतांत्रिक सत्ता पर एकाधिकार बनाने के लिए बेझिझक गलत-सही तौर-तरीका अपनानेवाली सर्वसत्तावादी राजनीति की सक्रियता के सामने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) कर ही क्या सकती है। आर्थिक कारोबार के नियमन और एकाधिकार के बनने को रोकने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कोई बड़ी कारगर पहल देखने में नहीं आई है।
यानी आर्थिक कारोबारियों को संघर्ष का समान अवसर (Level Playing Field) प्रदान कर उपभोक्ताओं के अनुकूल बाजार को बनाने या बनाये रखने में कोई सार्थक भूमिका निभाई हो, ऐसा नहीं दिखता है। राजनीतिक दलों के लिए विभिन्न चुनावों में संघर्ष का समान अवसर (Level Playing Field) प्रदान करने में भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) की भूमिका भी स्तरीय और सराहनीय नहीं दिखती है।
ऐसी स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) मुद्रा नियमन की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई नियंत्रण में सफल नहीं हो पाती है, तो इसे क्या कहा जा सकता है। कुल मिलाकर यह कि न सीसीआई, न ईसीआई और न ही आरबीआई ठीक से काम कर पा रही है। कोई भी ‘आई’ तब तक ठीक से काम नहीं कर सकती है, जब तक ‘जीओआई’ ‘गवमेंट ऑफ इंडिया’ ठीक से काम नहीं करती है। अर्थात लोकतांत्रिक सरकार के ठीक से काम करने के लक्षण संस्थाओं के ठीक से काम करने में दिखता है।
ऐसे में ‘पिछड़े’ हुए का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का सहारा देनेवाला कौन है, आम आदमी जिसकी राह तके! असहाय आदमी अपना पिचका सीना पीटते हुए ‘हाय-हाय’ करे या फिर हर जगह हुजूर के ‘छप्पन इंच’ सीना का ‘गुण-गान’ करे! किसे संविधान और लोकतंत्र की मूल प्रतिज्ञाओं का ध्यान दिलाये! कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बोलने की मंशा के पीछे अपनी पार्टी को हिंदुओं की पार्टी मनवाने के अलावा और कुछ नहीं होता है।
हिंदू-मुसलमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सही विकास का अवसर खो दिया। इतना बड़ा बहुमत मिला था, लेकिन क्या हुआ? इस बात पर गर्व करना लाजिमी है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। कार्य-काल का उल्लेख करते हुए सिर्फ ‘काल’ का ही क्यों ‘कार्य’ का भी तुलनात्मक आकलन किया जाना चाहिए। चाहिए ही नहीं, निश्चित ही किया भी जायेगा। सरकार के सरोकार के खो जाने को लोकतंत्र की सब से बड़ी राजनीतिक दुर्घटना के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।
ऐसे में गरीबी पर कौन सोचे! लेकिन सोचना तो होगा ही। सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को दूर करने और सार्वजनिक समृद्धि को सुनिश्चित करने की ओर देश को ले जाने में विफलता लोकतंत्र की निष्फलता की ही कहानी होती है। आर्थिक प्रगति का तब तक कोई बहुत बड़ा सामाजिक मतलब नहीं होता है जब तक सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने में आर्थिक प्रगति कोई बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में पहल नहीं करती है।
बहुत हो-हल्ला है कि भारत दुनिया की पांचवीं अर्थ व्यवस्था बन गई है। राजनीतिक विमर्श और प्रवक्ताओं की वाणी के अलावा लोगों के जीवन-स्तर में कहीं भी भारत की पांचवीं अर्थ व्यवस्था बन जाने का कोई प्रगतिकारक असर नहीं दिखता है। कई ‘बुद्धिजीवियों’ की तो यह भी मान्यता है कि लोकतंत्र का होना आर्थिक प्रगति में बाधक ही होता है। लोकतंत्र को आर्थिक प्रगति का विरोधी माननेवालों के हाथ में लोकतंत्र की शक्ति का केंद्रित हो जाना, जनता के लोकतांत्रिक लक्ष्य को राजनीतिक कूड़ेदान के हवाले कर देने के अलावा और क्या हो सकता है!
लोकतंत्र का मूल आशय है नागरिकों को सामाजिक अवसरों की समानता उपलब्ध करवाना और आर्थिक प्रगति का निष्पक्ष माहौल बनाना। लोकतंत्र के इस आशय से जुड़ने के लिए भी एक तरह की बुनियादी और न्यूनतम सामाजिक और आर्थिक हैसियत की भी जरूरत होती है। दुखद है कि अधिकतर लोगों की हैसियत इस न्यूनतम बुनियादी शर्त को पूरी नहीं करती है। साफ-साफ यह बात समझी जा सकती है कि बहुत बड़ी आबादी की परम गरीबी लोकतंत्र की अनुकूलता को बार-बार खंडित करती है। ‘मतदान’ का अधिकार जनता की राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी का प्राथमिक साक्षी तो हो सकता है, प्रमाण नहीं हो सकता है।
परम गरीबी, सापेक्षिक गरीबी आदि की सिद्धांतकी अपनी जगह लेकिन यह सच है कि भारत में परम गरीबी की स्थिति बहुत भयावह है। दुश्चक्र यह कि लोकतंत्र के बिना परम गरीबी दूर नहीं की जा सकती है और परम गरीबी के रहते सार्थक ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। ऐसे में परम गरीबी में जी रहे लोगों इन के लिए इस लोकतंत्र का कोई सार्थक मतलब नहीं बनता है। फैली हुई हथेली के दैन्य से लोकतंत्र कमजोर होता है और कमजोर लोकतंत्र स्वाभिमान की मुट्ठी को तनने नहीं देता है। ऐसी है यह ट्रेजडी नीच!
ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत की आर्थिक लूट मची रही। इसी लूट का नतीजा 1857 था। 1857 से लेकर 1947, यानी 90 साल भारत में बेरोक-टोक लूट-खसोट जारी रही। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में गरीबी को भारत का सब से बड़े सवाल के रूप में रेखांकित किया थ। आजादी मिलने के पहले से ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा गांधी सामाजिक समानता, आर्थिक प्रगति में अवसरों की समानता आदि के प्रति गंभीर थे। अपने-अपने तौर-तरीका से इस के लिए संघर्षशील थे।
भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान बाबासाहेब की उपस्थिति आंदोलन की न्याय-बुद्धि थी, तो महात्मा गांधी की उपस्थिति नैतिक-अंकुश का काम करती थी। आजादी मिलने के बाद इन दोनों का साथ छूट गया। कहना न होगा कि इस से आजाद भारत के शासन में धीरे-धीरे न्याय-बुद्धि और नैतिक-अंकुश का प्रभाव कम होता गया। बाहरी प्रेरणा के माध्यम से नैतिकता की उपयोगिता को समझाना मुश्किल होता है।
सामाजिक-राजनीतिक वातावरण में उपलब्ध और सक्रिय नैतिक चेतना को व्यक्ति अपनी प्रेरणा से आयातित और आत्मसात ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। जिस समाज में यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है या फिर रुक ही जाती है उस समाज की नैतिक धुरी ही टूट जाती है। जब समाज की ही नैतिक धुरी टूट जाये तो उस समाज की राजनीतिक प्रणाली, चाहे वह लोकतांत्रिक ही क्यों न हो, की नैतिक धुरी के टूटने में बहुत देर नहीं लगती है।
आजादी प्राप्त होने के ठीक पहले 1943 में पड़े भयावह अकाल से भारत की अर्थ व्यवस्था तहस-नहस हो गई थी। 4 साल पहले आज़ादी मिलने से ठीक पहले 1943 के बंगाल के भयावह अकाल से देश के अर्थव्यवस्था का ढांचा ही चरमरा गया था। आरंभिक कोशिशों के साथ स्थिति में धीमी रफ्तार सुधार जोर पकड़ ही रहा था कि भारत को युद्ध में घसिटा गया। इस बीच 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का और 11 जनवरी 1966 को लालबहादुर शास्त्री का निधन हो गया।
इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं। भारत की स्थिति यह थी कि वह वियतनाम युद्ध के संदर्भ में अमरीकी विदेश नीति की आलोचना भी करता रहा और मदद की भी गुहार करता रहा। हालत इतनी खराब थी कि 6 जून 1966 को इंदिरा गांधी को डॉलर के मुकाबला में भारत की मुद्रा का भारी अवमूल्यन करना पड़ गया। इंदिरा गांधी की समाजवादी पहल के चलते राजनीतिक घटना चक्र ऐसा घूमा कि कामराज ने 12 नवम्बर 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से सरकार तो बच गई लेकिन बहुमत की ताकत जरूर कम हो गई थी।
प्रिवी पर्स को समाप्त करने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे समाजवादी पहल से असहमत और परेशान कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया तो उन्होंने कांग्रेस (आई) का गठन कर लिया। ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के साथ कांग्रेस (आई) चुनावी राजनीति में अपनी पार्टी को असली कांग्रेस साबित करने में कामयाब रही। राजनीतिक उठा-पटक खूब हुई। इंदिरा गांधी ने समाजवाद की अपनी परिभाषा सामने रखी कि विकास करने का समान अवसर होना चाहिए और राष्ट्रीय संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। इंदिरा गांधी का समाजवाद यही था और इसी लक्ष्य को वे जल्द-से-से-जल्द हासिल करना चाहती थी।
इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों और उठा-पटक के बीच 26 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल घोषित हुई। इस इमरजेंसी के दौरान जबरदस्त राजनीतिक ज्यादतियां हुईं। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। जनता पार्टी की सरकार बहुत दिन नहीं चल पाई और इस बीच, 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में फिर से जबरदस्त वापसी हो गई। गरीबी हटाओ के नारे पर भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाली इंदिरा एक बार फिर ‘आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे’ के नारा के साथ सत्ता में आ गई। 31 अक्तूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इस के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजनीतिक उठा-पटक जारी रही। संचार क्रांति और इक्कीसवीं सदी के भारत का सपना देखने-दिखानेवाले राजीव गांधी भी सत्ता से बाहर हुए। इस बीच कई प्रधानमंत्री आये-गये।
चुनावी सभा के माहौल में 21 मई 1991 को राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। फिर पीवी नरसिम्हा राव, अटल विहारी बाजपेयी, डॉ मनमोहन सिंह का दौर आया और ‘अच्छे दिन’ के नारे के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की ‘अकेले दम’ सरकार चली और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
विडंबना यह कि राम मंदिर के जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चमकी थी, राम मंदिर बनने के बाद उस की चमक कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चमक में भले ही कमी आ गई हो उस के औद्धत्य में कहीं कोई कमी नहीं आई है। उस की विचारधारा का मिजाज ही लोकतांत्रिक नहीं है। वह जिन सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं को अमल में लाना की कोशिश में लगी हुई है, उस में एक भिन्न तरह की राजनीति की बात है। वह भिन्न तरह की बात लोकतंत्र की किताब के किसी अध्याय में नहीं है।
बातें और भी हैं। किस्से और भी हैं। मूल बात यह है कि तमाम तरह की राजनीतिक उठा-पटक होती रही लेकिन गरीबी नहीं मिटी। गरीबी की कई परिभाषाएं जरूर उभरी-मिटी लेकिन गरीबी नहीं मिटी। इंदिरा गांधी की समाजवाद की जो अवधारणा थी, अर्थात विकास का समान अवसर और राष्ट्रीय संसाधनों का समान वितरण, उसे राहुल गांधी ने कांग्रेस की सामाजिक न्याय की समकालीन अवधारणा से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। सच पूछा जाये तो इसी से कांग्रेस में नई चमक पैदा हुई है।
इंदिरा गांधी के जमाने से दुनिया आगे निकल गई है। अब उदार लोकतंत्र का जमाना आ गया है। दुनिया के नक्शे पर भिन्न स्थिति उभर आई है। दुनिया भर के शासकों और सरकारों में सरोकारों की भारी कमी आई है। विकास के चरित्र में भी मौलिक फर्क आ गया है। विकास के किसी मॉडल में विषमता-रोधी तत्व या युक्ति नहीं है।
राजनीति में हत्या और संगठित अपराध का बोलबाला खतरनाक ढंग से बढ़ा है। संचार तंत्र में गुणात्मक परिवर्तन आ गया है। मीडिया का चरित्र भी पहले जैसा नहीं है। बावजूद इस के विकास का समान अवसर और राष्ट्रीय संसाधनों का समान वितरण का राजनीतिक और सामाजिक दायित्व की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक आज है। दोहराव की कीमत पर भी कहना जरूरी है कि परम गरीबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही समाप्त हो सकती है और परम गरीबी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का माहौल बनना मुश्किल होता है। फैली हुई हथेली के दैन्य से लोकतंत्र कमजोर होता है और कमजोर लोकतंत्र लोकतांत्रिक स्वाभिमान की मुट्ठी को तनने नहीं देता है।
लड़ाई बाहर भी है, भीतर भी है। सवाल यह नहीं है कि गद्दी पर कौन बैठेगा, सवाल यह है कि गद्दी के सामने तनकर कौन खड़ा होगा! होगा। कोई-न-कोई जरूर होगा। इतिहास में ऐसे भी दौर आते हैं जिस दौर में आग के बीच में फूल के खिलने का मौसम बनकर लोग प्रकट होते हैं।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)