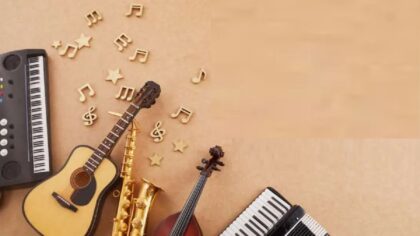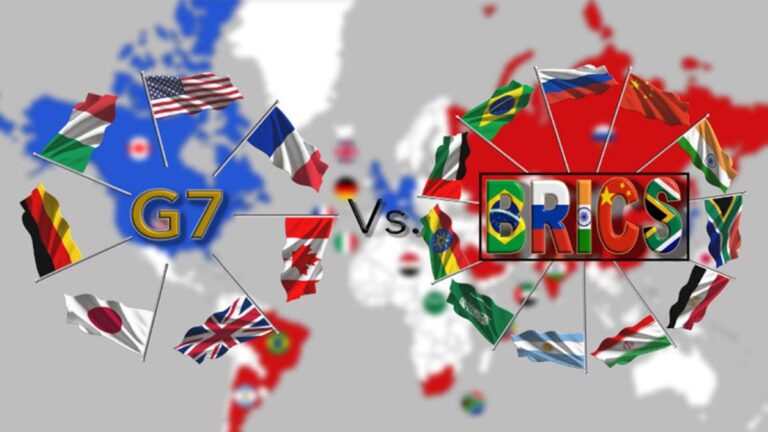पांच वर्ष बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की बैठक इस हफ्ते बीजिंग में हुई। हालांकि इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण सहमतियां बनीं, लेकिन यह भी साफ हुआ कि संबंध सुधारने के मुद्दे पर अभी भी दोनों देश एक धरातल पर नहीं हैं।
इसकी सबसे अहम मिसाल यही है कि अजित डोभाल और वांग यी की बीजिंग वार्ता के बाद कोई साझा विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। इसके विपरीत दोनों देशों ने अलग-अलग वक्तव्य जारी किए।
अलग वक्तव्यों में भी फर्क दिखा। जहां चीन की विज्ञप्ति में विस्तार से उन छह सूत्रों का जिक्र किया गया, जिन पर डोभाल-वांग वार्ता में सहमति बनी, वहीं भारत की विज्ञप्ति बारीकियों में जाने के बजाय मोटी बातों तक सीमित रही।
भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि दोनों देशों ने सामान्य संबंध बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ने का इरादा जताया है। सीमा पर आमने-सामने तैनाती की स्थिति से अपने सुरक्षा बलों को हटाने के लिए 21 अक्टूबर को हुए समझौते को लागू करने का संकल्प भारत और चीन ने दोहराया।
भारतीय बयान में उल्लेख किया गया कि 21 अक्टूबर के समझौते के तहत “प्रासंगिक इलाकों” में अब गश्त लगाई जा रही है तथा चरवाहे अपने पशुओं को ले जा पा रहे हैं।
इक्कीस अक्टूबर को रूस के शहर कजान में उपरोक्त समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से औपचारिक वार्ता हुई थी। उसके बाद वहीं डोभाल और वांग के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों को आमने-सामने तैनाती की स्थिति से वापस हटाने का फैसला हुआ था।
(भारतीय और चीनी दल ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन में भाग लेने कजान गया था।) उसी प्रक्रिया की अगली कड़ी के रूप में डोभाल बीजिंग गए। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगले साल वांग यी नई दिल्ली आएंगे।
भारत की तरफ से यह जानकारी भी दी गई, जिसकी रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया में प्रमुखता से हुई, कि तिब्बत के रास्ते मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। चीन की विज्ञप्ति में भी कहा गया कि भारतीय तीर्थयात्रियों की “शिजियांग” यात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा।
चीन में तिब्बत को शिजियांग कहा जाता है। भारतीय मीडिया में इस पहलू के खास जिक्र का जो मतलब है, उसे आसानी से समझा जा सकता है। चूंकि पिछले दस साल के दौरान भारतीय विदेश नीति प्रमुखतः सत्ताधारी पार्टी की घरेलू सियासी जरूरतों से प्रेरित रही है, इसलिए इस बिंदु के जरिए मतदाताओं के लक्ष्य वर्ग को सटीक पैगाम भेज दिया गया है।
चीनी विज्ञप्ति में जो छह सूत्र शामिल हैं, उनमें सबसे अहम दूसरा बिंदु है। इसमें कहा गया- ‘दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे का उचित, तार्किक और दोनों देशों को स्वीकार्य एकमुश्त समाधान ढूंढने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह समाधान दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 2005 में तय राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धातों के अनुरूप निकाला जाएगा।’
इस तरह 2005 में सीमा विवाद हल करने के तय हुए पैमानों को पुनर्जीवित कर दिया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ के निर्देशन में वे पैमाने तय हुए थे।
पैमाने क्या हैं, इस बारे में तो दोनों देशों ने कभी सार्वजनिक जानकारी नहीं दी, लेकिन इस बारे में मीडिया में सूत्रों के हवाले से कुछ सूचनाएं सामने आई थीं। उनके मुताबिक सीमा विवाद का एकमुश्त हल निकाला जाएगा, जिसका उल्लेख ताजा चीनी विज्ञप्ति में भी है।
एकमुश्त हल का अर्थ है कि पूरब यानी अरुणाचल और पश्चिम यानी लद्दाख- दोनों तरफ विवाद का समाधान एक पैकेज के रूप में होगा। हर ऐसा समझौता लेन-देन पर आधारित होता है। उस लिहाज से तब यह अनुमान लगाया गया था कि चीन चाहता है कि लद्दाख की तरफ उसका जो दावा है, उसे भारत स्वीकार कर ले।
पूरब की तरफ भारत का जो दावा है, संभवतः उसे चीन मान लेगा। बताया जाता है कि 1959 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई जब सीमा विवाद हल करने का चीनी फॉर्मूला लेकर नई दिल्ली आए थे, तो उसमें भी ऐसा संकेत दिया गया था। उस फॉर्मूले को जवाहर लाल नेहरू सरकार ने ठुकरा दिया था।
अब बहुत से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2019 में अक्साई चिन को भारत का हिस्सा बताते हुए जब नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, तो 2020 में जमीनी तौर पर आगे बढ़ते हुए चीन ने 1959 के दावे के मुताबिक व्यावहारिक कब्जा जमा लिया।
उनमें से सिर्फ देपसांग और देमचौक में चीनी सेना वापस लौटी है, हालांकि यह वापसी भी सशर्त हुई है। बाकी बिंदुओं पर बफर जोन बनाए गए हैं। इन रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये सारे बफर जोन उन क्षेत्रों में बने हैं, जिन पर अप्रैल 2020 तक भारत का नियंत्रण था।
अगर इस बात में कोई सच्चाई है, तो कहा जा सकता है कि लद्दाख सेक्टर में चीन ने अपने दावे पर 80 से 90 फीसदी तक अमल कर लिया है। चूंकि भारत सरकार उस इलाके में किसी नए चीनी कब्जे का खंडन करती रही है, तो जाहिर है कि (अगर वहां 2020 में चीन ने कोई अतिक्रमण किया) वहां कोई जमीन चीन से वापस मिलने का अब सवाल ही नहीं है।
इस रूप में सवाल उठेगा कि क्या चीन ने सीमा विवाद के आधे यानी पश्चिमी हिस्से को अपने दावे के मुताबिक हल करने लेने की पृष्ठभूमि बना ली है?
यह विवादास्पद सवाल है, क्योंकि अभी संसद के शीतकालीन सत्र में भी विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दोहराया कि नरेंद्र मोदी सरकार के शासन काल में भारत ने चीन के हाथों कोई जमीन भी नहीं गंवाई है।
बहरहाल, यह निर्विवाद है कि भारत और चीन के बीच बेहतर रिश्ते बनना दोनों देशों और उनकी जनता के हित में है। इस लिहाज से कजान से शुरू हुई प्रक्रिया का आगे बढ़ना राहत की बात है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत-चीन संबंध ना सुधरें, इसके लिए प्रयास करने वाली रसूखदार निहित स्वार्थी ताकतें मौजूद हैं।
इसे समझने के लिए एक मिसाल काफी होगी। 18 दिसंबर को डोभाल- वांग वार्ता होनी थी। उसी सुबह एक भारतीय अखबार में ये लीड खबर छापी गई कि चीन डोकलाम इलाके में भूटान की जमीन पर गांव बसा लिए हैं।
जबकि 2023 में भूटान के तत्कालीन लोताय शेरिंग ने दो टूक कहा था कि जिन इलाकों में ये गांव बसाए गए हैं, वो भूटान की सीमा के अंदर नहीं हैं। यानी गांव चीन ने सीमा पार अपने इलाके में बनाए हैं।
इसी तरह उसी रोज अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ- यानी अपनी जमीन पर 2020 में तैनात फौजी बल को वापस नहीं बुलाया है। सवाल है कि ये बात किसने कही है कि चीन ने ऐसा कर लिया है? समझौता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने-सामने तैनात बलों की वापसी का हुआ है- इसका नहीं कि सीमा के अपने क्षेत्र से दोनों देश सारे बल वापस कर लेंगे।
तो साफ है कि दुनिया की एक बड़ी ताकत-और उसके लॉबिस्ट्स भारत-चीन संबंधों में सुधार की हर कोशिश में अड़चन डालने को तैयार बैठे हैं। इस पृष्ठभूमि में बीजिंग वार्ता एक सकारात्मक घटनाक्रम मानी जाएगी। आशा है, ये सिलसिला अगले वर्ष नई दिल्ली में और फिर उसके बाद भी आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा होने में ही दोनों देशों के दो अरब 80 करोड़ लोगों का हित है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)