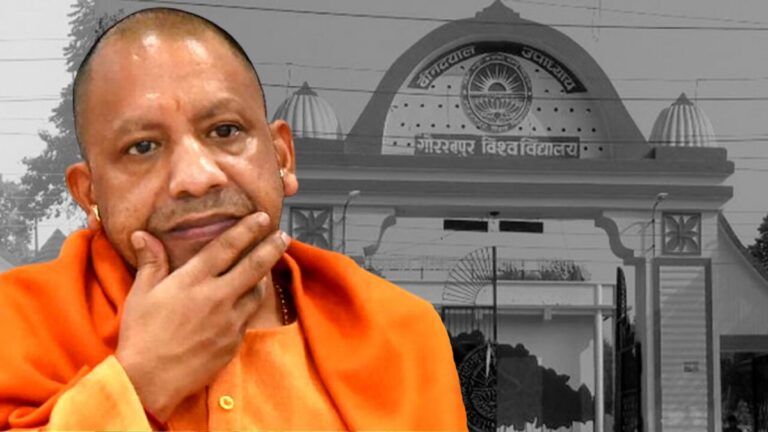नई दिल्ली। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन, भाषा-संस्कृति और पहचान पर अतिक्रमण जारी है। 2006 में वनाधिकार कानून बनने के बावजूद राज्य सरकारें आदिवासी गांवों में उसे लागू करने की पहल नहीं कर रही हैं। जबकि इस बात के पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य हैं कि वनाधिकार कानून (एफआरए) एक गेम-चेंजर है। जिन क्षेत्रों में वनाधिकार कानून लागू हुआ वहां वनोपज से आदिवासी समृद्ध हो रहे हैं।
महाराष्ट्र के यवतमाल में मिश्रित आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी वाले छह गांवों ने वर्षों के संघर्ष के बाद हाल ही में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार जीते हैं। उन्होंने इस गर्मी में सामूहिक रूप से तेंदू पत्तों की कटाई और नीलामी से 56 लाख रुपये अर्जित किया। लगभग एक हजार ग्रामीणों ने 17 दिनों के श्रम से 32 लाख रुपये कमाया। संपूर्ण लाभ में प्रति व्यक्ति औसतन 30-32,000 रुपये देने के बाद शेष राशि को छह ग्राम सभाओं ने अपने विकास कोष के लिए रख लिय़ा। इस धन से गांवों में सामूहिक कार्य होगा। पहली बार, इन ग्रामीणों को आगामी कृषि सीज़न से पहले कच्चा माल खरीदने के लिए निजी ऋणदाताओं से पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ख़रीफ़ सीज़न की तैयारी के लिए उनके हाथ में पर्याप्त नकदी थी।
इन गांवों को अब अन्य लघु वनोपजों से भी साल भर अधिक आय प्राप्त होगी। लेकिन वित्तीय लाभ से अधिक, इन गांवों ने अब सामूहिक ज्ञान और स्थानीय स्व-शासन के एक सर्वसम्मत मॉडल को संचालित करने का तरीका सीख लिया है। विडंबना यह है कि आदिवासियों ने स्थानीय स्वाशासन का यह तरीका ऐसे समय में ईजाद किया है जब भारतीय राजनीति भटक कर अधिनायकवाद की तरफ उन्मुख हो रही है। राष्ट्रीय स्तर यह उस आर्थिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जो वनाधिकार अधिनियम उन गांवों में ला सकता है जिन्हें उनके पारंपरिक रूप से संरक्षित वनों का अधिकार प्राप्त है।
सवाल यह है कि राज्य सरकारें भारत भर के हजारों गांवों के सीएफआर को स्वीकार करने की पहल क्यों नहीं कर रही हैं? भारतीय संसद द्वारा पारित सबसे प्रगतिशील कानूनों में से दो, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के 25 वर्ष और एफआरए के 15 वर्ष से अधिक हो गए हैं। फिर भी, औपनिवेशिक मानसिकता वाले नौकरशाह उनके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
नागरिक समाज समूहों का एक अनुमान कहता है कि एफआरए ने अपनी कुल क्षमता का केवल 15 प्रतिशत ही हासिल किया है क्योंकि सरकारें और प्रशासन क्षेत्र में अपना दखल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। विकेंद्रीकरण तभी परिवर्तन ला सकता है जब लोगों को वह शक्ति हासिल हो, जो राज्य उन्हें देने का वादा करते हैं।
महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल, समृद्ध जैव विविधता वाले घने जंगलों वाले जिलों में से एक, गढ़चिरोली के आर्थिक रूप से पिछड़े कई आदिवासी गांवों ने राज्य के कड़े प्रतिरोध के बावजूद पिछले 15 वर्षों में कड़ा संघर्ष कर सीएफआर हासिल किया। यह यात्रा उत्तरी गढ़चिरौली के एक छोटे से गांव मेंधा लेखा से शुरू हुई, जिसने 40 वर्षों तक युद्ध के नारे, “मावा नाते मावा राज (मेरा गांव, मेरा शासन)” के साथ संघर्ष किया। यह स्थानीय स्वशासन का एक ज्वलंत उदाहरण है।
जिन गांवों ने अपने जंगलों पर अधिकार हासिल कर लिया है, वे एक ऐसे आर्थिक परिवर्तन की पटकथा लिख रहे हैं जो कोई भी सरकारी कार्यक्रम या अनुदान उनके लिए कभी नहीं ला सका। दस साल पहले, इनमें से कई गांवों ने अपना सीएफआर हासिल कर लिया और लघु वन उपज- तेंदू, बांस, सब्जियां, फल आदि को सही तरीके से बेचना शुरू किया। उन्होंने उपज की नीलामी के लिए प्रक्रियाएं और मिसालें तैयार कीं। जब एफआरए प्रभावी नहीं था तब ग्रामीणों ने न केवल दिहाड़ी मजदूरों की तुलना में बेहतर आजीविका अर्जित की, बल्कि ग्राम परिषदों ने अपने स्वयं के विकास के लिए धन भी जुटाया। यहां तक कि दूरदराज के गांवों में भी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन देखा गया है जिसे अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है।
महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ भी इस मॉडल को अपना रहा है। लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के तहत लाने का विचार किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि आजीविका के विकल्प खुल गए हैं, शोषण कम हो गया है या बंद हो गया है और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है।
2014 के बाद जन-अधिकारों से संबंधित संवैधानिक नीतियों में बदलाव ने आदिवासी-मूलनिवासी समुदाय के अधिकारों पर हमला कर दिया है। अब पूंजीपरस्त नीतियों ने आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को समाप्त कर इसके स्थान में कॉरपोरेट हित को स्थापित कर दिया है।
पांचवी अनुसूची, पेसा कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जैसे सभी कानून अब कागजों में तो हैं, लेकिन इसे प्रभावहीन कर दिया जा रहा है। लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन से आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से पूंजीपतियों के कब्जे में जा रही है। रातों-रात जमीन रिकॉर्ड पर असली जमीन मालिक का नाम बदलकर दूसरे का नाम दर्ज हो रहा है।
दुनिया भर में 5 हजार से अधिक तरह के आदिवासी हैं। भारत में आदिवासियों की लगभग 461 जातियां निवास करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप आदिवासियों-मूलनिवासियों का सबसे पुराना निवास स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 10.45 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब यह आंकड़ा 14 करोड़ पार कर चुका है।
देश के अधिकांश राज्यों में आदिवासी-मूलनिवासियों की आबादी है। केंद्र सरकार ने आदिवासियों की आबादी को देखते हुए 593 अधिसूचित आदिवासी जिले घोषित किया हैं। भील जनजाति की जनसंख्या भारत में सबसे बड़ी है। गोंड जनजाति भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड, भील, संथाल, उरांव, मिनस, बोडो और मुंडा, सभी की आबादी कम से कम दस लाख है।
वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे।
(प्रदीप सिंह जनचौक के राजनीतिक संपादक हैं।)