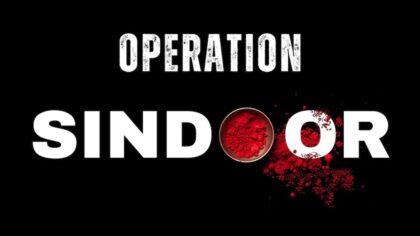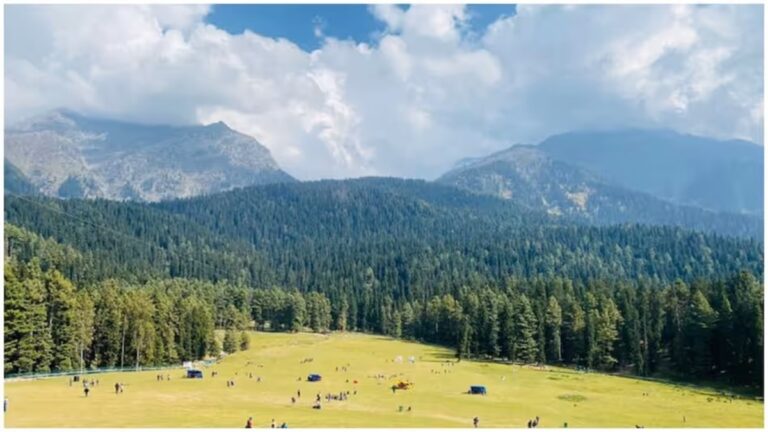उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद हिमालय की गोद में जन्मा उत्तराखण्ड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस नए राज्य में जितनी भी सरकारें आईं, सभी ने प्रगति की बुलंदियों तक पहुँचाने का दावा किया। वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य-अर्थात् सबसे प्रगतिशील, विकसित और रामराज्य के समतुल्य-बनाने की बात कही गई थी। लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 जो कहानी बयान कर रही है, वह राज्य की अब तक की सरकारों के दावों के बिल्कुल विपरीत है। अर्थ स्पष्ट है: यदि कानून का राज कमजोर हो, लोगों को न्याय न मिले और उनकी जान-माल की सुरक्षा न हो, तो ऐसी सरकारों के होने का औचित्य क्या है?
साल 2000 में जब उत्तराखण्ड को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला, तो यह केवल भौगोलिक या प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था। यह उन आंदोलनकारियों की सामूहिक चेतना की जीत थी, जो अपने लिए न्यायपूर्ण, संवेदनशील और उत्तरदायी शासन की माँग कर रहे थे। राज्य निर्माण का सपना केवल सड़कों, पुलों और भवनों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मूल उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जो आम जन को सुलभ और समयबद्ध न्याय प्रदान करे। लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 में उत्तराखण्ड की स्थिति देखकर यह सवाल उठता है: क्या राज्य गठन का वह सपना वास्तव में साकार हुआ?
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 के अनुसार, उत्तराखण्ड 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में 16वें स्थान पर है। यह आँकड़ा अपने आप में एक चेतावनी है। यह रिपोर्ट चार प्रमुख स्तंभों-पुलिस, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता-पर आधारित है, और इनके विश्लेषण से उत्तराखण्ड की न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आती है।
पुलिस व्यवस्था
इस स्तंभ में उत्तराखण्ड को 6.11 स्कोर के साथ 5वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। यह एकमात्र क्षेत्र है, जहाँ राज्य की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। पुलिस बल में नियुक्तियों में सुधार देखा गया है, लेकिन संसाधनों की कमी, विविधता का अभाव और न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस की भागीदारी की पारदर्शिता अब भी अपर्याप्त है। कई पुलिस थानों में पीड़ितों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, और कई बार पीड़ित को ही संदिग्ध बना दिया जाता है।
न्यायपालिका
न्यायपालिका के मामले में उत्तराखण्ड का स्थान 18 में से 16वाँ है, और इसका स्कोर 3.97 है। राज्य में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या आज भी राष्ट्रीय औसत से कम है। विधि आयोग की 1987 की सिफारिशों के अनुसार, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन उत्तराखण्ड में यह संख्या मुश्किल से 15 के आसपास है। न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे फैसले वर्षों तक लटके रहते हैं। विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के लोग इस विलंब से सबसे अधिक पीड़ित हैं। रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ कि उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी केवल 13 प्रतिशत है, जो लैंगिक न्याय के लिए गंभीर चुनौती है।
जेल व्यवस्था
जेल व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इस स्तंभ में उत्तराखण्ड को 2.58 स्कोर के साथ 18वाँ स्थान, अर्थात् सबसे निचला स्थान, प्राप्त हुआ है। राज्य की जेलें औसतन 183 प्रतिशत क्षमता से भरी हुई हैं, यानी जेलों में क्षमता से लगभग दोगुने कैदी रखे गए हैं। इनमें से 76 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं, जिन पर अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी वे वर्षों से फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि गरीब और प्रभावहीन व्यक्ति न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलता और विलंब का सबसे बड़ा शिकार बनता है। कई बंदियों को मामूली अपराधों के लिए वर्षों तक कैद में रहना पड़ता है, केवल इसलिए कि उनके पास जमानत के लिए धन या कानूनी जानकारी नहीं है।
कानूनी सहायता
कानूनी सहायता के क्षेत्र में उत्तराखण्ड ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य को 6.69 स्कोर के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। लोक अदालतें, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और मोबाइल कानूनी सहायता केंद्र सक्रिय हैं, लेकिन इनकी पहुँच और गुणवत्ता में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। कई दूरस्थ इलाकों में लोगों को यह भी नहीं पता कि वे मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं।
थीम आधारित श्रेणियाँ
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 की थीम आधारित श्रेणियों में उत्तराखण्ड का प्रदर्शन और भी निराशाजनक है। ‘रुझान’ में राज्य अंतिम, यानी 18वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि विगत वर्षों में कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ। ‘मानव संसाधन’ में उत्तराखण्ड को 14वाँ स्थान और ‘विविधता’ में 7वाँ स्थान मिला है, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक ढाँचे में सामाजिक और लैंगिक समावेश की कमी है।
इस समूचे परिदृश्य में सबसे पीड़ादायक तथ्य यह है कि जिन आदर्शों और सपनों के आधार पर उत्तराखण्ड की स्थापना हुई थी, वही अब सबसे अधिक उपेक्षित हैं। राज्य गठन का मुख्य उद्देश्य था-‘‘पहाड़ के लोगों को न्याय, अवसर और भागीदारी का अधिकार देना’’। लेकिन वर्तमान न्याय व्यवस्था में ये तीनों तत्व अनुपस्थित दिखते हैं। यह विडंबना है कि 25 वर्षों बाद भी राज्य में गरीबों के लिए न्याय दुर्लभ है। तकनीकी युग में, जहाँ डिजिटल कोर्ट और ई-गवर्नेंस की बातें हो रही हैं, वहाँ उत्तराखण्ड जैसे राज्य में न्यायिक नियुक्तियाँ अधूरी हैं, अदालतों का बुनियादी ढाँचा कमजोर है, और पीड़ित को ‘न्याय’ के लिए वर्षों इंतज़ार करना पड़ता है।
राज्य सरकारें अक्सर न्याय व्यवस्था को केवल “केंद्रीय विषय” मानकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रही हैं, लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यह साबित करती है कि राज्य सरकार की भूमिका-चाहे वह न्यायाधीशों की नियुक्तियों की अनुशंसा हो, अधीनस्थ अदालतों का बुनियादी ढाँचा हो, या पुलिस और जेल प्रशासन का प्रशिक्षण हो-निर्णायक होती है।
यह रिपोर्ट केवल आँकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। यह एक ऐसा आईना है, जिसमें उत्तराखण्ड को अपनी व्यवस्था का असली चेहरा पहचानना चाहिए। राज्य को न्यायिक सुधार को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि थानों, जेलों और समाज में भी होना चाहिए। इसके लिए एक दीर्घकालिक, समन्वित और पारदर्शी रणनीति की आवश्यकता है, जो न्याय को केवल किताबों में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में साकार करे।
उत्तराखण्ड ने 25 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया होगा, लेकिन यदि आम नागरिक को न्याय नहीं मिला, तो यह उपलब्धि अधूरी ही कहलाएगी। राज्य निर्माण का सपना तब तक अधूरा है, जब तक उसका नागरिक न्याय के लिए भटकता है, जेल में सड़ता है, या न्यायपालिका की लंबी कतारों में बूढ़ा हो जाता है।
(जयसिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं और देहरादून में रहते हैं)