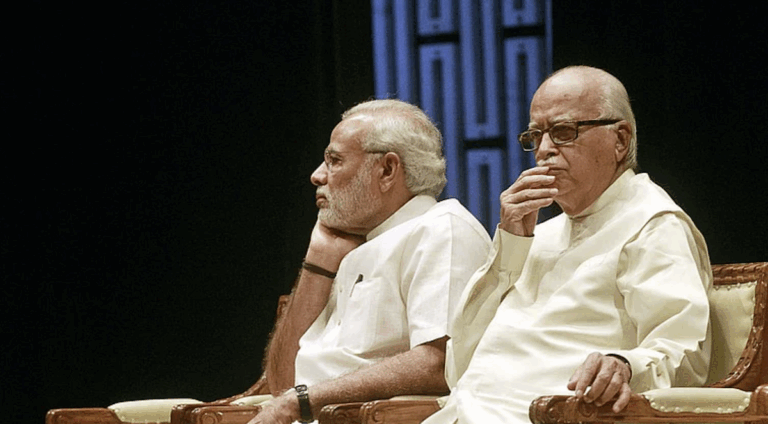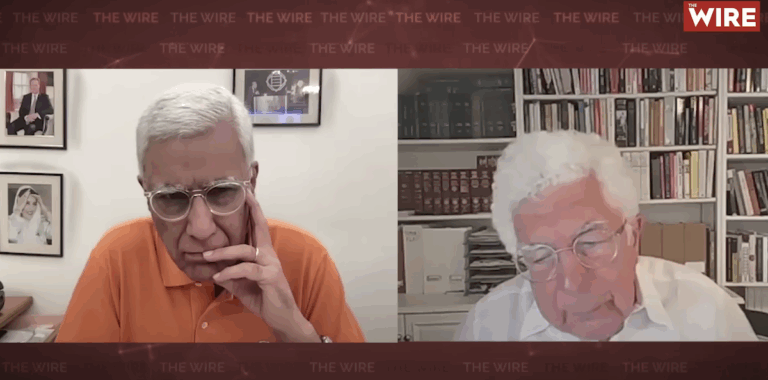भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक देश में हर एक घंटे में एक किसान और हर 40 मिनट में एक छात्र आत्महत्या कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय कैरियर और कॉलेज परामर्श (आईसी3) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारों से ज्यादा रोजगारशुदा लोग आत्महत्या कर रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक दिहाड़ी मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों की आत्महत्या की दर क्रमश: 25.6 और 9.7 फीसदी है, जबकि बेरोजगारों की आत्महत्या दर 8.4 फीसदी है।
देश के विभिन्न इलाकों में किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर पिछले 11 महीने से हजारों किसान फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को पूरे दो महीने हो गए हैं।
उधर सुदूर पूर्वोत्तर का मणिपुर डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से जातीय हिंसा की भीषण आग में झुलस रहा है। देश के विभिन्न इलाकों से जातीय और सांप्रदायिक उत्पीड़न की खबरें तो आती ही रहती हैं। इन्हीं सारी दर्दनाक खबरों के बीच हमारा भारतीय गणतंत्र तीन चौथाई सदी का सफर पूरा कर 76 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।
किसी भी राष्ट्र या गणतंत्र के जीवन में साढ़े सात दशक की अवधि अगर बहुत ज्यादा नहीं होती है तो बहुत कम भी नहीं होती। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय गणतंत्र ने अपने अब तक के सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन इसी अवधि में कई ऐसी चुनौतियां भी हमारे समक्ष आ खड़ी हुई हैं, जो हमारे गणतंत्र की मजबूती या सफलता को संदेहास्पद बनाती हैं, उस पर सवालिया निशान लगाती हैं।
भारत को आजादी हासिल होने से पहले ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल का मानना था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है, इसलिए अगर भारत को स्वतंत्र कर दिया गया तो भारतीय नेता शासन नहीं चला पाएंगे और यह देश बिखर जाएगा। चर्चिल ने यह बात भारत की आजादी को लेकर ब्रिटेन की संसद में हुई चर्चा के दौरान भी कही थी और बाद में भी कई बार दोहराई।
चर्चिल का कहना था कि आजादी के बाद भारत की सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। चर्चिल के इस पूर्वाग्रह को भारत अपनी आजादी के बाद 67 सालों तक झुठलाता रहा, लेकिन हाल के सालों में हुए कुछ घटनाक्रमों, अभी जारी घटनाओं और भारत पर शासन कर रही राजनीतिक शक्तियों की भाषा व भाव-भंगिमा पर गौर करें तो पाएंगे कि चर्चिल महाशय हर दिन, हर स्तर पर सही साबित हो रहे हैं।
बहरहाल, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और गणतंत्र का तो इतिहास ही भारत से शुरू होता है। ईसा से कोई छह सौ साल पहले लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई थी और उसके बाद दुनिया में जहां भी गणतंत्र को अपनाया गया, वहां किसी न किसी रूप में लिच्छवी गणराज्य की परंपराओं को स्वीकार किया गया।
आजादी के तीन साल बाद भारत भी उस दिन गणतंत्र बना, जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया। भारत में गणतंत्र की सार्थकता और उसके उत्सव का महत्व इसमें अंतर्निहित है कि संविधान की मूल भावना फलती-फूलती रहे।
संविधान की मूल भावना क्या है? देश की सर्वोच्च अदालत ने संविधान के बुनियादी ढांचे का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मोटे तौर पर उसे संविधान की मूल भावना कह सकते हैं। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल है तो देश में शासन की संघीय प्रणाली का संरक्षण भी शामिल है।
संवैधानिक संस्थाओं की स्वायतत्ता और उनकी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के तहत आता है। नागरिकों को अवसर की समानता और देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव भी संविधान की मूल भावना में परिलक्षित होते हैं।
संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी तय किए थे और हर नागरिक को धर्म चुनने और उसका पालन करने की आजादी भी दी थी। खान-पान और पहनावे की आजादी मौलिक अधिकारों के दायरे में आती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह सब याद दिलाने का मकसद यह है कि इन दिनों संविधान की कई मूल भावनाओं को विभिन्न स्तरों पर किसी न किसी रूप में गंभीर चुनौती मिल रही है।
एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत के सामने पहले भी कई चुनौतियां आई हैं और हर चुनौती ने भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को मजबूत बनाया है।
आजाद भारत में संविधान लागू होने के 25 साल बाद आपातकाल लगाए जाने और संविधान में 42वें संशोधन के जरिए उसकी मूल भावना को बदल देने के प्रयासों से कुछ समय के लिए ऐसा लगा था कि भारत का लोकतंत्र कमजोर पंगु हो गया है, लेकिन उसके बाद भारत का लोकतंत्र भी मजबूत हुआ और गणतंत्र भी।
आपातकाल हटने के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार ने संविधान के 44वें संशोधन से कई चीजों वापस पुराने रूप में बहाल किया, जो कि उसका अनिवार्य ऐतिहासिक दायित्व था। उसके कुछ ही समय बाद भारी बहुमत से सत्ता में लौटी इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल के दौरान किए गए फैसलों को वापस बहाल करने की गलती नहीं की, क्योंकि उन्हें सबक मिल चुका था।
आज एक बार फिर सरकार के कामकाज में संविधान के कुछ सिद्धांतों से भारी विचलन दिख रहा है। संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर खतरा मंडरा रहा है।
संवैधानिक सिद्धांतों से विचलन को छद्म विकास, हिंदू पुनर्ज़ागरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नारों व कर्मकांडों से ढका जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि देश की आजादी का अमृत काल चल रहा है और आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा।
देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्त कराने की बात कही जा रही है। हाल में यह भी कहा गया है कि देश को असली आजादी तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने पर मिली है। सरकार और सत्तारूढ़ दल की ओर से विज्ञापनों के जरिए प्रचारित किया जा रहा है कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है और दुनिया में भारत की आवाज अब ज्यादा मजबूती से सुनी जा रही है।
सरकार के मंत्री तो यह तक दावा कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो रहा है और दुनिया के तमाम देश अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हालांकि ऐसा कहने वाले मंत्री अपवाद नहीं हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी स्वामीभक्ति दिखाने के लिए इस तरह की बातें पहले भी होती रही थीं।
बहरहाल, सरकार की ओर से किए जा रहे दावे अपनी जगह है। दूसरी ओर एक हकीकत यह है कि संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग जैसी संस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा प्रभावित हो रही है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे बुनियादी जरुरत है कि चुनाव आयोग और उसकी गतिविधियां संदेह से परे रहे।
लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई व्यवस्था को बदल कर नई व्यवस्था के तहत सब कुछ सरकार का अपने हाथों में ले लेना उसकी बदनीयती दर्शाता है। इससे चुनाव की प्रक्रिया पर अविश्वास बढ़ रहा है, जो कि लाजिमी है।
विपक्षी पार्टियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के अंधाधुंध इस्तेमाल को लेकर भी सरकार कठघरे में है। यही नहीं, न्यायपालिका की साख पर भी संदेह का धुआं मंडरा रहा है।
सरकार ने एक देश-एक चुनाव का इरादा बना रखा है। यह इरादा सुनने में भले ही अच्छा लगता हो लेकिन उससे देश में लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सामने नई चुनौतियां पैदा होंगी।
लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इन चुनौतियों की ओर इशारा कर रही हैं, जिन्हें समझा जाना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग के सामने भी अपनी स्वायत्तता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की चुनौती है। इस समय चुनाव आयोग तमाम बदनामियां झेलते हुए भी सत्तारूढ़ दल का मददगार बना नजर आ रहा है।
कुछ साल पहले एक देश-एक टैक्स की व्यवस्था भी लागू की गई, जिसे बहुत आदर्श व्यवस्था बताया गया लेकिन उससे राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता खतरे में आई है। सभी राज्यों की आर्थिक दशा बदहाली की शिकार है। खुद केंद्र सरकार भी गले-गले तक कर्ज में डूबी हुई है लेकिन राज्यों की स्थिति ज्यादा खराब है।
जीएसटी लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संग्रहित कर में एक तिहाई हिस्सेदारी ही राज्यों को देना चाहते थे। हालांकि वित्त आयोग की सिफारिशों से 42 फीसदी हिस्सेदारी राज्यों को देना तय हुआ लेकिन उसे देने में भी केंद्र सरकार कई तरह से हीला-हवाला करती है- खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों को।
संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसके तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से विधायिका का कामकाज सवालों के घेरे में है।
कानून बनाने की प्रक्रिया में विपक्ष को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। संसदीय समितियों की भूमिका लगभग खत्म कर दी गई है और संसद में महत्वपूर्ण कानून चंद मिनटों में बिना सार्थक बहस या विचार विमर्श के ही पारित हो रहे हैं।
सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है।
सरकार अपने से असहमत हर व्यक्ति या दल को देशद्रोही करार देने में देर नहीं करती है। यह स्थिति देश के लिए कतई शुभ नहीं कही जा सकती। ऊपर लिच्छवी गणराज्य का संदर्भ देने का एक मकसद यह बताना भी था कि उस समय सब कुछ बहस या विमर्श के जरिए तय होता था।
अब भारत के लोकतांत्रिक गणतंत्र में विमर्श के लिए जगह कम होती जा रही है। जबकि गणतंत्र की खूबसूरती और मजबूती के लिए विमर्श की जगह होना अनिवार्य शर्त है।
(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और इंदौर में रहते हैं)