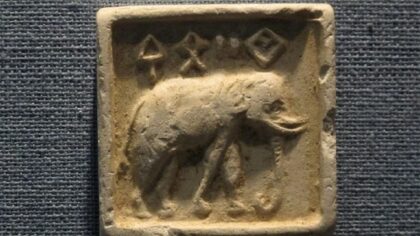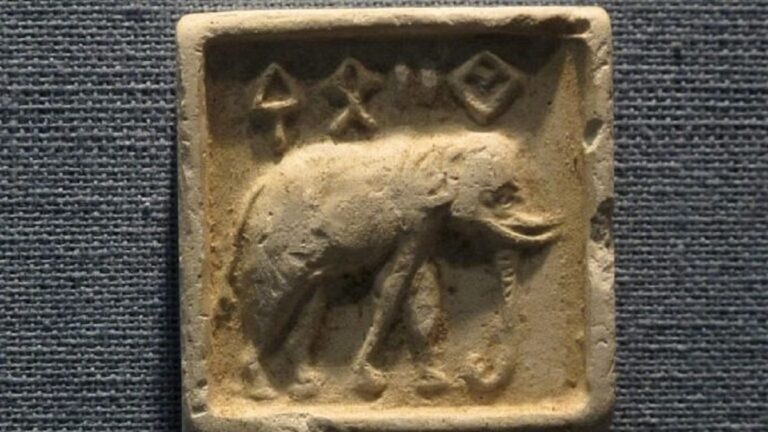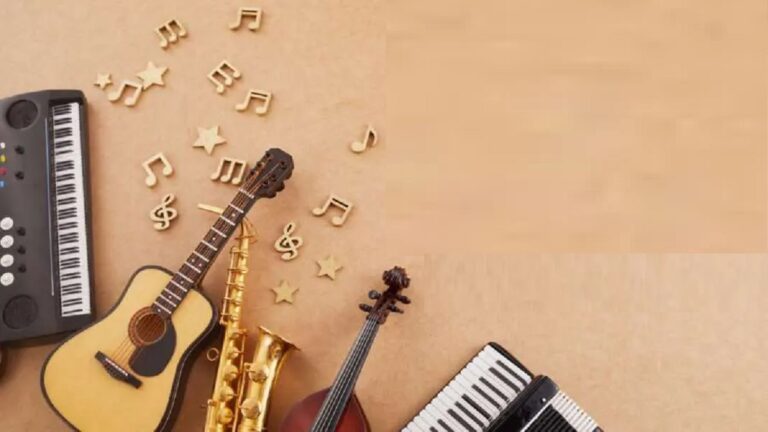शापुरजी सकलतवाला (1874-1936) ब्रिटेन की संसद के पहले और केवल चार कम्युनिस्ट सदस्यों में से एक थे। उनके दादा प्रख्यात उद्योगपति जमशेदजी टाटा के पिता नुसेरवांजी टाटा के रिश्तेदार और व्यापारिक साझेदार दोनों थे।
हाल ही में जिनकी 182वीं जयंती पर रतन टाटा ने उन्हें याद किया। सकलतवाला का जन्म बॉम्बे में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन जमशेद जी (जेएन टाटा) के घर में बिताया।
दरअसल शापुरजी जेएन टाटा के भांजे और उनकी बहन जेरबाई और जीजा दोराबजी सकलतवाला के बेटे थे। दोराबजी सकलतवाला के पिता और जेएन टाटा के पिता आपस में रिश्तेदार होने के साथ ही व्यवसायिक साझीदार भी थे। इस तरह से दोराबजी टाटा एंपायर के आधे के हिस्सेदार थे।
लेकिन उनको उससे वंचित कर दिया गया था और बाद में वह बेहद दुखद गति को प्राप्त हुए। हालांकि जेएन टाटा अपनी छोटी बहन जेरबाई को बहुत प्यार करते थे। लेकिन व्यवसायिक कारणों से अपने जीजा को नापसंद करते थे। और बताया जाता है कि जेरबाई और उनके पिता के बीच अलगाव का यही कारण भी था।
हालांकि जेएन टाटा शापुरजी को बहुत पसंद करते थे। और उनकी यह पसंद इस हद तक थी कि खुद उनके अपने बेटे दोराबजी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। दोराब जी को लगता था कि बुड्ढा, शापुरजी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पाल-पोस रहा है।
लेकिन उनका यह भय सही नहीं साबित हुआ। दोराबजी गलत आदमी नहीं थे। यह बात कुछ इसी तरह की थी जैसे किसी के मन में असुरक्षा का भाव पैदा हो जाए। और शापुरजी जैसा एक शख्स जो ज्यादा स्मार्ट और सुंदर था और वह एकाएक उनके पिता का चहेता बन गया था।
जेएन टाटा उस समय स्टील अंपायर स्थापित करने का ख्वाब देख रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने किशोर शापुरजी को एक अमेरिकी भूगर्भशास्त्री के साथ लोहे की खदानों की खोज के वास्ते मध्य भारत के इलाकों का दौरा करने के लिए भेजा।
महीनों के अथक परिश्रम और यात्राओं के बाद दोनों को आज के जमशेदपुर के पास अच्छी खासी मात्रा में लोहे की खदान के बारे में पता चला। लेकिन इसी दौरान मलेरिया और टीबी ने शापुरजी को एक साथ घेर लिया और उनके स्वास्थ्य को काफी क्षति पहुंचायी।
1926 तक भी सकलतवाला को यह लगता था कि उनके पिता दोराबजी और उनका परिवार उस संपत्ति के एक बड़े हिस्से से वंचित रह गया था जो टाटा परिवार को मिली। उसी वर्ष लिखे एक पत्र में उन्होंने बताया कि उनके पिता को ‘पूरी ज़िंदगी गरीबी में बितानी पड़ी और 14 साल की उम्र से ही उन्हें सारी संपत्ति और व्यापारिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया।’
उन्होंने पत्र में लिखा कि उनके पिता के साथ “बेहद क्रूर अन्याय” हुआ, जिसके कारण उनकी भावी पीढ़ी भी प्रभावित हुई। उनके पिता वर्षों तक ‘अन्याय और पीड़ा’ सहने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सकलतवाला ने यह भी उल्लेख किया कि 1868 में जब उनके दादा की मृत्यु हुई, तब उनके पिता सिर्फ 14 साल के थे, और टाटा परिवार ने उन्हें ‘आज्ञाकारी न मानते हुए, खराब व्यवहार वाला और अनुशासनहीन’ बताया, जिसके बाद उनके छोटे भाई बेराम की शिक्षा के लिए भी कोई सहायता नहीं की गई।
सकलतवाला की बेटी अपनी जीवनी में कहती है कि उनको विश्वास था कि उनके चाचा जमशेदजी टाटा ने उनके पिता को नष्ट कर दिया था और उनके माता-पिता के बीच वास्तविक अलगाव का कारण बने थे (सेहरी सकलतवाला, द फिफ्थ कमांडमेंट, 1991, पृष्ठ 13)।
इस पृष्ठभूमि में शापुरजी सकलतवाला की उस उल्लेखनीय यात्रा को समझा जा सकता है, जिसमें एक उच्चवर्गीय पारसी धीरे-धीरे वामपंथ की ओर बढ़ता गया, जब एक बार उसने भारत छोड़ा।
जॉन हिन्नेल्स की पुस्तक द ज़ोरोस्ट्रियन डायस्पोरा (ऑक्सफोर्ड, 2005) में सकलतवाला से संबंधित अंश में लिखा मिलता है:
जमशेदजी ने युवा शापुरजी को उनके अपने पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया और उन्हें इतना पसंद करने लगे कि खुद उनके अपने बेटे (दोराबजी, जन्म 1859) को उनसे ईर्ष्या होने लगी, जिसने बाद में सकलतवाला के लिए नई समस्याएं पैदा कीं। उन्होंने कैथोलिक सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की।
बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में, उन्होंने और कुछ दोस्तों ने बैक्टीरियोलॉजिस्ट प्रोफेसर व्लादिमीर हैफ्किन के साथ काम किया, जो बॉम्बे के गरीबों को ब्यूबोनिक प्लेग के खिलाफ टीका लगाते थे।
हैफ्किन रूस से ज़ार की खुफिया निगरानी से बचने के लिए आए थे, और यह माना जा सकता है कि उनकी समाजवादी विचारधारा ने सकलतवाला को प्रभावित किया। इस अनुभव के बाद, उन्होंने कुछ समय एक सैनेटोरियम में अवसादग्रस्त रहकर बिताया।
उन्होंने 1901 में टाटा समूह में शामिल होकर काम शुरू किया, और 1902 में दोराबजी टाटा और एक अमेरिकी के साथ मध्य भारत में लोहा और कोयला की खोज शुरू की।
उन्होंने इस खोज को टाटा परिवार के लक्ष्यों से भी अधिक दूर तक पहुंचाया, और उन्होंने यह काम एक हद तक अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हुए किया।
विशेष रूप से जंगलों और दलदलों में काम करते यह बेहद मुश्किल भरा था। दोराबजी की बढ़ती ईर्ष्या के कारण उनके करियर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
उन्होंने अपने सहयोगियों से अधिक समय मजदूरों के बीच बिताया और उनके साथ काम किया, संभवतः अपने बढ़ते समाजवादी विश्वासों के कारण, लेकिन निश्चित रूप से इससे उनका समाजवाद और मजबूत हुआ।
स्वास्थ्य के लिहाज से भी और कांग्रेस से जुड़े टाटा परिवार से अपने विचारों को अलग करने के लिए, उन्हें टाटा साम्राज्य के सुदूर हिस्से-लंदन भेजा गया।
कुछ किताबों ने इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया कि प्लेग से पीड़ित बॉम्बे और जंगलों में, सकलतवाला ने अपनी आधी ज़िंदगी गरीबों के लिए काम करते हुए बिताई।
जब शापुरजी सकलतवाला 1905 में लंदन पहुंचे, तो वे फिर से अवसादग्रस्त और बीमार थे। वे डर्बीशायर के स्पा शहर मैटलॉक गए, जहां उन्होंने एक होटल की वेट्रेस से प्रेम किया। एक साल बाद, उन्होंने एलिजाबेथ (जिन्हें सैली के नाम से जाना जाता था) से विवाह किया और उनका नाम बदलकर सेरी रखा।
सकलतवाला जब इंग्लैंड पहुंचे, तो वे लिबरल पार्टी के सदस्य थे, लेकिन धीरे-धीरे वामपंथ की ओर बढ़ते हुए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और फिर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। मार्क वाड्सवर्थ ने अपनी पुस्तक कॉमरेड साक (1998) में उनके राजनीतिक जीवन की बढ़ती सक्रियता का अच्छा वर्णन किया है।
बैटरसी निर्वाचन क्षेत्र की वामपंथी सहानुभूति के चलते एक भारतीय कम्युनिस्ट का ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना जाना शुरुआत में अविश्वसनीय लगती थी, और इस बात को समझा भी जा सकता है (दरअसल, वह वेस्टमिंस्टर में चुने जाने वाले एकमात्र कम्युनिस्ट थे)। उन्होंने 1923 में अपनी सीट खो दी, लेकिन एक साल बाद फिर से जीत गए।
सकलतवाला ने सोवियत संघ का दौरा किया, जिसने उन पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें यूएसए की संसदीय यात्रा पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया। वह खनिकों की हड़ताल और जनरल स्ट्राइक के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति थे।
1926 में, उन्हें ट्राफलगर स्क्वायर में एक भाषण देने के लिए दो महीने की कैद हुई, जिसमें उन्होंने सैनिकों से निहत्थे हड़तालियों के खिलाफ हथियार न उठाने का आह्वान किया था। अदालत में उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें जेल भेज दिया गया।
अपने जीवन के अधिकांश समय, विशेष रूप से जेल से रिहा होने के बाद, सकलतवाला पुलिस की निगरानी में रहे। खुफिया सेवाओं ने उनकी डाक को भी खोला। भले ही उनके किसी भी रैली में कभी हिंसा नहीं हुई थी, पुलिस अक्सर आखिरी क्षणों में उनके भाषण की अनुमति रद्द कर देती थी।
1927 में, शापुरजी सकलतवाला ने कराची से लेकर कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे तक का एक व्यापक राष्ट्रीय दौरा किया। उन्होंने कई शहरों में बड़ी सभाओं को संबोधित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेतृत्व के साथ उनके संबंध मिले-जुले थे।
सामान्यत: नेहरू उनके व्याख्यानों में शामिल होते थे, और सकलतवाला की मृत्यु पर उन्होंने शोक संदेश भी भेजा था। गांधी के साथ उनके संबंध काफी तनावपूर्ण थे। सकलतवाला गांधी के भारतीय औद्योगिकीकरण पर नकारात्मक दृष्टिकोण से असहमत थे और उन्हें इस बात पर भी आपत्ति थी कि गांधी ने खुद को श्रद्धा का पात्र बनने की अनुमति दी।
गांधी को सकलतवाला के मार्क्सवादी विचारों से बहुत कम सहानुभूति थी।
इस संदर्भ में, भारत के पारसी समुदाय की सकलतवाला के प्रति प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। बॉम्बे में समुदाय के नेताओं के बीच प्रतिक्रियाएं ध्रुवीकृत थीं।
सर फेरोज सेठना ने सकलतवाला के शहर आगमन पर उन्हें सम्मानित करने के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि चार अन्य पारसियों (जिनमें एफ.के. नरिमन भी शामिल थे) ने ऐसे सम्मान का समर्थन किया। नवसारी में एक सभा के दौरान सकलतवाला का सम्मान वरिष्ठ दास्तूर, दास्तूर मेहरजीराना ने किया।
जॉन हिन्नेल्स आगे लिखते हैं कि भारत से लौटने पर, सकलतवाला ने ज़ोरास्ट्रियन एसोसिएशन से अपने बच्चों के नवजोत (धार्मिक दीक्षा संस्कार) के लिए अनुमति मांगी। आखिरकार एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम के लिए सहमति दे दी, भले ही सकलतवाला ने समुदाय के बाहर शादी की थी और सेंट जेवियर्स में पढ़ाई के दौरान ईसाई बपतिस्मा ग्रहण किया था।
सकलतवाला ने एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि उन्होंने यह केवल यह देखने के लिए किया था कि कैसा लगता है, और कभी भी अपने पारसी धर्म से नाता नहीं तोड़ा। उसी वर्ष, 1927 में, एसोसिएशन ने उन्हें और उनके बच्चों को (लेकिन उनकी पत्नी को नहीं) ब्रूकवुड में दफनाने की भी अनुमति दी।
कम्युनिस्ट पार्टी ने मृत्यु के समय के मुकाबले जीवित रहते उनकी अधिक सराहना की। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में, पार्टी ने कभी-कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकारा था, उदाहरण के लिए, अपने बच्चों के नवजोत समारोह में शामिल होने को लेकर, जिसे पार्टी ने ‘अंधविश्वास’ माना था (हिन्नेल्स, द ज़ोरोस्ट्रियन डायस्पोरा, पृष्ठ 376 और आगे)।
शापुरजी सकलतवाला एक अद्वितीय वक्ता थे। प्रियम्वदा गोपाल की पुस्तक इन्सर्जेंट एम्पायर में उल्लेख है कि अपने अपेक्षाकृत छोटे लेकिन घटनापूर्ण संसदीय करियर में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में 500 से अधिक हस्तक्षेप किए।
7 नवंबर, 1928 को संसद में एक भाषण में उन्होंने कहा था, “दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसने इतना अधिक मानव जीवन को नष्ट किया हो और ब्रिटिश राष्ट्र और ब्रिटिश संसद से ज्यादा हत्याएं की हों।”
ब्रिटेन में तीन पारसी सांसदों (नौरोजी, भावनागरी और सकलतवाला) में से, सकलतवाला अकेले ऐसे थे, जिन्होंने संसद में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की थी। जॉन हिन्नेल्स लिखते हैं कि सकलतवाला ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाले अकेले पारसी सांसद थे।
यह सकलतवाला के दृढ़ और साहसी विचारों का प्रमाण है, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता था। जैरस बनर्जी द्वारा लिखे गए इस लेख से यह स्पष्ट होता है कि सकलतवाला का योगदान केवल ब्रिटेन की राजनीति में ही नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वैश्विक समर्थन में भी महत्वपूर्ण था।
(जैरस बनर्जी का लेख। कुछ इनपुट आदित्य सिन्हा के ट्वीट से लिए गए हैं।)
मूल लेख यहां पढ़ा जा सकता है।