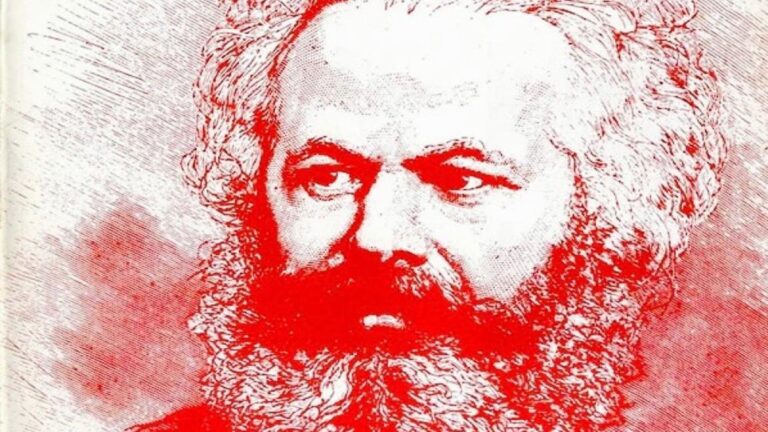विपक्ष अभी भी एक असरदार आलोचना के लिए सटीक भाषा और अवसर की तलाश में जूझ रहा है। फिलहाल तो यह उन्हीं लोगों से संवाद बना पा रहा है जो पहले से ही उससे सहमत हैं। हाल के विधानसभा चुनावों में उत्तर भारत में भाजपा की जोरदार जीत ने इस सवाल को फिर से खोल दिया है।
ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के लिए समुचित रणनीति क्या हो सकती है, जबकि उसका सामना एक अत्यधिक चालाक और लोकप्रिय प्रधानमंत्री से है, जिसके पास एक गहराई से जुड़ी हुई प्रेरणा और उत्साह से लबरेज, सभी संसाधनों से संपन्न, रणनीतिक रूप से स्मार्ट राजनीतिक मशीन है। और इसके साथ ही, जबकि अलग-अलग हिस्सों में आर्थिक असंतोषों के बावजूद केंद्र सरकार के खिलाफ असंतोष की कोई लहर भी मौजूद नहीं है?
विपक्ष के लिए चुनौती यह है कि वह सरकार की कोई ऐसी सुस्पष्ट आलोचना नहीं ईजाद कर पा रहा है, जिससे पीछा छुड़ा पाना उसके लिए नामुमकिन हो। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने हाल ही में कहा था कि हलांकि कांग्रेस का संप्रेषण बेहद शक्तिशाली था, लेकिन यह उन्हीं लोगों की ओर उन्मुख था जो पहले ही उससे सहमत हो चुके थे।
जैसा कि ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ द्वारा तैयार किए गए बेहद महत्वपूर्ण चुनाव विश्लेषण से पता चलता है, जिन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, वहां उसके वोट शेयर में खास कमी नहीं आयी है। विडम्बना यह हुई है कि विपक्ष द्वारा भाजपा-विरोधी वोटों को एकजुट करने के बजाय, खुद भाजपा कांग्रेस-विरोधी वोटों को एकजुट करने में कामयाब हो गयी है।
यह स्थिति छत्तीसगढ़ में सबसे गंभीर है जहां कांग्रेस का वोट शेयर लगभग स्थिर रहा है, जबकि भाजपा का वोट शेयर लगभग 12 प्रतिशत बढ़ गया है।
कुल वोट शेयर में स्थिरता के नीचे सूक्ष्म स्तर पर वोटों की इधर से उधर आवाजाही के आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस, ज्यादातर उन्हीं लोगों से मुखातिब रही है, जो पहले से ही उससे सहमत हो चुके हैं। आखिर इसके क्या कारण हो सकते हैं?
मुख्य समस्या यह है कि कांग्रेस का बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से उन वैचारिक परिवर्तनों के विपरीत है जिनकी उसे आवश्यकता है। दरअसल, एक सुस्त क़िस्म का सामाजिक नियतिवाद भारतीय राजनीति में वामपंथ और मध्यममार्गी दलों के लिए अभिशाप बन चुका है।
यह धड़ा वर्षों से, सर्वहारा वर्ग के समकक्ष किसी ऐसे स्वाभाविक सामाजिक समूह की तलाश कर रहा है, जिसे केवल उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर मुक्ति का एजेंट मान लिया जाए। कभी ये दलित होते हैं, कभी अल्पसंख्यक होते हैं तो कभी आमतौर पर जाति समूह होते हैं। नतीजतन आज राजनीति अनिवार्यतः सामाजिक पहचान के अंकगणित तक सिमट कर रह गयी है।
जाति जनगणना की वकालत करना इस गलती की नवीनतम अभिव्यक्ति थी। यह राजनीतिक रूप से अदूरदर्शी कदम था, क्योंकि विकास का कोई ऐसा गंभीर एजेंडा नहीं है जिसके लिए जाति जनगणना की आवश्यकता हो। यह सामाजिक नियतिवाद नैतिक रूप से घिनौना है।
यह मतदाताओं को जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने वाले राजनीतिक परिवर्तनकारी एजेंटों के बजाय एक बंधी हुई पहचान के एक स्थिर कथानक के रूप में मान लेता है। यह अनुभवों में भी ग़लत साबित हो चुका है, जैसा कि भाजपा ने दलितों, पिछड़ों और अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक पहचान में लाए गए प्रभावशाली परिवर्तन ने साबित कर दिया है।
भाजपा खुद भी हिंदुत्व की पहचान की राजनीति कर रही है। लेकिन यह कहीं अधिक सचेत है कि पहचानें राजनीतिक रूप से बनायी जाती हैं। वामपंथ का अस्मितावाद तो और भी पिंजड़े में बंद सा, और गहरे स्तर तक ग़ैरराजनीतिक है।
एक और नवीनतम अफवाह शुरू हो चुकी है- उत्तर-दक्षिण का भेद। उत्तर और दक्षिण में अंतर है, लेकिन कांग्रेस समर्थक अपने चारों ओर जो बौद्धिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह नकारात्मक है और नस्लवाद की सीमा तक पहुंच जाता है। यह इस तथ्य को झुठलाता है कि दक्षिण में, यहां तक कि केरल में भी सांप्रदायिकता उबल रही है।
एक सामाजिक संरचना के रूप में जाति तमिलनाडु जैसे राज्यों में उतनी ही दमनकारी है जितनी किसी और राज्य में। और यह दावा करना तो और भी अजीब है कि एक ही चुनाव में कर्नाटक बुराई से अच्छाई की ओर, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान अच्छाई से बुराई की ओर जा सकते हैं। यह दक्षिण में भाजपा की क्षमता को कम करके आंकता है।
ऐसी सोच से क्षुद्र विभाजन की राजनीति की गंध आती है, और यह भारत को आपस में बांधने वाली जटिल नसों के ज्ञान के बारे में नादानी को दिखाती है। ऐसी सोच राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की भव्यता के एजेंडे को पूरी तरह से भाजपा के रहमोकरम पर छोड़ देती हैं।
भाजपा की राजनीतिक प्रतिभा के बावजूद, तानाशाही और सांप्रदायिकता के बढ़ते जोखिमों को नकारना नैतिक रूप से अनुचित होगा। लेकिन, यह स्वीकार करना होगा कि इन खतरों को आम जनमानस द्वारा व्यापक रूप से महसूस या अनुभव नहीं किया जा रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक तथ्य है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं।
राज्य की लगभग सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है और हमारी स्वतंत्रता खतरे में है। लेकिन यह इस तरह से किया जा रहा है कि अधिकांश नागरिकों को शासन के अपने सामान्य अनुभव में इस अंतर का अनुभव नहीं हो रहा।
कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आम जनता द्वारा इसे अभी भी सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप ही देखा जा रहा है, और काफी लोगों को यह लगता है कि प्रतिस्पर्धा की राजनीति में यह सब एक मामूली विचलन है, कोई व्यवस्थित खतरा नहीं।
यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे समाज में केवल तभी व्यापक स्वीकार्यता मिल पाती है जब समाज में बेशुमार शक्ति रखने वाले लोग, इसके अभिजात वर्ग, ऐसे मुद्दों को उठाने और प्रसारित करने लगते हैं। दुर्भाग्य से, ये ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें विपक्ष आकर्षित या क़ायल कर सके।
हिंदुत्व पर विपक्ष की आलोचना दो कारणों से विफल हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा ने हिंदुओं के बीच एक ऐसा आधार समूह तैयार कर लिया है जो मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पर रखने और यहां तक कि उनके खिलाफ हिंसा को लेकर भी सहज है।
हिंसक मूल्यहीनता की स्वीकार्यता हमारी स्वीकृति की सीमाओं से कहीं ज्यादा फैल चुकी है। लेकिन अधिनायकवाद के खतरे की तरह ही, काफी लोग यह भी मान बैठै हैं कि अभी भी कोई इतनी व्यापक हिंसा नहीं हो रही है जो किसी के विवेक पर दबाव डालती हो, या अव्यवस्था की आशंका पैदा करती हो। उन्हें ऐसे ख़तरे की आशंकाएं बहुत दूर की बातें लगती हैं।
लेकिन विपक्ष हिंदुत्व पर बहसों के जाल में फंसता रहता है। विपक्ष की मुख्य चिंता का विषय संस्कृति को लेकर आपसी लड़ाई नहीं होना चाहिए; कांग्रेस का पारिस्थितिकी तंत्र उस लड़ाई को जीतने के लिए अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे हिंदू-विरोधी होने का आरोप झेलना पड़ता है और हर सांस्कृतिक लड़ाई इसे उस जाल में और ज्यादा फंसा देती है।
इस फंदे से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है, हर व्यक्ति की समान स्वतंत्रता और गरिमा की हिफाजत करना, यही बात उसे बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक ढांचे से ऊपर उठाती है। इसे ईशनिंदा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामलों, दंगों और राजनीतिक हत्याओं के मुद्दों और सभी समुदायों में व्यक्तियों के अधिकारों पर समुदायों के वर्चस्व की आलोचना पर लगातार एक ठोस रुख अपनाना होगा। बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक ढांचे में तो अल्पसंख्यक अंततः राजनीतिक रूप से हार ही जाएंगे।
कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की आलोचना को प्रमुखता दी है। इसमें दो समस्याएं हैं। ऐसा अभियान केवल उस परिस्थिति में काम करता है जब उसे कोई विश्वसनीय शख्सियत चलाये- या तो जयप्रकाश नारायण जैसा कोई बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी, या वीपी सिंह जैसा सत्तारूढ़ प्रणाली से बाहर निकला कोई बड़ा व्यक्ति हो।
दूसरी समस्या है आलोचना का स्तर- उदाहरण के लिए, भ्रष्ट विधायकों को लेकर बहुत असंतोष व्याप्त था, या परीक्षा भर्ती के बारे में काफी चिंताएं थीं। लेकिन इन मुद्दों को उठाने की बजाय अडानी की एक अमूर्त आलोचना करना जनता को समझ में आने वाले मुद्दों से एक विचलन था, वह भी तब जबकि राजस्थान जैसे राज्य में जहां 5,000 करोड़ रुपये का निवेश अडानी से प्राप्त हो रहा है।
समस्या का दूसरा पहलू अर्थव्यवस्था को लेकर है। यह एक जटिल मुद्दा है- राज्य को कल्याणकारी गठबंधनों को एक साथ जोड़ना पड़ता है, और प्रतिस्पर्धा अक्सर क्षमता के मामले में होती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष को तेजी से वामपंथ की ओर झुकते हुए देखा जा रहा है- बड़े व्यवसाय विरोधी और व्यवसाय विरोधी होने के बीच की रेखा को समझाना कठिन है। इसमें कोई नया प्रतिमान नहीं है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नया मार्ग खोलता हो।
इसलिए, नेतृत्व, रणनीति और संगठनात्मक मुद्दे के अलावा, विपक्ष, चाहे वह अकेले कांग्रेस हो या ‘इंडिया’ गठबंधन, विपक्ष अभी भी एक असरदार आलोचना के लिए सटीक भाषा और अवसर की तलाश में जूझ रहा है। फिलहाल तो यह उन्हीं लोगों से संवाद बना पा रहा है जो पहले से ही उससे सहमत हैं।
(‘इंडियन एक्सप्रेस’ से साभार, अनुवाद- शैलेश)