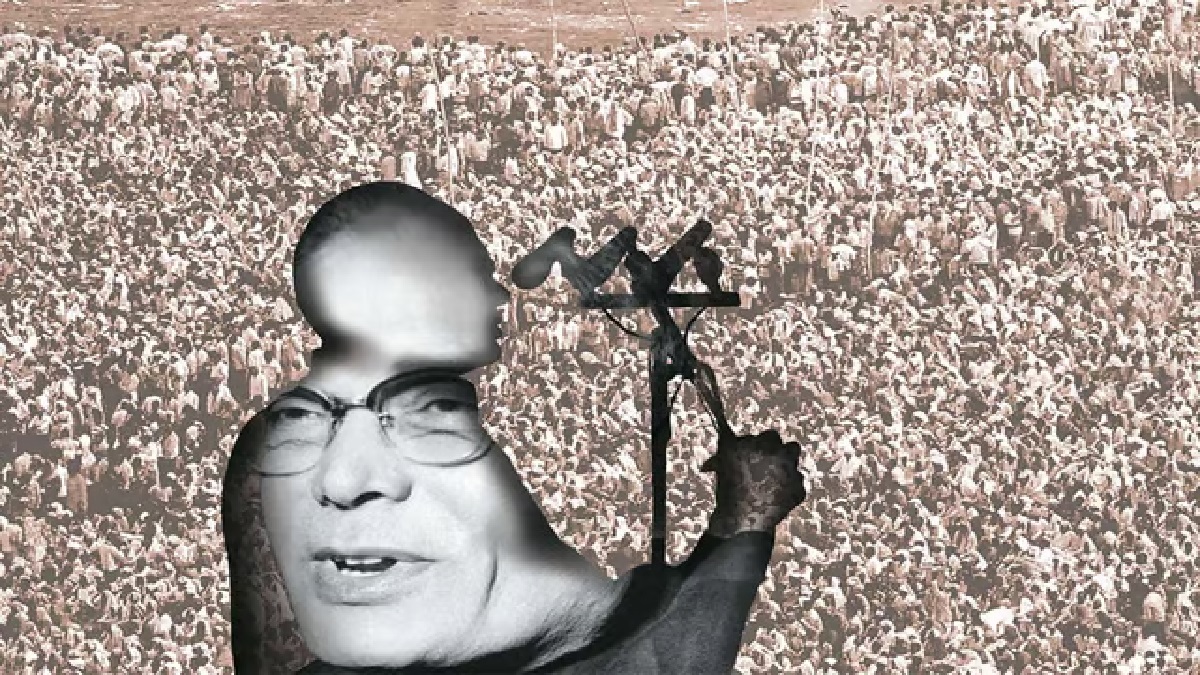सियासत की सियह-रात में राजनीतिक हवा सिहक रही है। सियासी मुद्दे मुंह दबाये फुसफुसाने लगे हैं। राजनीति के मौसम विज्ञानियों की नजर आकाश-पाताल नाप रही है। फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी है। राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक फुसफुसाहट पर कान धरने की कोशिश में लगे हैं।
कर्ण-पिशाचों, अर्थात विश्वस्त सूत्रों, की गतिविधि काफी तेज हो गई है। सियासी तूफान का केंद्र बिंदु बिहार है। कुल मिलाकर यह कि बिहार में वोटर की दलीय-निष्ठा में बदलाव की बयार बह रही है तो राजनीतिक दलों में भी सुगबुगाहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि समाजवाद के फिनिश्ड प्रोडक्ट फिर से करवट बदल रहे हैं।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन की गांठें भीतर से खुल रही है। दोनों राजनीतिक रूप से सावधान दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की नीति, नीयत के प्रति घटक दलों को भरपूर संदेह हो गया है। धीरे-धीरे भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भाजपा में भविष्य में सत्ता हासिल किये जाने की संभावनाओं और वर्तमान सत्ता को बचाये रखने के लिए किये जा रहे तिकड़मों को लेकर गहरा रणनीतिगत मतभेद उभर रहा है।
सत्ता और संगठन में व्यक्तियों में अपनी-अपनी सुरक्षित जगह घेरने और शक्ति की रस्साकशी है। यह कोई विचारधारात्मक संघर्ष नहीं है। न मुसलमानों को लेकर उनके नजरिये में कोई फर्क आया है और न ‘राज-काज’ और समाज व्यवस्था में सवर्णों के चिरकालिक वर्चस्व को वास्तविक चुनौती देने का ही कोई इरादा है। स्पष्ट कारणों से यह समझ में आने लायक बात है कि अटल विहारी बाजपेयी के शासन के समय के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और नरेंद्र मोदी के शासन-काल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चाल-चरित-चेहरा, घटक दलों की हैसियत में बहुत फर्क है।
अटल विहारी बाजपेयी घटक दलों की फुसफुसाहट की भी अनसुनी नहीं कर पाते थे और नरेंद्र मोदी घटक दलों की परंपरागत राजनीतिक सुविधा से जुड़ी किसी आवाज की कोई परवाह है। इस के पीछे की उन की रणनीतिगत समझ यह है कि वे घटक दलों को उनके परंपरागत वोट से विच्छिन्न कर अपने भीतर स्थाई रूप से समेट कर समाप्त किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के शासन को समर्थन दे रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के नेताओं को इस भाजपा की इस रणनीतिगत समझ की हवा लग चुकी है। कहा जा सकता है कि इस ‘रणनीतिगत समझ’ से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों की तिल-मिलाहट और बेचैनी काफी बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई तिलमिलाहट और बेचैनी के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राजनीतिक पकड़ से बाहर निकलने के लिए अपने-अपने पंख तौल रहे हैं।
घटक दलों की बेचैनी तो इंडिया गठबंधन में भी काफी बढ़ी हुई है। यह तो जाहिर ही है कि इंडिया गठबंधन के लगभग सभी राजनीतिक दलों की राजनीति कांग्रेस विरोध से निकली है। हालांकि कांग्रेस विरोध की उन की राजनीति का आधार मोटे तौर पर विचारधारा में उतना नहीं था जितना उन नेताओं की अपनी-अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में था। महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ कुछ अनदेखी न किये जाने लायक महत्वपूर्ण कारण भी जरूर थे।
इंदिरा गांधी के शासन-काल तक कांग्रेस की नीति वाम-झुकाव लिये बीच की स्थिति में रहती थी। इंदिरा गांधी के शासन में संजय गांधी के प्रभाव से कांग्रेस सरकार की कार्य-नीति में वाम-झुकाव लिये बीच की स्थिति हिलने लगी थी। जाने-अनजाने विभिन्न कारणों से इंदिरा गांधी और कांग्रेस की नीति में दक्षिण-पंथी रुझान ने जगह घेरना शुरू कर दिया था। इस दक्षिणपंथी रुझान में कहीं-न-कहीं हिंदू आग्रह और पूंजीवादी मजबूरी भी थी। राजीव गांधी के शासन-काल में हिंदू आग्रह और पूंजीवादी मजबूरी अधिक मुखर हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार (1 से 8 जून 1984), शाहबानो बेगम मामला (1985) मामलों और मंडल आयोग की सिफारिश (अगस्त 1990) को लागू करने तथा उस के बाद की राजनीतिक पृष्ठ-भूमि, परिस्थिति और प्रभाव का विश्वस्त संदर्भ लिया जा सकता है।
विकास की क्षेत्रीय जरूरतों और सवर्णों के सर्वोच्च वर्चस्व से निपटने में आजादी के आंदोलन के बाद कांग्रेस का रुख और रवैया बहुत ही कामचलाऊ किस्म का रहा था। कांग्रेस की यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की सांस्कृतिक समझ के बहुत करीब जा पहुंची थी। ऐसे में कांग्रेस विरोध की राजनीति को कहीं से गलत कहना अनुचित ही होगा।
कांग्रेस विरोध की राजनीति के चलते एक तरह से संसदीय राजनीति में अनिश्चितता और खालीपन का दौर आ गया। गठबंधन की राजनीति से इस अनिश्चितता और खालीपन का भराव शुरू हो गया। बीच चुनाव में राजीव गांधी की हत्या (21 मई 1991) के बाद बहुत ही दुखद परिस्थिति में कांग्रेस के नेता पी. वी. नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री और डॉ मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। यहां से उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण (उनिभू) के वैश्विक वातावरण में भारत की राजनीति में तेजी से बदलाव होना शुरू हो गया।
श्रीमती सोनिया गांधी और लगभग पूरे ‘गांधी परिवार’ का कांग्रेस से संबंध काफी शिथिल रहा। इस बदलाव में कांग्रेस विरोध की हवा फिर से बनने लग गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक अनिश्चितता और खालीपन में जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के समर्थन पर अटल विहारी बाजपेयी ने 1996 में तेरह दिन की, 1998 से 1999 में तेरह महीने की और फिर 1999 से 2004 तक पांच साल तक प्रधानमंत्री रहे।
इस बीच कांग्रेस ने फिर से ‘गांधी परिवार’ को कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय कर दिया। ‘शाइनिंग इंडिया’ अर्थात ‘दमकता इंडिया’ के नारा के साथ चुनाव लड़नेवाली भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) समेत बहुमत से पिछड़ गई। यह सब श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ। इस के साथ ही श्रीमती सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने की बात भी सियासत का मुद्दा बन कर उभरी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) बना।
तमाम तरह की राजनीतिक अनुकूलताओं के बावजूद स्पष्ट कारणों से राहुल गांधी के तीव्र विरोध के चलते श्रीमती सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने से रह गई। डॉ मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। डॉ मनमोहन सिंह की छवि बाजारवाद के पक्ष में थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) में वाम-पंथी राजनीति का निर्णायक दखल था। वाम-पंथ की आशंकाओं को न्यूनतम करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) तैयार हुआ। हां, डॉ मनमोहन सिंह की सरकार के लिए देश के कई जाने-माने को शामिल करते हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) का गठन किया गया था।
यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार दस साल (2004 से 2014) तक चली। कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये, कई महत्वपूर्ण कानून बने। कहना न होगा कि विकट राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार चली। विदेश नीति, खासकर परमाणु समझौता जुड़े मुद्दों पर यूपीए सरकार से वाम-पंथ का समर्थन वापस हो गया। और यही वह दौर था जब वाम-पंथ भारत की राजनीति की अनिश्चितता और खालीपन को भरने में बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई।
2012-13 से डॉ मनमोहन सिंह की सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये गये, घटक दलों के मंत्री न सिर्फ हटाये गये बल्कि जेल तक गये। किसन बाबूराव हजारे यानी अण्णा हजारे को सामने और समझा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ को पीछे रखकर, अरविंद केजरीवाल समेत कई गणमान्य लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल की नियुक्ति के मामलों पर जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया।
हालांकि न भ्रष्टाचार के आरोप अदालत में साबित किये जा सके न ढंग से लोकपाल की ही नियुक्ति हो पाई। हां वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘अच्छे दिन आयेंगे’ के सपनों के सामने डॉ मनमोहन सिंह सरकार का यथार्थ अच्छे-से पिछड़ गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ‘अकेले दम’ की सरकार बनाई। पांच साल बाद 2019 में तो पहले से भी अधिक बड़ी जीत हासिल हुई। राम मंदिर का संकल्प पूरा हो गया। हालांकि राम मंदिर क्षेत्र में पार्टी चुनाव हार गई।
फिर भी, चुनाव आयोग समेत अन्य संवैधानिक संस्थाओं की ‘सक्रियता’ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण फर्क भी आया। कैसा और क्या फर्क! तमाम तरह की प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थिति और ‘डर के माहौल’ में राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ संपन्न हुई, नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से बाहर निकलकर इंडिया अलायंस के संयोजन में लग गये।
हालांकि नीतीश कुमार 2024 की घोषणा के पहले ही ‘अच्छा’ नहीं लगने के कारण फिर से नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में वापस चले गये। कुल मिलाकर हुआ यह कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘चार सौ के पार’ के मंसूबा के साथ चुनाव लड़नेवाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ‘अकेले दम’ कामचलाऊ बहुमत से 32 अंक पीछे रह गई। अब सरकार के बनने का सारा दारोमदार जनता दल यूनाइटेड और तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) पर आकर टिक गया।
इस बीच हुए विधानसभा चुनावों में हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिन परिस्थितियों में और जिस तरह से जीत हासिल की है वह न सिर्फ चौंकानेवाली है, बल्कि डरानेवाली भी है। इधर शान से ‘भारत खोदो’ अभियान चल रहा है और उधर परेशान राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ प्रमुख तथा साधु-संत भेषधारी ‘महा-पुरुषों’ के असहमतिपरक बयानों से अलग ही कोहराम मचा हुआ है। इन परिस्थितियों में स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों के परंपरागत वोटर भी इधर-उधर हो रहे हैं।
हिंदुत्व की राजनीति अपनी जिस ‘सोशल इंजीनियरिंग’ के तहत हिंदू वोटों की एकता में अपने लिए स्थाई बहुमत का निश्चित जुगाड़ देख रही थी, उस में अब फांक और फाट साफ-साफ दिखता है। हिंदुत्व की राजनीति सवर्णों के सर्वोच्च वर्चस्व की आकांक्षा के न सिर्फ तात्कालिक रूप से, बल्कि चिरकालिक रूप से समाप्त होने की स्थिति से हिंदुत्व की राजनीति में परेशानी है। दूसरी तरफ साधु-संत भेषधारी सहित हिंदू मिजाज के सांगठनिक नियंत्रण और अनुशासन से बाहर निकलने के कारण भी हिंदुत्व की राजनीति की परेशानी कम नहीं है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की पकड़ से बाहर निकलनेवाले नेतागण अब कांग्रेस विरोध की राजनीति पर नये सिरे से चलने की इच्छा रखने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कार्रवाइयों के डर के कारण वे कांग्रेस के साथ हो लिये थे। अब उस डर के कम होते ही वे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के नेतृत्ववाले इंडिया गठबंधन से भी अलग और भिन्न रास्ता अख्तियार कर रहे हैं; अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और कुछ हद तक अखिलेश यादव के रुख पर बारीकी से गौर किया जा सकता है।
यानी गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा की राजनीति, पुराने मुहावरे में तीसरे मोर्चे की राजनीति की संभावनाओं में सुगबुगाहट है। ऐसा लग रहा है कि आगे भारत की राजनीति का रास्ता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गलियारों के बीच से गुजरेगी। इस में शुभ की भी संभावना है तो अशुभ की आशंका भी कम नहीं है। अभी तो राजनीतिक गुबार बन रहा है, न जाने राजनीति के किस तट पर यह जमीन से टकरायेगा।
किसानों के आंदोलन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग, छात्रों की पढ़ाई, रोजगार के लिए तरसती आबादी, बीमार की दवाई, बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, सामाजिक और आर्थिक अन्याय से पीड़ित लोगों, बदहाली में फंसी आर्थिक परिस्थितियों आदि का क्या होगा! संविधान और लोकतंत्र के प्रति कैसा राजनीतिक व्यवहार होगा यह तो बाद में पता चलेगा। हर हाल में अंततः ‘सब कुछ’ मतदाता समाज पर ही निर्भर करेगा। अभी तो शायद बहुत जल्दी उठनेवाले सियासी तूफान का थोड़ा-सा इंतजार।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)