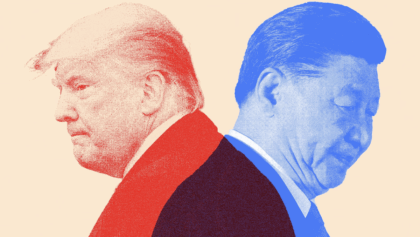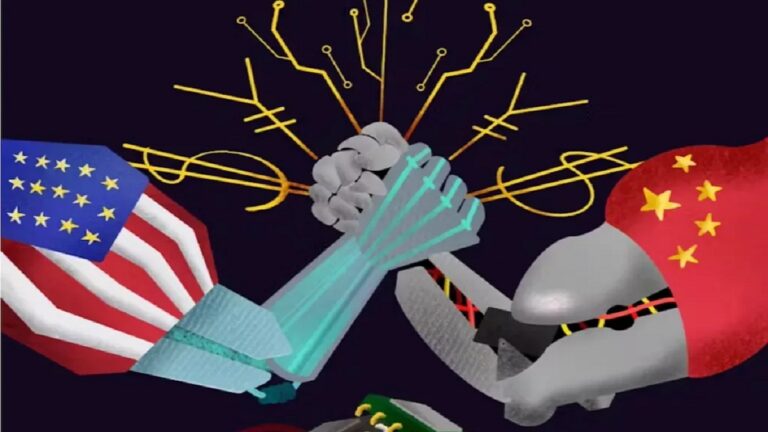जातिवार जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण और कुछ अनुदान-उपदान तक ही सीमित नहीं है। विषाक्त विषमता और घनघोर सामाजिक अन्याय, अ-सम्मान और जीवन के विभिन्न प्रसंगों तक जातिवार जनगणना का महत्व विस्तृत है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने जातिवार जनगणना की जायज दिख रही मांग को देश का प्रमुख और मुखर राजनीतिक एजेंडा बना दिया है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कई घटक दल तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले तक जातिवार जनगणना की मांग मुखरता से उठाते रहे हैं, हालांकि अभी लगभग खामोशी ओढ़े हुए हैं। जातिवार जनगणना के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीति और स्थिति शुरू से ही अलग-थलग रही है।
लंबे समय तक ‘सत्ता से अलगाव’ में रहे राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ जातिवार जनगणना के राजनीतिक प्रभाव को लेकर अब चिंतित है। इस चिंता पर विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श जारी रहा है।
अभी 31 अगस्त 2024 से राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की त्रि-दिवसीय सभा केरल के पालक्काड, में संपन्न हुआ है। इस आयोजन में 32 संगठनों के 230 प्रतिनिधि और लगभग सौ संघ पदाधिकारी की भागीदारी का इंतजाम था। राष्ट्रीय महत्व के विषय और सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा की महत्वाकांक्षाओं से यह आयोजन भरपूर था।
जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ जैसी अर्ध-गोपनीय संस्था अपनी सभा की कार्यवाही यथा-तथ्य सार्वजनिक कर दे, यह उम्मीद करना कुछ अधिक ही कहा जा सकता है। यह आयोजन विभिन्न संगठनों के अनुभव और व्यवहार में कार्यकारी समन्वय और कारगर ताल-मेल बैठाने के लिए समर्पित था।
असल में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ सत्ताधारी दल की प्रेरक और उनकी विचारधारा का नीति-निर्धारक अभिभावक है। बात सिर्फ राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के भारतीय जनता पार्टी का ‘प्रेरक और कठोर नीति-निर्धारक अभिभावक’ होने की नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी को मिले पूर्ण या खंडित जनादेश का सूत्र पकड़कर पिछले दरवाजे से भारत सरकार के ‘अभिभावक और नीति-निर्धारक’ हो जाने की भी है।
सत्ताधारी दल से जुड़े जन-प्रतिनिधियों की प्रेरणा के संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति अन्य संगठन की प्रेरणा और निर्धारण को ग्रहण करने में निश्चित ही नागरिक जमात जीवन के उपयुक्त भी कुछ होने के खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता है।
जाहिर है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के ऐसे आयोजनों के निष्कर्ष को पढ़ने-समझने में नागरिक समाज की स्वाभाविक दिलचस्पी है।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के लिए राष्ट्रीय महत्व का विषय क्या हो सकता है और साथ-साथ यह भी कि सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय क्या हो सकता है? कहने का तौर-तरीका सही नहीं हो तो बात का सही परिप्रेक्ष्य छिप जाता है।
मीडिया के एक अंश में खबर चल रही है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने देश भर में पूरे जोर-शोर उठ रही जातिवार जनगणना की जायज मांग का समर्थन किया है। समर्थन किया है या जातिवार जनगणना पर सहमति न प्रकट करने के चलते भारतीय जनता पार्टी के चुनावी परिणाम पर गलत असर से बचने के लिए इसके सामने झुकने का संकेत दिया है!
ऐसा समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी में जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर अपनी आपत्ति को स्थगित कर दिया है।
जातिवार जनगणना के आंकड़ों के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ चिंतित है। जातिवार जनगणना के आंकड़ों का कैसा राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है? शायद राजनीतिक इस्तेमाल से यहां आशय चुनावी राजनीति में वोट बटोरुआ रणनीति के रूप में इस्तेमाल से होगा।
पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में राजनीति का प्रसंग चुनावी जरूर होता है, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति भी सिर्फ चुनाव से सीमित नहीं होती है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का तो जो भी कदम उठता है, वोट बटोरने के लिए ही उठता है! ‘कल्याणकारी लोकतंत्र’ को पूरी तरह से ‘चुनावी लोकतंत्र’ में बदल देने का ‘गौरव’ भारतीय जनता पार्टी को ही हासिल है।
यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव में ‘धन’ और ‘धनवानों’ का भरपूर इस्तेमाल हो और ‘धन-हीनता’ एवं ‘धन-हीनों’ का इस्तेमाल बिल्कुल ही न हो! यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि चुनावी राजनीति में ‘धर्म’ का भरपूर इस्तेमाल हो, ‘धर्म-शास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर वर्णाश्रयी शोषण और वंचना की ‘संस्कृति’ के विरोध का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में बिल्कुल न हो!
सही है कि जातिवार जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, सही है। लेकिन, लोगों की ‘भलाई’ के लिए किस पर भरोसा किया जाये! क्या ‘स्थाई बहुमत’ के जुगाड़ के लक्ष्य साधने के लिए वोट बटोरुआ रणनीति लागू करते हुए देश के लोगों को ‘लड़ाने-भिड़ाने’ की जुगत में भिड़ी रहनेवाली जमात को लोगों की ‘भलाई’ का जिम्मा दिया जा सकता है?
जातिवार जनगणना के आंकड़ों के राजनीतिक इस्तेमाल से बचने के आग्रह में इसी जमात को भलाई का दायित्व इसी जमात को दिये जाने की अपील छिपी है।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के प्रचार प्रमुख, सुनील आंबेकर ने जातिगत जनगणना को देश की एकता-अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। कुछ देर के लिए याद कर लें, कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के पूर्व-प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘देश की एकता-अखंडता’ से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ‘पाप’ और देश की एकता-अखंडता के लिए खतरा बताया था।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ को देश चलाने का जनादेश प्राप्त नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को ही पूरा जनादेश प्राप्त है। जनादेश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को जरूर प्राप्त है। जातिवार जनगणना पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के रुख के बारे में देश को बताया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के ‘जन-नायक’ जातिवार जनगणना के मामला में फिलवक्त उतने मुखर नहीं हैं, कम-से-कम जितने मुखर होने की अपेक्षा उनसे रही है।
तर्क करनेवाले के तर्क होते हैं कि जाति की व्यवस्था समाज में श्रम विभाजन की तरकीब है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन के उपाय के रूप में नहीं, श्रमिक विभाजन के षड़यंत्र के रूप में पहचाना था।
जाति-वर्ण पर तर्क करनेवाले के तर्क को थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो भले ही पहले कभी काम के आधार पर जातियां बनी हों, बाद में जन्म से जाति का निर्धारण होने लगा। बाद की स्थिति में जाति काम के अनुसार निर्धारित नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत, जाति के आधार पर काम का निर्धारण होने लगता है।
इसलिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का यह कहना ठीक है कि जाति-वर्ण व्यवस्था श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन करती है। सवाल जाति-वर्ण व्यवस्था के पक्ष या विपक्ष में होने का नहीं है। जाति-वर्ण समाज का नक्शा नहीं स्वरूप है।
ऐसा स्वरूप जिसे सिर्फ दर्पण में ही देखा जा सकता है; कोई अपना चेहरा दर्पण में ही देख सकता है, वह भी पूरी तरह से कहां देखा जा सकता है! कई-कई दर्पण लगाकर भी नहीं दिखता है।
सामान्यतः दर्पण में किसी को अपना चेहरा बुरा नहीं दिखता है। बुरा दिखता तो लोग बार-बार दर्पण क्यों देखते! चेहरा जैसा भी हो, हर किसी किसी को अपने चेहरे से प्यार होता है। जाति-वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की कोशिशों का मतलब दर्पण को तोड़ने की कोशिश करना है। दर्पण टूटने पर भी रूप नहीं टूटता है।
जाहिर है कि कई लोग जो कोशिश करके अपने को जाति-वर्ण से मुक्त हो जाने की बात मानते हैं, वे कुछ और नहीं बस दर्पण की तरफ से मुंह मोड़ने की कवायद करते हैं या दर्पण को तोड़ने की कोशिश। कहने का आशय यह है कि सवाल जाति-वर्ण को तोड़ने की नहीं है।
बात जाति-वर्ण के आधार पर सदियों से किये जानेवाले भेद-भाव की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि की बिषमताकारी विषाक्त प्रथाओं से मुक्त होने की है। बात समताकारी ‘बहुजन-हिताय संवैधानिक प्रथाओं’ को अपनाने की निष्कलुष कोशिश को कामयाब करने की है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार के लिए इस ‘दर्पण’ का क्या उपयोग किया जा सकता है! जो भी उपाय किया जाये, इतना तो तय है कि न तो दर्पण से मुंह मोड़ा जा सकता है और न दर्पण को तोड़ा जा सकता है।
भारत की दक्षिण-पंथी विचारधारा यानी राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और हिंदुत्व की पारंपरिक राजनीति को बहुजन-हिताय संवैधानिक प्रथाओं को निष्कलुष मन से अपनाये जाने की राजनीति में दिक्कत है।
दक्षिण-पंथी विचारधारा बहुजन-हिताय के मसले को संवैधानिक अधिकार के माध्यम से नहीं, अपनी उदारता के ‘कृपा प्रसार’ के माध्यम से सुलझाना चाहती है।
जाति-वर्ण-लिंग के आधार पर बने वर्चस्वशाली समुदाय और आर्थिक आधार पर बने वर्चस्वशाली समूह के प्रति भेद-भावपूर्ण रवैये को ओझल करते हुए उनकी ‘कृपा के प्रसार’ के माध्यम से बहुजन-हिताय के मसले को सुलझाने के लिए ‘सोशल इंजीनियरिंग’ का राजनीतिक करतब करती रहती है।
कुल मिलाकर यह कि मामला ‘संवैधानिक अधिकार’ और ‘कृपा प्रसार’ के द्वंद्व-दोलन, अधिक सही शब्द है-ढुलमुलपन, पर आकर टिक जाता है। समझा जा सकता है कि कृपा प्राप्ति की कोशिश आदमी की हथेली को फैला देती है, गरदन को झुका देती है, माथे को ‘नत’ कर देती है।
अधिकार हासिल करने की तमन्ना फैली हुई हथेली को ‘मुट्ठी’ में बदल देती है, गरदन को सीधी और माथे को उन्नत बना देती है। अपने सामने फैली हुई हथेली और झुकी हुई गरदन देखकर दक्षिण-पंथ का चित्त प्रसन्न हो जाता है; वह फैली हुई हथेली पर ‘एक पैसा रखकर दस लाख’ बटोर लेने की तमन्ना से प्रेरित होता है।
नहीं-नहीं, कोई आरोप नहीं! छोटी, बहुत छोटी जिज्ञासा! बस इतनी कि ‘पचकेजिया मोटरी’ और ‘लाखों करोड़ की हेरा-फेरी’ में क्या दिखता है; इनके बीच के संबंध में कुछ दिखता है! कुछ दिखता भी है! कुछ भी नहीं दिखता है?
जब विचारधारा की राजनीति की बात करना जरूरी हो जाये तो विचारधारा की मानसिकता की बात करना बहुत जरूरी है। ‘तत्वमसि’ और ‘सोअहं’ कहता हुआ द्विज अपने को ‘ब्रह्म’ बताता है। उलटा ही सही, जप करनेवाले गैर-द्विज को ‘ब्रह्म’ तो नहीं, लेकिन हां, ‘ब्रह्म के समान’ मान लेता है।
किसी के ‘ब्रह्म’ या ‘ब्रह्म समान’ होने तक को भी दक्षिण-विचार मान लेता है। हजारों साल पहले कभी-कभार किसी गैर-ब्राह्मण के ‘ब्राह्मण’ हो जाने का कोई उदाहरण मिले तो मिले, लेकिन अब कोई लाख कोशिश कर ले समाज में वह ‘ब्राह्मण’ नहीं हो सकता है।
‘ब्राह्मण’ नहीं हो सकता का मतलब है, वर्तमान देह के साथ जन्म-जात वर्ण को बदल नहीं सकता है। हां हिंदुत्व की राजनीति को हिंदू धर्मावलंबियों से इतनी आंतरिक अपेक्षा जरूर होती है कि अंतर्ग्रस्त वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत अपरिवर्तनीय वर्ण के अनुसार अगले जन्म में अच्छे फल पाने के लिए स्थाई रूप से निर्धारित ‘कर्म’, अर्थात निश्चित सेवा-कार्य करे।
इस जन्म में जीवनयापन के लिए वर्णानुमोदित ‘काम’ यानी रोजगार करे। सेवा-कार्य यानी मजदूरी के बिना बेगार और काम यानी मजदूरी के साथ रोजगार, दोनों वर्ण के अनुसार।
वर्ण-व्यवस्था में इतनी कड़ाई का कारण यह है कि ब्रह्म-विचार गैर-भौतिक और ‘आध्यात्मिक’ प्रसंग है, जब कि हिंदू वर्ण-व्यवस्था भौतिक और सामाजिक प्रसंग है। जीवन के गैर-भौतिक प्रसंग में भले ही समानता का भ्रम पैदा करना संभव हो जाता हो, लेकिन पूजा और पाखंड में इतना नजदीकी रिश्ता कायम हो गया है कि आंख खुलते ही ‘भ्रम की टांटी’ उड़नछू हो जाती है।
जीवन के भौतिक प्रसंग को ‘पूजा पाखंड’ के आडंबर ने सदियों से आच्छादित कर रखा है। मध्य-काल में विकसित संत-साहित्य इस ‘पूजा पाखंड’ के आडंबर के खिलाफ सांस्कृतिक विद्रोह था। ‘आश्रम’ का ‘उच्च-विचार’ केवल उच्च-वर्ण के पुरुषों के लिए प्रयोजनीय है! वर्ण-व्यवस्था की रात-दिन चर्चा और ‘आश्रम’ कोई फुसफुसाहट भी नहीं! कमाल है!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की मान्यता थी कि ‘हिंदू समाज’ का कोई अस्तित्व नहीं है। हिंदू जातियों का एक समुच्चय मात्र है। अनुभव बताता है कि जाति का एहसास हिंदू जीवन में हमेशा जाग्रत और उग्र बना रहता है लेकिन एक धर्म से संबंधित होने का अच्छा एहसास या तो होता ही नहीं, जीवन के किसी अच्छे अवसर पर ‘एक धर्म’ से संबंधित होने का अच्छा एहसास बहुत कम होता है।
हां, हिंदू-मुसलमान संघर्ष के समय विभिन्न जातियों के व्यक्ति के मन में अपने हिंदू होने का एहसास जरूर जगता है। समझा जा सकता है कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए हिंदू-मुसलमान के नाम पर ‘चौबीसों घंटे’ उपद्रवी मुद्रा में रहना क्यों जरूरी होता है।
साफ-साफ समझा जो सकता है कि चूंकि हिंदू-मुसलमान के नाम पर ‘चौबीसों घंटे’ की उपद्रवी मुद्रा हिंदू के मन में जाति से जुड़ाव को कमजोर कर देती है, भुला देती है और ‘हिंदुत्व की राजनीतिक छतरी’ के नीचे डरे-डराये हिंदुओं को बटोर लेती है।
भयानक है कि ‘हिंदू एकता’ के लिए हिंदू-मुसलमान के मामलों को ‘ज्वलंत’ बनाये रखना जरूरी होता है। क्या गजब की स्थिति है! हिंदू एकता और हिंदुत्व की राजनीति की गतानुगतिकता (Sequential) के लिए मुसलमानों के प्रति उग्रता राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की एक ‘मजबूरी’ है! जितनी स्थाई यह उग्रता होगी उतनी ही स्थाई हिंदू एकता होगी।
‘स्थाई हिंदू एकता’ क्यों चाहिए? न्याय, लोकतंत्र और संविधान की ताकत की ‘अनदेखी’ करते हुए दिल-दिमाग की ताकत से बुलडोजर चलाने के लिए! समानता के भरोसेमंद आश्वासन के बिना ‘हिंदू एकता’ का उद्देश्य क्या हो सकता है।
एकता! ‘स्थाई बहुमत’ के जुगाड़ के लिए एकता! जाहिर है कि ‘स्थाई हिंदू-मुसलमान एकता’ और भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति की ताकत को हिंदुत्व की राजनीति गंभीर चुनौती के रूप में देखती है।
इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति के तहत हिंदुओं के मन में खुद के गढ़े ‘काल्पनिक डराव’ के धागों से बनाये गये रंग-बिरंगे भ्रम-जाल को फैलाने में लगी रहती है। जहां भी इन्हें ‘हिंदू-मुसलमान एका’ की गुंजाइश की कोई ‘आशंका’ झलकती है इनके कान खड़े और हाथ-पैर सक्रिय हो जाते हैं।
हिंदू-मुसलमान एकता की ताकत 1857 के समर में प्रकट हुई थी। इस ताकत को पूरी दुनिया ने देखा था, उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने देखा था और हुकूमत की कतार में खड़ी रहनेवाली सत्ता जमात ने भी देखा।
भारत में, पूंजीवाद की बिषमताकारी आर्थिक नीतियों और ब्राह्मणवाद की बिषमताकारी वर्णवादी नीतियों के वर्चस्व के लिए हिंदू-मुसलमान एकता चुनौती बन सकती है। जाहिर है कि कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद में एक तरह की समझदारी विकसित होती गई है।
लोकतंत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को देश का दुश्मन माना था और साथ-साथ सावधान भी किया था। कि ब्राह्मणवाद से उनका आशय ब्राह्मण जाति के लोगों से नहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समर्थित करनेवाली वर्णवादी ताकतों से था।
आज भारत के लोकतंत्र को बचाने में लगे राजनीतिक नेताओं और गैर-राजनीतिक नागरिक समाज के लोगों के सामने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों की अतियों से उत्पन्न उग्रता से जोरदार संघर्ष की चुनौती है और वह भी संतुलित पूंजीपतियों और वर्णवाद विरोधी तथाकथित ‘उच्च-वर्ण’ को साथ लेकर जोरदार संघर्ष की चुनौती है।
इस आधुनिक और उत्तर-आधुनिक काल में हिंदू-मुसलमान एकता पर विचार करना है तो निश्चित ही मध्य-काल के दौर के संत-साहित्य और भक्ति-साहित्य के सामाजिक संदर्भ और उनके अंतर्विरोध को समझना प्रासंगिक है। इसी क्रम में ब्रिटिश हुकूमत के जमने और उखड़ने और अंग्रेजी साहित्य की भूमिका पर भी गौर किया जाना आवश्यक होगा।
इतना संकेत काफी है, यहां बहुत फैलना यहां संभव नहीं है। मूल बात यह है कि भक्ति और धर्म के संबंध और भक्त और संत में अंतर पर बात करने से कुछ बातें साफ हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि भक्ति धर्म का विस्तार नहीं विकल्प है; भक्ति और धर्म में समानता है तो अंतर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात यह कि भक्त और संत में काफी समानता है तो अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हिंदुत्व की विचारधारा में सभी मनुष्य के समान मानने के सनातन सिद्धांत और व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है। बल्कि वर्ण-आधारित असमानता का जड़ आग्रह है। जाहिर है कि हिंदुत्व की राजनीति में ‘सब’ के लिए ‘समान और सामान्य’ का आश्वासन भ्रामक वाग्मिता के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, जैसे ‘सब का साथ, सब का विकास आदि’।
सभी नागरिकों के प्रति समान और सामान्य व्यवहार का सच्चा आश्वासन देने की हिंदुत्व की वैचारिक और व्यावहारिक अपंगता प्रथमतः लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतंत्र के ही विरुद्ध कर देती है और अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतंत्र का शत्रु बना देती है।
सभी नागरिकों के प्रति समान और सामान्य व्यवहार का आश्वासन लोकतंत्र का प्राण होता है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सभी नागरिकों के प्रति समान और सामान्य व्यवहार के आश्वासन के अभाव में भी लोकतंत्र के सुरक्षित रहने का भ्रम बनाने में मीडिया रात-दिन लगा रहता है; ‘उदार बुद्धिजीवी’ भी लगातार तर्क गढ़ते रहते हैं।
एकता और समानता में अंतर होता है। समानता के आश्वासन के अभाव में एकीकरण की सभी प्रक्रियाएं एकत्रीकरण की प्रक्रिया बनकर रह जाती है। असल में हिंदुत्व की राजनीति ‘हिंदू एकता’ की चिंता नहीं करती है, ‘स्थाई बहुमत’ के जुगाड़ के लिए ‘हिंदू एकत्रीकरण’ के राजनीतिक एजेंडा को लागू करने की कोशिश में लगी रहती है।
जातिवार जनगणना के बारे में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो भी राय हो देश की एकता-अखंडता और देश के लोगों की वास्तविक और संतुलित समृद्धि के लिए जातिवार जनगणना के दर्पण में भारत के लोकतंत्र का चेहरा, देखने का साहस से काम लेना जरूरी है।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)