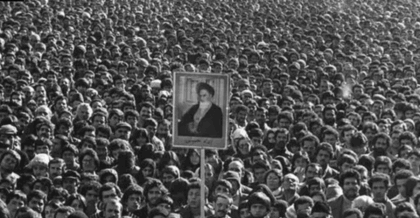आम चुनाव 2024 का सातवां और आखिरी चरण 1 जून को पूरा हो जायेगा।18वीं लोकसभा के गठन के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। जहां पर हितधारकों के एकत्र होने से निर्भय एवं शांतिमय माहौल में सभी के सहयोग, संवाद और सहमेल से जहां समस्या के समाधान की रोशनी, यानी आभा निकलती है उसे ही सभा कहते हैं। समाधानकारी आभा के निकलने देने में जो निष्क्रिय और सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं उन्हें सभ्य कहा जाता है। लोकसभा की कार्रवाई का सभ्यता-सूचकांक बने-मिले तो हमारी लोकतांत्रिक गुणवत्ता का अनुमान कुछ अधिक स्पष्ट और रेखांकनीय हो सकता है। विडंबना है कि हमारी व्यवस्था में ‘सभ्य’ नागरिक ‘स-भय’ अवस्था में जीवनयापन के लिए मजबूर हैं।
मतदान के माध्यम से नागरिक भारत के लोकतंत्र में अपनी क्या भूमिका अदा करता है इस पर गौर करना अ-प्रासंगिक नहीं होगा। मतदान की प्रक्रिया के निहितार्थ को समझना चाहिए। असल में, कई देशों की राज्य व्यवस्था में ईश्वर को ‘संप्रभु’ को माना गया है तो कहीं सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट को, कहीं संसद को ‘संप्रभु’ माना गया। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागरिक ‘संप्रभु’ होता है। चुनाव में मतदान के माध्यम से नागरिक अपने-अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी ‘संप्रभुता’ सौंपता है।जनप्रतिनिधि अपने नेता, अर्थात प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संविधान और राष्ट्र को सौंप देता है। इस तरह से ‘संप्रभुता चक्र’ पूरा होता है।
नागरिक अपने-अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी ‘संप्रभुता’ सौंपते हुए जनप्रतिनिधियों को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला भाईचारा विकसित करने का संवैधानिक दायित्व भी सौंपता है। संवैधानिक संस्थाओं को जनप्रतिनिधियों को मिले दायित्व को निभाना पड़ता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाये रखना जितना महत्वपूर्ण है, उस से कम महत्वपूर्ण नहीं है नागरिकों के बीच भाईचारा का बने रहना और बनाये रखना। ध्यान में रखना चाहिए कि ‘भाईचारा’ लिंग-निरपेक्ष पदबंध है, इस पदबंध में ‘बहनापा’ और बंधुत्व शामिल रहता है।
हिंदी के बड़े कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। सांसद भी रहे हैं। उनके नाम के आगे पहले लगता था, ‘राष्ट्र कवि’। हिंदी के एक ऐसे ही बड़े कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त। उनके नाम के पहले भी लगता था, ‘राष्ट्र कवि’। अब लगभग यह बंद हो गया है। हालांकि दिनकर ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर के लिए ‘राष्ट्र कवि’ का विशेषण उपयुक्त बताया था। लेकिन रवीन्द्रनाथ ठाकुर को ‘राष्ट्र कवि’ नहीं कहा गया। उनके नाम के पहले ‘विश्व कवि’ और ‘कवि गुरु’ लगता है।
किसी व्यक्ति के नाम के साथ ‘राष्ट्र’ और ‘विश्व’ के जुड़ने का रहस्य बड़ा विचित्र है। विचित्र ही नहीं आकर्षक भी बहुत है। अमर राष्ट्र नायक नेता जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा तो भारत के अधिकतर लोगों ने निःसंकोच भाव से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया। हमारे पास ‘राष्ट्र-गुरु’ का पद अभी भी रिक्त है! यह रिक्ति भरी जा सकती है, लेकिन अभी तो ‘विश्व-गुरु’ कहलाने का चलन हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व-गुरु कहते हुए अपने विश्व-गुरु होने के लक्ष्य को सामने रखकर काम कर रहे हैं। यह सब भावनाओं की बात है। इन बातों को भावुक सांद्रता से महसूस करनेवाले के प्रति अ-सम्मान की कोई बात नहीं है। बस इसे बुद्धिमत्ता से समझने की कोशिश करना बेकार है।
इन दिनों भारत की मुश्किलें यह है कि किसी एक क्षेत्र में दिखने लायक जगह बना चुके लोग बहुत आसानी से दूसरे क्षेत्र में भी जगह दखल करने की मानसिकता और ललक से भरे हुए प्रतीत होते हैं। इस ललक की चपेट में सबसे अधिक राजनीति में सक्रिय लोग पड़ गये हैं। राजनीतिक नेता के रूप में जगह बनानेवाले कभी धार्मिक बाना धरकर सामने आ जाते हैं, तो धार्मिक बाना के साथ जगह बनानेवाले राजनीतिक नेता के रूप में प्रकट हो जाते हैं।
कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नॉन-बायोलॉजिकल बताते हैं तो कभी महामहिम राष्ट्रपति बताती हैं, ‘आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही वास्तविक सशक्तिकरण है।’ 27 मई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित ‘स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण’ पर बोलते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही वास्तविक सशक्तिकरण होता है। ऐसा लगता है कि सभी तरह के शोषण अन्याय आदि का निदान इस ‘आध्यात्मिक सशक्तिकरण’ से ही संभव है! शोषण अन्याय आदि के निदान में सरकार, राज्य व्यवस्था, संविधान, कोट-कचहरी, लोकतंत्र आदि की भूमिका से अधिक बड़ी भूमिका ‘आध्यात्मिक सशक्तिकरण’ में लगी संस्थाओं की है? अजब कहें! गजब कहें! क्या कहें! ‘आध्यात्मिक सशक्तिकरण’ की बात धर्म-गुरु करें तो करें! इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोगों के लिए ‘आध्यात्मिक सशक्तिकरण’ महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन से सबके लिए मनुष्य ने अन्य माध्यम खोजे हैं जिन माध्यमों में राज्य व्यवस्था शामिल नहीं है।
भारत का संविधान तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए; उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण की बात का उल्लेख करता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ये बस संविधान की शोभा बढ़ाने के लिए हैं, अनुपालन की कोई अनिवार्यता नहीं है, किसी के लिए नहीं!
भूखी-नंगी बायोलॉजिकल, कुपोषित, रोजगारहीन जनता किसके पास जा कर फरियाद करे! वास्तविक सशक्तिकरण के लिए किसका, किस-किस का, किस ‘लोकल न्याय पुरुष’ शरण गहे! राज-सत्ता और जनप्रतिनिधियों से कुछ भी उम्मीद और अपेक्षा रखे या न रखे! भारत में संविधान शासित राज-सत्ता है या धर्म-शास्त्र अनुमोदित जीवन व्यवस्था है? क्या भारत एक द्वि-स्तरीय, बहु-स्तरीय राष्ट्र है? लगभग दस प्रतिशत के लिए संविधान है और बाकी के लिए धर्म-शास्त्र है! एक नागरिक के रूप में बहुत ही सम्मान के साथ जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी हैसियत क्या है? चुने हुए और संवैधानिक पद पर बैठे अपने ‘भाग्य विधाताओं’ से हमारा संबंध क्या है? क्या वे हमारे धर्म-गुरु हैं और हम उनके पटु शिष्य हैं? बहुत ही भयावह है आज के समय में इन प्रश्नों से जूझना! इस प्रवृत्ति का दुखद पहलू यह है कि जिन मामलों में उन्हें बोलना चाहिए, उन मामलों में वे शायद ही कभी मुंह खोलते हैं।
क्या जलते हुए मणिपुर के लोगों से, ऑलंपिक विजेता बेटियों से, किन-किन से कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नॉन-बायोलॉजिकल हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने ‘आध्यात्मिक सशक्तिकरण’ के लिए कहा है! अब कोई संवैधानिक-सशक्तिकरण की बात भी न सोचे! किन-किन से कहें? मुख्य चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि नॉन-बायोलॉजिकल लोग चुनाव में उम्मीदवार बनने और मतदान करने के पात्र होते हैं या नहीं होते हैं? लेकिन नहीं कोई नहीं मुंह खोलेगा! यदि यह भ्रामक घोषणा है तो चुनाव के दौरान भ्रामक घोषणा करनेवाले उम्मीदवारों के प्रति भारत का कानून क्या कहता है! शायद कुछ नहीं कहता है, कुछ कहता होता तो कोई-न-कोई तो सवाल उठाता! कोई-न-कोई कुछ-न-कुछ जरूर कहता!
सरकारी योजनाओं के तहत राशन देना क्या प्रधानमंत्री की तरफ से उनका निजी दान होता है? जिस दान से उन्हें पुण्य होता है। इस दान के बदले में वोट के रूप में प्रतिदान से वोटरों को पुण्य मिलता है? क्या राशन लेना नागरिकों को किसी भी अर्थ में ऋणी बनता है? बदले में वोट देकर नागरिक उऋण या ऋण-मुक्त होता है? क्या पता! क्या-क्या बातें करते रहते हैं हमारे नेतागण, साधारण नेता नहीं, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नेता! हम क्या पेट डेंगाते चांद-सितारों की सैर पर निकलनेवाले हैं!
कपोल-कल्पित बातों के माध्यम से जन-हित के मुद्दों को बहुत दिन तक भटकाना संभव नहीं होता है। पेट की आग में जलन चाहे जितनी भी होती हो, थोड़ी-बहुत रोशनी भी इस आग में जरूर होती है। वैसे तो चौबीस-घंटा-सातो दिन महिमा-मंडन यज्ञ चलता रहता है, इस बार के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के महिमा-मंडन की कोई कम कोशिश नहीं हुई है। यह कोशिश निष्फल हो गई। निष्फल होने का बड़ा कारण! कारण यह बना कि नरेंद्र मोदी के महिमा-मंडन के लिए राहुल गांधी के गरिमा-खंडन का सहारा लिया गया। महिमा-मंडन में दत्त-चित्त पुरोधाओं और मीडिया-साधकों ने अपनी संपूर्ण प्रज्ञा का इस्तेमाल किया, लेकिन समझकर भी नहीं समझ पाये कि जिस राहुल गांधी और उनकी जिस छवि का गरिमा-खंडन वे कर रहे हैं वह तो बस आभासी है, “नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः” की स्थिति में पहुंच चुका है।
‘भारत जोड़ो यात्रा’ के आरंभ में ही ये राहुल गांधी उस राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ आये थे। इस रहस्य को राहुल गांधी के बताने के बावजूद महिमा-मंडन में दत्त-चित्त पुरोधाओं और मीडिया-साधकों से समझने में भारी चूक हो गई। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के माध्यम से राहुल गांधी की छवि जिस तरह से ‘न्याय योद्धा’ की बनी उस पर तो महिमा-मंडनकारियों की आंख टिक भी नहीं पाई! गजब मामला! पुतली तेजी से नाचती रही, लेकिन नजर कहीं टिक नहीं पाई! राहुल गांधी की विश्वसनीयता उनकी पहले कही बातों से भी अब पुष्ट होती चली गई, चाहे वे बातें कोरोना महामारी से संबंधित हो या बे-रोजगारी, अग्निवीर योजना, महंगाई, इलेक्टोरल बांड, भ्रष्टाचार, अन्याय के विभिन्न संदर्भों आदि से ही क्यों न जुड़ी हों।
कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र जिसे ‘न्यायपत्र’ का नाम दिया गया उसमें रखे गये मुद्दे इतने साफ-साफ भाषा में इतने जीवंत, ज्वलंत और जनपक्षधर हैं कि सत्ताधारी जमात के पास कहने के लिए कुछ भी सार्थक और सटीक नहीं हाथ लगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें मुस्लिम लीग की छाप के होने की बात शुरू कर दी। भयावह विषमता को दूर करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए जाति-सर्वेक्षण की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर के दीवारों के एक्सरे करने, दो हो तो एक भैंस चुरा लेने, मछली-मटन, मुजरा, कहां-कहां न चले गये! क्या-क्या न कहते चले गये, न सिर, न पैर! उमड़-घुमड़कर भांति-भांति से ‘कपालभाति’ किया लेकिन न्यायपत्र के मुद्दों के विरोध में कुछ भी सार्थक नहीं कह पाये। कांग्रेस के न्यायपत्र ने कल के ‘श्रेष्ठ प्रचारक’ और आज के ‘स्टार प्रचारक’ के प्रचार की रेल-पेल को बेपटरी कर दिया! फिर कहां तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सिग्नल और कहां के सिग्नल-पोस्ट! सब बेकार। कोई भी चुनाव प्रचार की दशा-दिशा ठीक कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुआ।
आज कही बात का कल खंडन करने लगे। चयनित पत्रकारों से बार-बार इच्छा-वार्ता करना शुरू कर दिया। बौखलाहट इतनी कि दूसरों के मुंह में अपनी बात रखकर उसकी खिल्ली उड़ाने में सक्षम नरेंद्र मोदी ने तो एक पत्रकार को यह तक कह दिया कि आप अपनी बात मेरे मुंह में न डालें! राम मंदिर का हो या सनातन का हो ‘श्रेष्ठ प्रचारक’ और ‘स्टार प्रचारक’ का पूर्व-नियोजित मुद्दा चुनाव प्रचार में कुछ दूर भी नहीं चला। कहावत है कि ‘खिसियानी बिल्ली, खंभा नोचे’। नरेंद्र मोदी ने तो अपने दस साल के शासन-काल में एकोअहं में बाधक बनने की थोड़ी-सी भी संभावना रखनेवाले अपने सारे खंभों को पहले ही खुद उखाड़ फेंक दिया है। इस तरह नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के परिसर में ‘हम में, तुम में, इस में, उस में, खड़े खंभ में’ के राजनीतिक साहस के साथ भगवत भाव-भंगिमा और भाव-मुद्रा के माध्यम से ‘आध्यात्मिक सशक्तिकरण’ को हासिल कर चुके हैं।
बार-बार अपने ही वाग्जाल में फंसने से कितनी बौखलाहट होती है, यह भी कोई कहने की बात है भला! बौखलाहट से बाहर निकलने के लिए, जाहिर है आस-पास भारतीय जनता पार्टी का कोई ‘खंभा’ नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने बिहार के बक्सर की चुनाव सभा में चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को जेल भेजे जाने की बात कह दी। इस बात को जनता ने अच्छे अर्थ में नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने पलटकर सवाल कर दिया कि कौन जेल जायेगा या नहीं जायेगा इसका फैसला संवैधानिक संस्थाएं और अदालतें नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यही तो विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) कहता रहा है कि अरविंद केजरीवाल हों, हेमंत सोरेन हों या कोई अन्य विपक्षी नेता हों उनके मामले में फैसला संबंधित संस्थाएं नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यही तो संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग होता है। सत्ता के इसी दुरुपयोग की बात तो विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) के सारे नेता कहते रहे हैं। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से जेल भेजने की बात करना बिल्कुल गलत है। हालांकि व्यवहार में सब कुछ नहीं भी तो बहुत कुछ ‘नेता जी’ के इशारे पर या लोकल ‘न्याय पुरुष’ के कहने पर ही होता है। क्या इस बात में किसी को कोई संदेह है? शायद नहीं है।
कुल मिलाकर समाज है या राज हो, चलता जोरावरों के जोर से ही है। लोकतंत्र में शक्ति से अधिक वरीयता विवेक को मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इस समय तो विवेक ही विक्षिप्त हो गया है। विवेकाधिकार (Discretionary) के इस्तेमाल के सलीका (Pattern) के विश्लेषण से बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है। विवेकाधिकार का मिली-भगत (Quid Pro Quo) का औजार बन जाना कितना भयानक नागरिक प्रदूषण फैलाता है, कहने की जरूरत नहीं है।
राजनीतिक औद्धत्य की लहरें अकसर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादा को खंडित करती रहती है। कहीं कोई राजनीतिक सिहरन नहीं होती है। कमाल तो यह है कि क्षुद्रता के पास भद्रता का सबसे चमकीला पोशाक होता है। सत्य विलोपन के लिए क्षुद्रता के हाथ चमत्कारी छड़ी होती है। पैसा और पहुंच का लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत बन जाना आम आदमी की जिंदा रहने की शर्त को कठिन बना देता है। वर्चस्वशाली लोगों, न्याय पुरुषों से से मिलते-जुलते रहने से ही जीवनयापन का संभव रह जाना या ‘जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जायेंगे’ की समर्पणकारी मानसिकता का जीवन-मंत्र बन जाना लोकतंत्र में सबसे बड़ी नागरिक दुर्घटना होती है। ऐसे में सभ्य और बेहतर नागरिक जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है। राज-सत्ता की व्यवस्था की सारी कोशिश सत्ता रक्षण की चिंता से नियंत्रित होती है, किसी भी स्तर पर जीवन रक्षा के दायित्व से प्रेरित नहीं होती है।
इस भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है कि यह स्थिति कोई एक-दो-दिन में नहीं पैदा हुई है। न एक-दो-दिन में स्थिति सुधरनेवाली है। पहले तो इस स्थिति को बदतर होने से रोकने का कारगर इंतजाम करने की जरूरत है। यह कैसे होगा! लोकतंत्र में स्थिति परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की कुंजी लोक-उद्यम में होती है, आम मतदाताओं के पास होती है। चुनाव परिमाण आने और जनादेश के सम्मान तक लोक-उद्यम और लोक-विवेक को अधिकतम उत्कृष्ट मुद्रा में सावधान रहना होगा। जी, चुनाव परिमाण और जनादेश के सम्मान तक उत्कृष्ट मुद्रा में सावधान रहना होगा।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)