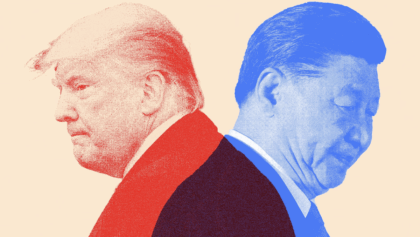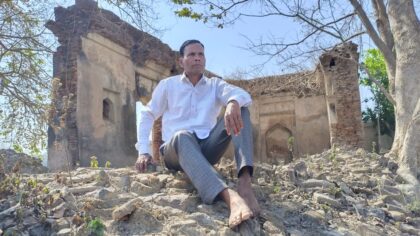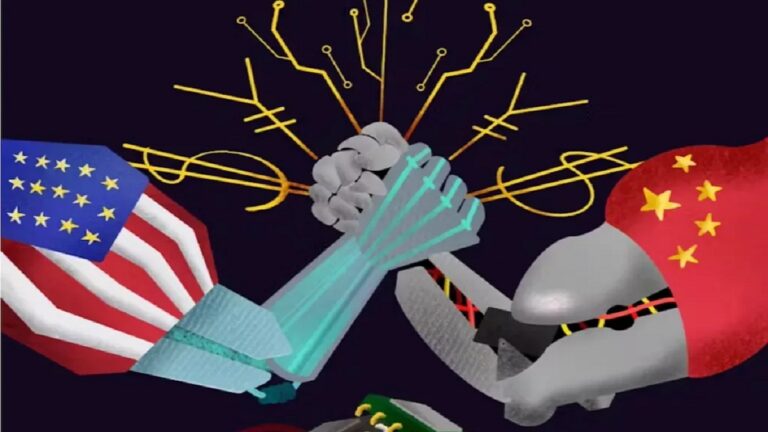आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। आज महिला दिवस की प्रेरणा और परिस्थिति को याद करने का दिन है। सभ्यता के परिप्रेक्ष्य को सही करने के लिए प्रयासों को दुहराते रहने के संकल्पों का दिन है। यों ही नहीं आया आज का दिन। मां की कोख से जैसे आता है शिशु वैसे ही आया यह दिन। ‘तुतलाती आवाजों’ को ‘स्पष्ट वाणी’ में बदलने वाली ताकत के आंतरिक मर्म और पीड़ा को सहकार, सहानुभूति, सम्मान और समर्पण से समझने का दिन है। ‘रोटी और शांति’ के लिए अपनी-अपनी पहली दूधिया मुसकान की प्रतिज्ञाओं को याद करने का दिन है। यह रिवाज नहीं, आवाज है। इतिहास की गहरी घाटियों से आती हुई आवाजें और उसकी अनुगूंजों को ध्यान से सुनने का दिन है।
8 मार्च दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लारा जेटकिन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव दिया था। उनके बारे में लेनिन ने एक बार टिप्पणी की थी-जर्मन कम्युनिस्टों के पास केवल एक अच्छा आदमी था-और वह एक महिला थी: क्लारा जेटकिन। किसी खास तारीख को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाये जाने के बारे में क्लारा के प्रस्ताव में उल्लेख नहीं था।
असल में, रूस में प्रचलित जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी 1917 को रूस की महिलाओं ने ‘रोटी और शांति’ की मांग के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। जूलियन कैलेंडर की 23 फरवरी 1917 पूरी दुनिया में प्रचलित मानक ग्रेगॉरियन कैलेंडर के हिसाब से 08 मार्च ठहरता था। उस आंदोलन के महत्व को ध्यान में रखकर 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उस आंदोलन के कारण तत्कालीन सत्ताधारी रूसी जार सत्ता से बेदखल हुआ। उसके बाद गठित अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया। इस तरह ‘रोटी और शांति’ के आंदोलन ने सरकार और सत्ता की संरचना को बदल देने को साथ ही महिलाओं का मताधिकार हासिल कर लिया।
भारत में महिला अधिकारों के लिए सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। महा आख्यानों के कथानकों और भारत की संस्कृति में जीवित पौराणिक मिथकथाओं की बात अपनी जगह है ही। इतिहास की बात करें तो भारत के राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन को याद करना चाहिए। सावित्री बाई फुले, ताराबाई शिंदे, रामाबाई को याद करना चाहिए। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन (डब्ल्यू.आई.ए.), अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (ए.आई.डब्ल्यू.सी.), अखिल भारतीय स्त्री परिषद (एन.सी.डब्ल्यू.आई.) को याद करना चाहिए। जिनके नाम का उल्लेख न हो सका उनसे माफी मांगते हुए याद किया जा सकता है: महिलाओं के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 15 दिसंबर 1917 को मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड से भेंट करके उन्हीं शर्तों के आधार पर मताधिकार की मांग की, जो शर्तें पुरुषों के लिए निर्धारित थीं। 1917 में कोलकाता (कलकत्ता) में एनी बेसेंट में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनके अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस में इस विश्वास व मत की पुष्टि हुई कि शिक्षा के संबंध में महिलाओं और पुरुषों पर एक समान ही नियम लागू होंगे।
वीमेंस इंडिया एसोसिएशन महिला श्रमिकों की मांगों को उठाने वाला पहला महिला संगठन था। मातृत्व अवकाश की मांग पहली बार 1921 की जमशेदपुर हड़ताल में सामने आई थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। 1931 में, बंगाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सरला देवी चौधरानी ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को स्थान देने में पुरुषों की भूमिका की सराहना की। उन्हें आशंका भी थी, और सही आशंका थी कि क्या पुरुष सचमुच महिलाओं की स्थिति में सुधार के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि कांग्रेस ने केवल महिलाओं को ‘कानून-तोड़ने वालों की स्थिति दी है, न कि कानून निर्माताओं की स्थिति’। यह 1931 की बात है, 2024 की स्थिति तो सामने ही है!
संक्षेप में यह कि आत्म निर्णय का अधिकार हो, चुनावों में मत दान का अधिकार हो, या स्त्री-पुरुष समानता का अधिकार हो इसके लिए स्वतंत्रता आंदोलन में महिला नेतृत्व ने स्थान बनाया। महिला नेतृत्व में इस बात की भी गहरी समझ थी कि उनकी मांग के पीछे पुरुष वर्चस्व का मुकाबला करने या स्त्री वर्चस्व कायम करने की प्रवृत्ति नहीं है, पीढ़ियों के पोषण की जिम्मेवारी और जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा है। इतिहास में महिलाओं की भूमिका के उल्लेख और मूल्यांकन का समुचित स्थान नहीं रहा है। इसलिए, बहुत पीड़ा के साथ इतिहास को ‘उनकी कथा’ (History : His Story) भी कहा और समझा जाता है।
सत्ता में हिस्सेदारी का जो सवाल 1931 में सरला देवी चौधरानी ने उठाया था वह आज भी महत्वपूर्ण है। सत्ता की प्रवृत्ति है, जनता को ‘कानून तोड़नेवालों’ के की स्थिति में रखकर खुद ‘कानून निर्माताओं’ विशेषाधिकार संपन्न स्थिति में बने रहो। सामने है कि किस तरह किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों को ‘कानून तोड़नेवालों’ की जमात बताकर स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक सरकार की तरफ से ‘प्रशासनिक कार्रवाई’ की गई।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है। न सिर्फ उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, बल्कि पीड़ित महिलाओं को न्याय देने-दिलाने के मामले में आपराधिक उदासीनता की प्रवृत्ति में इजाफा हो रहा है। न्याय देने-दिलाने में उदासीनता अपराध में वृद्धि को तो तीव्र करती है रोक-थाम की निवारकता को भी शिथिल कर देती है। घटनाओं की बहुलता के कारण हाथरस, मणिपुर आदि कुछ उदाहरणों का उल्लेख बेमानी हो जाता है। सार्वजनिक अवसरों और स्थानों पर छेड़छाड़, अभद्र इशारेबाजी और महिलाओं के आस-पास बढ़ती हुई भिनभिनाहटों की भयावहता अकथ्य है। यह सब अन्य अपराध और सामान्य कानून व्यवस्था के अलावा है।
यह सच है कि किसी अपराध को जड़ से खत्म करना मुश्किल काम है, लेकिन न्याय देने-दिलाने में तत्परता और रोक-थाम की निवारकता को चुस्त-दुरुस्त बनाकर अपराध पर सरकार निश्चित ही रोक लगा सकती है। सरकार अगर यह भी और इतना भी नहीं कर सकती है तो और क्या कर सकती है? यह सीधा और किसी तरह से इसे कोई सरकार टरका नहीं सकती है और न टालमटोल कर सकती है।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उत्तरोत्तर वृद्धि सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकने की कोशिश करने के बजाये सरकारों और राजनीतिक दलों की दिलचस्पी, विभिन्न तरीकों की लाभार्थी कुचेष्टाओं से वोट के लिए महिलाओं को बहलाने, फुसलाने, रिझाने, लुभाने का कपट जाल फैलाने में अधिक दिखती है। चुनावी प्रचार की शब्दावली, मुहावरों, जनविद्वेषी बयानबाजियों (Hate Speeches) ‘मर्दानगियों’ और ‘मर्दवादी रुझानों’ की भरमार का दुष्प्रभाव इतना भयानक होता है कि कभी-कभी महिला लोग भी आक्रोश में आकर विरोधी पुरुष नेताओं को चूड़ियों का उपहार भेजने की बात करने लगती हैं।
इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 96.8 करोड़ से अधिक नागरिक मतदान करेंगे। मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या के कारण भारत सब से बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। 96.8 करोड़ कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता और 47.1 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। 2019 की तुलना में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में क्रमशः 6.9% और 9.3% ज्यादा है। देश की आबादी का 66.8% है।
राजनीतिक विश्लेषण में अक्सर यह निष्कर्ष निकलने लगता है कि महिलाओं के मत प्रवाह के इधर-उधर मुड़ जाने से चुनावी नतीजों में भारी उथलपुथल हो जाता है। सोचने और समझने की बात यह है कि क्या सिर्फ महिलाओं का मत प्रवाह को बहला-फुसलाकर इधर-उधर मोड़ लिया जाता है! ऐसा नहीं है। उथल-पुथल से ‘परेशान पुरुष’ महिला मत प्रवाह को दायी बताकर अपने मानसिक उथलपुथल को शांत करने की कोशिश करते हैं। यह वैसा ही है, जैसे घर परिवार में भी बहुतेरे लोग ‘घर की अशांति’ के पीछे महिला पर शक करते हैं। पुरुष लोग ही क्यों, महिला भी महिला पर शक करती है। ध्यान रहे, महिला दिवस रिवाज नहीं, इतिहास की गहरी घाटियों से आती हुई आवाज है। आवाजें और उसकी अनुगूंजें आती रहेगी, राजनीतिक विश्लेषण होता रहेगा, आम चुनाव के बाद भी और बाद भी। एक प्रसंग प्रेमचंद के अमर उपन्यास ‘गोदान’ से साभार-
“दुखित स्वर में (धनिया: गोबर की मां) बोली -यह मंतर तुम्हें कौन दे रहा है बेटा, तुम तो ऐसे न थे। मां-बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है। यहां बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मरजाद बनाए रखोगे, तो तुम्हीं को सुख होगा। आदमी घरवालों ही के लिए धन कमाता है कि और किसी के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी, झुनिया नागिन बन कर हमीं को डसेगी।
गोबर (बेटा) ने तिनक कर कहा – अम्मां, मैं नादान नहीं हूं कि झुनिया मुझे मंतर पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गिरस्ती का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा, तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पांवों में बेड़ियाँ नहीं डाल सकता।”
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)