(तरक़्क़ीपसंद अदीब और जर्नलिस्ट हमीद अख़्तर (जन्म : 12 मार्च 1923, निधन : 17 अक्टूबर 2011), तरक़्क़ीपसंद तहरीक के उरूज के ज़माने से फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के दोस्त थे। फ़ैज़ से उनके बहुत अच्छे मरासिम थे। इन दोनों की दोस्ती आख़िरी दम तक क़ायम रही। अदब की ख़िदमत करने के साथ-साथ उन्होंने पत्रकारिता भी साथ की। फ़ैज़ को हमीद अख़्तर ने बेहद नज़दीकी से देखा और बेहतर तरीक़े से समझा। किताब ‘आशनाईयां क्या-क्या’ में उन्होंने फ़ैज़ पर एक लंबा मज़मून लिखा है। फै़ज़ अहमद फै़ज़ के स्मृति दिवस पर ‘जनचौक’ के पाठकों के लिए पेश है, उस लंबे लेख का एक मुख़्तसर हिस्सा। इस छोटे से हिस्से से फ़ैज़ की आला शख़्सियत हमारे सामने बेहतरीन ढंग से ब-ज़ाहिर होती है।)
फै़ज़ बड़े शायर थे, इसमें तो कोई कलाम नहीं। उनके फ़न और शे’री मोहसिन (एहसान) पर अदब के नक़्क़ाद लिखते रहे हैं। और आइंदा भी बहुत कुछ लिखा जाएगा। मगर ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि वो जितने बड़े शायर थे, उससे कहीं बडे़े इंसान थे। हो सकता है वो इसलिए बड़े शायर बने कि वो बड़े इंसान थे। मुहब्बत उनके जिस्म-ओ-जां से फूटती थी। आज से कोई बीस-बाइस बरस पहले पाकिस्तान की माया-ए-नाज़ मुग़न्नियां (प्रिय सिंगर) मादाम नूरजहां ने इस बारे में मुझसे बड़ी ख़ूबसूरत बात कही थी, उसने कहा,
‘‘मैं फै़ज़ से बेपनाह मुहब्बत करती हूं। मगर ये फ़ैसला नहीं कर पाती कि ये मुहब्बत किस क़िस्म की है? इसलिए कि कभी तो मुझे महसूस होता है, वो मेरे महबूब हैं। कभी उनको मैं अपना आशिक़ तसव्वुर करती हूं। कभी वो मुझे अपने बाप की तरह नज़र आते हैं। कभी शौहर, कभी बुजुर्ग और कभी बर-ख़ुरदार।’’
फै़ज़ की शख़्सियत और मुहब्बतों की इससे बेहतर तारीफ़ शायद मुमकिन न हो। उन्होंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी बसर की। उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं। जो उन्हें ज़िंदगी भर हाथों में उठाए फिरते रहे। उनकी बज़ाहिर दरवेशाना और क़लंदराना ज़िंदगी में शाहों की ज़िंदगी से ज़्यादा शान थी। उन्होंने किसी के आगे सर ख़म (झुकाया) नहीं किया। सिवाय अपने मक़सद और वतन के। बड़े-बडे़ रऊसा और उमरा (समृद्ध और धनवान लोग) उनके सामने सर झुकाते रहे। ये शे’र वही कह सकते थे,
इस इश्क़ न उस इश्क़ पे नादिम है मगर दिल
हर दाग़ है इस दिल में ब-जुज़-दाग़-ए-नदामत।
बीस बरस पुराना एक वाक़िआ याद आ रहा है। मादाम नूरजहाँ के घर पर फै़ज़ की दावत थी। मदऊईन (आमंत्रितों) की फ़ेहरिस्त बनाने और उन्हें बुलाने की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी। जिस शाम ये दावत थी, उसी रोज़ सुबह मेरे घर पर एक अजनबी का फोन आया। उसने कहा,
‘‘हमीद साहब, आप मुझे नहीं जानते। शायद नाम से वाक़िफ़ हों, मुझे यूसुफ़ सहगल कहते हैं। मुझे मालूम हुआ कि आज नूरजहाँ के घर पर फै़ज़ साहब की दावत है। मेहमानों की फ़ेहरिस्त आपने बनाई है। क्या मुझे इस महफ़िल में शिरकत की दावत मिल सकती है?’’
मैंने उन्हें मदऊ (आमंत्रित) कर लिया। जब वो दावत में आए, तो कुछ बेचैन से नज़र आ रहे थे। पूछा, तो कहने लगे,
“आपकी बेगम साथ हैं? दूसरी ख़वातीन भी मौजूद हैं? मेरी बीवी सुबह से तक़ाज़ा कर रही थी कि वो भी साथ आएगी। क्यूंकि वो फै़ज़ साहब को देखना चाहती हैं। मेरा ख़याल था शायद इस महफ़िल में ख़वातीन मदऊ नहीं हैं। इसलिए मैं उन्हें नहीं लाया। क्या ये मुमकिन है कि वो भी आ जाएं?’’
चुनांचे उनकी बेगम को बुला लिया गया। ये महफ़िल सुबह तक जारी रही। दोस्तों ने रात भर फ़ैज़ का कलाम, फै़ज़ और नूरजहाँ से सुना। ये एक कभी न भूलने वाली महफ़िल थी।
नाम-ओ-निहाद रावलपिंडी साजिश केस से रिहाई के फ़ौरन बाद, राजा ग़ज़नफ़र अली ख़ाँ, जो उस वक़्त हिंदुस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर (राजदूत) थे। फै़ज़ को अपने साथ देहली ले गए। एक शाम उन्होंने दोस्तों को अपने यहां फै़ज़ का कलाम सुनाने के लिए मदऊ किया। बहुत से लोग आ गए। बुलाए जाने वाले भी और बिन बुलाए भी। हत्ता कि (इतना कि) मकान से बाहर की सड़क तक लोगों का हुजूम था। ये महफ़िल शबाब पर थी कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू का फ़ोन आया, वो राजा साहब से गिला (शिकायत) कर रहे थे कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया।
फिर वो उनसे इजाज़त लेकर निस्फ़ शब (आधी रात) को वहां पहुंचे और आख़िर तक बैठे रहे। इस क़िस्से के साथ चंद बरस पहले का एक वाक़िआ सुनाना भी ज़रूरी है। चंद बरस पहले फै़ज़ कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान गए थे। उनकी वापसी के बाद देहली में पाकिस्तानी सिफ़ारत-ख़ाने (एम्बेसी) की तरफ़ से हुकूमत-ए-पाकिस्तान की वज़ारत-ए-ख़ारिजा (विदेश मंत्रालय) को एक पैग़ाम भेजा गया। जिसमें लिखा था,
“फै़ज़ अहमद फै़ज़ की मेहरबानी से हमारी रसाई (पहुंच) हिंदुस्तान के मुक़्तदिर हल्क़ों (सत्तावान क्षेत्रों) के उन गोशों तक हो गई, जहां पहुंचने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे।”
मरासले (चिट्ठी) के आख़िर में तजवीज़ (सुझाव) किया गया था कि ‘‘फै़ज़ अगर किसी तरह सरकारी या गै़र सरकारी हैसियत में वज़ारत-ए-ख़ारिजा से मुंसलिक (शामिल) हो जाएं, तो इससे मुल्क को बहुत फ़ायदा हो सकता है।’’
वज़ारत के बाज़ लोगों ने इस तजवीज़ पर सुआद किया। और उस पर अमल करने की सिफ़ारिश भी की। मगर जिन्हें आख़िरी फै़सला करना था, वो मुल्क के फ़ायदे की बजाय दूसरी बातें सोचते रहे। शायद, आने वाले किसी ज़माने में इस मस्अले के मख़्फ़ी गोशों (गुप्त कोनों) से पर्दा उठे। तभी इस मुल्क के बदनसीब अवाम को पता चल सकता है कि यहां उमूर-ए-मुम्लिकत (राष्ट्र के काम) किस तरह अंजाम दिए जाते हैं।
फै़ज़ साहब ब-ज़ाहिर बहुत ढीले-ढाले और सुस्त इंसान नज़र आते थे। घरेलू ज़िंदगी में वो किसी हद तक ऐसे ही थे। मसलन उनके नाखून उम्र भर एलिस काटती रही। बाल कटवाने के लिए वो ज़बर्दस्ती उन्हें बार्बर शॉप भेजती थीं। यार लोगों में उनकी काहिली (आलस्य) और बे-नियाज़ी (किसी चीज़ की इच्छा न होना) के बहुत से क़िस्से मशहूर थे। मसलन एक रवायत ये है कि इंक़लाब-ए-चीन के बाद वो चीन गए। और माओत्से तुंग से मिले, तो माओ ने कहा,
“हम अपने मुल्क में इंक़लाब ले आए हैं। अब आप लोग भी कुछ करें।”
मशहूर ये है कि फै़ज़ साहब ने ये बात सुनी। सिगरेट के दो-तीन लंबे-लंबे कश लिए और कहा,
“हूं.., इंक़लाब..! हां-हां, हो जाएगा..! हमारे यहां भी इंक़लाब बरपा कर देंगे, हम भी..!’’
(हमीद अख़्तर का लेख, उर्दू से हिंदी लिप्यंतरण- ज़ाहिद ख़ान और इशरत ग्वालियरी।)






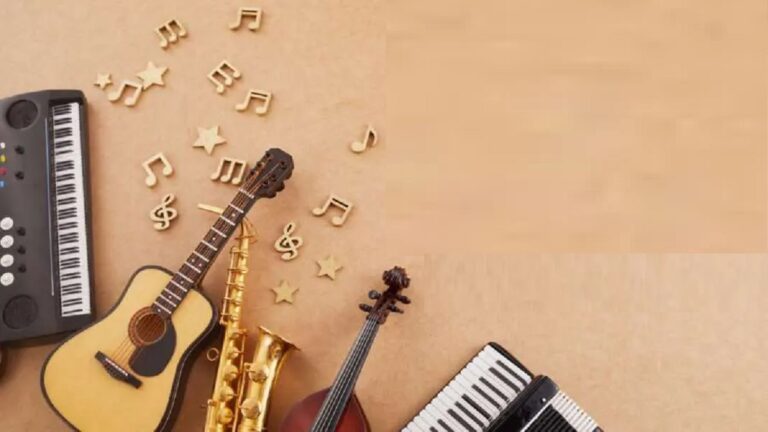







बहुत शानदार।
sahi bishleshan,