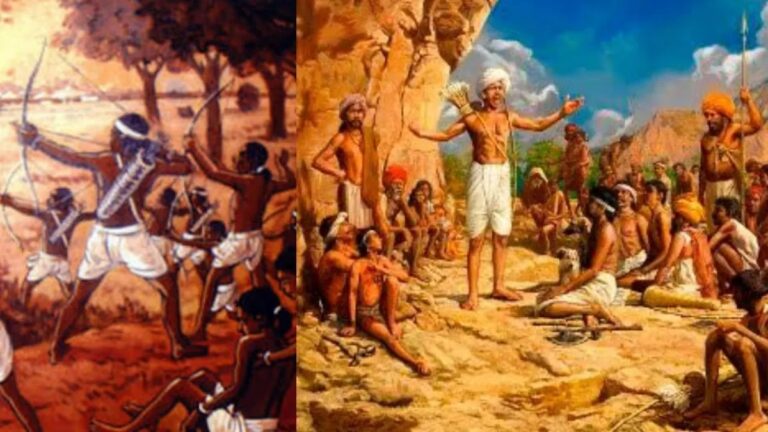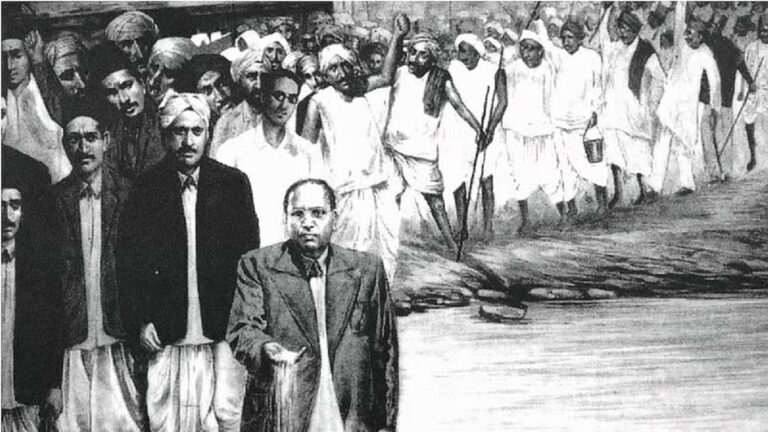भारत में वर्तमान संघ परिवार की फासीवादी राजनीति के संदर्भ में इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों तथा राज्ञनीतिज्ञों के बड़े वर्ग द्वारा इस तथ्य को बड़े ज़ोर-शोर से स्थापित किया जा रहा है कि हमारे देश में इतिहास के हर दौर में साम्प्रदायिक सौहार्द था। उपनिवेशवाद के दौर में उपनिवेशवादियों की ‘फूट डालो, राज करो’ की नीति से साम्प्रदायिक विभाजन पैदा हुआ, जिसके फलस्वरूप देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों की जानें गईं।
आज जब हिन्दुत्व की राजनीति ने तथा समाज और देश के अधिकांश हिस्से में उसके वर्चस्व ने भारतीयता की संकल्पना को हिन्दूधर्म की एक राजनीति-प्रेरित अवधारणा से जोड़ देने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है। ऊपर से पूंजी और धनबल ने भी अपने हित साधने के लिए हिन्दुत्व की राजनीतिक रणनीति को सम्पूर्ण समर्थन देना तय कर लिया है। भारतीयता की हिन्दुत्ववादी संकल्पना एक ऐसे सघन और अपवर्जक (Exclusionary) राष्ट्रवाद को लोक-स्वीकार्य बनाती है, जिसके सामने उदारवादी, संविधान-सम्मत, नागरिक राष्ट्रवाद दुर्बल और कमज़ोर साबित हो रहा है।
आज इस प्रकार के पपहचान आधारित और दक्षिणपंथी सघन राष्ट्रवाद के उभार की परिघटना किसी न किसी हद तक दुनिया भर में देखी जा रही है। नागरिक राष्ट्रवाद के सहारे इसका सामना कर पाना दुनिया भर में मुश्किल होता जा रहा है,लेकिन यह भी सच है कि दूसरी रणनीतियां इस काम के लिए और भी नाकाफ़ी साबित हो रही है।
वास्तव में इस सारे परिदृश्य को समझने के लिए तथा फासीवाद के ख़िलाफ़ नयी रणनीतियों को विकसित करने के लिए भारतीय फासीवाद तथा भारतीय राष्ट्रवाद के जड़ों की तलाश करनी होगी। पिछले दिनों दिल्ली में ‘भारतीयता, प्रगतिशीलता, प्राचीन सभ्यता, आधुनिक राष्ट्र-राज्य और समकालीन राजनीति’ पर हुई एक संगोष्ठी में ‘सुप्रसिद्ध इतिहासकार आदित्य मुखर्जी’ ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं, जो विचारणीय हैं, उनका मानना है कि “भारतीय समाज में हमेशा विभिन्न धर्मों में; विशेष रूप से हिन्दू-मुस्लिमों के बीच सौहार्द की स्थिति रही है, लेकिन उपनिवेशवादियों ने उनके बीच फूट के बीज बोए।” इसके लिए वे दो-तीन उदाहरण देते हैं, जैसे-
- ‘अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही या सुलह कुल की नीति की स्थापना’, जिसमें सभी धर्मों के बीच एकता की बातें की गईं थीं, यहां तक कि उसमें स्त्रियों के अधिकारों तक की बातें थीं।
- दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण उन्होंने ‘1857 के सैनिक विद्रोह’ का दिया,जिसमें हिन्दू-मुसलमान सभी मिलकर लड़े, यहां तक कि हिन्दू ब्राह्मणों तक ने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना नेता और देश का सम्राट तक घोषित कर दिया।
- एक बात और वे कहते हैं कि “संघ के फासीवाद की जड़ें भारतीय इतिहास में न होकर मूलतः जर्मनी और इटली से हैं, इसका भारतीय इतिहास और परंपराओं से कुछ भी लेना-देना नहीं है।”
आदित्य मुखर्जी जी की ‘भारतीय स्वाधीनता संग्राम’ नामक पुस्तक में इन चीज़ों का विस्तृत वर्णन है।
अब हम इन तथ्यों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। इतिहास के रंगमंच पर व्यक्तियों से अधिक उन शक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो इतिहास की गति को आगे बढ़ाते हैं। किसी एक अकबर, दाराशिकोह, औरंगजेब और शिवाजी के उदय से इतिहास की गति को नहीं समझा जा सकता। अगर हम भारतीय इतिहास को देखें, तो इसमें विभिन्न जातियों तथा धर्मों के बीच एकता से ज़्यादा संघर्ष के तत्व प्रभावी हैं। हिन्दूधर्म के भीतर ही विभिन्न धार्मिक समूहों जैसे-’शैव-वैष्णव या फ़िर आर्यों-अनार्यों के बीच हुए ख़ूनी टकराव या फ़िर बौद्ध धर्म का व्यापक विनाश।’ इसमें बहुसंख्यक बौद्धभिक्षुओं की हत्याएं, यहां तक कि उनके मठों-विहारों को नष्ट करके उन्हें हिन्दू मंदिरों में परिवर्तित कर दिया।
‘इतिहासकार डी एन झा के शोध’ से यह पता चलता है कि ‘नालंदा बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय’ को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने ही नष्ट किया था। इतिहासकार भगवत शरण उपाध्याय अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति के स्रोत में लिखते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही शक, हूण, कुषाण जैसी विभिन्न जातियां हमलावर के रूप में आती रहीं, लेकिन हिन्दूधर्म ने उन्हें अपने में आत्मसात कर लिया, यहां तक कि ब्राह्मणों ने इनमें से ही कुछ लोगों को ही उच्च जातियों में ले लिया तथा कुछ को पिछड़ी जातियों में; क्योंकि वे जातियां पहले ही से मूर्तिपूजक थी, इसलिए वे आसानी से हिन्दूधर्म में घुल-मिल गईं। भारतीय स्थापत्य तथा मूर्तिकला पर; विशेष रूप से कुषाण वंश का गहरा प्रभाव पड़ा, जो आज भी देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास में सोलहवीं-सत्तरहवीं शताब्दी में आए इस्लाम ने पहली बार हिन्दूवादी वर्चस्व को बड़ी चुनौती दी। इस्लाम एक पंथ और एक पुस्तक पर आधारित एकेश्वरवादी धर्म है। मूल इस्लाम में काफ़ी हद तक भाईचारे और बन्धुत्व की बातें भी थीं, उसमें ऊंच-नीच और छुआछूत की वैसी अवधारणा नहीं थी, जैसी हिन्दूधर्म में। यही कारण है कि दलित पिछड़ों में इसके प्रति जबरदस्त आकर्षण भी पैदा हुआ।”
भारत में इस्लाम हमलावरों द्वारा लाया गया। बड़े पैमाने पर बलपूर्वक भी धर्मांतरण हुआ, इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि सूफी संतों की प्रेरणा से भी बड़े पैमाने पर हिन्दू-मुस्लिम बने, परन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता, कि भारत में समूचे मुस्लिम शासनकाल में हिंसा के तत्व प्रधान थे, अभी हाल में मध्यकालीन इतिहास के सबसे बड़े इतिहासकार इरफ़ान हबीब ने एक साक्षात्कार में कहा कि “हमें इस तथ्य से इंकार नहीं करना चाहिए कि मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर सहित ढेरों मंदिरों को गिराकर मस्ज़िदें बनाई थीं, लेकिन आधुनिक समय में हम इतिहास को बदल या दोहरा नहीं सकते।”
अकसर इतिहासकारों का एक वर्ग इन तथ्यों को इसलिए ख़ारिज़ करता है, क्योंकि इससे साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ेगा, ये बात सही नहीं है। भारत में इन चीज़ों के नकार ने ही हिन्दू फासीवाद को अपना आधार विकसित करने में बहुत मदद पहुंचाई। दो धर्म या जातियाँ अगर सैकड़ों साल तक एक-दूसरे के साथ रहती हैं, तो उनमें संस्कृतीकरण की प्रक्रिया होती है अर्थात दोनों पर एक-दूसरे का प्रभाव पड़ता है। ऐसा भारत में भी हुआ। यहां पर एक मिली-जुली तहज़ीब पैदा हुई, जिसे गंगा-जमुनी तहज़ीब का नाम दिया गया, परन्तु इस चीज़ को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। लम्बे समय तक मुसलमानों की शासक वर्ग के रूप में मौज़ूदगी ने हिन्दुओं में एक हीन-भावना पैदा की, जिसका फ़ायदा उपनिवेशवादियों ने उठाया और वर्तमान समय में संघ समर्थित हिन्दू फासीवादी भी उठा रहे हैं।
1857 के सैनिक विद्रोह को भी हिन्दू-मुस्लिम की एकता के रूप में देखा जाता है। सावरकर से लेकर वामपंथी इतिहासकारों तक ने इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना है, परन्तु इसमें कितनी सच्चाई है? प्लासी के युद्ध के सौ साल बाद 1857 का विद्रोह हुआ था, परन्तु उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा ही उत्पन्न नहीं हुई थी। 1857 से पहले आदिवासियों और किसानों के भी ढेरों विद्रोह हुए थे, परन्तु ये भारतीय सामंतों और ज़मींदारों के ख़िलाफ़ ज़्यादा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कम थे। उस समय तक पूरा देश छोटी-छोटी जागीरों में बँटा हुआ था, अधिकांश जागीरदार अंग्रेज़ों द्वारा उनकी जागीरों को हड़पने के ख़िलाफ़ थे। चाहे वो झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई हों या कानपुर के नानाजी पेशवा राव।
वास्तव में यह उत्तर भारतीय उच्चजाति के सामंतों का अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंतिम प्रतिरोध था, जिसे अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। वे मूलत: अपने लिए लड़ रहे थे,उनके सामने एक देश या राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी। विद्रोहियों ने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना नेता और सम्राट ज़रूर घोषित किया,लेकिन इस अंतिम मुग़ल बादशाह की हैसियत उस समय तक केवल लालकिले तक ही सीमित थी।
1857 के बारे में ज्योतिबा फुले का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने लिखा था कि “अगर अंग्रेज़ हार जाते,तो पेशवा राज पुनः लौट आता।” इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि उस समय तक दलित-पिछड़ों के लिए अंग्रेजी शासन एक वरदान था,जिन्होंने उनकी शिक्षा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें संदेह नहीं है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत ही क्रूरता और निर्ममता दिखाई। हज़ारों लोगों की हत्याएं की गईं। गांव के गांव जला दिए गए, परन्तु इस सबके बावज़ूद इस विद्रोह का पुनर्मूल्यांकन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम के संबंधों के विश्लेषण के लिए भी यह एक ज़रूरी चीज़ है।
समाज में कोई भी परिघटना एकाएक नहीं पैदा होता है, इसकी जड़ें समाज में बहुत गहराई से पैठी होती हैं, जिस तरह धरती ऊपर से बिलकुल सपाट दिखती है, लेकिन उसके मीलों नीचे गहरी दरारें होती हैं तथा उनके टकराने से भूकंप आते हैं या फ़िर ज्वालामुखी फूटते हैं, जिसका गर्म लावा सदियों से धरती के नीचे दबा हुआ था। भारत में हिन्दू-मुसलमानों के संबंधों के बारे में भी यही बात है। एकाएक जब उनके बीच टकराव होता है, तब हमें पता लगता है कि ये चीज़ें तो समाज के गर्भ में लम्बे समय से धधक रही हैं। वर्तमान फासीवाद से लड़ने के लिए हमें इन तथ्यों पर गहराई से विचार करना होगा, तभी हम इसके ख़िलाफ़ एक व्यापक रणनीति विकसित कर पाएंगे।
(स्वदेश कुमार सिन्हा स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)