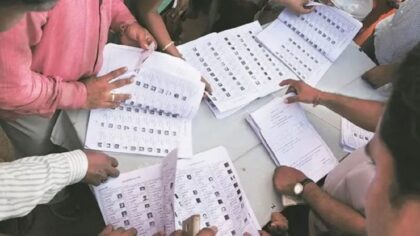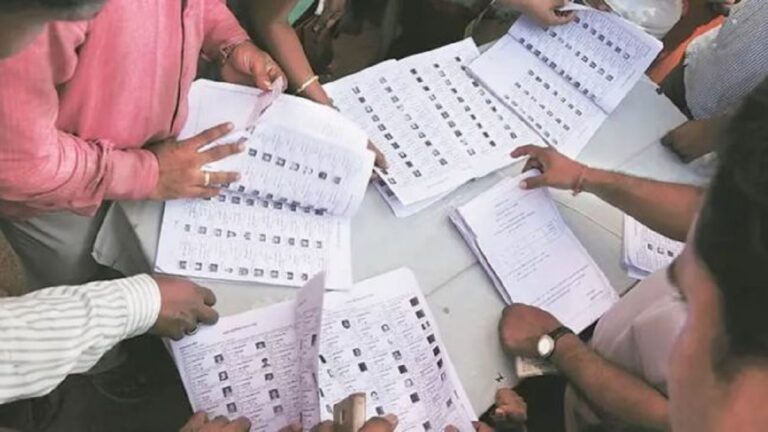एक ओर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नये आपराधिक न्याय कानून पर कहा है कि भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है और नए आपराधिक कानून ऐसे प्रावधान बनाते हैं जो हमारे समय के अनुरूप हैं वहीं उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार कानून नेटवर्क के संस्थापक डॉ. कॉलिन गोंजाल्विस के अनुसार नया आपराधिक न्याय कानून जनविरोधी ही नहीं, क्रूरतम भी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता और दिल्ली और ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर ने कहा है कि हाल ही में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने कोई नाटकीय बदलाव नहीं किया है या कानून को उपनिवेश से मुक्त नहीं किया है।
इसके अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को आशंका है कि नए आपराधिक कानून भारत को एक पुलिस राज्य बना देंगे। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए नव अधिनियमित कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – 1 जुलाई से लागू होंगे।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि नए अधिनियमित कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिजिटल युग में अपराधों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल करती है।
कॉलिन गोंजाल्विस के अनुसार नया आपराधिक न्याय कानून जनविरोधी ही नहीं, क्रूरतम भी है। कानून में आकस्मिक बदलावों का यह अध्याय कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जो बात बहुत साफ है, वह यह कि यह सब करने के पीछे सरकार की मंशा मानवाधिकार संरक्षण का ताना-बाना नष्ट करने, नागरिकों पर दमन के लिए अपनी शक्तियां अपरिमित करने की है।
केंद्र सरकार ने कुछ नया करने के नाम पर कुटिलता से तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों (जो अब कानून बन चुके हैं) को इस आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की है कि मौजूदा कानून ‘औपनिवेशिक’ तो था ही, बदला गया कानून भारत विरोधी भी था। लेकिन पुराने कानून से तुलना करने पर पता चलता है कि नए कानून स्वतंत्रता-पूर्व ब्रिटिश कानून की तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिगामी और कठोर हैं। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके नए कानून विपक्ष के निलंबित 146 सांसदों की अनुपस्थिति में संसद द्वारा पारित करा लिए गए।
यह मान लेना कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी कानून, खासकर आपराधिक न्यायशास्त्र के क्षेत्र में जनविरोधी और मानवाधिकार विरोधी थे, एक गलती होगी। अंग्रेजों ने आपराधिक कानून के कुछ सिद्धांत विकसित किए थे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे और यही कारण है कि आजादी के बाद कई मौजूदा आपराधिक कानून भारतीय संसद ने भी अपनाए। वास्तव में, ब्रिटिश काल से लेकर आधुनिक भारत तक वक्त के साथ आपराधिक कानून संरक्षण में कैसी गिरावट आई है, इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत में कानून निर्माण पहले से ही बाधित आजादी को कुचलने के लिए एक ऐसे डिजाइन की ओर तेजी से उन्मुख हुआ है जो अत्यंत दमनकारी है। तीनों नए कानून इसका उदाहारण हैं।
आपराधिक कानून महज कानून के कुछ शब्द नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा न्यायिक व्याख्या द्वारा बहुत सोच-समझ कर अपनाए गए शब्द हैं। जब कानूनों को यंत्रवत और जैसे-तैसे बदल दिया जाता है, तो न्यायशास्त्र का व्यापक सोच भी कानून के साथ लोप हो जाता है। कानून निर्माताओं द्वारा कानून बदलने का एक अनियमित निर्णय कानूनी लड़ाइयों का इतिहास ही खत्म कर देता है। आखिरकार, जैसा कि मौजूदा मामले में हुआ, कानून में आकस्मिक बदलावों का यह अध्याय कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। यह अतीत की अच्छाइयों को नष्ट और वर्तमान को दिग्भ्रमित करता है। इस मामले में जो बात बहुत साफ है, वह यह कि यह सब करने के पीछे सरकार की मंशा देश में मानवाधिकार संरक्षण का ताना-बाना नष्ट करने, नागरिकों को नियंत्रित करने, उन पर दमन करने के लिए अपनी शक्तियां अपरिमित करने की है।
आईपीसी की धारा 124ए में उत्कीर्ण राजद्रोह कानून को ही लें जिसकी शुरुआत ही होती है ‘जो कोई भी शब्दों से…’। राजद्रोह कानून बोलने की आजादी पर कुठाराघात (दंडित) करता है। इसे असहमति, विशेषकर अहिंसक असहमति को अपराध घोषित करने के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत, राजा के खिलाफ इस्तेमाल किए गए कड़े शब्द अपने आप में, राजद्रोह के आरोप और जेल में लंबे समय तक कैद की सजा का पात्र बनने के लिए पर्याप्त थे। नये कानून में ‘राजद्रोह’ शब्द के प्रयोग को हटा दिया है। इसके बाद पुरानी धारा (राज्य के खिलाफ अपराध, धारा 152) को नए आवरण में दोबारा सामने लाती है और उसकी शुरुआत को बरकरार रखती है, यानी यहां भी बात शब्दों से शुरू होती है, ‘जो कोई…शब्दों से…’, यानी भले ही हिंसक कृत्य नहीं हुए हों, अकेले शब्द ही अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त होंगे।
अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में दी गई एक अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा है। जाति-आधारित आरक्षण की आलोचना के आरोप में प्रतिबंधित फिल्म ‘ओरे ओरु ग्रामाथिले’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में अपने फैसले (एस. रंगराजन बनाम जगजीवन राम) में कहा था कि ‘प्रदर्शन और जुलूस की धमकी या हिंसा की धमकियों के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला नहीं जा सकता।’यही कारण है कि नए कानूनों का सबसे कठोर हिस्सा भाषण और असहमति को दबाना है।
ब्रिटिश कानून के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था। ये पुलिस लॉकअप ही हैं जहां अत्याचार होते हैं। यहां तक कि अंग्रेज भी समझते थे कि यदि अत्याचार कम करना है तो पुलिस हिरासत को न्यूनतम रखना होगा। अब सरकार ने पुलिस हिरासत को 90 दिनों तक बढ़ाने वाला एक स्वदेशी कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। दुनिया के किसी भी देश में इतना भयावह कानूनी प्रावधान नहीं है।
यह समझते हुए कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद की अवधि का उपयोग पुलिस द्वारा यातना देने के लिए किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु मामले (डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1996) में गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति में पालन किए जाने वाले बुनियादी दिशा-निर्देश तय कर दिए थे।
इनके अनुसार, गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिस को गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करना होगा जिसमें गिरफ्तारी का स्थान, तारीख और समय बताना होगा। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होने थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस के लिए यह आम बात थी कि कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती थी और कई-कई दिनों तक यातना देती रहती थी; फिर आरोपी को बाद की किसी तारीख में गिरफ्तार दिखाकर पेश करती थी ताकि उसके शरीर पर चोट का कोई निशान रहे भी तो गिरफ्तारी के पहले का प्रतीत हो या साबित किया जा सके।
दूसरे, गिरफ्तार व्यक्ति की हर 48 घंटे में एक सार्वजनिक अस्पताल में जांच होनी जरूरी थी और इसका एक मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करना था। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का मेमो और मेडिकल रिकॉर्ड भी एफआईआर के साथ मजिस्ट्रेट को भेजने थे। कोर्ट के दिशा-निर्देशों को हर थाने के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना था। ये सारे दिशानिर्देश नए कानूनों में अब ढूंढे नहीं मिलेंगे। इसीलिए नए कानून यातना को बढ़ावा देने वाले कानून हैं।
जनता की शिकायतें न लेने और गंभीर अपराधों, विशेषकर ताकतवर लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से इनकार करने की पुलिस की आम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ही, सुप्रीम कोर्ट के पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने ललिता कुमारी मामले (ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार 2013) में फैसला देते हुए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया।
अदालत ने एफआईआर तुरंत दर्ज करने का आदेश देते हुए पुलिस का वह बहाना खारिज कर दिया कि एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं की गई क्योंकि वह प्रारंभिक जांच कर रही थी। नए कानून में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत प्रारंभिक जांच कराने को सामान्य नियम बना दिया है।
अंतत:, आतंकवाद के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान को सामान्य आपराधिक कानून में बदल दिया गया है। नकल का कारण ढूंढना मुश्किल नहीं है। हर तरफ से अत्यंत खतरनाक बताए जाने वाले यूएपीए में भी दो सुरक्षा उपाय थे जो जांच अधिकारी (आईओ) की शक्तियों को सीमित करते थे।
सबसे पहले, आईओ को सबूत इकट्ठा करने के बाद सरकार से मंजूरी लेनी होती थी और उसके अभाव में अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता था। दूसरा, एकत्र किए गए सबूतों का आकलन करने और एक रिपोर्ट बनाने के लिए अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को ‘सक्षम अधिकारी’ के तौर पर नियुक्त किया गया था जिसे तय करना था कि क्या यह अभियोजन ‘आतंकवाद’ के आरोप के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं।
इन दोनों सुरक्षा उपायों को पूरी तरह से लागू हुए बिना मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता था। ये दोनों सुरक्षा उपाय भी नए कानून में मौजूद नहीं हैं। यानी एक अत्यंत गंभीर कानून दो जरूरी सुरक्षा उपायों के बिना लागू कर दिया गया है, जो नए कानून को दोगुना सख्त बना देता है।
दूसरी ओर सीजेआई ने कहा, ‘संसद द्वारा इन कानूनों का अधिनियमित होना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी उपकरणों की जरूरत है। हमारे कानूनों का लक्ष्य पीड़ितों को आपराधिक प्रक्रिया में एजेंसी और नियंत्रण की भावना के साथ-साथ न्याय की भावना देना होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के साथ, हम उन खामियों और क्षेत्रों की खोज करेंगे जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि हमारे कानूनों को गवाहों की जांच में देरी, मुकदमे के समापन, जेलों में भीड़भाड़ और विचाराधीन कैदियों के मुद्दे जैसे सदियों पुराने मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है। सीजेआई ने राजधानी में ‘प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ’ विषय पर एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा, ‘बीएनएसएस डिजिटल युग में अपराधों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। यह सात साल से अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए तलाशी और जब्ती की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग और अपराध स्थल पर एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति को निर्धारित करता है’।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि तलाशी और जब्ती की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग अभियोजन के साथ-साथ नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। न्यायिक जांच तलाशी और जब्ती के दौरान प्रक्रियात्मक अनौचित्य के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि बीएनएसएस की धारा 532 कोड के तहत सभी परीक्षणों, पूछताछ और कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने की अनुमति देती है। यह जोड़ जितना प्रशंसनीय है। हमें कार्यवाही के डिजिटलीकरण और डिजिटल साक्ष्य बनाते समय लगातार आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और आरोपी के साथ-साथ पीड़ित की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। डिजिटल युग में, व्यक्ति के डेटा और संवेदनशील जानकारी को अत्यधिक महत्व मिल गया है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जोर देकर कहा कि नए आपराधिक कानून ऐसे प्रावधान बनाते हैं जो हमारे समय के अनुरूप हैं। सीजेआई ने कहा कि छोटे और कम गंभीर अपराधों के लिए सारांश सुनवाई अनिवार्य कर दी गई है। मजिस्ट्रेट प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया गया है। उन्होंने आगे जोर दिया कि हमारे पुलिस बलों के बुनियादी ढांचे और क्षमता को बढ़ावा देना जरूरी है।
आलोचकों का कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सबसे बड़े बदलावों में से एक पुलिस हिरासत से संबंधित है जिसमें धारा 187(2) और 187(3) से यह समझ आता है कि पुलिस हिरासत 60 या 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है जो पहले शुरुआत के 15 दिन थी। इसके अलावा न्यायिक हिरासत के बाद पुनः पुलिस हिरासत का भी प्रावधान है जो पुलिस जांच के लिए गिरफ्तारी के 40 या 60 दिन बाद तक ली जा सकती। इसका जमानत पर भी प्रभाव पड़ सकता क्योंकि पुलिस जांच के नाम पर पुनः हिरासत की मांग कर सकती है। इस संहिता में ट्रायल के वक़्त आगे की जांच का भी प्रावधान है और उस वक़्त गिरफ्तारी या हिरासत से सबंधित क्या नियम होंगे, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
जमानत सबंधित प्रावधानों में एक बदलाव विचारधीन कैदियों से सबंधित है, जिसमें मौजूदा नियमों के अनुसार केस के विचाराधीन रहते हुए अधिकतम सजा की आधी अवधि कैदी द्वारा जेल में रहने पर उसको जमानत दी जा सकती है; परंतु नई संहिता के लागू होने पर जिन विचारधीन कैदियों पर एक से ज्यादा केस चल रहे या एक केस में एक से ज्यादा धारा लगाई हो वो जमानत के इस प्रावधान का लाभ नहीं ले पाएंगे।
ये जमानत के मूल सिद्धांत ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद है’ के भी विरोध में है। यह आम समझ है कि कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उसमें एक से ज्यादा धाराएं लगाई जाती हैं। ऐसे में विचारधीन कैदियों को जेल में ही रखना उनके ‘दोषी साबित होने से पहले बेगुनाह’ होने के न्याय सिद्धांत के भी विरोध में है।
गौरतलब है कि विचारधीन कैदियों में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जेलों में बंद 75% से ज्यादा कैदी विचारधीन हैं; जिसमें 30 प्रतिशत एससी और एसटी, 35% ओबीसी और 19.3% मुस्लिम हैं। ऐसी स्थिति में जमानत सबंधित प्रावधानों में कठोरता लाना हाशिये पर पड़े वर्गों के अपराधीकरण को बढ़ावा देगा।
यह नए बदलाव साफ तौर पर हमारी न्याय व्यवस्था को पुलिस की जवाबदेही के सिद्धांत से दूर और पुलिस को ज्यादा शक्तियां देने की दिशा में है। और इन शक्तियों के गलत इस्तेमाल का इतिहास देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये नया कानून इसी प्रकार लागू होता है तो पिछड़े वर्गों, जनजातीय समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा इन क़ानूनों का दुरुपयोग बढ़ सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता और दिल्ली और ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर ने रविवार को कहा कि हाल ही में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने कोई नाटकीय बदलाव नहीं किया है या कानून को उपनिवेश से मुक्त नहीं किया है।
डॉ. मुरलीधर ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि आजादी के 76 साल बाद भी आपराधिक कानून के कुछ पहलू अपरिवर्तित हैं, जिसका उपयोग अभी भी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है।
डॉ. मुरलीधर ने टिप्पणी की, “इसलिए, आप जो बयान सुन रहे हैं, उससे प्रभावित न हों कि इन तीन नए (आपराधिक) कानूनों ने नाटकीय बदलाव ला दिया है और कानून को उपनिवेशविहीन कर दिया है। इनमें से कुछ भी नहीं है।
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि 1915 का भारत रक्षा अधिनियम स्वतंत्रता के बाद के निवारक निरोध कानूनों का आधार है। उन्होंने बताया कि कानून के भीतर जमानत प्रावधान गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और कंपनी अधिनियम जैसे कानूनों की एक श्रृंखला में समान प्रावधानों में देखे गए दोहरे परीक्षण के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं।
इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 पर, जो निवारक हिरासत की अनुमति देता है, डॉ. मुरलीधर ने कहा कि निवारक हिरासत क़ानून को आपातकालीन स्थितियों में अस्थायी उपाय माना जाता है। हालांकि, प्रोफ़ेसर उपेन्द्र बक्सी के हवाले से उन्होंने कहा, निवारक हिरासत के माध्यम से शासन करना एक विधायी आदत बन गई है और ऐसी निवारक हिरासत में हस्तक्षेप न करना एक न्यायिक आदत बन गई है।
हालांकि, लड़ाई जारी रहनी चाहिए, डॉ. मुरलीधर ने कहा, नए आपराधिक कानून दुर्भावनापूर्ण रूप से मुकदमा चलाने वालों के मुआवजे पर विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 358, जो गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजे के रूप में मात्र ₹1,000 देती है, को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में बरकरार रखा गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 211, जो झूठे मामले को फंसाने से संबंधित है, में भी बहुत कम या कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और नए कानून में भी इसे बरकरार रखा गया है।
डॉ. मुरलीधर ने कहा, “यह मुठभेड़ों, गायब होने की बात नहीं करता, यह सामूहिक अपराधों की बात नहीं करता। यह मानवता के ख़िलाफ़ अपराध की बात नहीं करता। नए कानून उन वास्तविक मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं जहां हमारे देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। यह सिर्फ आईपीसी के बारे में नहीं है बल्कि विशेष और स्थानीय कानूनों की एक श्रृंखला के बारे में है।”
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)