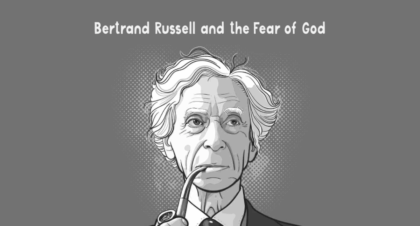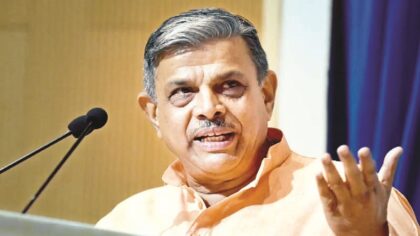मेरी टाइलर एक ब्रिटिश महिला पत्रकार थीं। 70 के दशक में जब भारत के एक बडे़ भाग में; विशेष रूप से बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन चल रहा था, उस दौर में वे भारत आई थीं। आंदोलन को निकट से देखने के लिए वे अपने मित्र के साथ बंगाल के वीरभूम जिले के कई गांवों में गईं, जहां बाद में उन्हें इस आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया कि वे नक्सलवादियों की सहायता करने के लिए ब्रिटेन से भारत आई हैं। उन्होंने भारतीय जेलों में क़रीब 5 साल गुज़ारे। बाद में कोई आरोप सिद्ध न होने पर वे रिहा कर दी गईं। लंदन लौटने पर 1977 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी ‘My Years In An Indian prison’, उसी वर्ष यह पुस्तक हिन्दी में ’भारतीय जेलों में पांच साल’ नाम से प्रकाशित हुई।
अपनी पुस्तक में लेखिका ने भारत के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों; विशेष रूप से महिला कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि, “कैदियों के साथ जाति के अनुसार भेदभाव किया जाता है। ज़्यादातर जेलें दलित पिछड़ी और आदिवासी जाति के कैदियों से भरी रहती हैं तथा जाति के अनुसार ही कैदियों को काम भी दिए जाते हैं, जैसे जेलों में सफ़ाई और अन्य काम दलित महिला कैदी को दिए जाते थे।” उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है कि किस तरह जेल में एक दलित कैदी को बच्चा होने को हुआ, तो जेल की महिला डॉक्टर ने उसे छूने से इसलिए इंकार कर दिया, क्योंकि वो डॉक्टर ब्राह्मण थी। इस कारण से उचित चिकित्सा न मिल पाने के कारण बच्चे की मौत हो गई और उस कैदी की जान भी बहुत मुश्किल से बच पाई।
आज इस पुस्तक को प्रकाशित हुए क़रीब 51साल बीत गए, लेकिन क्या इस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया। एक रिपोर्ट के अनुसार देश की जेलों पर नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि भारतीय जेलों में बंद दो तिहाई कैदी दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं,19% मुसलमान हैं और 4.66 लाख कैदियों में से 66% या तो निरक्षर हैं या उन्होंने दसवीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं की है। राज्यों में; उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित कैदियों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश में आदिवासी कैदियों का अनुपात सबसे अधिक है। ये आंकड़े जेल सांख्यिकी 2018 में दिए गए हैं, जिसे बुधवार को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था, 2016 और 2017 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्टों में धर्म और जाति के विवरण को छोड़ दिया गया था। दोषियों और विचाराधीन कैदियों दोनों के लिए 2018 के आंकड़े-33.49% ओबीसी, 20.68% अनुसूचित जाति,11.56% अनुसूचित जनजाति,18.81% मुस्लिम-2015 की रिपोर्ट में देखी गई प्रवृत्ति के समान हैं।
4.66 लाख कैदियों में से हिंदू कैदियों की संख्या 3.12 लाख है, उसके बाद मुस्लिम (87,673), सिख (16,989) और ईसाई (13,886) हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जेलों में भीड़भाड़ बनी हुई है और स्थिति बदतर होती जा रही है। 2018 में कैदियों की संख्या बढ़कर 117.6% (4.66 लाख) हो गई, जबकि 2017 में यह 115.1% (4.50 लाख), 2016 में 113.7% (4.33 लाख) और 2015 में 114.4% (4.19 लाख) थी। 2018 के अंत में भारतीय जेलों की क्षमता 3.96 लाख थी, जबकि 2017 में यह 3.91 लाख, 2016 में 3.8 लाख और 2015 में 3.6 लाख थी।
मुस्लिम कैदियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27,459 मुस्लिम कैदी हैं (देश में कुल मुस्लिम कैदियों का 31.31%),दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल (8,401) है। कर्नाटक में ऐसे 2,798 कैदी हैं। जाति के आधार पर विश्लेषण से पता चला कि 1.56 लाख कैदी ओबीसी से थे, जबकि 96,420 दलित और 53,916 आदिवासी थे। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 66.51% या तो निरक्षर (1.33 लाख) थे या फिर वे जिन्होंने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है (1.76 लाख)। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के कैदियों की संख्या भी सबसे अधिक है-24,489 या ऐसे कैदियों का 25.39%, जबकि मध्य प्रदेश में 8,935 और कर्नाटक में 2,803 हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 15,500 आदिवासी कैदी हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (6890) का स्थान है। 4.66 लाख कैदियों में से हिंदू कैदियों की संख्या 3.12 लाख है, उसके बाद मुस्लिम (87,673), सिख (16,989) और ईसाई (13,886) हैं।
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जेलों में भीड़भाड़ बनी हुई है और स्थिति बदतर होती जा रही है। 2018 में कैदियों की संख्या बढ़कर 117.6% (4.66 लाख) हो गई, जबकि 2017 में यह 115.1% (4.50 लाख), 2016 में 113.7% (4.33 लाख) और 2015 में 114.4% (4.19 लाख) थी। 2018 के अंत में भारतीय जेलों की क्षमता 3.96 लाख थी, जबकि 2017 में यह 3.91 लाख, 2016 में 3.8 लाख और 2015 में 3.6 लाख थी। मुस्लिम कैदियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27,459 मुस्लिम कैदी हैं (देश में कुल मुस्लिम कैदियों का 31.31%), दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल (8,401) है।
कर्नाटक में ऐसे 2,798 कैदी हैं। जाति के आधार पर विश्लेषण से पता चला कि 1.56 लाख कैदी ओबीसी से थे, जबकि 96,420 दलित और 53,916 आदिवासी थे। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 66.51% या तो निरक्षर (1.33 लाख) थे या फिर वे जिन्होंने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की है (1.76 लाख)। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के कैदियों की संख्या भी सबसे अधिक है-24,489 या ऐसे कैदियों का 25.39%,जबकि मध्य प्रदेश में 8,935 और कर्नाटक में 2,803 हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 15,500 आदिवासी कैदी हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ (6890) का स्थान है। कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों के 1,254 कैदी हैं।
भारतीय जेलों में दलित, पिछड़े, अनुसूचित जातियों तथा मुस्लिमों की इतनी बड़ी संख्या को देखकर क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या इन समुदायों के लोग ज़्यादा अपराधों में लिप्त हैं। वास्तव में यह निष्कर्ष तथ्यत: ग़लत है वास्तविकता यह है कि भारत में इन समुदायों में ग़रीबी सबसे ज़्यादा है तथा छोटे-मोटे अपराधों में जेल में जाने पर भी वे वकील नहीं कर पाते, उन्हें ज़मानतदार नहीं मिल पाते, इन कारणों से वे लोग लम्बे समय तक बिना ज़मानत के जेलों में बंद रहते हैं। दूसरा यह महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों का इन जातियों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया भी है, इन कारणों से भी इन्हें ज़मानत मिलने में मुश्किल आती है, जबकि आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे मनु शर्मा जैसे लोग बड़े-बड़े वकील करके आसानी से ज़मानत पा जाते हैं। इसका एक पक्ष और भी है कि जेलों में बंद कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, कामों का वितरण भी उसी के आधार पर होता है और इनमें से कुछ चीज़ें तो जेल के मैनुअल में बाकायदा लिखी गई हैं।
“मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सहित 10 से अधिक राज्यों के जेल मैनुअल में अभी भी ऐसे प्रावधान हैं जो जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और जबरन श्रम को मंजूरी देते हैं।” उच्चतम न्यायालय ने 3 जनवरी,2024 को कहा था कि देश भर की जेलों की चारदीवारी के भीतर कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव, जाति-पदानुक्रम के अनुसार उनके बीच शारीरिक कार्यों का पृथक्करण और विमुक्त जनजातियों के कैदियों के साथ ‘आदतन अपराधी’ जैसा व्यवहार एक ‘बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा’ है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सहित 10 से अधिक राज्यों के जेल मैनुअल में अभी भी ऐसे प्रावधान हैं जो जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और जबरन श्रम को मंजूरी देते हैं।
न्यायालय ने पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका पर राज्यों और केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर और अधिवक्ता प्रसन्ना एस.श्री मुरलीधर ने कहा कि जेलों के अंदर सदियों से जातिगत भेदभाव जारी है। श्रम को जाति के आधार पर अलग किया जाता है। ऐसा लगता है कि जेलों में सुधार को बढ़ावा देने वाले आधुनिक मैनुअल जेल की दीवारों में प्रवेश नहीं कर पाए है।
वरिष्ठ वकील ने कहा, “जेलों में दलितों के लिए अलग वार्ड भी है… जेल मैनुअल में बदलाव के बावजूद जातिगत भेदभाव जारी है। राज्यों के जेल मैनुअल में इन प्रावधानों को निरस्त किया जाना चाहिए।” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मामले में मदद करने के लिए अदालत ने बुलाया था। “मैंने जेल की स्थिति के आधार पर अलगाव देखा है-जैसे कि दोषियों को विचाराधीन कैदियों से अलग किया जाता है-लेकिन जाति आधारित भेदभाव नहीं। यह एक गंभीर मुद्दा है।”
श्री मेहता ने कहा याचिका में बताया गया कि राजस्थान कारागार नियम 1951 के तहत मेहतरों को शौचालयों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ब्राह्मणों या ‘काफी उच्च जाति के हिंदू कैदियों’ को रसोईघर की जिम्मेदारी दी गई है। सुश्री शांता; जिनकी इस मुद्दे पर रिपोर्ट पुलित्जर सेंटर से प्राप्त अनुदान का हिस्सा थी, द्वारा दायर याचिका में कहा गया, “तमिलनाडु के पलायमकोट्टई सेंट्रल जेल में थेवर, नादर, पल्लार को अलग-अलग खंड आवंटित किए गए हैं, जो बैरकों के जाति-आधारित पृथक्करण का एक ज्वलंत उदाहरण है।” एक अन्य उदाहरण में, याचिकाओं में कहा गया कि पश्चिम बंगाल जेल संहिता में यह प्रावधान है कि मेथर या हरि जाति, चांडाल या अन्य जातियों के कैदी झाड़ू लगाने जैसे तुच्छ कार्य करेंगे। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल कैदी होने के कारण उसके मौलिक अधिकारों या समानता संहिता से वंचित नहीं किया जा सकता। याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों पर सुनील बत्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कहा गया, “एक कैदी को सभी संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हैं, सिवाय उन अधिकारों और सुरक्षा के जो कारावास के परिणामस्वरूप स्वाभाविक और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।”
(स्वदेश कुमार सिन्हा स्वतंत्र पत्रकार हैं।)