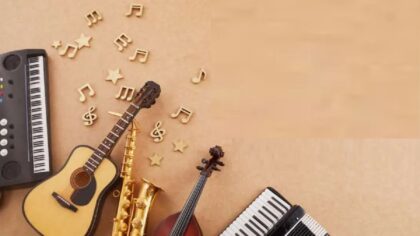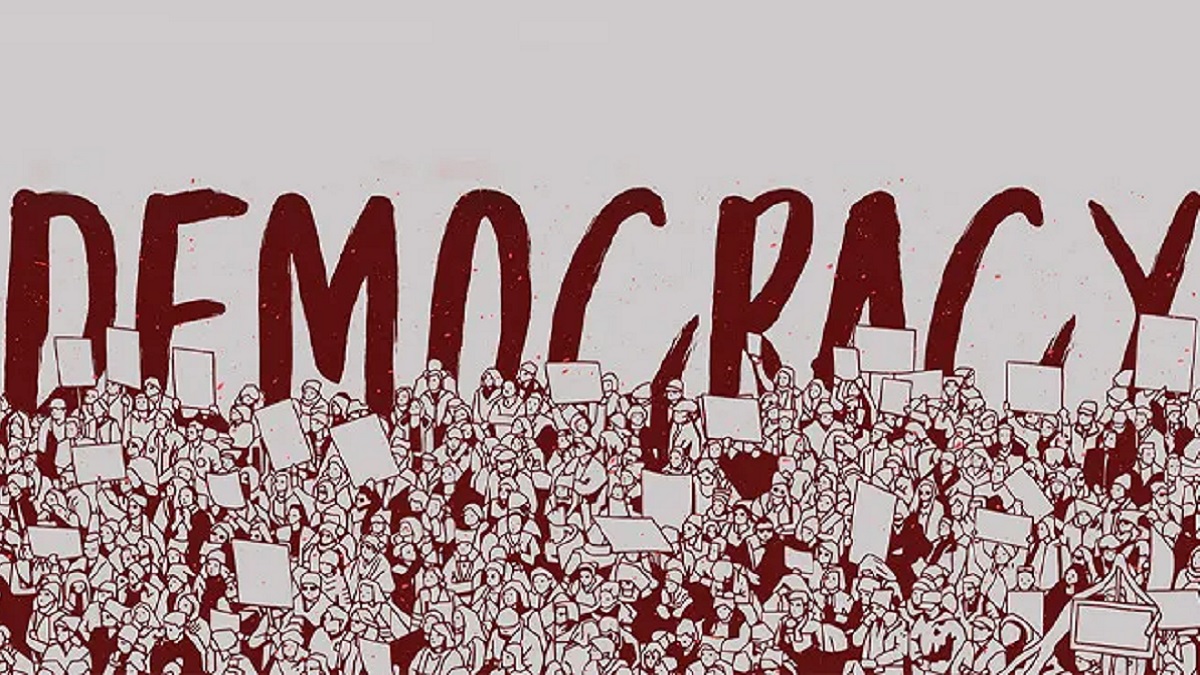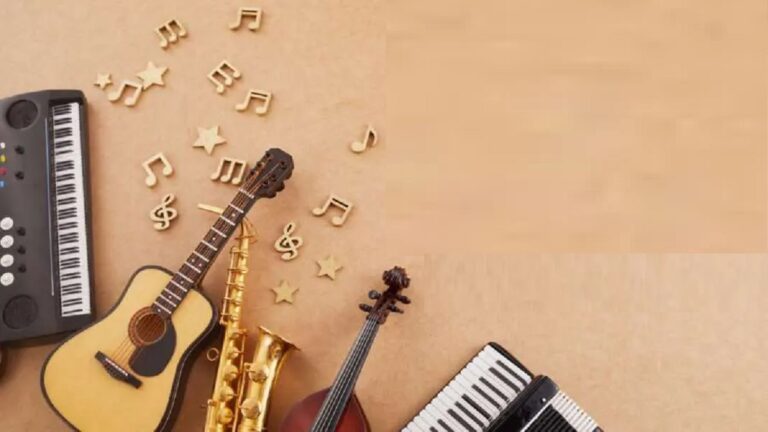यह माना जाता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए समानता और न्याय को सिद्धांत और व्यवहार में मनाना राज्य, संस्थाओं, और व्यक्तियों का अनिवार्य गुण होना चाहिए। समानता और न्याय, बंधुत्व के लिए एक पूर्व-शर्त हैI Equality and justice are pre-conditions for fraternity. समानता और न्याय के विचार के प्रति समर्पण के बिना नागरिकों में बन्धुत्त्व का विचार और व्यवहार विकसित नहीं हो सकता I कुछ वर्चस्ववादी संगठन और लोग समानता और न्याय को नकारकर, समरसता के विचार पर अपने विशेषाधिकारों को बनाए रखने की राजनैतिक और सांस्कृतिक कोशिशों में लगे हुए हैंI
भारत में फॉर्मल लेवल पर भले ही समानता की घोषणा हो गयी हो, लेकिन भारत के काफ़ी लोग सांस्कृतिक, सामाजिक, और आर्थिक असमानताओं को जरूरी समझते हैंI
अभी कुछ समय पहले ही बारहवीं कक्षा में पढ़ रहे एक दलित छात्र का अपहरण करके उसे केवल इसलिए पीटा गया ताकि वह बोर्ड की परीक्षा न दे पाएI तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने उस छात्र से कहा कि उसका काम पढ़ना नहीं, बल्कि मजदूरी करना है I अपहरण के कारण वह छात्र बारहवीं के बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर नहीं दे पाया I तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने उस छात्र के करियर को खत्म करने की कोशिश कीI
तो भारत ऐसा देश है जहाँ किसी उत्पीड़ित समूह के बच्चे का अपहरण उसे शिक्षा से दूर रखने के लिए किया जाता हैI इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि भारत में कुछ हद तक फॉर्मल इकुवेलिटी भले ही आ गयी हो, लेकिन भारत सामाजिक लोकतंत्र से अभी बहुत दूर हैI
पिछले दिनों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य सभा के सदस्य मनोज झा द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में संसद के माध्यम से सरकार की तरफ से एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिससे पता चलता है कि भारत की राजनीति, प्रशाशन, संस्थाएँ, और लोग, आज भी one person one vote जैसी फॉर्मल डेमोक्रेसी की चेतना से आगे नहीं बढ़ पाये हैं I मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड सोशल जस्टिस ने संसद को बताया कि 2018 से भारत के हाईकोर्टस में जितने जजों की नियुक्ति हुई उनमें से 77% जज सवर्ण हैं। हाईकोर्टस 2018 से नियुक्त जजों में से करीब 3% शेड्यूल्ड कास्ट, 2% शेड्यूल्ड ट्राइब, 12% ओबीसी और 5% अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं।
कुछ मासूम और कुछ चालक लोग कहेंगे कि किसी श्रेणी के लोगों की संख्या नहीं गिननी चाहिए, बल्कि एफिशिएंसी देखी जानी चाहिए I पहली बात तो ये हैं कि किसी की भी एफिशिएंसी किसी पद पर काम करते हुए ही आंकी जा सकती हैI अगर किन्हीं समूहों को किन्हीं पदों तक पहुँचने के दरवाजे बंद कर दिये जाएँ तो उस समूह के लोगों की एफिशिएंसी कैसे नापी जा सकती है? दूसरी बात ये है कि एफिशिएंसी का सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी के साथ गहरा संबंध होता है I तीसरी बात ये है कि क्या भारत में एफिशिएंसी को मापने का कोई प्रमाणिक मॉडल उपलब्ध है?
चौथी बात ये है कि एफिशिएंसी का सवाल उठाने वालों में से अनेक लोग बार-बार “डेमोग्राफिक चेंज” का मुद्दा उठाते रहते हैं I उस समय वे एफिशिएंसी के तर्क को सामने नहीं रखते ! पांचवीं बात ये है कि एफिशिएंसी का तर्क देने वाले ही “UPSC जिहाद” जैसी साम्प्रदायिक और झूठी खबरों पर चर्चा करते हैं I और छठी बात एक सूत्र है जिस पर एफिशिएंसी का तर्क देने वालों की नीयत को टेस्ट किया जा सकता हैI
जिस सूत्र पर यह टेस्ट किया जा सकता है कि एफिशिएंसी के पक्ष में दिया जाने वाला उनका तर्क भेदभाव बढ़ाने वाला है या न्याय को प्रोत्साहन देने वाला? ये सूत्र नाइजीरिया की फेमिनिस्ट लेखिका Chimamanda Ngozi Adichie का दिया हुआ है I ये सूत्र कहता है कि- “can you reverse X and get the same results?” इस सूत्र में X कोई भी सामाजिक-सांस्कृतिक कारक हो सकता है I मान लीजिए कि X कोई महिला है और आप X के फ्री-डोमेस्टिक लेबर करने को सही मानते या मानती हैं?
अब X को reverse कर दीजिएI अब X को पुरुष मान लीजिए I क्या अब भी आप X के फ्री-डोमेस्टिक लेबर करने को सही मानते या मानती हैं? अगर नहीं तो यह मान लीजिए कि आप जेंडर के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं I क्योंकि X को reverse करने से परिणाम समान नहीं आया I यानि जब आपने X को महिला समझा तो परिणाम कुछ था और जब आपने X को पुरुष माना तो परिणाम कुछ और ही आया I
अब इस सूत्र को जजों की भर्ती के संदर्भ में समझिएI आप “सवर्ण” को X मान लीजिए और इस खबर को पढ़िए कि “2018 के बाद हाईकोर्टस में 77% सवर्ण जजों की नियुक्ति हुई”I अब इस खबर में X को reverse कर दीजिए और लिखिए- “2018 के बाद हाईकोर्टस में 77% “अनुसूचित जाति” के जजों की नियुक्ति हुई”I क्या अब भी आपके दिमाग में एफिशिएंसी का विचार मजबूती के साथ टिका हुआ हैI अगर जजों की नियुक्ति की खबर में “सवर्ण” की जगह “अनुसूचित जाति” लिख देने से स्वीकारिता के स्तर में अंतर आ जाता है तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी का तर्क वर्चस्व को बनाए रखने के लिए दिया जा रहा था, पारदर्शिता, उत्पादकता, और न्याय को बढ़ाने के लिए नहींI
ऐसा नहीं कि नियुक्तियों में सवर्णों का अनुपात उनकी संख्या के अनुपात से बहुत ज्यादा केवल जजों की नियुक्तियों में ही है! शिक्षा संस्थाओं में टीचर्स, विद्यार्थी, और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियों में भी सवर्ण टीचर्स, विद्यार्थियों, और नॉन-टीचिंग स्टाफ में सवर्णों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत ज्यादा है I
कर्मचारियों के रूप में ज्यादातर कर्मचारियों में सवर्णों को रखे जाने का मतलब यह है कि राज्य जनता के खजाने का पैसा मुख्यतः सवर्णों को बाँट रही हैI किसी को नौकरी देने से राज्य उस व्यक्ति की पहुँच राज्य के संसाधनों तक होने देती हैI किसी को नौकरी देने का मतलब यह भी है राज्य नीति बनाने और नीतियों को लागू करवाने के लिए उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को अवसर दे रहा हैI
शिक्षा: राज्य का विचारधारात्मक उपकरण
अल्थूजर फ़्रांस के एक दार्शनिक हुए I सन 1970 में उन्होंने एक बेहद महत्त्वपूर्ण निबंध लिखा हिया I उस निबंध का शीर्षक है – Ideology and Ideological State Apparatuses. उनका मत है कि राज्य अपनी विचारधारा को दो तरीकों से मनवाती या फैलाती हैI इनमें से एक को वे “Repressive state apparatus” कहते हैं और दूसरे को वे “the Ideological State Apparatuses” कहते हैंI जिन साधनों के द्वारा राज्य हिंसा करके अपनी विचारधारा को मानने पर मजबूर करता है उन्हें “Repressive state apparatus” कहते हैं I जैसे – सरकार, प्रशासन, सेना, पुलिस, अदालतें, जेल आदि।
अल्थूजर ने समझाया था कि राज्य केवल हिंसा के सहारे ही अपनी विचारधारा को नहीं फैलताI वो “Repressive state apparatus” के साथ-साथ “Ideological State Apparatuses” का भी प्रयोग करता हैI शिक्षा भी राज्य का एक “Ideological State Apparatuses” हैं I इसका उपयोग करके राज्य अपने हित की विचारधारा को लोगों द्वारा मान लेने के लिए मानस और माहौल तैयार करता हैI
निजी विश्विद्यालय: वर्ण–व्यवस्था की रक्षा के दुर्ग
संसद के माध्यम से जो जानकारियां सामने आई हैं उनसे पता चल रहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और विशेषकर प्राइवेट विश्वविद्यालयों की व्यवस्था, अन्याय और गैर-बराबरी के सिद्धांतों और व्यवहारों पर टिकी वर्ण-व्यवस्था को बनाए रखने की व्यवस्थाएँ हैंI
भारत में लोकतंत्र के हालातों को बताने वाला एक और डरावना आंकड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी की 364 वीं रिपोर्ट में सामने आया है I इस रिपोर्ट को 26 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में केवल पांच प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट और केवल एक प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब विद्यार्थी का नामांकन हो रखा है। (refer to page 88-91 of the parliamentry report)I
इस रिपोर्ट के तथ्यों को कुछ और समझने के लिए Manipal Academy of Higher Education का उदाहरण लेते हैं I इस विश्वविद्यालय में कुल 4741 विद्यार्थियों का नामांकन हो रखा है। इनमें से शेड्यूल्ड कास्ट के 22 और शेड्यूल ट्राइब के 17 विद्यार्थी हैं। यानी Manipal Academy of Higher Education में शेड्यूल्ड कास्ट के 0.46 प्रतिशत विद्यार्थियों का नामांकन हो रखा है। यानी आधा प्रतिशत से भी कम। इस विश्वविद्यालय में शेड्यूल्ड ट्राइब के केवल 0.35% विद्यार्थियों का नामांकन हो रखा है। (refer to page 88 of the parliamentry report) I
अगर Manipal Academy of Higher Education में फैकेल्टी पोजीशंस की बात करें तो स्थिति बेहद अन्यायपूर्ण है I इस विश्वविद्यालय में कुल 186 शिक्षक हैं। उनमें से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब श्रेणी के एक-एक शिक्षक हैं। यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के शिक्षकों का प्रतिशत केवल 0.54 है।
अब एक आंकड़ा Manipal Academy of Higher Education में नॉन टीचिंग स्टाफ से सम्बंधित हैI इस विश्वविद्यालय में कुल 967 नॉन टीचिंग कर्मचारी हैं। इन 967 कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, और ओबीसी श्रेणी का नहीं हैI यानी इस विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन जीरो है। यह आंकड़ा भी भारत में लोकतंत्र की बेहद खराब स्थिति को बयान करता है।
वर्ण-व्यवस्था के पक्ष में Birla Institute of Technology & Sciences, Pilani का आंकड़ा और भी डरावना है। इस इंस्टिट्यूट में 11,865 विद्यार्थियों का नामांकन हो रखा ह। इन 11,865 विद्यार्थियों में से एक भी विद्यार्थी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी श्रेणी का नहीं है। यानी इंस्टिट्यूट के सभी विद्यार्थी सवर्ण हैंI (refer to page 89 of the parliamentry report)I
इसका अर्थ यह है कि इन इंस्टिट्यूटस में सरकार और संस्थान दोनों की तरफ से अवसरों की समानता को सुनिश्चित नहीं किया गया है I अवसरों की समानता का न होना अपने आप में लोकतान्त्रिक मूल्यों के खिलाफ़ है I आजादी के 75 साल बाद भी एक “लोकतान्त्रिक राष्ट्र” की अनुमति से चलने वाले ये विश्वविद्यालय उन “गुरुकुलों” की तरह चल रहे हैं जिनमें “एकलव्य” का दाखिला नहीं हो सकता है I जो लोग समानता, न्याय, और बन्धुत्त्व जैसे संवैधानिक मूल्य पर भरोसा करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि सवर्ण कितना और पा लेंगे कि उनका मन भर जाएगा?
समानता के दो प्रकार: फॉर्मल और सबस्टेंटिव
जानकारों ने समानता को कम-से-कम दो रूपों में समझने की कोशिश की है I फॉर्मल इकुवेलिटी और सबस्टेंटिव इकुवेलिटी I फॉर्मल इकुवेलिटी के अंतर्गत अवसरों तक समान पहुँच को सुनिश्चित किया जाता है I सबस्टेंटिव इकुवेलिटी में विचार और पहचान के स्तर पर समानता के होने या न होने को परखा जाता है I लेख के आगे के भाग में मैं आपको फॉर्मल इकुवेलिटी के संदर्भ को समझने के लिए चार उदाहरण दे रहा हूँ और मैं एक उदाहरण सबस्टेंटिव इकुवेलिटी को समझने के लिए भी दूंगा I
इन उदाहरणों से आप समझ पाएंगे कि भारत में दोनों प्रकार की समानता के ऊँचे स्तर को हासिल करने के लिए अभी राज्य और नागरिकों के पास इच्छा की कमी है I इन उदाहरणों से हमें पता चलेगा कि भारतीय राज्य और भारतीय समाज अभी दोनों प्रकार की समानताओं से दूर है I
फॉर्मल इकुवेलिटी का पहला उदाहरण
2018 से हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में से 80% सवर्ण हैं I यानि जिन पदों में आरक्षण नहीं है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति होना लगभग असंभव है I
फॉर्मल इकुवेलिटी का दूसरा उदाहरण
भारत की टॉप 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में केवल पांच प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जाति से हैं और केवल एक प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से हैं। इस आंकड़े से भी पता चलता है कि जहां आरक्षण नहीं है वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना बेहद मुश्किल हैI यह कहा जा सकता है कि ये विश्वविद्यालय बाकी मानकों में भले ही कमजोर हों, लेकिन वर्ण-व्यवस्था को बनाए रखने में ये विश्वविद्यालय टॉप पर हैंI
1931 की जनगणना
1931 की जनगणना के अनुसार भारत में ब्राह्मणों की संख्या 4% थी I 1931 की जनगणना के अनुसार बॉम्बे प्रेसीडेंसी में ब्राह्मण पुरुषों की साक्षरता दर 79% थी और ब्राह्मण महिलाओं की साक्षरता दर 23% थी I जबकि 1931 की जनगणना के अनुसार मुंबई प्रेसिडेंसी में ही भील जाति के पुरुषों की साक्षरता दर एक प्रतिशत थी I मद्रास प्रेसीडेंसी में 80% ब्राह्मण पुरुष साक्षर थे और 28% ब्राह्मण महिलाएं साक्षर थी। Bangal प्रेसीडेंसी में 64.5% ब्राह्मण पुरुष साक्षर थे और 22 % ब्राह्मण महिलाएं साक्षर थी। 1931 के पंजाब प्रांत में ब्राह्मण की साक्षरता दर 27% थी, जबकि ब्राह्मण महिलाओं की साक्षरता दर 34% थी I
पाठ्यपुस्तक समितियों के सदस्यों में विविधता की वकालत क्यों की जाती है?
मैं फॉर्मल इकुवेलिटी के दो उदाहरण पहले दे चुका हूँ और अब दो उदाहरण और दे रहा हूँ I इससे पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि स्कूलों के लिए तैयार की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की निर्माण समिति के सदस्यों में विविधता का होना शैक्षिक दृष्टि से एक बेहतर विकल्प क्यों हैI
समावेशी पाठ्यपुस्तक समितियों की अक्सर वकालत की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक सामग्री विभिन्न दृष्टिकोणों, अनुभवों और पहचानों को प्रतिबिंबित करे। उम्मीद यह की जानी चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए ऐसी किताबें बनाई जाए जो विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के अनुभवों के साथ तालमेल बिठा सके और पूर्वाग्रहों या रूढ़ियों को बनाए रखने से बचे।
पाठ्यपुस्तक समितियों में विभिन्न लैंगिक, जातीय, नस्लीय, भौगोलिक, धार्मिक आदि पृष्ठभूमियों के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो इस बात पर विचार कर सकें कि क्या पढ़ाया जाए और पाठ-सामग्री को कैसे प्रस्तुत किया जाए।
यह माना जाता है कि पाठ्यपुस्तकें, विद्यार्थियों के सोचने और उनके दुनिया से जुड़ने के तरीकों को आकार देती हैं और उनके द्वारा दुनिया को देखने के तरीकों को प्रभावित करती हैं। यदि विषय-वस्तु संकीर्ण है तो ये कक्षाओं में अनेक विद्यार्थियों को अलग-थलग कर सकती हैं या उनकी समझ में खतरनाक पक्षों को छोड़ सकती हैं।
पाठ्यपुस्तक समितियों के समावेशी होने के पक्ष में तर्क देने के बाद मैं फॉर्मल इकुवेलिटी का तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ I 2024 में प्रकाशित NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में 24 सदस्य हैं I 24 में से कम-से-कम 9 सदस्य ब्राह्मण हैं, जबकि 24 में से 17 सदस्य सवर्ण हैं I 24 में से 19 सदस्य पुरुष हैं और पांच सदस्य महिलाएं हैं I
कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में कम-से-कम 38% सदस्य ब्राह्मण है और 71%सदस्य सवर्ण हैं I जनसंख्या में जिनका रिप्रजेंटेशन 4% है छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में उनका रिप्रजेंटेशन 38% प्रतिशत है I इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण समिति के 79% सदस्य पुरुष हैं और 21% सदस्य महिलाएं हैं I इन आंकड़ों के आधार परयह बात आसानी से कहीं जा सकती है कि कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति वास्तव में सवर्ण पुरुषों की समिति है I
अब मैं आपके सामने फॉर्मल इकुवेलिटी का चौथा उदाहरण पेश कर रहा हूँ I 2007 में पहली बार प्रकाशित और 2022 में पुनर्प्रकाशित एनसीईआरटी की कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में 13 सदस्य हैं I इस समिति के 13 में से 10 सदस्य ब्राह्मण हैं और 12 सदस्य सवर्ण हैं I यानि 77% सदस्य ब्राह्मण हैं और 92% सदस्य सवर्ण हैं I जनसंख्या में जिनका रिप्रजेंटेशन 4% है कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में उनका रिप्रजेंटेशन 77% प्रतिशत है I 13 में से केवल दो सदस्य महिलाएं हैं I
तीसरे और चौथे उदाहरण के आधार पर यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति सवर्ण पुरुषों की समिति है तो एनसीईआरटी की ही कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ब्राह्मण पुरुषों की समिति है I
फॉर्मल इकुवेलिटी को समझाने के लिए चार उदाहरण देने के बाद मैं एक उदाहरण सबस्टेंटिव इकुवेलिटी को समझाने के लिए दे रहा हूँ I
अगर तमाम समितियों में विविधता को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाएँ और उनका पालन भी करवाया जाए तो इस तरह के नियम की ये कमजोरी हो सकती है कि रिप्रजेंटेशन को पेडागोजी से ज्यादा महत्त्वपूर्ण माना जाने लगे I इसलिए पाठ्यपुस्तक समितियों में सदस्यों की विविधता के साथ-साथ उनमें वैचारिक लोकतंत्र भी अनिवार्य है I
सबस्टेंटिव इकुवेलिटी का उदाहरण
NCERT की पाठ्यपुस्तकों के कुछ पाठों में विद्यार्थी की शैक्षिक जरूरतों और संवैधानिक नैतिकताओं से ज्यादा जरुरी किन्हीं जातियों की विश्व-दृष्टि को माना जा रहा है I उदाहरण के लिए NCERT द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसंत के एक पाठ “खान पान की बदलती तस्वीर” का विश्लेषण किया जा सकता है I इस पाठ की विषय-वस्तु और इस पाठ पर पूछे गये प्रश्नों के द्वारा केवल और केवल शाकाहारी समूहों की मान्यताओं का प्रचार किया जा रहा है I भारत के लोग मुख्यतः मांसाहारी हैं I भारत के करीब 70% लोग मांस खाते हैं I
केरल राज्य में करीब 100% लोग मांस खाते हैं I भारत की महिलाओं की तुलना में भारत के ज्यादा पुरुष मांस खाते हैं I क्योंकि पितृसत्ता के कारण पुरुषों का पैसे पर नियंत्रण रहता है और साथ ही वे घर के बाहर जाकर आसानी से खा लेते हैंI भारत के ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में भारत के शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादा मांस खाते हैं, क्योंकि पैसे का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। भारत के 35% ब्राह्मण मांसाहारी हैं। अमीरी बढ़ने के साथ-साथ शाकाहार बढ़ता है और गरीबी बढ़ने के साथ मांसाहार बढ़ता हैI
हमने देखा कि चाहे 2018 से हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में स्वर्ण के 77% होने का तथ्य हो ,और चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में केवल एक प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब विद्यार्थियों के होने का आंकड़ा हो, और चाहे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक समितियों में वंचित तबकों के सदस्यों की अनुपस्थिति का आंकड़ा हो, ये तीनों आंकड़े भारत की संस्थाओं, उसके प्रशाशन, और भारत के समाज के बारे में एक सच्चाई को एक बार फिर से सामने ले आए हैं कि जहां-जहां आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वहां-वहां वंचित और उत्पीड़ित समूहों के नागरिकों की पहुंच असंभव ही बनी हुई है।
ये आंकड़े अपने आप में इस बात को साबित करते हैं कि भारत में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी और अन्य पीड़ित तबकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का होना निहयतर जरूरी है। क्योंकि जहां कहीं भी आरक्षण का कानून लागू नहीं है, वहां वंचित और उत्पीड़न समूह के लोगों के आने के दरवाजे सदियों से बंद थे और अभी भी लगभग बंद ही हैं I
दलितों के लिए कोई होमलैंड नहीं है !
14 अप्रैल को डॉ. आंबेडकर का जन्म-दिन था I हम उनका जन्म-दिन क्यों मनाएँ? इसलिए भी कि हम जाँच कर सकें कि उनके समय से लेकर अब तक “ओप्प्रेसेड क्लासेज” के लोगों के मानवधिकारों पर कितना और किस तरह का फर्क पड़ा है I
हाईकोर्टस में जजों की नियुक्ति का मामला हो, निजी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के एनरोलमेंट का मामला हो, निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति का मामला हो, NCERT की पाठ्यपुस्तकों की निर्माण समिति में सदस्यों का मामला हो, या पाठ्यपुस्तकों के पथों के जरिए दिए जाने वाले संदेशों का मामला हो, इस तरह की सभी जगहों में प्रवेश करने के लिए दलितों, आदिवासियों, और अल्पसंख्यक समूह के लोगों को वीसा का इंतजार है I इन जगहों में प्रवेश किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसे तय करने का अधिकार क़ानूनी और व्यवहारिक तौर पर अभी भी काफ़ी हद तक सवर्णों के पास है और दलिट्स इस अन्तजार में हैं कि उन्हें इन जगहों में प्रवेश के लिए कभी वीसा मिलेगा I
यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि डॉ. आंबेडकर की आत्मकथा का नाम है “waiting for a visa”. अपनी आत्मकथा में डॉ. आंबेडकर को भारत में बैलगाड़ी में बैठने, मकान किराए पर लेने, मटके से पानी पीने, पढ़ने, नौकरी करने, सराय में रहने, इलाज करवाने आदि के लिए वीसा की जरुरत पड़ी I जबकि भारत के सवर्णों को इस प्रकार के कामों और मौकों के लिए वीजा की जरूरत न तो तब पड़ती थी, और न ही अब पड़ती हैI
अपने ही देश में दलितों के साथ विदेशियों से भी बुरा व्यवहार तब भी किया जाता था, और अब भी किया जाता है I मेरे राज्य उत्तराखंड के सवर्ण किसी विदेशी को तो अपना मकान किराए पर दे देंगे लेकिन उत्तराखंड के ही किसी दलित को नहीं देंगे I उत्तराखंड के लोग किसी विदेशी को अपनी किचन में आदर के साथ बिठाकर भोजन करवा लेंगे, किसी दलित को अपने आँगन में बैठने तक नहीं देते I इसलिए कहा कि भारत में, भारत के लोग, भारत के दलितों के मानवाधिकार विदेशियों से भी कम मानते हैं I
सौ साल पहले, डॉ. अम्बेडकर को भारत में जिन जगहों पर जाने के लिए सवर्ण होने का वीजा माँगा गया था, उन्हीं जगहों पर जाने के लिए दलितों से आज भी सवर्ण होने का वीजा माँगा जा रहा है I चाहे वह जगह भारत के हाईकोर्ट में जज बनना हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी बना हो, वहाँ टीचर या कर्मचारी बनना हो या शैक्षिक संस्थानों की विभिन्न समितियों में सदस्य बनना हो I इन तमाम जगहों के लिए आज भी सवर्ण होने का वीजा मांगा जा रहा हैI
भारत के वर्तमान और इतिहास को देखते हुए यह समझना जरुरी है कि वह कौन सी हतासा रही होगी जब पूना पेक्ट के दौरान डॉ. आंबेडकर ने गाँधी से कहा होगा कि उनका कोई होमलैंड नहीं हैI
और अंत में उत्तराखंड के शानदार कवि मोहन मुक्त के काव्य-संग्रह हिमालय दलित है से एक कविता सुनिएI कविता का शीर्षक है “आंबेडकर की नज़र”।
नज़र…
ज़रूरी नहीं कि
नैपोलियन…
ख़ून से सनी तलवार लिये
बख़्तरबंद पहने हुए
सवार होकर आये घोडे पर
वह अधनंगा…
लकड़ी की चप्पल पहने हो सकता है
ज़रूरी नहीं कि
वह कहलाना चाहे विश्व विजेता
हो सकता है उसे शांतिदूत की उपाधि पसंद हो
लेकिन याद रहे…
नैपोलियन हमेशा होता है हिंसक
आमरण अनशन अहिंसा नहीं, हिंसा होती है
कास्त्रो के कांधे पर बैठा कबूतर
नेहरू की अचकन में टंगा गुलाब
और गोर्वाचेफ के माथे पर बने
बाइबिल के निशान तो दिख जाते हैं सभी को लेकिन…
यरवदा की जेल के भीतर
अनशन पर बैठे…
गांधी के सर पर…
नैपोलियन का टोप देखने के लिये…
आंबेडकर की नज़र चाहिए …
(बीरेंद्र सिंह रावत, शिक्षा विभाग, दिल्ली-विश्वविद्यालय)
Links:
1. संघ की सामाजिक समरसता की अवधारणा के पीछे छिपा झूठ
2. Gujarat: Dalit teenager tied to tree and beaten up in Patan, police arrest two men
- NCERT. Class VI Hindi. Malhar.
- NCERT. Class VII Hindi. Vasant.
- 77% of high court judges appointed since 2018 from upper castes. https://indianexpress.com/article/india/law-ministry-parliament-high-court-judges-appointed-upper-castes-9906965/
- India’s top 30 pvt universities have 5% SC students, less than 1% ST students