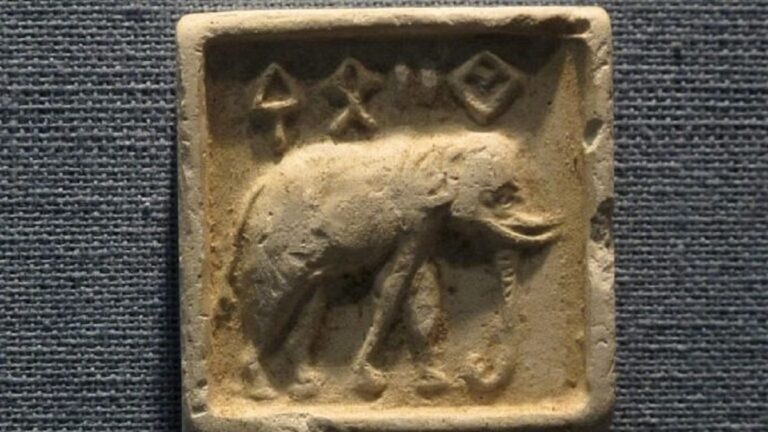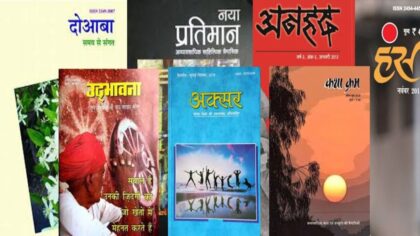पहलगाम में हुई हत्याओं को लेकर कश्मीरी लोगों ने जिस मानवीयता और दरियादिली का परिचय दिया, वह आज के भारत के लिए एक मिसाल है। इसके सामने हिंदुत्व की नफरत की राजनीति करने वालों को रखें, तो उनकी सारी विकृतियाँ और हैवानियत का चेहरा और अधिक साफ दिखने लगता है। लेकिन जब शोर हो और शोर करने वालों की संख्या बहुसंख्यक दिखने लगे, तब ऐसे उदाहरण बेबस उदाहरण बनकर रह जाते हैं।
पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद देश में युद्ध का शोर बढ़ गया है। ‘मिट्टी में मिला देने’ की बात जिस तरह और जहाँ से आई, वह किसी नाटक में बोले गए एक संवाद-सी थी। इस संवाद से पहले युद्ध के शोर पर उछल-कूद करने वाली मीडिया अपने लिए फुटेज ढूँढ़ने में व्यस्त थी और पुराने क्लिप भी चला रही थी। सोशल मीडिया पर धर्म-युद्ध की भाषा का प्रयोग खुलेआम शुरू हो गया था। बेरोक-टोक ललकारने की भाषा सड़कों को खून से भर देने की उतावली में बदलने के लिए बेचैन दिख रही थी।
अभी कुछ दिन पहले, जब पहलगाम की घटना नहीं हुई थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ‘गृहयुद्ध’ छेड़ने का आरोप लगा दिया। वक्फ को लेकर बनाए जा रहे कानून पर उठे सवालों को हल करने के बजाय युद्ध जैसी भाषा का प्रयोग क्यों किया गया? इसके कुछ दिन पहले, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक रामनवमी के अवसर पर निकले जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन और कई जगहों पर मस्जिदों व मकबरों पर भगवा झंडा लहराने का माहौल बनाया गया। यह सड़क पर धर्म-युद्ध उतार लाने वाले दृश्य से कम भयावह नहीं था।
इन्हीं दृश्यों से एक हफ्ते पहले, जब मस्जिदों को सुरक्षित करने के नाम पर तिरपाल से ढँक दिया गया और सड़क पर नमाज़ पढ़ने को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया, तब का दृश्य मानो आने वाले समय का एक प्रदर्शन बन रहा था। आगरा में एक खास जाति के लोग एक सांसद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जिस तरह जमा हुए और हथियारों का खुलकर प्रदर्शन किया गया, वह दृश्य किसी भी लोकतंत्र के मुँह पर तमाचा था। प्रदर्शनों को लेकर जिस तरह की पक्षधरता दिखाई गई, उससे इतना तो ज़रूर लगने लगा कि यह देश कुछ लोगों के हिस्से में अधिक हो गया है।
लेकिन सवाल वही है: अपने देश में युद्ध का इतना शोर क्यों है? क्यों कोई और आवाज़ गुम कर दी जा रही है? न्यायाधीशों से लेकर विपक्षी नेताओं, आदिवासियों से लेकर धार्मिक समुदायों, यहाँ तक कि कई हिंदू मठाधीशों, छात्रों से लेकर आम मज़दूर कार्यकर्ताओं पर युद्ध छेड़ने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप कहीं और से नहीं, सत्तापक्ष और उसकी पार्टी व संगठनों से आ रहे हैं।
हालाँकि, ऐसे लोग किसी युद्ध की बात नहीं कर रहे होते, लेकिन उन पर यही आरोप लगाया जाता है। और जो लोग खुलेआम युद्ध की बात कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्रभक्तों की श्रेणी में गिना जा रहा है। ऐसे लोग तब नहीं उबलते, जब अपने देश के नागरिकों को अमेरिका हथकड़ियों में बाँधकर अपने सैन्य विमानों से भारत भेजता है, जब भारत पर टैरिफ थोप दिया जाता है, या जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहता है। यही स्थिति चीन को लेकर है। तब क्या यह माना जाए कि भारत में राष्ट्रवाद का उन्माद तभी पैदा होता है, जब उसमें धर्म का पक्ष जुड़ जाए? या इसके अलावा भी कोई और बात है?
राजनय की भाषा में कहें तो गृहनीति का विस्तार ही विदेश नीति होती है। भारत की गृहनीति क्या है? भारत पिछले 15 सालों से विकास की ऊँचाइयाँ छूने का दावा कर रहा है, लेकिन सारे दावों के बावजूद अपने समकालीन अर्थव्यवस्थाओं से पीछे छूटता गया है। आज चीन अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है।
भारत एक उत्पादक देश की बजाय सेवा प्रदान करने वाली अर्थव्यवस्था में बदलता गया है। कई मानकों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत का राजकीय खर्च का बड़ा हिस्सा गैर-उत्पादक करों और नौकरीपेशा लोगों की आय से आ रहा है। अपरोक्ष कर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों से खर्च निकाला जा रहा है। विनिर्माण के आँकड़े न तो रोज़गार सृजन के साथ मेल खा रहे हैं और न ही पूँजी निर्माण की माँग को पूरा कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात, पिछले दस सालों से खेती का संकट न केवल आय के मामले में, बल्कि रोज़गार के मामले में भी बढ़ा है। खेती पर जन दबाव बढ़ा है। मज़दूरों की आय निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही मूल्यों में घटती दिख रही है, जबकि कॉरपोरेट की आय हर तरह से कई गुना बढ़ रही है। ऐसी आय, जो उत्पादन की ज़मीन पर न होकर कहीं और से हो रही है। इस आय को अब खुली लूट का नाम दिया जा रहा है।
भारत की जो अर्थव्यवस्था की गृहनीति है, उसका विस्तार हमें विदेश नीति में कतई नहीं दिखता। भारत की भूमि चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ी है। भारत जिस तरह इतिहास और भूगोल की बात पाकिस्तान के साथ करता रहता है, वैसा किसी अन्य देश के साथ नहीं दिखता, जबकि चीन और भारत एक-दूसरे पर ज़मीन कब्ज़ा करने का आरोप लगाते रहे हैं और हिंसक झड़पों में दो-चार भी होते रहे हैं।
पिछले 15 सालों में भारत की विदेश नीति, जिसमें भारत ‘विश्व गुरु’ बनने का दावा करने लगा था, उसका मानमर्दन अमेरिका ने भारत के नागरिकों को हथकड़ियों में बाँधकर अपने सैन्य विमानों से भारत की धरती पर पहुँचाकर कर दिया। यूरोप की यात्राओं का अंतिम नतीजा अभी भी रूस से हासिल कच्चे तेल को साफ कर उसे बेचने से आगे नहीं जा सका। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय इस्पात की खरीद पर कई सवाल खड़े किए। विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा एक जमींदार की ढहती हवेली जैसा ही दर्दनाक है, जिसमें घर है, ज़मीन है, लोग हैं… बस आगे जाने का शौर नहीं है।
भारत की विदेश नीति की असफलता को सफलता में बदलने की सारी कवायद हम या तो नेताओं की बयानबाज़ी में देख सकते हैं या गोदी और सोशल मीडिया के धुरंधरों द्वारा बनाए गए अनगिनत झूठों में। कभी हम ट्रंप और पुतिन को संगम पर नहाने वाली खबरों में देखते हैं, तो कभी युद्ध रुकवा देने वाले प्रचार में।
लेकिन यह सवाल ज़रूर है कि भारत की गृहनीति में युद्ध की भाषा और शब्दों का प्रयोग इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ा है? देश में विचारों की जगह शोर का प्रभाव इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? इस देश का एक उद्योगपति मुर्गी बचाने वाले की तरह दिखाकर क्या संदेश देना चाहता है? एक उद्योगपति 70 घंटे काम करने की माँग करता है, जबकि सच्चाई यह है कि मज़दूर इतना काम एक स्थिर मूल्य सूचकांक पर गिरती मज़दूरी पाकर भी कर रहा है। अडानी पर आए दिन आने वाली खबरें मानो दम तोड़ने के लिए अभिशप्त हैं। फिल्मों में बायोपिक बनाने की होड़-सी लग गई है और उन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया। लेकिन ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म क्यों अटक गई? इन सारे सवालों के पीछे एक ही सवाल है: भारत में जो चल रहा है, वह किस नीति का प्रदर्शन है?
जिस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी पूँजी हो, वहाँ इससे पैदा हुए अंतर्विरोधों को हल करना ही इसकी राजनीति होती है। कहते हैं, पूँजी का कोई धर्म नहीं होता। भारत में, और विस्तार में जाएँ तो पूरे दक्षिण एशिया में, यह बात उतनी सच नहीं है। यहाँ धर्म ने पूँजी का दामन थामा और पूँजी ने विस्तार के लिए धर्म की पीठ पर सवारी की। दक्षिण एशियाई देशों की राजनीति में यह परिलक्षित होता है और पार्टियों में अभिव्यक्त भी होता है।
यहाँ पूँजी का संकट धर्म के संकट में बदलता दिखता है। इस हिस्से में भारत एक बड़ा देश है। अपने देश में क्या हो रहा है? 1980 के दशक में इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी ने धर्म का प्रयोग भारत की अर्थव्यवस्था में पैदा हुए अंतर्विरोधों को हल करने में किया था। कांग्रेस की मनमोहन सरकार की असफलता पर गुजरात मॉडल पेश किया गया।
आज उस मॉडल की बात करने वाले ही मोदी की असफलता पर किताबें लिख रहे हैं। विकास का ख्वाब युद्ध के शोर में बदलता गया है। राजनीति में बेबसी एक स्थायी भाव में बदल गई है। पिछले दस सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुज़रा, जब युद्ध के उन्माद की भाषा और कई बार युद्ध हो जाने की आशंका हमें छूते हुए नहीं गुज़री हो। हमें यह ज़रूर पूछना चाहिए: क्या इनसे इस देश की अर्थव्यवस्था और इससे पैदा हुआ संकट हल हो रहा है, या यह और तबाही की ओर जा रहा है?
मैं कई बार देश की राजनीति को उस फैक्ट्री मालिक के व्यवहार की तरह देखता हूँ, जिसमें जब मालिक को मज़दूरों की छँटनी करनी होती है, तब वह मज़दूरों के समूह पर कामचोरी, फैक्ट्री को नुकसान पहुँचाने, या मालिक के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाता है। फिर उन्हें काम से निकालने की नोटिस दे देता है। विरोध करने पर अपने गुंडों से पिटवाता है और साथ ही वैधानिक कार्रवाई का रास्ता अपनाता है। हमारे यहाँ इस फैक्ट्री व्यवस्था से कहीं अधिक बदतर स्थिति बना दी गई है।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं)