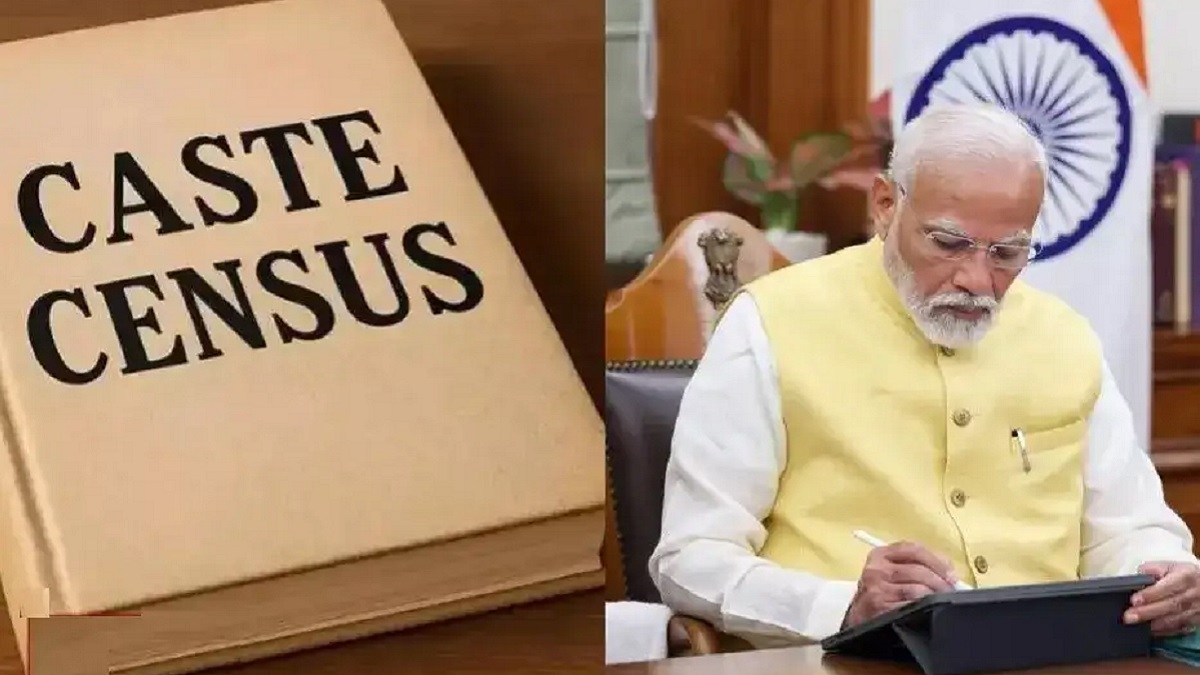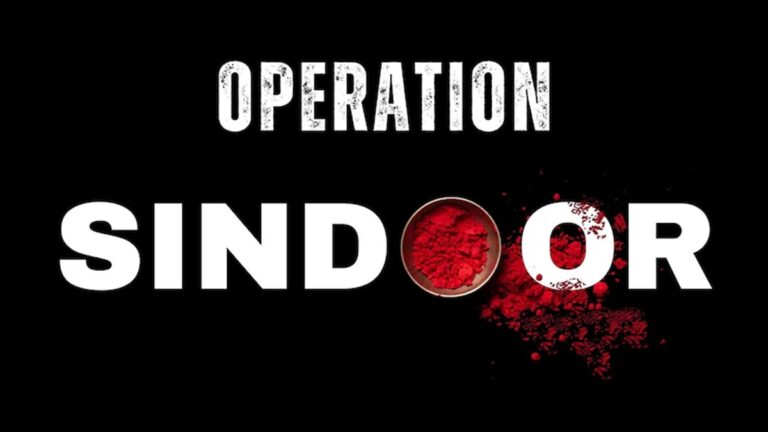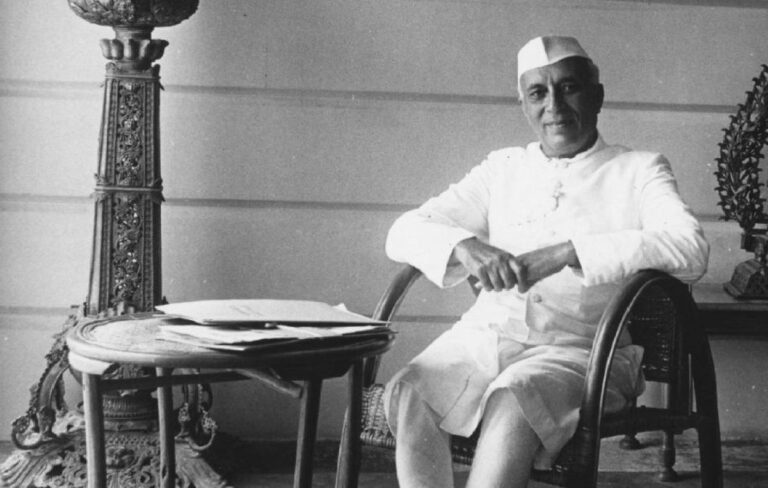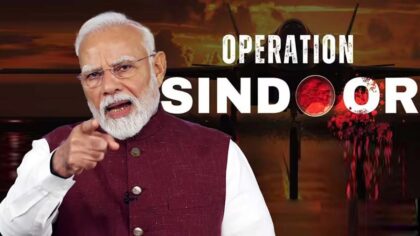5 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी आदेश के जरिए प्रदेश के स्कूलों में इस साल की गर्मी की छुट्टियों के दौरान रामायण और वेद पर आधारित कार्यशालाएं अनिवार्य कर दी हैं।
यह आदेश एक आईएएस अधिकारी संतोष कुमार शर्मा की ओर से जारी किया गया है। शर्मा अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के निदेशक हैं। यह संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया है। संस्थान के निदेशक ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को गर्मी की छुट्टियों में अपने-अपने कार्यक्षेत्र में रामायण और वेद से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित करने की व्यवस्था करने को कहा है।
कार्यशालाएं कम-से-कम पांच और अधिक-से-अधिक दस दिनों की होंगी। जिन स्कूलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, उनकी सूची भी अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रदान की गई है। इन कार्यशालाओं के समन्वयकों की सूची भी संस्थान द्वारा ही तैयार की गई है, और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उसी के अनुसार कार्य करना होगा। यदि कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी समन्वयक को बदलता है, तो उसे इसकी सूचना संस्थान के निदेशक को देनी होगी।
इन कार्यशालाओं में विद्यार्थियों को रामचरितमानस और वेदों का गायन सिखाया जाएगा। साथ ही, वेदों से संबंधित सामान्य जानकारी दी जाएगी। कार्यशालाओं में रामायण पर आधारित चित्र बनाना भी सिखाया जाएगा। क्या राम द्वारा शंबूक की हत्या के चित्रों को स्वीकार और सराहा जाएगा? शंबूक, जो एक शूद्र था, को वाल्मीकि रामायण में पढ़ाई करने के कारण मार दिया गया था, क्योंकि उसे वर्णव्यवस्था के अनुसार पढ़ने की अनुमति नहीं थी। चित्रकला के अलावा, इन कार्यशालाओं में रामायण के पात्रों के मुखौटे बनाना भी सिखाया जाएगा।
इस सरकारी आदेश के खिलाफ डॉ. चतुरानन झा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। डॉ. झा The All India Forum for Right to Education (AIFRTE) से भी जुड़े हैं। इस फोरम का गठन 2009 में हुआ था, और इसका उद्देश्य भारत में सभी बच्चों के लिए समान गुणवत्ता वाली, सामान्य स्कूल प्रणाली पर आधारित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाना है।
अच्छा हुआ कि सरकार के इस असंवैधानिक आदेश के खिलाफ डॉ. झा ने हाईकोर्ट में PIL दायर की है। मैं इस सरकारी आदेश को असंवैधानिक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत की संविधान सभा ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुदेशन (religious instruction) देने से इनकार किया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक अनुदेशन को असंवैधानिक मानता है। यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।
12 सितंबर 2002 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुदेशन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 28 धार्मिक अनुदेशन पर रोक लगाता है, लेकिन धर्मों के बारे में शिक्षा (education about religions) पर रोक नहीं लगाता।
अनुदेशन और शिक्षा
प्रश्न यह है कि अनुदेशन (instruction) और शिक्षा (education) में क्या अंतर है? अनुदेशन का उद्देश्य यह होता है कि प्राप्तकर्ता उसका पालन करें और उसके अनुसार आचरण करें। अनुदेशन देने की प्रक्रिया में सारी शक्ति अनुदेशक के पास होती है, और दूसरों को केवल अनुदेशों का पालन करना होता है। अनुदेशन के विपरीत व्यवहार को गलत माना जाता है। अनुदेशन की प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता शक्तिहीन होता है और उसे अनुदेशों का यांत्रिक रूप से पालन करना पड़ता है। अनुदेशन में बताई गई बातों को मानना अनिवार्य होता है।
इसके विपरीत, शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के पास तथ्यों और विचारों के आधार पर किसी बात को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होती है। शिक्षा में शिक्षक द्वारा बताई गई बातों का पालन करने की अपेक्षा नहीं होती। विद्यार्थी को शिक्षक की बातों से असहमत होने का अधिकार होता है। शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहस और विवाद के लिए सम्मानजनक स्थान होता है। शिक्षा की प्रक्रिया में बताई गई बातों का आलोचनात्मक विश्लेषण (critical analysis) और मूल्यांकन (critical evaluation) अपेक्षित होता है, जबकि अनुदेशन में ऐसा करने की न तो अपेक्षा होती है और न ही अनुमति। शिक्षा में आलोचनात्मक विश्लेषण को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि अनुदेशन में इसे गलत माना जाता है।
इसलिए, अनुदेशन अनुयायी (followers) पैदा करता है, जबकि शिक्षा विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, और समाज सुधारक पैदा करती है। यही कारण है कि संविधान में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक अनुदेशन को असंवैधानिक माना गया है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी स्कूल में यह पढ़ाया जाता है कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे, तो क्या उत्तर प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे इस बात का आलोचनात्मक विश्लेषण करें? क्या उनके पास यह पूछने का अधिकार होगा कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे, इसके प्रमाण क्या हैं? यदि विद्यार्थियों को यह अधिकार नहीं होगा, तो यह धार्मिक अनुदेशन होगा, जो सरकारी स्कूलों में असंवैधानिक है।
इसी तरह, यदि किसी निजी मदरसे में पढ़ाया जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे और विद्यार्थियों को इसके पक्ष में प्रमाण मांगने का अधिकार नहीं है, तो यह धार्मिक अनुदेशन है, लेकिन यह संविधान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि यह निजी संस्थान में हो रहा है। लेकिन यदि यही बात सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो यह असंवैधानिक हो जाता है।
इसी प्रकार, मंदिर में यह कहना कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे, असंवैधानिक नहीं है। लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भगवान राम या हजरत मोहम्मद के बारे में बिना आलोचनात्मक विश्लेषण के अनुदेशन देना असंवैधानिक है। अर्थात, जो बातें मंदिर या मदरसे में संवैधानिक हैं, वही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में असंवैधानिक हो जाती हैं।
अपनी संस्कृति, पराई संस्कृति: फूट डालो, राज करो
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि इन कार्यशालाओं का उद्देश्य “बच्चों में अपनी संस्कृति के संस्कार” विकसित करना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि “अपनी संस्कृति” किसकी संस्कृति है और इसके जरिए विद्यार्थियों में किस तरह के संस्कार डाले जाने हैं?
उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान भी कार्यरत हैं। तो क्या बौद्ध संस्कृति और जैन संस्कृति “अपनी संस्कृति” नहीं हैं? क्या केवल रामायण और वेदों पर आधारित संस्कृति ही “अपनी संस्कृति” है? क्या भारत का संविधान संस्कृति की इस संकीर्ण और सीमित समझ को स्वीकार करता है?
उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान, 0.7% बौद्ध, और 0.12% जैन आबादी है। 19% आबादी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत कोई अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम शोध संस्थान नहीं बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मुस्लिम संस्कृति “अपनी संस्कृति” के दायरे में नहीं आती। सरकार के दृष्टिकोण से मुस्लिम संस्कृति “पराई संस्कृति” है।
हालांकि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं, लेकिन बौद्ध और जैन संस्कृतियाँ भी उत्तर प्रदेश की “अपनी संस्कृति” के दायरे में शामिल नहीं हो पाई हैं।
कुछ समय पहले उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए धार्मिक ग्रंथों की सामग्री को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी कह चुके हैं कि भगवद्गीता में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड ने गुजरात से दो कदम आगे बढ़कर स्कूली पाठ्यक्रम में गीता के साथ-साथ वेद, रामायण, और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों को शामिल करने की घोषणा की थी।
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की घोषणा के समय भी दो प्रमुख सवाल उठे थे:
- जिस “अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा” की बात की जा रही है, क्या वह उत्तराखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए “अपनी” है? क्या उत्तराखंड के दलित ब्राह्मणवादी उत्पीड़नकारी ज्ञान परंपरा को “अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा” मानते हैं? क्या उत्तराखंड की महिलाएँ पितृसत्तात्मक परंपराओं को “अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा” मानती हैं?
- शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अनुदेशन देने के बारे में भारत का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है?
उत्तराखंड: किसकी संस्कृति, किसकी परंपरा
उत्तर प्रदेश के स्कूलों में रामायण और वेद से संबंधित कार्यशालाओं के आदेश पर लौटने से पहले मैं उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता पर कुछ बातें करना चाहता हूँ।
उत्तराखंड के इतिहासकार प्रो. शेखर पाठक ने अपनी पुस्तक दास्तान-ए-हिमालय (भाग 2) के पृष्ठ 74 और 75 पर लिखा है कि शिल्पकार, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। इसके बावजूद, उन्हें समाज के सबसे निचले तबके में रखा जाता है। उन्हें आज भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, और वे धार्मिक यात्राओं में शामिल नहीं हो सकते। वे शिक्षा और रोजगार से भी काफी हद तक वंचित हैं।
प्रो. पाठक ने उसी पुस्तक के पृष्ठ 111 पर लिखा है कि उत्तराखंड की निम्न जातियों, जो जनसंख्या का 10% हैं, के पास केवल 2% जमीन है। गढ़वाल राजाओं के समय में निम्न जातियों को जमीन और मकान रखने का अधिकार नहीं था, और यह परंपरा औपनिवेशिक काल में धीरे-धीरे समाप्त होने लगी।
क्या भेदभाव और उत्पीड़न की ऐसी परंपराएँ भी “अपनी संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा” का हिस्सा हैं? वह कौन-सी “संस्कृति और समृद्ध ज्ञान परंपरा” है, जिसके आधार पर उत्तराखंड में आज भी दलितों के साथ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएँ सामने आती रहती हैं? क्या उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित धार्मिक शिक्षा से विद्यार्थियों में जाति, धर्म, और नस्ल से संबंधित अत्याचारों और उत्पीड़न के प्रति आलोचनात्मक समझ विकसित होगी? क्या यह शिक्षा संसाधनों के असमान वितरण के कारणों और उनके समाधान की समझ पैदा कर सकती है?
जिन धार्मिक ग्रंथों को उत्तराखंड के स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात की जा रही है, वे एक विशेष समुदाय से संबंधित हैं, जबकि उत्तराखंड में अनेक समुदाय रहते हैं। भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक उत्तराखंड की भाषाएँ के संपादकीय में उमा भट्ट और शेखर पाठक लिखते हैं कि उत्तराखंड को किसी एक धार्मिक समुदाय के धार्मिक ग्रंथों से जोड़ना न तो ऐतिहासिक और न ही नैतिक रूप से उचित है।
वे लिखते हैं कि उत्तराखंड में शिल्पकार, शौका, वनराजी, थारू, बोक्सा, गूजर, नेपाली, और मध्यकाल व आधुनिक काल में आई विभिन्न स्वर्ण जातियों और जनजातियों की उपस्थिति इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। उनके अनुसार, उत्तराखंड को “आर्यों का देश” कहा गया है, लेकिन आर्यों से पहले यहाँ अन्य मानव समूह रहते थे। उदाहरण के लिए, खस समुदाय ऋग्वैदिक आर्यों से पहले यहाँ निवास करता था। कोल और मंगोल जैसे मानव समूह भी यहाँ रहते थे।
उमा भट्ट और शेखर पाठक के अनुसार, मुंडा मानव समूह से जुड़े कोल उत्तराखंड के सबसे पुराने निवासी हैं और उन्हें ऑस्ट्रो-एशियाटिक समूह का हिस्सा माना जाता है। शिल्पकार समुदाय कोल मानव समूह का प्रतिनिधित्व करता है और उत्तराखंड के लोक जीवन की अधिकांश अभिव्यक्तियों, उपकरणों के निर्माण, और तकनीकों का आविष्कारक व संरक्षक रहा है। इस समुदाय ने उत्तराखंड की नदियों, गधेरों, और बस्तियों के नाम रखे, जो आज भी प्रचलित हैं। लेकिन जब “अपनी संस्कृति” की बात होती है, तो उत्तराखंड का समाज, शासन, और राजनीति इन समुदायों को जानबूझकर “अपनी संस्कृति” के दायरे से बाहर रखते हैं।
प्रो. पाठक लिखते हैं कि आर्य जाति संभवतः हिमालय के उत्तर-पश्चिमी मार्गों से भारत में आई थी। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि आर्यों के आने से पहले उत्तराखंड में द्रविड़ समुदाय रहता था। ऐसी विविधता से भरे प्रदेश को एक समुदाय का प्रदेश बताने का प्रयास इतिहास के प्रति अज्ञानता या अनदेखी को दर्शाता है।
उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है। इतनी बड़ी आबादी को “अपनी संस्कृति” के दायरे से बाहर रखना न तो राज्य के विकास के लिए और न ही भारत के संविधान की मूल भावना के अनुकूल है। ऐसा कोई प्रयास प्रदेश की समृद्धि के लिए हानिकारक हो सकता है।
धार्मिक शिक्षा नहीं, धर्मों के बारे में शिक्षा
अब हम दूसरे सवाल पर लौटते हैं: शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अनुदेशन देने के बारे में भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 28 स्पष्ट रूप से कहता है कि “राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।” यह अनुच्छेद सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें जिन स्कूलों में वेद, गीता, और रामायण से संबंधित पाठ पढ़ाना चाहती हैं, वे जनता के धन से संचालित हैं। इसलिए, संवैधानिक रूप से उनमें धार्मिक अनुदेशन नहीं दिया जा सकता।
12 सितंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 28 की व्याख्या करते हुए कहा कि यह धार्मिक अनुदेशन पर रोक लगाता है, लेकिन धर्मों के बारे में शिक्षा पर रोक नहीं लगाता। धर्मों के बारे में शिक्षा का अर्थ है कि इसमें किसी धर्म के संस्कार, अनुष्ठान, या पूजा-पद्धति से जुड़े निर्देश नहीं दिए जा सकते।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा के बीच की रेखा बहुत पतली है। इसलिए, धर्मों के बारे में शिक्षा देने की आड़ में धार्मिक अनुदेशन देने से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मों के बारे में पाठ्यक्रम तैयार करते समय धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा के बीच अंतर बनाए रखना अनिवार्य है।
धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा के बीच अंतर को समझने के लिए हम डॉ. बी.आर. आंबेडकर के विचारों की ओर चलते हैं। 7 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में इस विषय पर उठे सवालों का जवाब देते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा कि धार्मिक अनुदेशन को धर्मों के अध्ययन या अनुसंधान से अलग करना चाहिए। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि इस्लाम में हजरत मोहम्मद को अंतिम पैगंबर माना जाता है। इस विश्वास को पढ़ाना धार्मिक अनुदेशन है, जिसे उन्होंने “धर्मसिद्धांत” (dogma) कहा। उन्होंने कहा कि धर्मसिद्धांत और अध्ययन (study) में बहुत अंतर है।
धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा के बीच अंतर तभी बनाया जा सकता है, जब विद्यार्थियों को संदेह करने, सवाल उठाने, विश्लेषण करने, तुलना करने, मूल्यांकन करने, और बताई गई बातों को न मानने का शैक्षिक अधिकार हो।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि धर्मों के बारे में शिक्षा का पाठ्यक्रम “धार्मिक बहुलतावाद” (religious pluralism) पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट के अनुसार, धार्मिक बहुलतावाद विशेषतावाद (exclusivism) का विरोध करता है और समावेशवाद (inclusivism) को प्रोत्साहित करता है। धर्मों के बारे में शिक्षा बिना मतारोपण (indoctrination) और स्वतंत्र चिंतन (free thinking) को बाधित किए दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी अपने और दूसरों के धर्मों को समझ सकें, लेकिन इसका अर्थ उनके अनुसार जीवन जीना नहीं है।
धर्मों के बारे में शिक्षा का मतलब किसी विशेष पूजा-पद्धति या धार्मिक मूल्यों को अपनाने का प्रशिक्षण देना नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के 5 मई 2025 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि रामायण और वेद पर आधारित कार्यशालाएँ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण (training) देने के लिए हैं, न कि शिक्षा प्रदान करने के लिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि धर्मों के बारे में शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में व्यवहार विकसित करने का एक माध्यम हो सकती है। यह विद्यार्थियों को अपने और अन्य नागरिकों के धर्मों को समझने में मदद करती है। इसके अलावा, यह विभिन्न धर्मों की आंतरिक कमियों को पहचानने और लोकतांत्रिक व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए, धर्मों के बारे में शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी पितृसत्ता और असमानता जैसे सिद्धांतों को पहचान सकते हैं और अपने व्यवहार को अधिक लोकतांत्रिक बना सकते हैं।
राज्यों को क्या करना चाहिए?
यदि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, या कोई अन्य राज्य सरकार अपने स्कूली पाठ्यक्रम में धर्मों के बारे में शिक्षा शामिल करना चाहती है, तो उसे संवैधानिक रूप से दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा:
- धार्मिक बहुलतावाद: सरकार को अपने राज्य में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन करवाना होगा ताकि पाठ्यक्रम में सभी धर्मों को समान रूप से शामिल किया जा सके।
- अनुदेशन बनाम शिक्षा: सरकार को “धार्मिक अनुदेशन” और “धर्मों के बारे में शिक्षा” के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझकर पाठ्यक्रम तैयार करना होगा।
यदि ये दो शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो इससे न केवल विभिन्न धर्मों के प्रति अज्ञानता के कारण कट्टरता और असहिष्णुता बढ़ेगी, बल्कि अपने ही धर्म के प्रति आलोचनात्मक समझ का अभाव भी पैदा होगा। ये दोनों बातें लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं।
(बीरेंद्र सिंह रावत, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय)