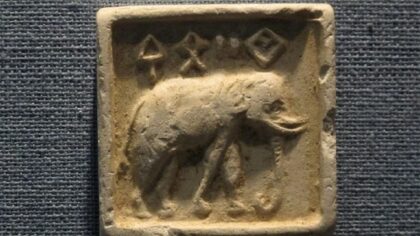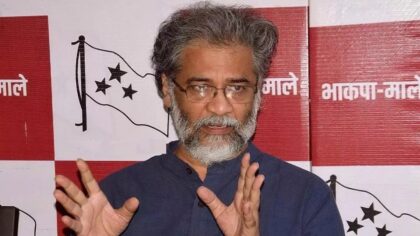कैंसियन अर्थनीति को नकारते हुए जब नव उदारवादी नीति को अपनाया जा रहा था तब अंतरराष्ट्रीय बाजार के बड़े पैरोकारों ने यह दावा किया था कि जब बाजार फेल होगा तो सरकार को अपने कदम खींच लेने चाहिए और निजी निवेशकर्ताओं को उसकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। इस दावे के साथ एक और दावा था जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार कभी फेल हो ही नहीं सकता, निराश कर ही नहीं सकता। क्या यह हकीकत है या महज जुमला, इसका प्रमाण हम देख ही चुके हैं जब विश्व 2008 के सदी के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और अभी तक ढंग से उबर नहीं पाया। जब 1997–98 में एशियन टाइगर्स (सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान तथा थाईलैंड) की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी जो इससे पूर्व पूरी तरीके से नई अर्थनीति के पीछे बढ़ चुके थे।
बजट के आते के साथ ही तमाम अर्थशास्त्री बजट के आंकलन और उसके प्रभाव को देखने-जानने में लग गए हैं। जिसमें कई लोगों ने अपने विश्लेषण में कहा है कि यह अमीरों के लिए बजट है, राजकोषीय खर्च लोगों के लिए कम किए गए हैं, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है। परन्तु इन सब में कुछ भी नया नहीं है। यह निरंतर प्रत्येक बजट में एक बढ़ते ट्रेंड के साथ आगे बढ़ा है। अर्थव्यवस्था में नवोन्वेश के नाम पर लगातार “मुद्रास्फीति को नियंत्रित” रखने की कवायद को दोहराया गया है। परन्तु ऐसा ही क्यों हो रहा है, सरकार लगातार एक ही प्रकार के शब्दों को अलग-अलग तरीके से हर अगली बजट में क्यों पेश कर रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास हमेशा इसका एक सरल और सीधा जवाब है जो देशवासियों के लिए प्रभावकारी भी है, कि इससे भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, हमारे यहां बड़ी कंपनियां निवेश करने आएंगी, और उससे हमारी अर्थव्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी। इस लेख में मैं इन्हीं तीन बिंदुओं को खोलने का प्रयास करूंगा, परन्तु सतही रूप से वर्तमान बजट के आंकड़ों को थोड़ा सा नीचे रखकर। अगले लेख में हम उसके आंकड़ों के साथ भी बात करेंगे।
1943 में कलेकी नाम के एक अर्थशास्त्री ने एक घोषणा की जो कार्ल मार्क्स के “रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर” की संकल्पना से मिलती जुलती है जब उन्होंने यह कहा कि भविष्य में भी लेबर की मांग और उनके विद्रोहियों को कुचलने के लिए एक “साइकिलिक इकॉनमी” के तौर पर बेरोजगारी के चक्र को चलाया जाता रहेगा जिसके कारण मजदूरों की व्यापक छंटनी कर दी जाएगी और श्रम बाजार में मांग लगातार उच्च बनी रहेगी और मजदूर कम वेज (मजदूरी) पर भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे।”
आखिर यह अर्थशास्त्री 1943 में ऐसा क्या देख पा रहा था जिसके कारण वह आने वाले तीस साल पहले का मूल्यांकन कर सकता था और आखिर कार्ल मार्क्स क्या देख रहा था जो आने वाले दो सौ साल के आगे की बात देख पा रहा था। इसलिए मेरा मत है कि अर्थशास्त्रीय नीति को बनाते हुए आप कौन सी विचारधारा केंद्र में रखते हैं इससे तय होगा कि आप किसके हित में नियम बनाते है। इसलिए केवल यह कह देना कभी भी काफी नहीं है कि कोई सरकार अर्थनीति बना रही है बल्कि उसे पूरा करना बेहद जरूरी है कि किस वर्ग के हित के लिए मूलतः नीति बना रही है। बहरहाल जब केलेकी ने जब यह दावा किया तब दुनिया के बड़े यूरोपीय देश केन्सियन अर्थनीति का अनुपालन कर रहे थे।
कैंसियन अर्थनीति के केंद्र में डोमेस्टिक मार्केट था अर्थात घरेलू बाजार। जिसमें सरकार का मुख्य ध्यान घरेलू मांगों में वृद्धि पर था और उसके द्वारा मांग का संचालन करना था। जिससे रोजगार के सृजन में वृद्धि हुई और लोगों के क्रय की क्षमता बढ़ने लगी। परन्तु यह व्यवस्था बाहरी प्रभावों को काफी नियंत्रित करती थी जिसे बाहरी वित्तीय पूंजी का प्रभाव भी कहते है।
बाहरी वित्तीय पूंजी से ही विकास संभव है इस संकल्पना को रशिया ने पहले ही खारिज कर दिया था जब 1917 में जारशाही को समाप्त करने वाला रसिया महज 10-12 साल में दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के समकक्ष आने लग गया था। कैंसियन अर्थतंत्र ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का काम किया और इसके बाद एक दौर चल जब देशों ने आंतरिक सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया।
परन्तु यह विदेशी वित्तीय पूंजी के हित में नहीं था इसीलिए 1944 में ही विश्व व्यापार संगठन जिसे उस समय जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड भी कहा जाता था के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात आईएमएफ की स्थापना की गई। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार हेतु देशों की सीमाओं को खोलना और बाजार के मातहत अर्थतंत्र को चलाना था।
इन्हें यह मौका तब मिल गया जब 1970 के शुरुआती सालों में मिडिल ईस्ट युद्ध को शुरू किया गया और तेल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई और कैंसियन अर्थतंत्र पर बैक बड़ा सवाल खड़ा हुआ और देशों को व्यापार घंटे का सामना शुरू करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का यह भी मानना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका द्वारा प्रायोजित युद्ध को प्रश्रय देने का प्रमुख मकसद कैंसियन अर्थतंत्र की सीमाओं को दिखाते हुए नव उदारवादी नीतियों के लिए विश्व तो तैयार करना था और वह इसमें कामयाब भी रहे।
यह सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नवउदारवादी नीतियों के लिए कैंसियन व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करना क्यों जरूरी था? इसकी पहली वजह कैंसियन व्यवस्था एक प्रकार से बंद या बहुत ही सीमित रूप से बाहरी शक्तियों के नियंत्रण को बल देती थी। दूसरा कैंसियन व्यवस्था निजी हित से ज्यादा एक हद तक सामाजिक हित को केंद्र में रख कर अर्थनीति को बनाने का प्रयास करता था जो सीधे तौर पर बड़े निजी निवेशकों के हित के विरुद्ध था क्योंकि अगर कोई प्राइवेट निवेशक श्रम बाजार पर ज्यादा खर्च कर देगा तो उसे अपने लाभ में कटौती करनी पड़ेगी, जो उन्हें खारिज करना था। तीसरा, हितकारी अर्थनीति जहां हर तबके पर ध्यान देने का प्रयास किया जाएगा वहां आर्थिक वर्चस्व या मोनोपॉली स्थापित करने के मौके कम होते हैं।
इन तीनों कारणों को एक साथ रख दिया जाए तब हमें आगे की सारी नीतियां स्पष्ट हो जाएंगी कि विश्व की अर्थनीति, खास कर अर्द्ध औपनिवेशिक देशों में आर्थिक नीतियों ने कैसे करवट ली है। मॉनिटरिजम, अर्थात ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया जाता है वहीं रोजगार बाजार को लगभग नकार दिया जाता है। यह ट्रेंड वैश्विक स्तर पर 1980 के दशक में ही आ गया था परन्तु भारतीय परिपेक्ष में इसे 1990 के दशक से स्पष्ट समझा जा सकता है।
इस नीति के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के तौर पर डोमेस्टिक या घरेलू बाजार पर होने वाले खर्च को अंतरराष्ट्रीय दबावों द्वारा कम किया गया जिससे कि लोगों के मध्य जानबूझ कर बेरोजगारी को बढ़ावा दिया गया और पुरानी व्यवस्था को निरर्थक साबित किया गया। वहीं इसी बीच आफ आर बी एम (फ़िसकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट) बिल को भी पास कराया गया जिसके कारण घरेलू वित्तीय खर्च को कम किया गया। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रही और अनेक क्षेत्रकों को विदेशी पूंजी के निवेश के लिए लगातार खोला जाता था।
हर के सरकार ने लोगों से बेहतर नौकरी के दावे किए लेकिन कभी नहीं दिया और हमारा ध्यान जी डी पी पर बनाए रखा। जिसका फायदा किसे हुआ इसका आंकलन धीमे धीमे गायब किया जाता रहा। बाद के दौर में लेयर्ड, निकल, जैकमैन जैसे अर्थशास्त्रियों ने बड़े चालाकी से “बेरोजगारी की प्राकृतिक चक्र” की थ्योरी द्वारा इसे बिल्कुल सामान्यीकृत करने का लगभग सफल प्रयास किया। परन्तु एक पक्ष जो छूट रहा है वह ये है कि आखिर राजकोषीय संतुलन को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को क्यों चुना गया?
मुद्रास्फीति के बढ़ने का तात्पर्य है कि वह व्यवस्था निवेश के लिए माकूल नहीं रही तो यह ज्यादा विदेशी निवेश को नहीं आकर्षित कर सकती है। इस “ईजी मनी” (विदेशी निवेश) को अपनाते हुए सरकार ने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जिसमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना अहम था इसलिए राजकोषीय नियंत्रण के साथ केवल मुद्रास्फीति को इतनी वरीयता दी जा रही है।
इस नई व्यवस्था ने विकास के नए मानक स्थापित किया जहां देश के आंतरिक बाजार में मांग और रोजगार को बढ़ावा देने और क्षमता से दूर होकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात में वृद्धि करके ज्यादा मुनाफा कमाने पर बल दिया गया। इससे दो फायदे बड़ी कंपनियां को हुए, जिसमें यह था कि निवेश में उत्पादन के वृद्धि के नाम पर खुली छूट मिल गई और वह अर्ध उपनिवेशों में उत्पादन केंद्रों को स्थापित करने में लग गई वहीं दूसरी तरफ बहुत से टैक्स हैवेंस भी बन गए जब भी बड़े देश टैक्स नीति में इजाफा कर देते थे तब यह फ़ुटलूज़ कंपनी अपने को आराम से ऐसे क्षेत्रों में शिफ्ट कर सकती थीं जो हाथ पसार कर निवेश के लिए हर चीज करने को तैयार हैं।
(निशांत आनंद स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)