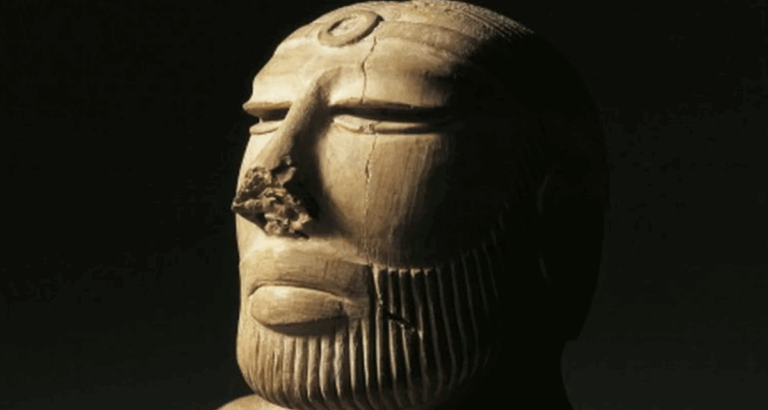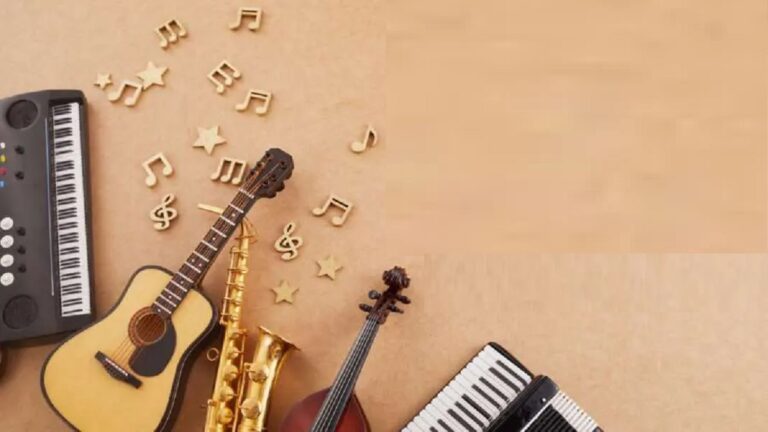देश और राज्यों की अपराध की स्थिति का अगर अध्ययन किया जाए तो सबसे चिंताजनक और भयावह आंकड़े, महिलाओं के प्रति अपराध या घरेलू हिंसा के मिलते हैं। महिलाओं के प्रति, सामान्य छेड़छाड़, आपराधिक मनोभाव से पीछा करना जैसे सामान्य अपराधों से लेकर, बलात्कार, गैंगरेप और फिर बेहद बर्बरतापूर्ण तरह से हत्या कर देने वाली घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। यह समस्या, किसी एक प्रदेश या समाज की नहीं है, बल्कि यह देश भर में तेजी से बढ़ रही है। घरों के अंदर होने वाली हिंसा की घटनाएं, जो अक्सर कम ही रिपोर्ट होती हैं, वे भी इसमें जोड़ लें तो स्थिति और भी भयावह है।
शायद ही किसी दिन के अखबार का कोई मुख्य पृष्ठ ऐसी दिल दहला देने वाली खबरों से वंचित दिखे। सरकार और समाज ऐसी घटनाओं पर चिंतित भी है, वीमेन हेल्पलाइन, महिला परामर्श केंद्र, ऑपरेशन शक्ति जैसे आकर्षक नाम वाली योजनाओं के बाद भी ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, बल्कि इनकी बर्बरता बढ़ती जा रही है। कानून सख्त भी होते जा रहे हैं, लोग इन सबके प्रति सजग भी हैं, अदालतों ने भी अपना रवैय्या सख्त कर दिया है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार तथा पुलिस जन आक्रोश के निशाने पर आए दिन आ जा रही है ।
अब कुछ आंकड़ो पर नज़र डालते हैं। एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में 2018 की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई है। 2018 में देश में दर्ज कुल अपराधों की संख्या, 3,78,236 थी, जबकि 2019 में यह संख्या 7.3% बढ़ कर 4,05,167 हो गई है। 2020 अभी चल रहा है। इनमें से अधिकतर मुक़दमे, विवाहित महिलाओं के पति या उनके अन्य परिजनों द्वारा उनके घरों में हुई हिंसक घटनाओं के संदर्भ में दर्ज हुए हैं। ऐसी घटनाओं का प्रतिशत 30.9 है। महिलाओं से छेड़छाड़ से जुड़ी हिंसक घटनाओं का प्रतिशत 21.8, महिलाओं के अपहरण की घटनाओं का प्रतिशत 17.9, और बलात्कार की घटनाओं का प्रतिशत 7.9 है। प्रति एक लाख महिला आबादी पर, 2018 में अपराध का आंकड़ा, 58.8 रहा, जबकि 2019 में इस शीर्ष में अपराध की बढ़ोतरी से यह प्रतिशत बढ़ कर 62.4 हो गया।
यदि मुकदमों की संख्या के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करें तो उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के दर्ज मुकदमों में पहले स्थान पर हैं। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में भी, उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों की कुल दर्ज संख्या 59,853 है, जो देश में कुल दर्ज महिलाओं के विरुद्ध अपराध का 14.7% है। इसके बाद, 41,550 दर्ज मुकदमों और 10.2% के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र, 37,144 दर्ज मुक़दमों और 9.2 % के साथ तीसरे स्थान पर है।
प्रति एक लाख की जनसंख्या पर दर्ज 177.8 मुकदमों के साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में असम सबसे ऊपर है। उसके बाद, 110.4 और 108.5 प्रति एक लाख महिला आबादी पर, राजस्थान और हरियाणा आते हैं। इस प्रकार दर्ज अपराधों की संख्या में भले ही उत्तर प्रदेश अग्रणी हो, पर प्रति एक लाख महिला आबादी पर अपराध के आंकड़ों में सबसे अधिक महिलाओं के प्रति हिंसा में असम सबसे आगे है और तब राजस्थान और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है।
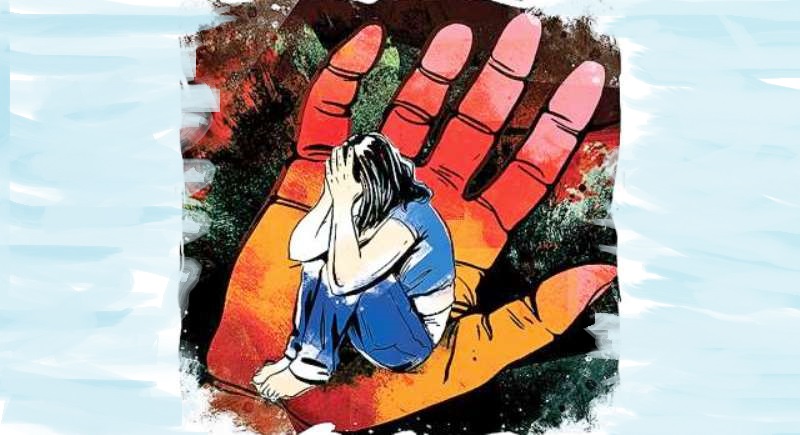
अब अगर बलात्कार से जुड़े अपराध के आंकड़ों को देखें तो, राजस्थान में सबसे अधिक, 5,997 मुक़दमे दर्ज हैं। इसके बाद, उत्तर प्रदेश, 3,065 और मध्य प्रदेश में 2,485 दर्ज मुक़दमों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अगर इन्हें प्रति एक लाख महिला आबादी में बदल दें तो, राजस्थान 15.9 के साथ पहले स्थान पर और 11.1 के साथ केरल दूसरे और 10.9 अंक के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर आता है।
नाबालिग बच्चे और लड़कियों के प्रति दर्ज अपराध जो पास्को कानून में दर्ज होते हैं, में 2019 में, देश भर में सबसे अधिक, कुल 7,444 मुक़दमे उतर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में, कुल 6,402 और तीसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश आता है, जहां कुल 6,053 मुक़दमे दर्ज हुए हैं, लेकिन, प्रति एक लाख की महिला आबादी पर, 27.1 अपराध के साथ सिक्किम, पहले स्थान पर, 15.1 के साथ एमपी दूसरे स्थान तथा तीसरे स्थान पर 14.6 अंक के साथ हरियाणा आता है।
दहेज से जुड़ी हत्याओं के दर्ज मुकदमों में यूपी में, कुल 2,410 मुक़दमें दर्ज हुए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। प्रति एक लाख महिला आबादी पर यह आंकड़ा 2.2 पर आता है। दहेज हत्या के मामलों में, 1,120 मुक़दमे बिहार के हैं। 2019 में कुल 150 एसिड हमले की घटनाएं देश भर में हुई हैं, जिनमें से 42 उत्तर प्रदेश में और 36 पश्चिम बंगाल की हैं।
अपराध के यह आंकड़े, एनसीआरबी की 1500 पृष्ठों की रिपोर्ट जो तीन खंडों में प्रकाशित है से लिए गए हैं। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की सबसे अधिक 554 घटनाएं, राजस्थान में, 537, उत्तर प्रदेश और 510 मध्य प्रदेश में दर्ज हुई हैं, लेकिन प्रति लाख महिला आबादी पर दलित महिलाओं से बलात्कार की दर केरल में सर्वाधिक है जो, 4.6 है। फिर एमपी और राजस्थान दोनों ही 4.5 अंक पर टिकते हैं।
उपरोक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि महिलाओं के प्रति हमारा समाज न केवल अनुदार है बल्कि हिंसक भी है। पूरे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा के अपराध कमोबेश जारी हैं। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, तब पूरे देश में गैंगरेप के खिलाफ एक व्यापक जनाक्रोश फैल गया था और अभियुक्तों को फांसी देने की मांग हुई। कानून बदलने की और शीघ्र ट्रॉयल के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट गठन की भी मांग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जनाक्रोश को भांपा और इस जघन्यतम अपराध के ट्रायल में शीघ्र सुनवाई के लिए कई निर्देश और सरकार को नोटिस जारी की। निर्भया बलात्कार कांड की गंभीर घटना के बाद केंद्र सरकार ने भी एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई, जस्टिस जेएस वर्मा और अन्य सदस्यों में हाई कोर्ट की सेवानिवृत जज जस्टिस लीला सेठ और देश के पूर्व सॉलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम भी शामिल थे।

जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी का गठन यौन अपराधों से संबंधित आपराधिक कानूनों में जरूरी संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। कमेटी को रेप, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाएं, पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण के अतिरिक्त पुलिस और शिक्षा से संबंधित सुधार प्रक्रिया से संबंधित कानूनों पर सिफारिशें सुझाने का काम सौंपा गया था। इस कमेटी ने 23 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
लम्बे समय तक, इस कमेटी की संस्तुतियां सरकार के पास लंबित रहीं। इन्हें लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनः एक याचिका दायर की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। बाद में यह संस्तुतियां सरकार ने स्वीकार कर लीं। समिति ने कहा है,
● यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए किसी भी ‘अवांछित व्यवहार’ को शिकायतकर्त्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिए।
● यदि एक नियोक्ता यौन उत्पीड़न को प्रोत्साहन देता है, ऐसे माहौल की अनुमति देता है, जहां यौन दुर्व्यवहार व्यापक और व्यवस्थित हो जाता है, जहां नियोक्ता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीति का खुलासा करने और जिस तरीके से कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उस में विफल रहता है, साथ ही ट्रिब्यूनल को शिकायत अग्रेषित करने में विफल रहता है तो इसके लिए नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
● कंपनी शिकायतकर्त्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।
● महिलाओं को आगे आने और शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई सुझाव भी दिए थे। मिसाल के तौर पर, समिति ने झूठी शिकायतों के लिए महिलाओं को दंडित करने का विरोध किया और इसे ‘कानून के उद्देश्य को खत्म करने से प्रेरित एक अपमानजनक प्रावधान’ कहा।
● शिकायत दर्ज करने के लिए तीन महीने की समय सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए और शिकायतकर्त्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
महिला अधिकारों के लिए देश में पिछले सालों से समाज में जागरूकता आई है, विशेषकर निर्भया कांड के समय पूरा देश एकजुट था, जैसे लगता था कि जनता की सहनशक्ति अब चुक गई है। दिल्ली में आंदोलन के दौरान एक नन्ही बालिका के हाथों में तख्ती पर लिखा एक कैप्शन, ‘नजर तेरी गंदी और परदा मैं करूं’ बेहद लोकप्रिय हुआ था। निर्भया के कातिलों को तमाम कानूनी पेचीदगियों के बाद भी फांसी हो ही गई। पर गैंगरेप की घटनाओं में कमी नहीं आई। हैदराबाद गैंगरेप और हाथरस गैंगरेप जैसी अनेक घटनाएं हुईं और उन पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। हैदराबाद के अभियुक्त तो पुलिस मुठभेड़ में मार डाले गए। हाथरस घटना की जांच सीबीआई कर रही है।
महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, के अनुसार, देश में करीब 2.70 करोड़ महिलाएं कमाती हैं और अपने दम पर परिवार चलाती हैं। जहां तक देश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, कानून तो पर्याप्त हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार कर अपराध होते रहते हैं। 2009 में सीबीआई के अनुमान के मुताबिक 30 लाख लड़कियों की तस्करी की गई, जिनमें से 90 फीसदी देह-व्यापार में धकेल दी गईं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का कहना है कि 1971 से 2012 के बीच दुष्कर्म के मामलों में 880 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।

गत तीन वर्षों में कन्या भ्रूण हत्या के 1.2 करोड़ मामले दर्ज हुए हैं, यहां तक कि ग्रामीण इलाकों की 56 फीसदी महिलाएं सुरक्षा कारणों से स्कूल-कॉलेज नहीं जातीं। हर साल नौ हजार महिलाएं दहेज हत्या की शिकार हो जाती हैं। दुनिया भर में नारी को समानता का अधिकार तो है, लेकिन विडंबना यही है कि उसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जुल्मों का शिकार बनाया जाता है। इन जुल्मों से निपटने के लिए कानून तो हैं ही, लेकिन समाज जब पूरी तरह जागरूक नहीं होगा तब तक यह ज़ुल्मत छंटने वाली नहीं है। साक्षर, स्वावलंबी और आत्म-निर्भर होने पर ही महिलाओं से जुड़े अपराध कम होंगे।
देश में स्त्री-पुरुष अनुपात का फासला भी कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अनुमान है कि देश में हर साल 50 लाख बालिकाएं जन्म ही नहीं ले पातीं। गौ-हत्या के प्रति शास्त्रों का उद्धरण देने वाला हमारा समाज बालिका शिशु और कन्या भ्रूण की हत्या पर खामोशी ओढ़ लेता है? पंजाब-हरियाणा जैसे राज्यों में ही नहीं चंडीगढ़ दिल्ली जैसे आधुनिक महानगरों में भी स्त्री-पुरुष अनुपात का फासला बढ़ रहा है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार देश में हर वर्ष 50 लाख कन्या भ्रूणों का गर्भपात होता है। भ्रूण परीक्षण संबंधी पीएनडीटी, अधिनियम 1994 में लागू तो है, लेकिन उसका बहुत असर नहीं पड़ा है। महाराष्ट्र में एक स्वयंसेवी संस्था के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि भ्रूण परीक्षण के बाद जो आठ हजार गर्भपात कराए गए थे, उनमें 7999 बालिकाएं थीं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 15 सेकंड में एक महिला मारपीट या किसी प्रकार के अत्याचार का शिकार होती है। हर साल करीब सात लाख महिलाएं दुष्कर्म की पीड़ा झेलती हैं। रिपोर्ट का दुखद पहलू यह है कि 40 प्रतिशत भारतीय महिलाएं पति की प्रताड़ना की शिकार बनती हैं। यह आंकड़ा तो तब है जब घरेलू हिंसा यौन शोषण के 50 प्रकरणों में से एक की ही शिकायत पुलिस तक पहुंच पाती है।
आज हम एक सामान्य संसार में नहीं जी रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। इसका असर हमारे उद्योग धंधों और आर्थिकी पर तो पड़ ही रहा है, पर इसका लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर बहुत पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था की मंदी और जिम्मेदारियों के निर्वाह में होने वाली बाधाओं के साथ लगातार घरों में कैद रहने की बाध्यता ने लोगों को अवसाद की ओर भी धकेलना शुरू कर दिया है। इसका असर महिलाओं के प्रति हिंसा और घरेलू हिंसा पर भी पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक हैंस क्लूज ने कहा है, “अप्रैल 2020 में घरों में रहने वाली महिलाओं को उनके पतियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले मामलों में 60% तक की वृध्दि हुई है।”

यह वैश्विक आंकड़ा है। इसका कारण मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, घरों में निरंतर बंद रहने की बाध्यता तो है ही, साथ ही महामारी के प्रकोप की अनिश्चितता भी है। झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन और बात-बात पर घरेलू विवादों के उठने से भी ऐसे मामले बढ़ रहे हैं।
आम तौर पर घर, सबसे सुरक्षित स्थान समझा जाता है, पर महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा चाहे वह घरेलू हिंसा हो या सड़क पर होने वाले अपराध, सबकी जड़ में अगर गंभीरता से छानबीन की जाए तो घर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मिलती है। कोरोना काल हो या सामान्य काल, समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा की कमी, पितृसत्तात्मक समाज का दंभ, लड़कों या पुरुषों को तरजीह देने की मानसिकता, मर्दवाद की ग्रंथि, आदि तरह तरह के कारणों से समाज का जो माइंडसेट बन गया है, के कारण, यौन हिंसा या महिलाओं के प्रति हिंसा या घरेलू हिंसा की शुरुआत होती है।
इस अपराध की एक बड़ी विडंबना यह है कि पीड़ित ही पहली नज़र में दोषी या अभियुक्त भाव से देखी जाने लगती है और उसकी न सिर्फ लानत मलामत होती है, बल्कि उसी से समाज, पुलिस और तंत्र यही उम्मीद करता है कि वह खुद को सुरक्षित रखने के बारे में अधिक सोचें या चिंतातुर रहें। यहां अभियुक्त अगर दोषसिद्ध भी हो जाए तो भी समाज के मन में विकसित हो चुकी ग्रन्थि यही सोचने को बाध्य करती है कि लड़के ने तो जो किया सो किया, पर लड़की को तो सोचना चाहिए था।
महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का सर्वे कहता है कि भारत महिलाओं के लिए चौथे नंबर का सबसे खतरनाक देश है। भारतीय दंड संहिता, आईटी एक्ट, स्त्री का अशिष्ट रूपण (रोकथाम) अधिनियम 1986 तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में सुरक्षा के तमाम प्रावधान है, लेकिन बढ़ती समस्याओं के आगे वे भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस स्थिति में तब फर्क आएगा जब सोच बदलेगी। कुछ धर्म गुरु, खाप पंचायतें और कट्टरपंथी संगठन भी अपनी उलजुलूल बंदिशों, फतवों, बेतुके फैसलों से महिलाओं की असुरक्षा में इजाफा कर देते हैं।
जब तक मनुष्य और मानव समाज है, तब तक अपराध का अस्तित्व रहेगा। अपराध का उन्मूलन न तो संभव है और न यह होने जा रहा है। अपराध नियंत्रित किया जा सकता है, अपराधियों को पकड़ कर उन्हें सजा दिलाई जा सकती है, पर अपराध को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। यह एक तल्ख हक़ीक़त है। कोई भी अपराध केवल, पुलिस या न्याय तंत्र के बल पर रोका भी नहीं जा सकता है।

पुलिस कितनी भी आदर्श और सक्षम हो, पर जब तक समाज की मानसिकता में महिलाओं के प्रति सोच, लैंगिग भेदभाव, औऱ पुरुष सत्ता के श्रेष्ठतावाद का लेशमात्र भी शेष रहेगा, तब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे। घरों से जन्मने वाले इस अपराध को रोकने की कवायद भी घरों से ही शुरू करनी होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी एक यह भी है कि मनुष्य उस व्यवस्था में एक उपभोक्ता या जिंस हो जाता है। हर चीज क्रय-विक्रय, क्रेता-विक्रेता के पैमाने से देखी जाने लगती है।
हम हैं मता-ए-कूचा-ओ-बाज़ार की तरह
उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह
यह मनोवृत्ति, और स्त्री शासित होने के लिए ही है, का यह भाव ही इस प्रकार के अपराध के मूल मेंसेरिया को जन्म देता है। समाज की घृणा, आक्रोश, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, हर्ष, विषाद, आदि सारे मनोभावों का नजला झेलती रहती है यह स्त्री।
जो मानसिकता समाज की बन गई है, कमोबेस वही सोच पुलिस की भी बन चुकी है। आखिर पुलिस आती भी तो इसी समाज से है। एक बार मेरे कार्यकाल में बलात्कार की एक घटना के बारे में जब थाने से उसका विस्तृत विवरण मेरे द्वारा पूछा गया तो, पहला ही उत्तर यह मिला कि सर, लड़की बदचलन थी। अब अगर लड़की जो भी हो तो, क्या उसके साथ हुआ बलात्कार, अपराध की गुरुता को कम कर देगा? बिलकुल नहीं, लेकिन लैंगिक भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी पैठी हैं कि यह वाक्य कहने वाले अफसर को लेशमात्र भी यह ध्यान नहीं रहा होगा कि वह कह क्या रहा है।
निर्भया कांड ने निश्चित रूप से महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नई सोच का सूत्रपात किया है। कानून और दंड प्रक्रिया संहिता में हुए सकारात्मक बदलाव से महिला अधिकारों को नए आयाम मिले हैं। एक सवाल महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी है। जब नारी, पुरुष के समान स्वतंत्रता अनुभव करेगी तब स्थितियां बेहतर होंगी।
(विजय शंकर सिंह रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं और आजकल कानपुर में रहते हैं।)