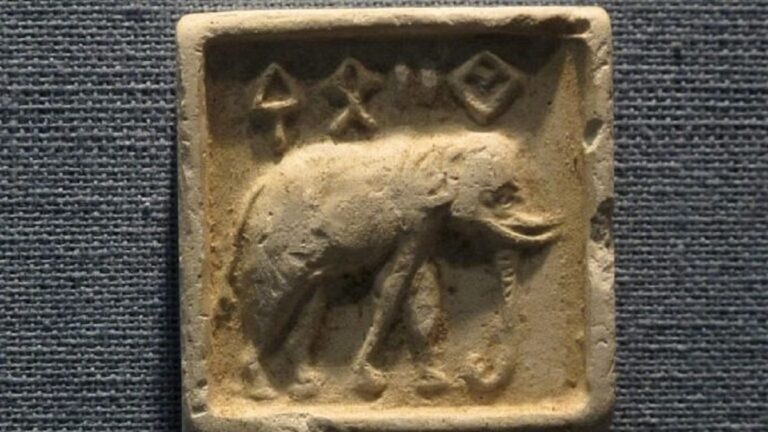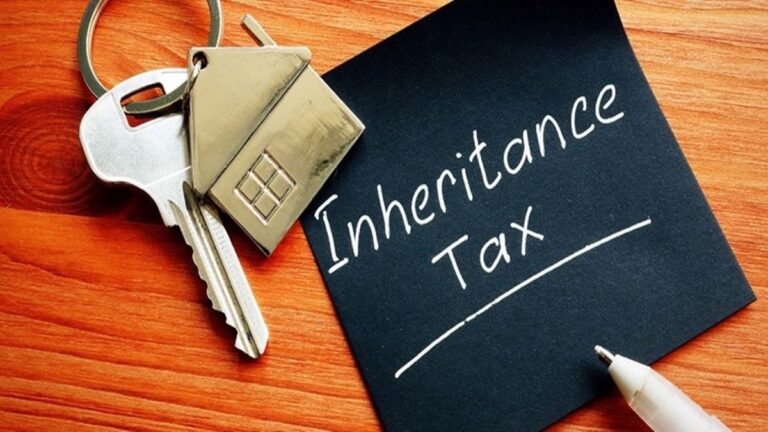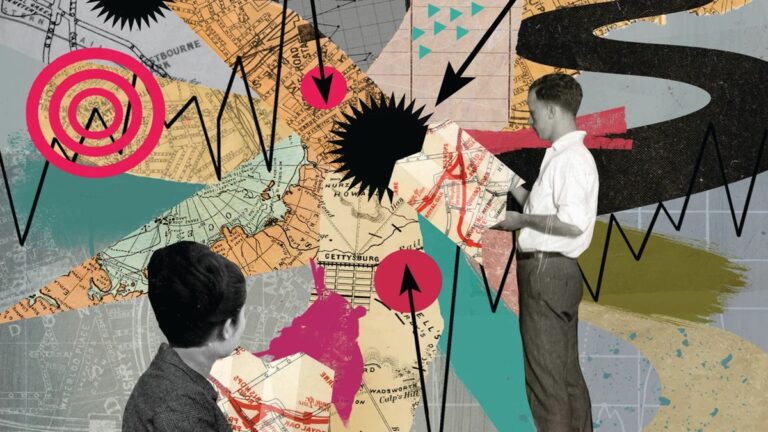परवर्ती दौर के पूंजीवाद में मेहनतकशों पर होने वाला हमला, पूंजीवाद के शुरुआती हमले के दौर की याद दिलाता है। और यह हमला विश्वव्यापी है न सिर्फ तीसरी दुनिया के देशों में बल्कि विकसित पूंजीवादी देशों में भी है। यह हमला 3 स्तरों पर है- आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक। आर्थिक हमले की चर्चा तो खूब होती है और यह उच्च मुद्रास्फीति और बेहद बढ़ी हुई बेरोजगारी का परिणाम है।
ऊंची मुद्रास्फीति विशेषकर अमेरिका में बड़ी पूंजी के बढ़े हुए लाभांश से शुरू हुई और फिर पूरी पूंजीवादी दुनिया में फैल गई।
बढ़ी हुई बेरोजगारी नतीजा है वैश्विक पूंजीवाद के संकट और सचेत ढंग से पूंजीवादी सरकारों द्वारा रोजगार में कटौती करके मेहनतकशों की कीमत पर मुद्रास्फीति कम करने के सचेत सरकारी प्रयासों से। सरकारी उम्मीद है कि बेरोजगारी बढ़ने से मेहनतकशों की मोलभाव की क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए वे महंगाई के अनुरूप मजदूरी बढ़ाने की मांग नहीं कर पाएंगे और फिर धीरे-धीरे मुद्रास्फीति अपने आप कम हो जाएगी।
हॉब्सबाम जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के शुरुआती सालों में पूंजीवाद में गरीबी में बढ़ोत्तरी हुई। ठीक इसी तरह आज का पूंजीवाद भी मेहनतकशों की चरम दरिद्रता का साक्षी है। Joseph Stiglitz के अनुसार एक पुरुष अमेरिकी मजदूर की 2011 में औसत वास्तविक मजदूरी 1968 से थोड़ी कम है। मौजूदा मुद्रास्फीति में यह और कम रह जाएगी। 1968 की तुलना में आज बढ़ी हुई बेरोजगारी इसमें जोड़ दें तो अमेरिकी मजदूरों की बढ़ी हुई दरिद्रता में शायद ही कोई शक बचे। यही बात दूसरे विकसित पूंजीवादी देशों के मजदूरों के बारे में भी कही जा सकती है।
भारत और तीसरी दुनिया के दूसरे देशों के बारे में मेहनतकश आबादी को मिलने वाले पौष्टिक आहार में कमी के स्पष्ट सुबूत हैं, अगर है उन्हें 1980के बाद से मिलने वाले खाद्यान्न के उपभोग की दृष्टि से देखें। इससे कोई भी यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकता है कि मेहनतकशों की गरीबी के निरपेक्ष स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे साफ है कि पूंजीवादी दुनिया में मेहनतकश आबादी विशेषकर गरीबों पर आर्थिक हमले तेज हुए हैं।
जाहिर है इस तरह का आर्थिक हमला उनके राजनीतिक अधिकारों में कटौती के बिना असंभव है। यानी आर्थिक और राजनीतिक हमले साथ साथ चलते हैं। इस आर्थिक हमले ने नव फासीवादी रूप ग्रहण किया है जो बड़े पैमाने पर पूरे पूंजीवादी जगत में आज उभार पर है। नव फासीवादी नेता आज दुनिया के तमाम देशों में राज कर रहे हैं।
अर्जेंटीना में मिलेई, इटली में मेलोनी, अमेरिका में ट्रंप से लेकर भारत में मोदी तक, हंगरी में ओरबन से लेकर तुर्की में एरडोगन, इजरायल के नेतन्याहू जिनकी एक अलग ही श्रेणी है, तक; और बहुत से दूसरे देशों में नव फासीवादी ताकतें इंतजार में बैठीं हैं, मसलन जर्मनी में AFD और फ्रांस में ला पेन की पार्टी (जिसे अब तक संयुक्त वामपंथ ने रोक रखा है )।
ये हमले एक तो सीधे मजदूर नेताओं के दमन के रूप में हैं, दूसरे उनके अधिकारों की वैधानिक कटौती के रूप में हैं। इसके अलावा वे एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करके, उसे पराया बताकर उसके खिलाफ बहुसंख्यकों के अंदर नफरत पैदा करते हैं। इसके माध्यम से वे पूरे विमर्श को ही बदल देते हैं और समाज में एक नया विमर्श खड़ा कर देते है। विमर्श में यह बदलाव मेहनतकशों के दैनंदिन जीवन के ठोस सवालों को न सिर्फ पीछे धकेल देता है, बल्कि उनको धार्मिक और एथनिक आधार पर बांट देता है। इसलिए वे अपने ऊपर होने वाले हमले का एकजुट होकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
अब जो चीज खास तौर से ध्यान आकर्षित कर रही है वह है मेहनतकशों पर आर्थिक राजनैतिक हमले के साथ साथ विचारधारात्मक हमला। यह बात इस या उस आदमी द्वारा यदा कदा किसी टिप्पणी तक सीमित नहीं है। ऐसे मजदूर विरोधी बयान पूरी दुनिया में दिए जा रहे हैं जो दिखाता है कि मजदूर विरोधी विचारधारा के हमले का यह एक खास मोड़ है।
भारत में आर्थिक विपन्नता के माहौल में तमाम राजनीतिक दल जो रोजगार पैदा करने वाली नीतियां दे पाने में असमर्थ हैं, वे पैसा ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। पैसे का यह नकद ट्रांसफर इतना कम है कि मेहनतकशों की दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता (वरना हमें वह पोषण की कमी न दिखती, जिसका पहले जिक्र किया गया है।) फिर भी इन्हें सत्तारूढ़ नव फासीवादियों और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी मुफ्त की रेवड़ी कहा जा रहा है।हालांकि शासक पार्टी अब खुद चुनावी दबाव के कारण ऐसे नगद ट्रांसफर के लिए मजबूर है। अब यह मोर्चा दूसरे लोगों ने संभाल लिया है।
जिस बिजनेस एक्जीक्यूटिव ने अभी हाल ही में मजदूरों के 90 घंटे साप्ताहिक काम की वकालत की थी, वे भी अब इन रेवड़ियों के खिलाफ कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि यह मेहनतकशों को कामचोरी के लिए प्रेरित करेगा। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस कोरस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने फरमाया है कि यह लोगों को कामचोर बनाएगा क्योंकि अब वे आराम से घर पर बैठ सकते हैं और बिना कुछ काम किए मुफ्त में रेवड़ियां पा सकते हैं। जज महोदय ने अगर सरकारों के लिए लोगों को रेवड़ियों के बदले योग्यतानुसार अच्छे रोजगार देना अनिवार्य कर दिया होता, तो अलग बात होती। लेकिन उनकी यह टिप्पणी केवल पैसा ट्रांसफर के खिलाफ थी, रोजगार देने के बारे में नहीं थी।
निश्चय ही ऐसे लोग तर्क देंगे कि नौकरियां हैं लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है। लेकिन ऐसे दावे के लिए वे न सिर्फ कोई सुबूत पेश नहीं करते, बल्कि इन उपेक्षित नौकरियों के लिए मजदूरी का स्तर क्या है, इसके लिए ही कोई तथ्य देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO ने खुद यह पाया है कि भारत में अच्छी नौकरियों के अवसरों का घोर अभाव है।
सरकार के रोजगार के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी है, क्योंकि पारिवारिक उद्यमों में महिलाओं का अवैतनिक श्रम बढ़ रहा है। इसको वे इस रूप में पेश करते हैं जैसे रोजगार बढ़ रहा हो। लेकिन यह विकास वास्तव में इस बात की अभिव्यक्ति है कि किसी दूसरी जगह उनके लिए लाभप्रद रोजगार उपलब्ध नहीं है। और इसलिए दरअसल यह अर्थशास्त्रियों की भाषा में छिपी हुई बेरोजगारी (diguised unemployment) है।
ठीक यही विचारधारात्मक हमला अमेरिका में भी हो रहा है। एलान मस्क जो ट्रंप द्वारा बनाए गए “Department of Government Efficiency” (DOGE) के मुखिया हैं, उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वह गरीबों के लिया बनाए गए Medicaid, Medicare and Social Security के लाभों में कटौती करने जा रहे हैं, जिसकी आशंका हाल ही में सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने व्यक्त की है। और गरीबों को नकद ट्रांसफर पर यह हमला सैंडर्स के अनुसार इसलिए किया जा रहा है ताकि उस पैसे को धनवान तबकों की टैक्स कटौती की ओर डायवर्ट किया जा सके जिसमें स्वयं मस्क जैसे लोग ही शामिल हैं, जैसे जेफ बेजॉस और मार्क जुकरबर्ग। यह ज़बरदस्त विचारधारात्मक हमला है, जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के अनुरूप है।
उदारवादी अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गेलब्रेथ ने कहा था कि “supply-side economics” का सार यह समझ है कि “यदि धनवानों को पैसा मिले तो वे बेहतर काम करते हैं, जबकि गरीब तब बेहतर काम करते हैं जब उन्हें कम पैसा मिले। यही आज ट्रंप और मस्क जैसों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन यहां एक विडंबना है।
गरीबों से पैसा निचोड़ कर धनवानों को देने की इस विचारधारा पर चलने से पूंजीवादी संकट और गहरा ही होगा। क्योंकि गरीबों के पास जो एक डॉलर आता है, उससे वे अमीरों की तुलना में अधिक खर्च करते हैं। इसलिए उपभोग में इस तरह की सिकुड़न से कुल उपभोग मांग में और कमी आएगी। और क्योंकि पूंजिपतियों का निवेश बाजार के अनुमानित विकास पर निर्भर करता है और वह बाजार में वृद्धि के वास्तविक अनुभव पर निर्भर करता है, इसलिए केवल उनको टैक्स में छूट देने से उनके निवेश में जरा भी वृद्धि होने वाली नहीं है।
कुल मिलाकर नतीजा यह होगा कि कुल मांग घट जाएगी। (उपभोग और निवेश मिलाकर) जिससे संकट और गहरा हो जाएगा। जॉन मेनार्ड कींस ने 1930 में, जो पूंजीवाद के समर्थक और रक्षक थे, और डरे हुए थे कि बोलशेविक क्रांति जैसी कोई चीज पश्चिमी पूंजीवाद को भी अपनी चपेट में ले सकती है, ने सुझाव दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने के लिए यह जरूरी था कि सरकारी प्रयास से कुल मांग बढ़ाई जाय। आज हम समकालीन पूंजीवाद में जो देख रहे हैं, वह इसका ठीक उल्टा हो रहा है। इसके बेशक दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ होंगे।
( People’s Democracy में प्रकाशित प्रो. प्रभात पटनायक के लेख का अनुवाद : लाल बहादुर सिंह ने किया है)