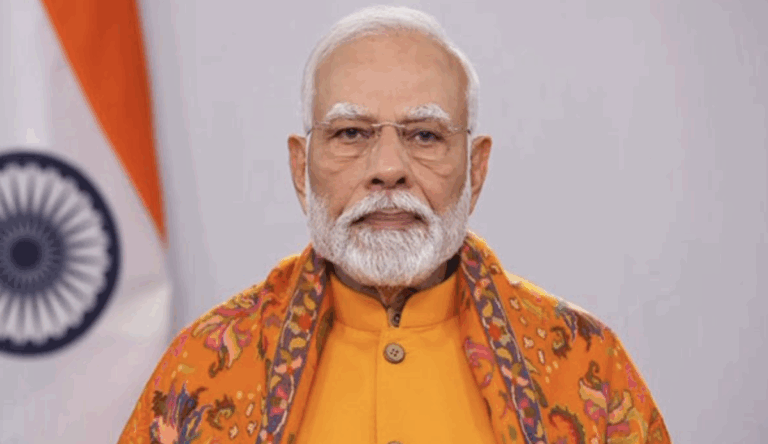वैसे तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का हारना और भारतीय जनता पार्टी का जीतना कोई अनहोनी नहीं है। ऐसा कई राज्यों में होता है, जब विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी हार जाती है और विपक्षी पार्टी जीत कर सत्ता में आ जाती है। लेकिन दिल्ली का मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इस चुनाव का नतीजा पिछले एक दशक के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में आए महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है।
दरअसल इस चुनाव का नतीजा सिर्फ दिल्ली के जनजीवन को ही प्रभावित करने वाला नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की हार स्पष्ट रूप से विचारधारा मुक्त राजनीति की हार है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उनकी इस हार से विचारहीन राजनीति का जीवन समाप्त हो गया है। केजरीवाल और उनके साथी समूह ने लगभग 15 वर्षों तक बिना किसी वैचारिक आधार के अपनी राजनीति चलाई और ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अण्णा हजारे और अरविंद केजरीवाल का ‘प्रायोजित’ आंदोलन साल 2011 में हुआ था। जब वह आंदोलन चरम पर था तब अक्सर उसकी तुलना मीडिया के एक बड़े हिस्से में अरब स्प्रिंग और काहिरा (मिस्र) के तहरीर चौक पर हुई क्रांति से की जाती थी। कॉरपोरेट घरानों से पोषित टेलीविजन चैनलों पर उस आंदोलन का 24 घंटे सीधा प्रसारण होता था। अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के मंच से तमाम नेताओं को चोर, बेईमान और भ्रष्ट करार देते हुए राजनीति से अपनी नफरत का इजहार करते थे।
उसी आंदोलन की कोख से जन्मी थी आम आदमी पार्टी। यह शहरी मध्य वर्ग के ग़ुस्से का प्रतिनिधित्व करती हुई एक विद्रोही पार्टी मानी गई, जिसका सड़कों पर विरोध-प्रदर्शनों से गर्भधारण हुआ था। राजनीति को बुरा बताने वाले अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के माध्यम से राजनीति में आ गए और छा भी गए। तब केजरीवाल, उनके साथियों, प्रशंसकों और मीडिया के भी एक बड़े हिस्से ने आम आदमी पार्टी के उदय को एक ‘नई राजनीति’ के रूप में पेश किया था। हालांकि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास और राजनीति को पर्दे के पीछे से संचालित करने वाली ताकतों से परिचित लोग तब भी इस ‘नयेपन’ की हकीकत से वाकिफ थे।
अण्णा-केजरीवाल के आंदोलन को काफी कुछ बौद्धिक ऊर्जा विवेकानंद फाउंडेशन से मिली थी, जो व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का थिंक टैंक है। उस आंदोलन के लिए सभी जरूरी साधन-संसाधन जुटाने में भी संघ का परोक्ष सहयोग था। आंदोलन के दौरान भाजपा नेताओं के साथ केजरीवाल और उनके साथियों की बैठकें भी होती थीं।
हालांकि आम लोगों के सामने भी इस ‘नयेपन की राजनीति’ को उजागर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जब 2014 आते-आते उस आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरे भाजपा से जुड़ते गए केंद्र में उसकी सरकार बनने पर ऊंचे-ऊंचे पदों को प्राप्त हो गए। आंदोलन के दौरान इन्हीं लोगों की मुखर आवाजें टीवी चैनलों पर होने वाली बहसों में बार-बार यही कहते सुनी जाती थीं कि यूपीए की सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार हैं।
फिर भी यह सच है कि इतना जब कुछ उजागर होने के बावजूद कम से कम राष्ट्रीय राजधानी के बाशिंदों ने आम आदमी पार्टी से बहुत ऊंची-ऊंची उम्मीदें जोड़ते हुए उसे अपने सिर-आंखों पर बैठाया। अरविंद केजरीवाल दस साल मुख्यमंत्री भी रह लिए। लेकिन अब जबकि वे खुद और उनकी आम आदमी पार्टी भी हार कर सत्ता से बाहर हो गई है तो उनकी राजनीति के संभावना-विहीन हो जाने की धारणा बनना लाजिमी है। यह सवाल भी उनसे पूछा जाएगा कि पार्टनर आखिर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?
हालांकि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 10 साल सत्ता में रह कर हारने के बावजूद इस बार विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 43.6 प्रतिशत हासिल किए हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर बार की तरह इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का मुकाबला भाजपा के विकराल तंत्र से था। फिर भी तमाम संकेत है कि आम आदमी पार्टी ने जो वोट हासिल किए, उनमें ज्यादातर हिस्सा गरीब वर्ग का है, जो केजरीवाल सरकार की शुरू की गई कुछ कल्याणकारी योजनाओं से काफी राहत महसूस कर रहा था।
दरअसल आम आदमी पार्टी की हार का प्रमुख कारण मध्य और संपन्न वर्ग में पार्टी के लिए घटा समर्थन है। इससे संकेत ग्रहण किया जा सकता है कि आम आदमी के कल्याणकारी शासन के मॉडल का आकर्षण वंचित तबकों के एक बड़े हिस्से में अभी भी बना हुआ है। इस मॉडल की आलोचना ‘रेवड़ी’ बांटने का मॉडल कह कर की गई है। दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर भी कहा गया। लेकिन ऐसी चर्चा के क्रम में यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है कि नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत के बाद से बाकी पार्टियों ने इसके अलावा कौन-सा मॉडल अपनाया है? केजरीवाल के मॉडल में तो फिर भी सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करना और मुफ्त या नाम मात्र के शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का पहलू शामिल रहा है।
बहरहाल इस सबके बावजूद यह सामने है कि आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है। इस हार के पीछे तमाम वजहों में से एक बड़ी वजह उसका विचारधारा मुक्त होना भी है। बिना किसी वैचारिक आधार के ‘सब चोर है जी’…और…’सब मिले हुए हैं जी’ जैसी बातें जनता के बीच उछाल कर केजरीवाल ने राजनीति में अपनी जगह तो बना ली लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नया और ठोस नहीं था जो उन्हें प्रासंगिक बनाए रख सकता।
दरअसल केजरीवाल के पास अपनी राजनीति का कोई मौलिक विचार नहीं था। उन्होंने अपने को भाजपा से भी बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने के लिए कई हास्यास्पद उपक्रम किए। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए करेंसी नोटों पर लक्ष्मी-गणेश की तस्वीरें छापने जैसी मूर्खतापूर्ण मांग भी की। अपने को हनुमान भक्त बताया और लोगों को सरकारी खर्च पर अयोध्या सहित तमाम तीर्थस्थलों की यात्राएं भी कराईं। कोरोना महामारी के दौरान भाजपा की तर्ज पर तब्लीगी जमात के जरिए मुसलमानों बदनाम करने में भी उनकी सरकार ने कोई कोताही नहीं की और दिल्ली में दंगों के दौरान भी उनकी सरकार व पार्टी पीड़ितों के साथ न खडी होकर पुलिस के साथ और प्रकारांतर से भाजपा के साथ खड़ी दिखी।
इस सबके बावजूद वे भाजपा के हिंदुत्व से ज़्यादा बड़े हिंदुत्ववादी नहीं हो सकते थे, क्योंकि जब बाजार में असली माल उपलब्ध तो उस माल के उपभोक्ता नकली माल क्यों खरीदने लगे? बायें से मध्य की राजनीति उन्हें कांग्रेस की अनुगामी दिखा सकती थी। ऐसे में सवाल है कि वे किसके साथ खड़े थे? यही वह सवाल है, जिसका जवाब देने से वे चतुराई से बचते रहे। राजनीतिक अवसरवाद दिखाने में कोई शर्म-संकोच नहीं दिखाया। कई मौकों पर उन्होंने गांधी की समाधि पर जाकर अपने को गांधी के प्रति आस्थावान दिखाया तो मौका आने पर अपनी पार्टी और सरकार के दफ्तरों में महात्मा गांधी की तस्वीरें हटा कर उनकी जगह भगत सिंह और डॉक्टर आंबेडकर की तस्वीरों का इस्तेमाल करने लगे।
केजरीवाल को दिल्ली में पहली बार सरकार बनाने के लिए उस कांग्रेस से भी समर्थन लेने में कोई संकोच नहीं हुआ, जिसकी 15 साल पुरानी सरकार को उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हराया था। यह सब करना उनके लिए इसलिए आसान था, क्योंकि उनके ऊपर विचारधारा का कोई बोझ नहीं था।
अनुच्छेद 370, राम मंदिर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर केजरीवाल भाजपा के साथ रहे। फिर जब उन्हें सुविधाजनक लगा तो वह कांग्रेस के साथ चले गए। उनकी राजनीति में बुनियादी विरोधाभास यह है कि उन्हें कांग्रेस के साथ भी रहना है, लेकिन वे कांग्रेस की राजनीतिक जमीन में सेंध भी लगाना चाहते हैं। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के वोटों को एक हद तक पूरी तरह साफ़ कर दिया था। पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। वे गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों में भी घुसे। उनकी पार्टी को चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल हो गया। उनकी अखिल भारतीय महत्वाकांक्षा कांग्रेस की जगह लेकर भाजपा का विकल्प बनने की थी। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में इसका बदला चुका दिया है।
केजरीवाल की राजनीति सिर्फ विचारधारा विहीन ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी संगठनात्मक शक्ल देने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और केजरीवाल इसके संयोजक बने थे। तब से लेकर आज तक वे ही इसके संयोजक बने हुए हैं। दिखावे के तौर पर पार्टी में एक राष्ट्रीय सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 34 सदस्यीय एक राष्ट्रीय निकाय भी हैं। लेकिन व्यावहारिक तौर पर इन सबका कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल पार्टी के सुप्रीमो हैं और सारे फैसले वे ही करते हैं।
तो जहां विचारधारा की अनुपस्थिति हो, कोई विधिवत बना हुआ सांगठनिक ढांचा न हो, वहां मूल्य पनप नहीं सकते। यही कारण है कि डिजाइनर आंदोलन के अति उत्साह से निकला राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल का निजी उपक्रम बन कर रह गया जिसमें असहमतियों के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके कोई राजनीतिक मूल्य नहीं थे।
आम आदमी पार्टी कभी भी इस आरोप के साये से बाहर नहीं निकल सकी कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आनुषंगिक उपकरणों की एक कड़ी मात्र अथवा भाजपा की बी टीम है। इसलिए भले ही उसे भाजपा से महज दो फीसदी वोट कम मिले हो, लेकिन जिन कारणों से उसे हार का सामना करना पड़ा है, लगता नहीं कि वे कारण उसे फिर से उबरने देंगे। कुल मिला कर उसकी वही गति हो सकती है, जो असम में चार दशक पहले बनी असम गण परिषद की हुई है। असम के छात्रों की वह पार्टी भी आंदोलन से जन्मी थी और धूमधाम से ताजा हवा के झोंके की तरह सत्ता में आई थी लेकिन एक दशक के भीतर ही असम की राजनीति में उसने अपनी भूमिका खो दी।
(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं।)