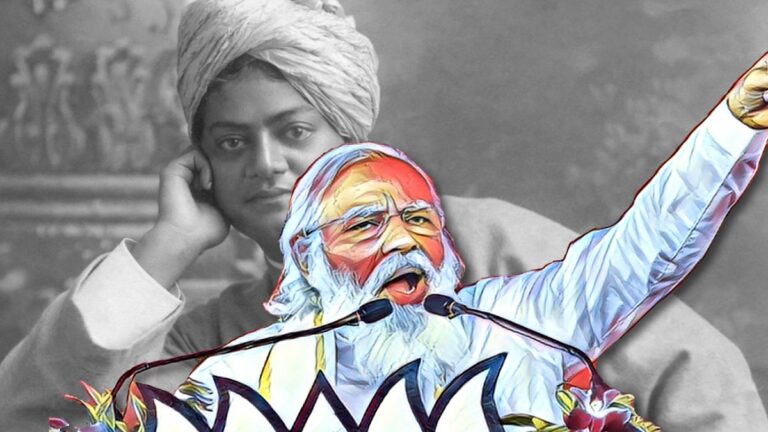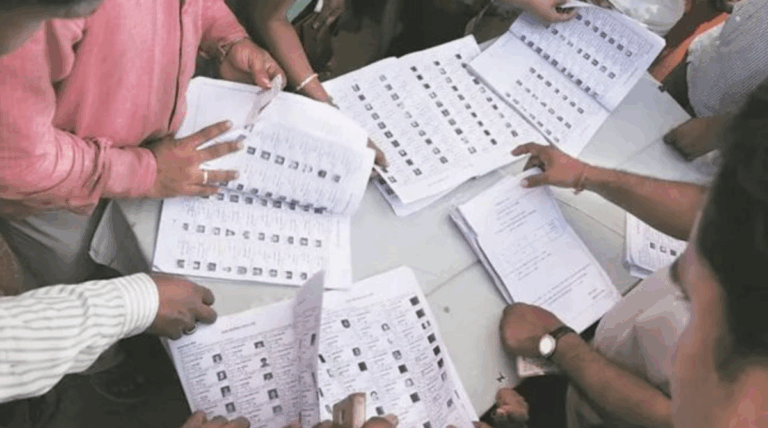हम अपने जीवन में ही पोयला बैशाख से जुड़ी बंगवासियों की अस्मिता के पहलू के नाना आयामों और उनके क्रमिक क्षरण के साक्षी रहे हैं। हर साल बांग्ला पत्र-पत्रिकाओं में हम इस पर एक प्रकार के विलाप के स्वरों को भी सुना करते हैं।
किसी जमाने में पूरब और पश्चिम, दोनों बंगाल में यह अंग्रेज़ी नव वर्ष की तुलना में कम उत्साह और उद्दीपन के साथ घर-घर में नहीं मनाया जाता था। बांग्ला अख़बारों के पन्ने तो आज भी इस अवसर के आयोजनों के विज्ञापनों से भरे होते हैं। अर्थात् सार्वजनिक आयोजनों और उत्सवों में शायद बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है । बल्कि इनका शोर शायद पहले से कुछ बढ़ा ही है ।
किसी वक्त यह बंगाल के हर दुकानदार के लिए नए बही-खाते का उत्सव का दिन होता था । दुकान पर आने वाले हर ग्राहक का मिठाई और बांग्ला कैलेंडर के उपहार से स्वागत किया जाता था । अतिथियों को आमंत्रित भी किया जाता था ।
कैलेंडर के व्यवसाय में बांग्ला कैलेंडर यहाँ एक बड़ी बिक्री का सीजन माना जाता था । यह अंग्रेज़ी कैलेंडर से कम नहीं होता था । इस दिन आम दुकानों पर भी लाखों की संख्या में बांग्ला पंजिका बिका करती थी ।
अब नया खाता सरकार के आयकर के असेसमेंट ईयर से बंध गया है । नया खाता का कोई मायने नहीं बचा है । बांग्ला कैलेंडर का प्रकाशन भी सीमित होकर बस एक रश्म अदायगी बन कर रह गया है ।
यह सच है कि हम जैसे कोलकाता निवासी ने तो बांग्ला महीनों के नाम के ज़रिए ही विक्रम संवत् के महीनों के नाम जाने। आज तो बंगाब्द और विक्रम संवत् के मास तो दूर की बात, नई पीढ़ी के लिए दिनों के हिंदी नाम तक याद रखना भी दुश्वार हो रहा है । महीनों के अंग्रेज़ी नाम तो हिंदी में रोमन अंकों की तरह ही अपना लिए गए हैं ।
बहरहाल, रवीन्द्रनाथ के वक्त तक के बांग्ला साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें अंग्रेज़ी वर्ष का उल्लेख ही नहीं होता था। खुद रवीन्द्रनाथ की कविताओं पर सिर्फ बंगाब्द के अनुसार तिथियाँ मिलती हैं, जिनके आधार पर उन्हें अंग्रेज़ी वर्ष के अनुसार समझने में खासी मशक़्क़त करनी पड़ती है । एक अंग्रेज़ी वर्ष में दो बांग्ला वर्ष शामिल रहते हैं । हम सबकी दिक़्क़त यह है कि हमारी इतिहास के कालखंडों की अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार पहचान करने की ऐसी आदत बन गई है कि इसके लिए जैसे और कोई अतिरिक्त परिश्रम का औचित्य नहीं लगता । यह समाज की सामूहिक चेतना की ही हमारे विचार और व्यवहार में भी काल और स्थान के स्तर पर सार्वकालिक नियमों की ऐसी ही अभिव्यक्ति है जिनसे हमारा अवचेतन क्रियाशील हुआ करता है । किसी दूसरी काल पंजिका के आधार पर विवेचन करने के लिए हमें उस काल की पहचान के चिन्हों का अनुवाद असहज करता है ।
आज हम जिसे जातियों की अस्मिताओं का संकट कहते हैं, उनमें काल बोध के संकेतीकरण का यह पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और शायद इसी के प्रति संवेदनशीलता के कारण सारी दुनिया में स्थानीय कैलेंडरों के अनुसार भारी धूमधाम से वहाँ के नव वर्ष के उत्सव मनाए जाते हैं । पर व्यावहारिक जीवन में हर जगह अंग्रेज़ी वर्ष की गणनाओं का ही धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है । सार्वभौमिकता के गहरे सांस्कृतिक आग्रहों के बावजूद अंग्रेज़ी वर्ष के अनुसार चलने की बाध्यता से किसी की मुक्ति जैसे संभव नहीं लगती है !
इस प्रकार, कहना न होगा, हर बीतते दिन के साथ, काल के भाषाई अथवा स्थानीय गणितीय चिन्हों से भी जुड़ा हुआ हमारा जातीय बोध जितना हमसे छूट रहा है, उतना ही हमारे जातीय अहम् का विलय अंकगणित के कुछ वैश्विक चिन्हों में पूरी तरह सिमटता चला जा रहा है। अस्मिता का गणितीय संकेतों में सिमटना मनुष्य के दर्शन की भाषा के विकास की शायद वह पराकाष्ठा है जिसमें उसका अंतर मानो अपने को पूरी तरह से उलीच कर वाह्य संकेतकों में सिमट जाने को प्रेरित रहता है। इसीलिए गणित को ईश्वर की भाषा कहा जाता है क्योंकि इसमें सत्य और उसके प्रकट रूप के बीच कोई फ़र्क़ नहीं होता है । माना जाता है कि हर अस्मिता का सत्य इसमें अपने को पूरी तरह से उलीच देता है । उसका अव्यक्त कुछ भी शेष नहीं रहता है ।
मनुष्य के नाते, प्रकृति पर अपनी ख़ास पहचान के हस्ताक्षर वाले अहम् के पुंज के नाते, अपने क्रमिक विरेचन के इन स्वरूपों से हम भले कितने ही विचलित क्यों न हों, पर जीवन में जिसे परमार्थ की सर्वकालिकता कहते हैं, वह वास्तव में यही तो है । परम की प्राप्ति का कोई भी स्वरूप आत्म को तिरोहित किए बिना संभव नहीं हो सकता है । तब फिर काल बोध के निजी प्रतीक चिन्हों के विलोपन पर कोई विलाप क्यों ?
जैसे मिथकीय कथाओं का तभी तक अस्तित्व या कोई अर्थ होता है, जब तक उन पर सामूहिक रूप में विश्वास किया जाता है। अन्यथा उन्हें कितना भी सहेज कर क्यों न रखा जाए, उनसे कुछ नीति-नैतिकताओं के बहुत हल्के से उद्देश्यपूर्ण संकेतों के अलावा मनुष्य के जीवन के यथार्थ का बहुत कुछ ज़ाहिर नहीं होता है । सनातन धर्म की असल शिक्षा तो यही है । इसमें कथा का हर तत्व किसी बाहरी क्षेपक की तरह ही होता है जिसे हर रोज़ बनाया और रोज़ बिगाड़ा भी जा सकता है।
(अरुण माहेश्वरी लेखक और चिंतक हैं।)