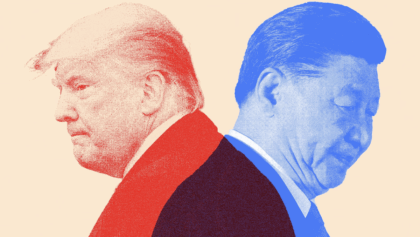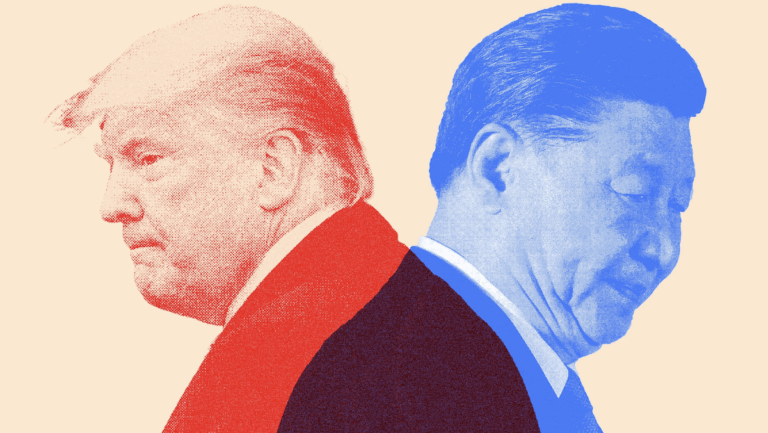जैसे-जैसे 2024 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे भारत के राजनीतिक दलों की गतिविधियों में तेजी आ रही है। स्वाभाविक है कि वैचारिक और सांगठनिक उलट-फेर और फेर-बदल हो रहे हैं। राजनीतिक दलों में सीटों के बटवारे को लेकर, सतह के ऊपर दिखने वाली और सतह के नीचे न दिखने वाली अफरा-तफरी मची हुई है।
आम नागरिकों के हित से जुड़े मुद्दों की भी चर्चा राजनीतिक दलों के भीतर से उठ जाया करती है। कई तो, खेल पलटने की बात करते-करते खुद ही पलट जा रहे हैं। इस समय भारत का लोकतंत्र सर्वाधिक जोखिम के दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक दलों और उनके अधिकतर नेताओं की विश्वसनीयता अपने न्यूनतम नहीं भी तो, न्यूनतर स्तर पर जरूर पहुँच गई है।
पहले कभी देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ देश की आर्थिक नीतियों को संचालित करती थी। अब वैश्विक आर्थिक नीतियाँ मानो स्वतः, देश के राजनीतिक दलों के सहारे देश की राजनीतिक परिस्थितियों की अनदेखी करती हुई देश की आर्थिक नीतियाँ तय कर रही हैं।
देश की राजनीति सत्ता की छीना-झपटी के लिए चाहे जितनी तिकड़म कर ले, सत्ता में आते ही राजनीतिक दल आर्थिक मामलों में लाचार होते चले जाते हैं। कबूल करे कोई या न करे, लेकिन यह सच है जिसे न झुठलाना आसान है, न झूठ के पर्दों में छिपाना आसान है।
जनता के ‘मनोरंजन’ के लिए सच को झूठ और झूठ को सच झलकाने का खेल सफलता और सफाई से राजनीति के मंच पर कर लिया जाता है। मंच जितना भी जादुई हो, उसका नेपथ्य उतना ही जादू-भंजक होता है। राजनीति के मंच पर जितना अधिक जादू चलता है, नेपथ्य में उतना ही अधिक कोहराम मचता रहता है।
क्या नजारा है! क्रीड़ा और कोहराम, कोहराम और क्रीड़ा! क्रीड़ा जितना मनोरंजक, कोहराम उतना ही घातक! आज पूरी दुनिया वैश्विक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तरह-तरह की हिंसा से और तरह-तरह की अ-स्थिरताओं और पारस्परिक अस्वीकार से परेशान है। भारत की दलगत राजनीति के नेपथ्य के अंशीदार टुकड़ों-टुकड़ों में मंच के खेल में शामिल होने की तिकड़म में लगे रहते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में फिसलते रहे हैं।
वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक परिस्थितियाँ भी लोकतंत्र की अनुकूलताओं के लिहाज से ठीक नहीं है। आस-पास के देशों की परिस्थितियों पर भी गौर कर लेने से बात समझ में आ जा सकती है। राष्ट्रीय और व्यक्ति स्तर पर भी आय-व्यय और खपत-बचत में भारी असंतुलन का भयावह दृश्य है। राष्ट्र पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण का बोझ, व्यक्ति पर ऋण और चुकौती अक्षमता के कारण अनैतिक आर्थिकी की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं।
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया! निम्न मध्यवर्ग के घर में पेटी-बक्सा तो, पहले से ही ढन-ढना रहा था अब पेटीएम (Pay Through Mobile) का हाल सामने है। यह कम बड़ी बात नहीं है कि सिर पर चुनाव है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक को इस तरह के कड़े कदम उठाने पर रहे हैं। पहली नजर में भारतीय रिज़र्व बैंक का यह रूटीन काम लगता है, है भी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। पेटीएम (Pay Through Mobile) के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना ही होगा।
अन-अर्जक आस्तियों की समस्या तब तक समाप्त नहीं हो सकती, जब तक अन-अर्जक आबादी अर्जन-शील आबादी में नहीं बदल जाती है। बेरोजगारी और अन-अर्जक आस्तियों की पारस्परिकता की उपेक्षा से उपजी समस्याओं के रूप में इसे समझना होगा। राजनीतिक समस्याओं और लोकतंत्र के संकट के मूल में यह एक प्रमुख कारक है।
इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी को सिर्फ व्यक्तिगत अयोग्यता कहकर संतोष कर लेना अपराध होगा। इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी निश्चित रूप से व्यवस्था की सामूहिक अकर्मण्यता को ही दर्शाती है। सबसे बड़ी युवा संख्यावाले देश में इतनी अधिक बेरोजगारी का होना बड़े संकट का सूचक है।
रोजगार की तलाश में श्रमशक्ति का इस तरह से देश-विदेश में भटकाव इसलिए भी भयावह है कि वैश्विक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तरह-तरह की हिंसा से परेशान है इतना ही नहीं वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं हैं और श्रम सुरक्षा का परिवेश भी कई जगह मानक स्तर से नीचे है, मानवाधिकारों से संबंधित स्थिति तो, भयानक है ही।
किसी भी संकट से निकलने में संवाद और स्वस्थ आलोचना की बड़ी भूमिका होती है। लोकतंत्र समस्याओं और समाधानों में लोक की भागीदारी सुनिश्चित कर व्यापक सहभागिता का मनोरम आधार तैयार करता है। लोकतंत्र स्वस्थ और सकारात्मक आलोचना की परिस्थिति तैयार करता है। स्वस्थ और सकारात्मक आलोचना लोकतंत्र को लोक-कल्याणकर बनाता है। दोनों अन्योनाश्रित होते हैं। इस ‘अन्योनाश्रिता’ को बचाये और कारगर बनाये रखने में लोकतांत्रिक सत्ता की बड़ी भूमिका होती है।
यहाँ लोकतांत्रिक सत्ता का उपयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, इस में सरकार और विपक्ष को अलग-अलग समूहों में नहीं रखा गया है, बल्कि, संसदीय अर्थ में किया गया है। संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता तो, संसद के पास होती है। सरकार तो, अपने अस्तित्व के लिए संवैधानिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होती ही है, व्यावहारिक रूप से विपक्ष भी संसद के प्रति उतना ही जवाबदेह होता है। संसद के प्रति सभी को जवाबदेही से जोड़े रखना मुख्य रूप से सरकार का काम है।
मुश्किल यह है कि पूर्ण या दुर्जेय बहुमत सरकार को निरंकुश बना देती है। कहना न होगा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाग्रत विवेक के ढीला पड़ते ही निरंकुशता सारी मर्यादाओं को तहस-नहस कर देती है। सरकार के मुखिया को पता ही नहीं चलता कि कब वह तानाशाह में बदल गया! जब तक पता चलता है, काफी देर हो चुकी होती है। घर में आग लग जाती है, घर के ही चिराग से। घर में लगी आग को तानाशाह रोशनी का उदात्त इंतजाम बताने लगता है। चतुर लोग उस आग पर अपनी तवा चढ़ा लेने के चक्कर में लग जाते हैं।
इन मुहावरों से बाहर वह आलोचना और संवाद को बेकार की बात मानकर आलोचना के प्रति कटु व्यवहार करने लगता है। आर्थिक मामले में उदारता और राजनीतिक मामलों में कट्टरता ऐसा तनाव और दबाव एक साथ पैदा करता है जिस के चलते लोकतंत्र का दम घुटने लगता है। जबरा मारे तो मारे, हकरकर रोने भी न दे! अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तरह-तरह से रोक लगनी शुरू हो जाती है।
गंभीर विचारक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने की राजकीय प्रवृत्ति को लोकतंत्र के संकुचित या समाप्त होते जाने के लक्षण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साफ-साफ शब्दों में कहा जाये तो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा-सरल तात्पर्य आलोचना की स्वतंत्रता से होता है। अभिव्यक्ति और आलोचना में समानता और अंतर पर भी ध्यान दिये बिना यह समझ पाना मुश्किल ही होगा कि असल में इस समय भारत में सरकारें और इसके प्रधान दरअसल, चाहते क्या रहे हैं।
हमारी सांस्कृतिक दीर्घसूत्री विविधताओं और उसकी जटिलताओं और चोटिलताओं के चलते हमारे सुदूर अतीत की वृहत्कथाओं में एक-से-एक मिथकीय बिंब हैं, और वे उसी परिसर में बने रहकर हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। वहाँ से ऐसे-ऐसे कथानकों को आयात करके वे उनके संबंधों और सूत्रों के सहारे, समकालीन राजनीतिक परिदृश्यों को परिभाषित करवाना चाहते हैं, क्यों? क्या लोगों को उसी दुनिया का नागरिक बना दिये जाने की परियोजना का हिस्सा है यह- प्रजा शरणागत और प्रभु प्रजा-वत्सल, प्रभु! यह सब ऊपर से, मनोहारी होता है लेकिन भीतर से ‘मनी (Money) हारी’!
सरकार और राज्य-व्यवस्था अपनी प्रशंसा, जो अक्सर झूठे आधारों पर होती हैं, करनेवालों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पूरी छूट देती है। यह छूट उन लोगों को भी मिलती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाकर दूसरों की निंदा, जो अक्सर झूठे आधारों पर होती है, करते नहीं अघाते हैं। यहाँ देखें तो, सरकार और राज्य-व्यवस्था अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा दोनों के लिए ‘झूठ का आधार’ बनाने की पूरी छूट देती है।
इस अर्थ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर न सिर्फ झूठ को छूट देती है बल्कि, इसके लिए विभिन्न तरीके से बढ़ावा भी देती रहती है। इसमें लगे लोगों को विभिन्न तरह के लाभ का अवसर देती है। जाहिर है, ऐसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लाभ का अवसर पाने के लिए लाभुक जी जान से लगे रहते हैं। यदि, ऐसे लोगों को अवसरवादी कहा जा सकता हो तो, इस अर्थ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित ही, अवसरवाद का राज-द्वार खोल देती है।
सरकारें और राज्य-व्यवस्था अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा के लिए व्यवहार में लाये गये ‘झूठ के आधार’ को खूब पहचानती हैं, और अपने राजनीतिक लाभ के अवसर को ध्यान में रखकर इसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ढंग से खूब बढ़ावा देती है। अ-राजनीतिक मुद्दों पर बात करने में अमूमन, कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन आम नागरिकों का डरा हुआ मन इस परिस्थिति में भी सावधान करता रहता है, मन मनाही में लगा रहता है। दुष्यंत कुमार के शब्दों में- मत कहो, आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आलोचना की स्वतंत्रता के अर्थ में देखने पर विपत्ति का सामना होता है। ‘झूठ का आधार’ अपनानेवालों के श्रीमुख से ‘अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा’ को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सहर्ष स्वीकार करनेवाली राज्य-व्यवस्था सच्चे आधार पर भी ‘अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा’ को बर्दाश्त नहीं करती है। आलोचना की स्वतंत्रता को ध्वनित करनेवाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तरह-तरह से रोकने का काम करती है। कानूनी रूप से सेंसर आदि की स्थिति तो, फिर भी समझ में आ सकती है।
मुश्किल तब होती है, जब ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवसरवादियों’ के ऊलजलूल और ‘हेट स्पीच’ के सामने स्वस्थ आलोचना करनेवालों को खड़ा कर दिया जाता है। हमारे अनुभव में तो, यह भी है कि मुख्य-धारा की मीडिया अपनी समृद्धि का अवसर देखकर, खुद ऊलजलूल में शामिल हो जाता है। ‘हेट स्पीच’ के मामले में भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जता चुका है।
भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हाल पहले से बहुत अधिक बुरा हो गया है। मुसीबत यह भी है कि मामला कहा-सुनी तक सीमित न होकर मार-पिटाई और जानलेवा हमलों तक पहुँच जाती है। अपने किसी अधिकारों के छिनने पर भी किसी के बोलने को, चाहे जैसे भी हो, बाधित किया जाता है। हक और हुकूक का सवाल पर आवाज उठाना राजनीतिक नहीं, अ-राजनीतिक प्रसंग भी है, लेकिन इसे भी आलोचना के खाते में डाल दिया जाता है।
हकमारी के किसी प्रसंग को मुख्य-धारा की मीडिया कभी ढंग से उठाती ही नहीं है। लोगों के मुहँ में अपनी बात डालने में मीडिया को महारत हासिल है। गाँव का अनुभव है कि गरीब-गुरबा के कान में ‘मालिक लोगों’ की बात इस तरीके से डाली जाती है कि उनके मुहँ से वह बात उनकी ही हो कर निकलती है, आखिर उनकी भी कोई इज्जत होती है।
अपनी इज्जत तो, खुद ही बचानी पड़ती है। इज्जत के मसले को समझना आसान नहीं है, ‘मालिक लोगों’ की इज्जत की हकीकत को जानते हुए भी, उसे अपनी इज्जत तो, बचानी ही पड़ती है। इज्जत से बहुत भारी होता है इज्जत का ढोंग। जिस के माथे भूख का जितना बोझ, उसकी फटी जेब पर इज्जत का उतना ही दबाव रहता है, इज्जत का नहीं, इज्जत के ढोंग का बोझ होता है।
गाँवों, खासकर, उत्तर भारतीय गाँवों में जायें तो, सामाजिक व्यय का सबसे बड़ा प्रवाह पूजा, भजन-कीर्तन, शादी-ब्याह, यज्ञ, जजमान, कर्मकांड, भोज-भात जैसे क्षेत्रों में दिखेगा। पैसेवाले लोगों के लिए इस अनौपचारिक ढंग से बहुत उच्च ब्याज दर पर ‘पैसा खटाने’ का अवसर होता है। आज छोटी व्यापारिक पूँजी ही नहीं उत्पादक पूँजी भी टूट गई है और समाज में ‘टूट पूँजियों’ की भी संख्या बहुत भारी है- नंगा नहाये क्या, निचोड़े क्या!
उम्मीद की जानी चाहिए कि अवसरवाद को खत्म करने के नाम पर सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संकुचित या समाप्त करने के बदले अवसरवादियों को हतोत्साहित करे तथा आम नागरिकों के मन में स्वस्थ आलोचना का अवसर उपलब्ध रहे। आपदा में अवसर का मतलब, अवसरवादियों को खुली छूट मिलना नहीं हो सकता है!
आलोचना के लिए तर्क-वितर्क सबसे बड़ा औजार होता है। यह तर्क-वितर्क तब भ्रामक हो जाता है जब तर्क की जगह वितंडा ले लेता है या तर्क के नाम पर भाषा व्यवहार को तर्क हीनता में फंसा दिया जाता है।
ऐसे समय में जाग्रत विवेक की जरूरत होती है। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है, और बिना विवेक के सत्संग हो नहीं हो सकता है। फासीवादी जनविमुखी व्यवस्था कुसंग के अवसर को बढ़ावा देने में लगी रहती है, विवेक सम्मत सत्संग का रास्ता अवरुद्ध होता जाता है। स्थिति पलट भी सकती है, तब तक, तुलसीदास के रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ, साभार—
“सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ।।
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कलपहि घालइ हरहाई।।
खलन्ह हृदयँ अति ताप बिसेषी। जरहिं सदा पर संपति देखी।।
जहँ कहुँ निंदा सुनहिं पराई। हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई।।
काम क्रोध मद लोभ परायन। निर्दय कपटी कुटिल मलायन।।
बयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों।।
झूठइ लेना झूठइ देना। झूठइ भोजन झूठ चबेना।।
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अति हृदय कठोरा।”
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं।)