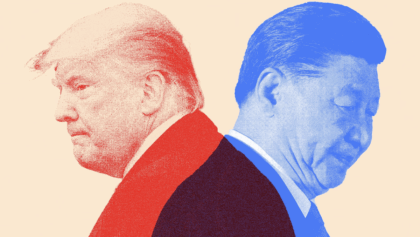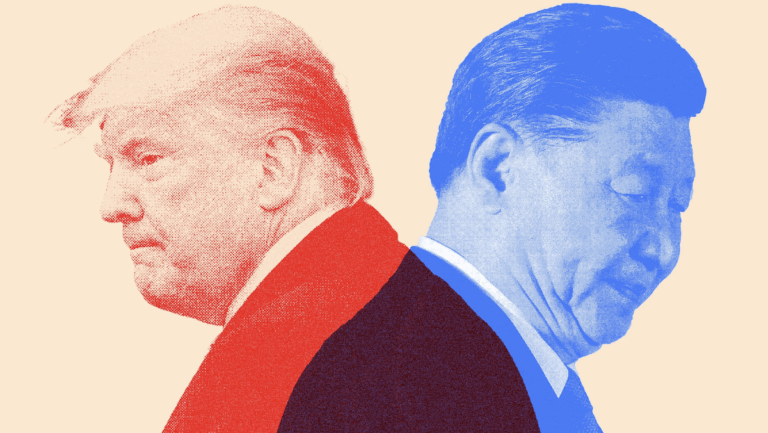अपने पुराने मित्र और जाने-माने प्रकाशक श्याम बिहारी राय पर संस्मरण लिखते हुए (समयांतर, अप्रैल, 2020) मैं कुछ ऐसे तथ्यों पर पहुंच गया था, जिनका इस उपमहाद्वीप के वर्तमान इतिहास से गहरा संबंध है। वह है इसकी राजनीति और उसमें अमेरिकी हस्तक्षेप।
आप सोचेंगे यह तो ठीक है कि श्याम बिहारी राय हिंदी के विशिष्ट प्रकाशन गृह ग्रंथ शिल्पी के संस्थापक थे, पर अंतरराष्ट्रीय महत्व का होने के लिए यह कौन-सी खासियत हो सकती है ! क्या यह कि यमुना पार के घने बाजार के पिछवाड़े की भूल-भुलैया सी एक गली में, जुगाड़ आर्किटेक्चर की प्रतिभा के कमाल एक चौमंजिले मकान के तीसरे माले में वह, 86 वर्ष पार कर लेने के बावजूद, रोज सुरक्षित चढ़-उतर जाते थे और उसके आधे हिस्से में फैले दफ्तर में, पिछली सदी के छठे दशक के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर वाले अंदाज में, सुबह ऐन दस बजे से शाम के ‘करेक्ट’ पांच बजे तक बेनागा कड़क बैठा करते थे? उनके दफ्तर जाने की मजबूरी वाले हम जैसे ठेठ पहाड़ी को भी सलाह दी जाती थी कि बेहतर हो बीमा करवाने के बाद ही जाएं। ऐसे आम आदमी का इतने बड़े उपमहाद्वीप की इतनी जटिल राजनीति से क्या संबंध हो सकता है?
सच तो वैसे यह है कि आप चाहे कितने ही बड़े या कितने ही छोटे आदमी क्यों न हों, पर अपने समय की राजनीति से आपका संबंध न हो, यह असंभव है। पर श्याम बिहारी राय से मेरे परिचय और मित्रता से 1971 के भारत-पाक युद्ध का संबंध, मात्र संयोग होने के बावजूद, जितना भी क्षुद्र सही, पर महत्वपूर्ण तो है ही।
सन् 1972 के आखिरी दिनों में हमारा परिचय हुआ था। वह तब हिंदी विकास समिति में काम कर रहे थे, जो हिंदी में सामाजिक विषयों का विश्वकोश बनाने में लगी हुई थी। उसी दौरान मुझे पता चला था कि श्याम बिहारी राय वहां आने से पहले, अमेरिकी संस्था ‘पीस कोर’ में थे, जहां उनके साथ नाटककार-उपन्यासकार सुरेंद्र वर्मा भी कार्यरत थे। वे लोग, कॉलेजों से निकलते ही सीधे ‘समाज सेवा’ के लिए भारत आए अमेरिकी युवाओं को हिंदी और स्थानीय संस्कृति के बारे में बताते थे। स्पष्ट है कि यह कम से कम राय साहब की मजबूरी थी। मात्र विचारधारात्मक ही नहीं बल्कि एक पीएचडी किए व्यक्ति के लिए नौसिखियों को हिंदी सिखाना किसी पीड़ा से कम नहीं हो सकता है।
अब सवाल यह है, और यह कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है, कि उन्होंने पीस कोर क्यों छोड़ा? किसी सैद्धांतिक कारण से या कोई ऐसा कारण था, जो उनके वश में नहीं था। यह प्रश्न इसलिए भी प्रासंगिक है कि वह पीस कोर छोड़ कर किसी अकादमिक यानी अध्यापन कार्य से भी नहीं जुड़े थे, जबकि उनकी शिक्षा-दीक्षा इस बात का प्रमाण थी कि वह अकादमिक करियर के लिए शिक्षित हुए हैं।
पीस कोर की कहानी
पीस कोर छोडऩे का कारण न उन्होंने बतलाया और न ही मैंने पूछा। इधर उन्हें याद करने के दौरान मैं ऐसे तथ्यों से जा टकराया जिनका संबंध पीस कोर से है। इन तथ्यों को जांचने के बाद अब पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उनका नौकरी छोड़ने का कारण पीस कोर का बंद होना था। यानी नौकरी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। पीस कोर के बंद होने के कारण पर बात करते हुए लगे हाथों मैं कूटनीति या डिप्लोमेसी पर भी हाथ आजमाने का लाभ उठा लेता हूं।
कूटनीति का मूल सिद्धांत कुल मिलाकर यह है कि चूंकि दो देशों के संबंधों का आधार लेन-देन पर टिका होता है इसलिए इन संबंधों की सफलता इस बात से नापी जाती है कि कौन किससे कितना लाभ उठा ले जाता है।
अब लौटते हैं पीस कोर उर्फ ‘शांति सेना’ पर। इसका उद्देश्य अमेरिकी युवाओं को दुनिया के रहन-सहन और वहां की संस्कृति से परिचित करवाना है। जॉन एफ कैनेडी के इस ‘ब्रेन चाइल्ड’ के पीछे यह विचार काम कर रहा था कि जो ‘मानव सेवा’ सौ वर्ष पहले तक ईसाई पादरी कर रहे थे, उसे मार्च 1961 में स्थापित पीस कोर आगे बढ़ाएगा। तीसरी दुनिया के लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह ‘मानव सेवा’ किस प्रकार हुई। डेसमंड टूटू ने इसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाया है। उनके अनुसार : ”जब मिशनरी अफ्रीका आए उनके पासबाइबिल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने कहा-आओ प्रार्थना करें। हमने अपनी आंखें बंद कीं। जब हमने उन्हें खोला हमारे पास बाइबिल थी और उनके पास जमीन।”
यहां बड़ी बात यह है कि पीस कोर के बंद किए जाने का सीधा संबंध 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध था। अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला था कि वह तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप न करे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस पर राजी नहीं हुईं। दंड स्वरूप अमेरिका ने, जैसा कि वह करता आया है और आज भी ईरान और वेनेजुएला के साथ कर रहा है, भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे। उनमें से एक, पीस कोर की भारत की गतिविधियों को बंद करना भी था। उस दौरान भारत में पीस कोर के कुछ नहीं तो चार-पांच हजार स्वयं सेवक तो होंगे ही। और इन्हें देखने के लिए लंबा चौड़ा तामझाम भी था। दूसरे शब्दों में इससे भारत में खासी बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर आता था। इसके अलावा इस कदम से पीस कोर से जुड़े हजार-पांच सौ भारतीय भी जरूर बेरोजगार हुए होंगे। स्पष्ट है कि यह अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ की गई कई दंडात्मक कार्रवाइयों में से एक था।
अगले वर्ष बांग्लादेश के जन्म की अर्द्ध शती होने जा रही है। इन पांच दशकों में एक दर्जन राजनीतिक नेता प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं, इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। फिलहाल यह जानना कम मजेदार नहीं होगा कि सन 1971 से लेकर अब तक पीस कोर भारत में नहीं लौट पाया है। यहां प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या पीस कोर बंद हो गया है? या फिर अमेरिका की अब भारत में रुचि नहीं रही है? सच यह है कि पीस कोर आज भी 60 देशों में सक्रिय है और इन 50 वर्षों में अमेरिका न जाने कितनी बार कोशिश कर चुका है कि पीस कोर भारत फिर से आए, पर उसे आने नहीं दिया गया है। यह काम भी सफाई से किया गया है। पीस कोर के आने पर पाबंदी नहीं है, बस सिर्फ कुछ ऐसी शर्तें लगाई गई हैं कि जिन्हें पालन करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है।
हां, यह जरूर है कि अब, जबकि ‘ट्रंप केम छो’ हो रहा है, आगे क्या होगा, कहना मुश्किल है। इससे यह भी सवाल जुड़ा है कि क्या ट्रंप फिर से जीतेंगे? और क्या उनका ध्यान पीस कोर की ओर जाएगा? और अगर गया तो वर्तमान सरकार का क्या रुख होगा? क्या वैसा ही जैसा कि हाड्रक्सीक्लोरोक्वीन के मामले में हुआ है?
पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के विभाजन और इस उपमहाद्वीप में एक नए राष्ट्र के उदय की इस कहानी में श्याम बिहारी राय की नौकरी एक बहुत ही नामाकूल-सी चीज मानी जाएगी। और मेरे लिए तो उस पर अफसोस करने का कोई कारण ही नहीं है। अगर वह पीस कोर में ही रहते तो हमारी शायद ही कभी मुलाकात हो पाती। पर हां, यह इंदिरा गांधी की दूरदृष्टि और दृढ़ प्रतिज्ञा का उदाहरण जरूर है। और इसे उसी रूप में याद करना गलत नहीं होगा।
इंदिरा गांधी से दूरी
चूंकि प्रसंग इंदिरा गांधी तक पहुंच गया है इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक स्पष्टीकरण की इजाजत चाहता हूं।
मैं कभी भी इंदिरा गांधी का प्रशंसक नहीं रहा हूं। विशेषकर, उनके लगाए आपातकाल के दौरान जो हुआ वह किसी तरह भुलाया नहीं जा सकता। कम से कम उन लोगों के लिए जो उस दौर में थे। इस अकेले अलोकतांत्रिक और संकीर्ण मानसिकता वाले कदम ने भारतीय लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंचाया उसके दुष्परिणाम यह देश आज भी भोग रहा है। उसी दौर में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बना और उसके साथ ही हर सरकारी संस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घुसपैठ संभव हुई।
एक नागरिक के रूप में उस दौर में स्वयं मैंने जो भोगा, यद्यपि वह अप्रत्यक्ष मानसिक प्रताड़ना थी इस पर भी मैं आतंक की उस अनुभूति से कभी उबर नहीं पाया हूं जो मुझे आपातकाल के 21 महीनों के दौरान चारों पहर भोगनी पड़ी थी। उस यंत्रणा को मैंने 1975 में लिखी कहानी ‘खोखल’ में अभिव्यक्ति देने की कोशिश भी की है। इसके अलावा आपातकाल पर लिखे अपने लेख में भी मैंने उस उत्पीड़न का विस्तार से वर्णन किया है। संभवत: तानाशाही का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होता है कि असंख्य निर्दोष और तटस्थ लोग भी अंतत: शंका और फिर अपरिहार्य दमन का शिकार बनते हैं।
इसके बरक्स शायद फरवरी, 2016 के उस अनुभव ने, जब मेरे घर रात 12 बजे पुलिस और इंटेलिजेंस के पांच अधिकारी आ धमके थे, डर जैसी किसी चीज को जन्म नहीं दिया। जबकि मैं यह भी जानता था कि इंटेलिजेंस वाले सोसाइटी के आस पास मेरी गतिविधियों और मेरे घर आने वालों पर नजर रखने के लिए महीनों तक तैनात रहे थे। निश्चय ही आपातकाल का डर और घुटन इससे कई गुना विकराल थी। बहुत संभव है उसी ‘ट्रेनिंग’ ने मुझे मजबूत बनाया हो।
यह सारी पृष्ठभूमि इसलिए कि मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। निश्चित ही यह आपातकाल से पहले का है। यहां याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आपातकाल से पहले यह देश कुछ और ही था। कैसा था, यह सब बताने के लिए हजारों किताबें लिखी गई हैं, एक और लिखी जा सकती है। मैं वह नहीं करने जा रहा हूं। बस एक छोटा-सा किस्सा सुन लीजिए।
मैं इंदिरा गांधी को सुनने न कभी किसी आम सभा में गया और न ही किसी अन्य सरकारी समारोह में। सच यह है कि मैंने उससे पहले उन्हें सशरीर कभी दूर से भी नहीं देखा था। यह बात 1974 के आसपास की होनी चाहिए। मैं और ज्योत्स्ना अक्सर शाम को नाटक या एक्जीबीशन देखने मंडी हाउस की ओर चले जाया करते थे।
एक बार विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर अश्विन गाथा के चित्रों की प्रदर्शनी त्रिवेणी कला संगम में लगी हुई थी। अश्विन कहीं विदेश में रहा करते थे और अपनी फैशन फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे। टहलते हुए एक दिन हम वहां पहुंच गए। ऐसे ही कोई पांच बजे के आसपास का समय रहा होगा। प्रदर्शनी श्रीराम सेंटर के मुख्य द्वार से लगी श्रीधराणी गैलरी में थी। जब हम पहुंचे उस समय गैलरी लगभग खाली थी। फोटोग्राफर, उनकी ब्रिटिश पत्नी तो थी हीं, दर्शकों के नाम पर हम दो के अलावा एक और सज्जन नजर आ रहे थे।
हमने अभी चित्र देखने शुरू ही किए थे कि अचानक वहां एक लंबी-चौड़ी कद काठी का आदमी लपकता हुआ घुसा और हमें हाथ से चलिए-चलिए कहता हुआ बाहर निकलने का आदेश देने लगा। मैं हक्का-बक्का अभी समझ भी नहीं पाया था कि हो क्या रहा है कि तभी स्थिर कदमों से चलते हुए एक महिला ने गैलरी में प्रवेश किया। कुछ पल विश्वास नहीं हुआ कि जो देख रहा हूं वह क्या है। सामने वाकई इंदिरा गांधी थीं, भारत की प्रधानमंत्री। अश्विन गाथा और उनकी पत्नी इंदिरा गांधी का स्वागत करने के लिए अभी संभल भी नहीं पाए थे कि इंदिरा गांधी ने अपना रुख उस आदमी की ओर किया जो हमें बाहर खदेड़ने पर उतारू था। अश्विन गाथा के स्वागत का जवाब देने से पहले उन्होंने कुछ हतप्रभ-सी आवाज में कहा, ”अरे, अरे, यह क्या कर रहे हैं? इन्हें क्यों निकाल रहे हैं? ”
फिर हमारी तरफ देखकर वह मुस्कराईं, जिसका तात्पर्य कुछ भी हो सकता था, पर मैंने लगाया, आप लोग देखिये।
पहले सुरक्षाकर्मी के अभद्र रुखे, बल्कि अपमानजनक व्यवहार और फिर इंदिरा गांधी के प्रकट होने से, तब तक मैं बुरी तरह अस्थिर हो चुका था। पर उनका सम्मान करते हुए मैंने थोड़ी देर चित्रों में ध्यान लगाने की कोशिश की पर इंदिरा गांधी की उपस्थिति के दबाव ने मुझे सहज नहीं होने दिया। इस बीच मैंने उन्हें कनखियों से देखा भी, वह औसत कद की महिला थीं पर जो विशिष्ट बात मैं नोट कर पाया वह यह कि इंदिरा गांधी की पलकें बहुत तेजी से झपकती रहती थीं। कह नहीं सकता यह उनका स्थायी भाव था या फिर उस दौरान कोई समस्या थी।
मेरे लिए वहां रहना जल्दी ही मुश्किल हो गया। मैंने ज्योत्स्ना से कहा, चलें? वह उल्टा मुझे ही रोकने लगीं। स्पष्टत: अश्विन गाथा उनके लिए गौण हो गए थे। मैं बिना बोले बाहर निकल आया।
थोड़ी दूरी पर एक जीप और साथ ही एक सफेद एंबेस्डर गाड़ी खड़ी थी, जो उन दिनों भारत सरकार का ट्रेड मार्क हुआ करती थी। ऐसा कहीं कोई चिन्ह नहीं था जो गलती से भी आभास दे रहा हो कि आस-पास वीवीआईपी जैसी कोई चीज हो सकती है। ज्योत्स्ना कुल मिलाकर इंदिरा गांधी के कुछ ही कदम पीछे बाहर आईं। प्रधानमंत्री निकलीं और सहजता से वहां खड़ी एंबेस्डर में बैठकर चली गईं। उनके आगे सिर्फ पायलेट वैन थी जिसमें न कोई सायरन था और न ही कोई सशस्त्र रक्षक। स्टेनगन या मशीनगन जैसे किसी हथियार की तो कल्पना ही संभव नहीं थी। दुर्भाग्य से इस घटना के बाद देश में स्थितियां ऐसी नहीं रहीं। एक ही साल के अंतराल में जिस तरह सब कुछ उलट-पुलट हो गया, वह अब भी अकल्पनीय है। 25 जून, 1975 आया और जो आतंक मचा, इंदिरा गांधी के प्रति मेरा विकर्षण स्थायी भाव में बदल गया।
मगर से दोस्ती
इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत को धमकाया और भारतीय प्रधानमंत्री ने खड़े-खड़े पाला बदला, उसने मुझे एक तरह से चकित कर दिया है। ट्रंप अमेरिका में उस ताकतवर पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनके देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की नीतियों को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। कोरोना के कारण वहां जो मौत का तांडव हो रहा है और जिसे रोकने में ट्रंप की कोई गंभीर रुचि नहीं दिखलाई देती, उसका सीधा संबंध पूंजी के हितों से है। वहां के पूंजीपति और व्यापारी – वह खुद भी एक बड़े पूंजीपति हैं – नहीं चाहते कि देश में बंदी (लॉकडाउन) जैसी कोई चीज हो। आदमी किसी समाज में पूंजी के अनुपात में घटता या फिर बढ़ता है। दुनिया में ज्यों-ज्यों पूंजी विकराल होती गई है, आदमी उतना ही सिमटता गया है। यह अचानक नहीं है कि अमेरिकी सरकार के लिए आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण पूंजी हो चुकी नजर आ रही है। इसलिए जिसने मरना है मरे, व्यापार को किसी कीमत पर थमना नहीं चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति से बेहतर यह कौन जान सकता है कि इससे उच्च वर्ग के लोग नहीं मरने वाले हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से निजी क्षेत्र में हैं और यह किसी तरह की जनसेवा नहीं बल्कि मानवीय पीड़ा का बड़ा व्यापार है। माइकेल मूर की फिल्म सीको इसका सबसे बड़ा दस्तावेज है। आपका इलाज यानी आपकी जान आपके बैंक बैलेंस पर निर्भर करती है। (दुर्भाग्य से भारत भी उसी रास्ते पर है।) इसलिए अमेरिका में मौतें तो आम आदमियों की होंगी और हो रही हैं। आम आदमी का मतलब है अश्वेत, हैस्पियन और एशियाई। इधर, 9 अप्रैल को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मिशिगन में अफ्रीकी-अमेरिकियों की कुल जनसंख्या मात्र 14 प्रतिशत है जबकि कोविड से मरने वालों में उनका प्रतिशत 40 है। लुसियाना में उनका प्रतिशत 32 है, जबकि मरने वालों का प्रतिशत 70 है। इसी तरह शिकागो में अफ्रीकी-अमेरिकियों की जनसंख्या जहां 30 प्रतिशत है, वहीं मरने वालों में उनकी संख्या 68 प्रतिशत है। (देखें: यशवंत राज की वाशिंगटन से रिपोर्ट, हिंदुस्तानटाइम्स, 9 अप्रैल, 2020) इस तरह के दस-बीस हजार लोगों के मरने को अमेरिकी सत्ताधारी कभी अहमियत नहीं देते।
अगर देते तो वहां हर वर्ष सिर्फ लाइसेंसी बंदूकों की गोलियां चलने से ही बेमतलब 30 से 35 हजार लोगों की जानें नहीं जातीं। लोगों की इन हिंसक मौतों से ज्यादा महत्वपूर्ण वहां के सत्ताधारियों के लिए आग्नेय अस्त्रों का उद्योग है। अमेरिका दुनिया में शायद ऐसा अकेला देश है जहां बंदूकें आलू-प्याज की तरह बिकती हैं और यह धंधा नागरिक अधिकार के नाम पर होता है। वहां की जनता के अधिकारों में एक है बंदूक रखने का अधिकार। यानी वहां आदमी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण बंदूक रखने का अधिकार है। ऐसे में जो हो सकता है वही होता है। इस लेख के लिखे जाने तक संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस ने 57 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी 10 लाख से ऊपर लोग संक्रमित थे, पर राष्ट्रपति महोदय अपनी बात पर अड़े हुए थे। यानी जो हो पर बाजार और व्यापार चलता रहेगा।
हमें याद रखना चाहिए कि मोदी जी का अमेरिकी ‘कनेक्शन’ अपनी ही तरह का है। जब देखिये ट्रंप और मोदी गले मिलते नजर आते हैं। यह अजीब नजारा है, किसी एब्सर्ड नाटक जैसा। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों की इससे भव्य झांकी क्या हो सकती है! पहले दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य स्वागत नरेंद्र मोदी का अमेरिका में ही हुआ है और अगर ट्रंप जीत गए तो सब कुछ के बावजूद भविष्य में भी होगा। पर ‘हाउडीमोदी’ जैसा ‘इवेंट’ (भूलिएगा नहीं इस शब्द के साथ मैनेजमेंट भी जुड़ा है) दुनिया में कहीं और क्यों नहीं होता? क्या मोदी अगला चुनाव अमेरिका में लड़ेंगे? इसका मुख्य कारण अमेरिका में गुजरातियों की बड़ी संख्या है, जो ब्रिटिश उपनिवेशों से होते हुए तो आए ही हैं, अब सीधे भी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। पर यह कहना भी गलत होगा कि उनके भक्तों में सिर्फ गुजराती प्रवासी ही शामिल हैं। उच्च जातियां, चाहे वह जहां हों, मोदी की ‘दैवीय शक्ति’ पर मुग्ध हैं।
‘हाउडीमोदी’ हुए अब कुछ वक्त गुजर चुका है। इस बार ट्रंप की बारी थी मेहमान नवाजी का सुख उठाने की। ट्रंप ने याद दिलाते हुए, कुछ चुनौती वाले अंदाज में कहा था कि मोदी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वह मेरा इतना भव्य स्वागत करवाएंगे, जितना दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ है। इस वर्ष नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप प्रत्याशी हैं। भारतीय प्रवासियों की वहां बड़ी संख्या है, जो मतदाता हैं, और मोदी के कारण ट्रंप के साथ जा सकती है। ट्रंप भारत इसीलिए आए। और उनका ‘सबसे बड़ा स्वागत’ 24 फरवरी को वाकई अहमदाबाद में, दुनिया के ‘सबसे बड़े’ क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में किया गया जो उस दिन सवा लाख जनता से खचाखच भरा ‘केम छो’ ट्रंप के नारे लगा रहा था। मोदी ने अपना वायदा भरपूर तरीके से पूरा कर दिखाया था, ट्रंप को यह बात माननी पड़ी थी। पाठकों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि गुजरात मोदी का गृह राज्य है।
24 फरवरी, 2020 के दिन की यह बात है जिस दिन दुनिया के दो बड़े राजनीतिक नेता एक बार फिर एक दूसरे से गले मिले थे और हाथ में हाथ डाल कर चले थे। उसी दिन ट्रंप ने घोषणा की थी, नरेंद्र मोदी ”असाधारण नेता हैं…एक ऐसे नेता जिसे अपना मित्र कहते हुए मैं गौरवान्वित हूं। हर व्यक्ति उन्हें प्यार करता है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, वह बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं।”
इससे बेहतरीन सर्टिफिकेट क्या हो सकता था! ममला एकतरफा नहीं गया। मोदी ने ट्रंप के बारे में भी उतने ही उदार और अनुपम शब्दों का इस्तेमाल किया, ”अब भारत और अमेरिका के संबंध आम भागीदारी वाले नहीं हैं, ये कई गुना विशाल और निकट के संबंध हैं।”
प्रश्न है, कितने निकट के?
यहां तक सब कुछ पटकथा के अनुकूल हो रहा था। इस हद तक कि दुनिया पर मंडराते उस खतरे को भी भुला दिया गया, जिसकी डरावनी छाया दिसंबर 2019 से ही वुहान से चलकर सारी दुनिया पर छाती जा रही थी। देखने की बात यह है कि इस घातक महामारी की चपेट में, अमेरिका भारत से भी ज्यादा और विनाशकारी तरीके से, आ चुका है।
खैर, इतनी विशाल सभा के आयोजन और वहां अभिव्यक्त उद्गारों के बाद क्या शंका रह जाती है कि दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ता के चरम पर थे! पर मित्रता के इस शंखनाद को डेढ़ महीना भी नहीं हो पाया था कि इस अहो ध्वनिम अहो रूपम को गुर्राहट में बदलने में देर नहीं लगी।
एक पुरानी सीख है, दोस्ती समानता के स्तर पर ही संभव है। बाघ और बकरी में दोस्ती हो तो भी श्रेयष्कर यही है कि, बिना कोरोना वायरस के भी, ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ होनी चाहिए।
‘आप ही बताइए, ‘ , तर्जनी अंगुली उठाकर पूछा जा रहा है, ‘होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ‘
नहीं होगी तो वही होगा जो हुआ है। यानी पोल-पट्टी को खुलते देर नहीं लगेगी।
बाअदब बामुलाहिजा
घटनाक्रम ने कुछ यूं रूप लिया :
4 अप्रैल को भारत सरकार ने घोषणा की कि मलेरिया निरोधक दवा हाड्रक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) का निर्यात करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यह इसलिए किया गया क्योंकि इस दवा के कोविड-19 को रोकने में असरकारी साबित होने की बात की जा रही थी। चूंकि भारत में जिस तेजी से यह बीमारी फैल रही थी और वैसे भी भारत में पहले से ही व्यापक मलेरिया के कारण, बड़ी मात्रा में यह इस्तेमाल होती है, इसका उत्पादन भी होता है, इसलिए यह सस्ती भी है। वैसे भी भारत में जिस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा चुकी हैं और जितनी बड़ी जनसंख्या की सुरक्षा की चुनौती हमारे सामने है उसे देखते हुए इस दवा का और भी व्यापक प्रयोग होने की पूरी संभावना थी। इन तथ्यों को ध्यान में रख, नीति बनी कि इसे बाहर न जाने दिया जाए।
निश्चय ही कोविड ने अमेरिका पर जबर्दस्त हमला किया हुआ है और इसकी बदइंतजामी के लिए नरेंद्र मोदी की तरह ही ट्रंप महोदय ही जिम्मेदार हैं। अगर मोदी की गलती समय पर कदम नहीं उठाना है तो ट्रंप की गलती अपने पूंजीपति भाइयों के हितों को आम जनता के हितों से ऊपर रखना है। नतीजा यह है अमेरिका में बीमारी तेजी से और व्यापक स्तर पर फैली है।
ऐसे में जो होना था वही हुआ। ट्रंप भारत के निर्णय से विचलित हुए बिना नहीं रहे। क्योंकि भारत का यह निर्णय उनकी जो रणनीति चल रही है, उसके विरुद्ध जा रहा था। अन्यथा भी उनका ज्यादा शालीन भाषा और व्यवहार में विश्वास कभी नजर नहीं आता है।
भारत सरकार के द्वारा एचसीक्यू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया और मोदी ने, शुरू में तो लगा, दोस्ती निभाते हुए, प्रतिबंध उठा लिया। यह इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रेस रिलीज की भाषा जितनी मानवीय नजर आ रही थी उससे लगा मोदी सरकार व्यापक मानवीय सरोकारों से ओतप्रोत होकर अपने पहले निर्णय को वापस ले रही है। पर अगले दिन ट्रंप ने जो किया वह अपने ही तरह की गुंडई थी। ऐसी जो किसी का लिहाज करना नहीं जानती है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ”मैंने कल (प्रधानमंत्री मोदी से) बात की, अच्छी बात हुई। मुझे आश्चर्य होगा (अगर भारत ने एचसीक्यू नहीं भेजा तो) क्योंकि यूएस ने भारत का खासा ध्यान रखा है। कई वर्षों से वे अमेरिका के साथ व्यापार में लाभ उठा रहे हैं…। मैंने उनसे बात की और कहा, आप अगर दवा आने देंगे तो हम उसकी तारीफ करेंगे। अगर वह इसे नहीं आने देंगे, तो भी ठीक ही है। लेकिन निश्चय ही बदले की कार्रवाई होगी। और क्यों न हो? ”
यह तो स्पष्ट है कि ट्रंप से हुई बातचीत के दौरान ही भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात मान ली थी और अगले ही दिन उस पर अमल भी कर दिया गया था। सवाल है इसके बावजूद ट्रंप ने उस बातचीत को सार्वजनिक क्यों किया? इसलिए कि ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वह किसी से ‘ना’ सुनने के आदी नहीं हैं, तब तक कि दूसरा नेता भी उतना ही दृढ़प्रतिज्ञ और साहसी न हो।
एक तरफ ट्रंप ने सिद्ध कर दिया कि वह मोदी को अपने बराबर नहीं मानते और अमेरिका के सामने भारत कुछ नहीं है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने यह मान लिया कि उनके पास इतना साहस नहीं है कि वह अमेरिकी चुनौती को स्वीकार कर सकें। क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक जीत और उस नरेंद्र मोदी की, जिसने ट्रंप को बुलाकर पूरे अहमदाबाद शहर को कोविड 19 के मुंह में डाल दिया है, हार नहीं कहलाएगी?
यहां प्रश्न किया जा सकता है कि क्या अमेरिका के सामने हमारे पूर्व के कई प्रधानमंत्रियों का व्यवहार सदा ऐसा ही रहा है, अमेरिकी दादागिरी के सामने सीधे आत्मसमर्पण वाला?
नहीं, ऐसा नहीं था। इसका प्रमाण यह है कि उस दौर में भारत की तीसरी दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका यूं ही नहीं थी।
नेतृत्व का महत्व
पर इस प्रसंग का अगला चरण ज्यादा रोमांचकारी और गौरव योग्य है।
जिस प्रसंग की मैं बात करने जा रहा हूं वह भी उसी दौर यानी 1971 से संबंधित है जिससे श्याम बिहारी राय और बांग्लादेश युद्ध जुड़ा है। जब यह स्पष्ट हो गया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करने जा रहा है तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के माध्यम से भारत सरकार को साम-दाम-दंड-भेद से नियंत्रित करने की कोशिश की। पर जब भारत किसी तरह मानता नजर नहीं आया तो अमेरिका ने बदले की कार्रवाई की। और उसी के तहत कई और पाबंदियों के साथ पीस कोर को भी बंद कर दिया गया था।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उससे जिस तरह निपटा वह अपने आप में नेतृत्व का कीर्तिमान है।
दिसंबर, 2006 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के इतिहासकार (हिस्टोरियन) ने अमेरिका के विदेश संबंधी 11वें खंड को सार्वजनिक किया था जिसमें दक्षिण एशिया के 1971 के संकट से संबंधित दस्तावेज थे। दस्तावेज इस बात का प्रमाण हैं कि निक्सन और किसिंजर ने साफ तौर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया और भारत को डराने-धमकाने की हर चंद कोशिश की। इतिहास यह है कि इंदिरा गांधी ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अमेरिकियों को ठिकाने लगा दिया था।
इन प्रकाशित दस्तावेजों की व्यापक चर्चा हुई थी। फ्रांसीसी मूल के पत्रकार क्लॉद आर्पी ने भी इस 11वें खंड पर एक लेख लिखा था। यह लेख 26 दिसंबर, 2006 को ‘1971 वार : हाउ द यूएस ट्राइड टु कॉर्नर इंडिया’ (1971 का युद्ध:अमेरिका ने किस तरह से भारत को किनारे लगाने की कोशिश की) शीर्षक से रेडिफ डॉट कॉम वेबसाइट में प्रकाशित हुआ था। आर्पी की सैन्य मामलों में विशेष रुचि है और वह बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं तथा दलाई लामा के निकट हैं। इस लेख में भी तिब्बतियों के प्रति उनका लगाव स्पष्ट नजर आता है। लेख में भारत द्वारा तैयार तिब्बतियों की एक सैन्य टुकड़ी का उल्लेख है जिसने इस युद्ध में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया था।
निश्चित ही इस लेख में भारतीय विजय का गुणगान है, पर यहां उद्देश्य एक और प्रसंग का है, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस दौर की महत्वपूर्ण नेत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता को जरूर दर्शाता है। आर्पी ने लिखा है :
”मैं आप को एक किस्सा सुनाता हूं जो मुझे मेजर जनरल केके तिवारी, चीफ सिग्नल ऑफिसर पूर्वी कमांड, ने 1971 के युद्ध के दौरान सुनाया था।
”जनरल तिवारी उस बातचीत (ब्रीफिंग) के दौरान उपस्थित थे जिसका आयोजन सेना के तीनों विभागों ने इंदिरा गांधी के लिए आयोजित किया था। एक ओर थल सेना के सेनापति जनरल एसएचएफ मानेकशॉ थे, और दूसरी ओर नौसेना के प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा।
”बातचीत चल रही थी कि एडमिरल नंदा ने बीच में टोक कर कहा: ‘मैडम यूएस का 8 वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा है।’ कहीं कोई असर नहीं हुआ और बातचीत जारी रही। कुछ अंतराल के बाद एडमिरल ने फिर दोहराया, ‘मैडम मैं बताना चाहता हूं कि 8वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहा है।’ इंदिरा गांधी ने उन्हें तत्काल बीच में ही टोक कर कहा, ‘एडमिरल मैंने आपकी बात पहली बार में ही सुन ली थी, बातचीत चालू रहने दीजिए’।”
”वहां उपस्थित सारे अधिकारी स्तब्ध रह गए। अंतत: प्रधानमंत्री की मुद्रा से उनकी जबर्दस्त हौसला अफजाई हुई। उन्होंने (इंदिरा गांधी) अमेरिकी घुड़की के प्रति चरम घृणा अभिव्यक्त कर दी थी।”
अंत में अपनी बात से इस प्रसंग की समाप्ति चाहता हूं। सन 1971-72 के दौरान मेरे बड़े मामा, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे, बरेली में नियुक्त थे। उसी दौरान मुझे वहां जाने का मौका मिला। संयोग से उन दिनों वहां पाकिस्तानी सेना के युद्धबंदी रखे हुए थे। बरेली में वैसे उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। अधिकांश को दिल्ली के लाल किले और ग्वालियर के किले में रखा गया था।
ममेरे भाई-बहन बड़े उत्साह से मुझे युद्धबंदी दिखाने ले गए थे। पाकिस्तानी बंदी, बहुत बड़े बाड़े में, जो कांटेदार तारों से चारों ओर से घेरा हुआ था, रखे गए थे। बाड़ कम से कम 20 फिट ऊंची तो होगी ही। अंदर कोई बंदिश नजर नहीं आ रही थी। बंदी अप्रत्यक्ष अनुशासन के साथ इधर-उधर सहज रूप से आते-जाते देखे जा सकते थे। पर वे हमारी ओर देख ही नहीं रहे थे, मानो हम दर्शकों का कोई अस्तित्व हो ही नहीं। शायद किसी बहन ने कहा था, ”ये आंख नहीं मिलाते। मिलाएंगे कैसे! ”
तब मुझे उन पर दया आई थी। पर उनके व्यवहार का तात्पर्य मुझे अब समझ में आया है।
युद्ध बंदी कैसे होते हैं
खैर, जब हम उन सैनिकों को देखने जा रहे थे, मैं सोच रहा था न जाने युद्ध बंदी कैसे होते होंगे। इसके बावजूद कि मैं तब तक न जाने कितनी युद्धकथाओं वाली हॉलीवुड की फिल्में, जिनका उन दिनों जोर था, देख चुका था। इनमें से कुछ फिल्में मुझे अब भी याद हैं। जैसे कि लॉन्गेस्टडे, ग्रेटएस्केप, ब्रिजऑनदरीवरक्वाई और पैटन । पैटन विशेष रूप से इसलिए भी याद है कि मैं और रामशरण जोशी कनॉट प्लेस के ओडियन सिनेमा में शाम के शो में उसे देखने जाने वाले थे कि भारत-पाक युद्ध छिड़ गया और उसी शाम से ब्लैक आउट शुरू हो गया। सौभाग्य से शो कैंसिल नहीं हुआ और हमने फिल्म देखी। फिल्म का अंदाज गजब का था। शुरू में ही मुख्य पात्र यानी जनरल पैटन कहता है, ”..नोबास्टर्डएवरवनकेवॉरबाईडाईंगफॉरहिजकंट्री।हीवनइटबाईमेकिंगअदरडम्मबास्टर्डरडाइफॉरहिजकंट्री।” (…कोई भी उल्लू का पटृठा अपने देश के लिए मर कर युद्ध नहीं जीतता है बल्कि दूसरे उल्लू के पट्ठों को अपने देश के लिए मरने पर मजबूर करके जीतता है। )
पर जब बंदियों को साक्षात देखने का मौका आया, मैं ज्यादा देर देख नहीं पाया था। उनकी चाल-ढाल, चेहरा-मोहरा सब पहचाना हुआ था। कुछ भी अलग नहीं। और होता भी क्यों, दोनों का उत्स एक ही था – एक ही संस्कृति एक ही समाज। यहां तक कि उसी ब्रिटिश सेना की प्रशिक्षण परंपरा जो देहरादून से सेंडहस्र्ट तक जाती थी। जिस स्थिति में वे थे, उसके लिए उन्हें किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता था? जो दमन और अत्याचार पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था, क्या मात्र इन सैनिकों की मनमानी का नतीजा हो सकता था? मेरा मतलब है, एक साधारण सिपाही से है, जो मशीन की तरह आदेशों का पालन करता है?
संभवत: यह सवाल उठाने का हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कोई क्यों सिपाही बनता है। आम आदमी के लिए सिपाही बनना रोटी-रोजी से जुड़ा मसला है। मुझे उस संदर्भ में वह आदमी भी याद आया जिससे मेरी संभवत: 63-64 में कभी दिलशाद गार्डन, दिल्ली में जीटी रोड की उस चाय की दुकान में मुलाकात हुई थी जहां मैं और मेरा दोस्त मोहम्मद बसी बिनाका गीतमाला या क्रिकेट की कमेंट्री सुनने जमा हुआ करते थे। तब हमारे घर में रेडियो सेट नहीं था। वह आदमी, जो चाय की दुकान वाले का कोई दूर का संबंधी था, चीन में पीओडब्लू रह चुका था। वह सेना से संभवत: स्वास्थ्य के कारणों से बाहर हुआ होगा और जो बातें वह हमें बताता था, मुझे नहीं लगता उसमें कोई विशेष तार्किकता, समझ या रोचकता हुआ करती थी। उसकी निरीहता मुझे बहुत बाद में समझ में आई थी। तब तक वह गायब हो चुका था।
यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान के पूरे पूर्वी कमान ने हथियार डाल दिए थे और 93 हजार सैनिक अपने कमांडर जनरल नियाजी के साथ युद्धबंदी बन लिए गए थे। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को जितना बड़ा झटका इंदिरा गांधी ने दिया उतना बड़ा शायद ही किसी और ने दिया हो। पर इंदिरा गांधी ने कभी पाकिस्तान की इतनी बड़ी हार को भी मुसलमानों की हार के रूप में नहीं भुनाया।
सरकार ने पांच महीने के भीतर ही शिमला समझौता किया और पाकिस्तानी सैनिकों को उनके देश के हवाले कर दिया। यहां तक कि भारत ने उन कुछ सैनिकों को भी माफ कर दिया, जिन पर युद्ध अपराधी होने का आरोप था।
(प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका समयांतरकेसंपादकपंकजबिष्टकालेख।लेखसमयांतरसेसाभार।)