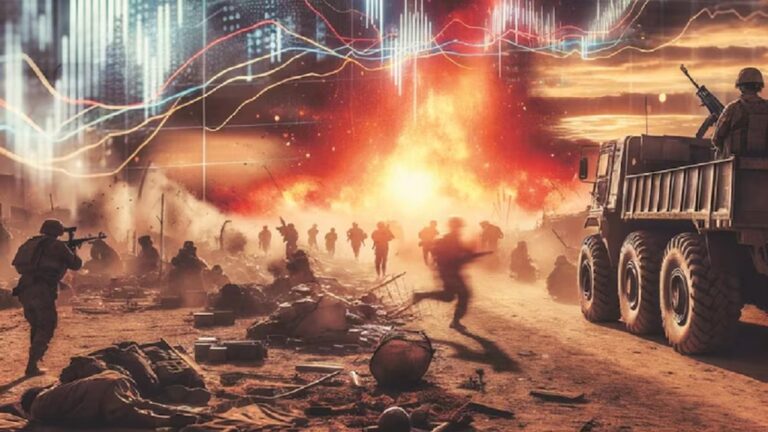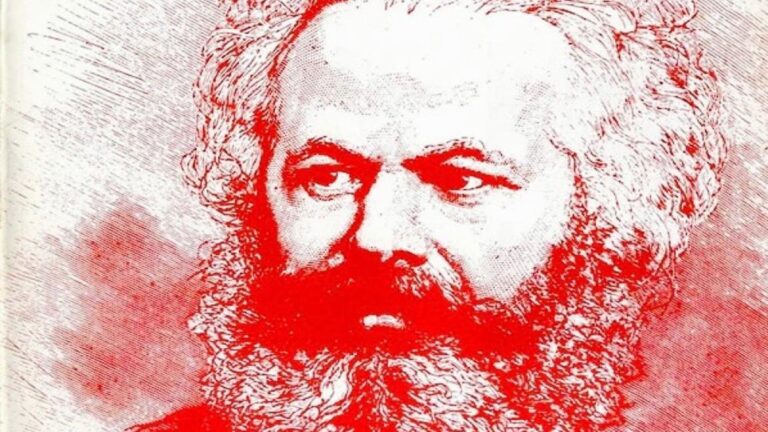मोदी 3.0 की सरकार का जब विशाल मंत्रिमंडल घोषित हुआ तो उसमें कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं था। भाजपा से कोई भी मुसलमान उम्मीदवार सांसद नहीं चुना गया। उसने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारा था। इस घटक सरकार के मुख्य समर्थक टीडीपी और जनता दल-यूनाईटेड से भी कोई मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं आया। पूरे एनडीए गठजोड़ से कोई भी मुस्लिम सांसद चुनकर संसद नहीं पहुंचा है।
इस बार कुल 24 मुस्लिम सांसद चुने गये हैं। जो भारत के लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे कम और 2014 में चुने गये 23 सांसदों से महज एक सीट ज्यादा है। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में सर्वाधिक मुस्लिम सांसदों की संख्या 1980 में 49 थी जो प्रतिशत में 9.04 था। 1952-77 तक यह औसत 5 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रहा। 1980-96 तक यह औसतन 6 प्रतिशत की सीमा से थोड़ा ही ऊपर है। इसके बाद की स्थिति बदतर होती गई है। सिर्फ 2004 में यह 6.45 प्रतिशत के आंकड़े तक गया। बाकी चुनावों में यह औसतन 4 से 5 प्रतिशत के बीच बना रहा।
इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 2019 के 34 सीट की उम्मीदवारी से कम करके 19 मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े किये, लेकिन पिछली बार के 4 सीटों पर जीत के मुकाबले इस बार 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। यह इस लोकसभा चुनाव में एक पार्टी द्वारा बसपा के बाद सर्वाधिक दी गई सीट थी। बसपा का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता। इसने 37 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था। टीएमसी ने पिछली बार 13 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किये थे, 4 पर जीत हुई थी। इस बार सिर्फ 6 सीटें दी, जिसमें से 5 पर जीत हुई। सपा ने भी पिछली बार के मुकाबले आधा 4 उम्मीदवारों को ही खड़ा किया जिसमें से 3 की जीत हुई। भाजपा ने 2019 में 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किये थे, इस बार सिर्फ 1 और जीत इसमें से किसी की भी नहीं हुई थी। राष्ट्रीय कही जाने वाली पार्टियों से इस बार कुल 16 सांसद चुने गये। बाकी सांसदों में स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र और स्थानीय पार्टी से चुने गये। इस बार कुल बड़ी पार्टियों की ओर से मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 82 थी, 2019 में यह 115 और 2014 में 191 थी।
इन आंकड़ों को उसके ऐतिहासिक क्रम और पार्टियों के संदर्भ में रखा जाये, तब ये बहुत कुछ कहते हैं। लोकसभा के चुनाव को भारतीय संसदीय राजनीति की आत्मा कहा जाता है। इसमें भारत की जनता को अंतिम निर्णायक माना जाता है और उसके वोट पैटर्न और उससे हासिल निर्णय से कई सारे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये हमारे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की सच्चाई को सामने लाने वाले आंकड़े भी होते हैं। तब निश्चित ही खड़े हुए और चुने हुए मुस्लिम उम्मीदावारों की संख्या, मुस्लिम वोट और उसका पैटर्न निश्चित ही भारत के उस राजनीतिक-अर्थशास्त्र को सामने लाता है जिसमें हम मुस्लिम भागीदारी को एक घटते हुए क्रम में देख रहे हैं। जबकि चुनावों के दौरान उसे भारतीय राजनीति और समाज में एक ‘बड़े कारक’ के रुप में देखा जाता है और उसे चुनाव का मुख्य ‘मुद्दा बना दिया’ जाता है।
1947-77 तक, जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढलने और संकट से निकलकर मजबूत होने की ओर बढ़ने का समय है। इस दौरान वह राज्यों को पुनर्संयोजित करती है और पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में उलझी हुई दिखती है। इस दौरान भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी संकट में दिखता है। इस समय तक अन्य धार्मिक समुदायों और राष्ट्रीयताओं के प्रतिनिधित्व का भी संकट है जिससे इस समय तक उनके संगठित प्रतिरोध और संघर्ष सामने आने लगते हैं।
1980-95 तक अपने राज्य अपने को कहीं अधिक मजबूत कर लेता है और साम्राज्यवाद के साथ समझौतों में अपनी शर्तों को सामने रखने की स्थिति में आ जाता है। इस समय तक भारत की विस्तारवादी नीति की दिखाई देने लगती है। इस समय मुस्लिम सांसदों की संख्या में पिछले के मुकाबले वृद्धि देखी गई। लेकिन, जैसे-जैसे उदारवादी दौर और वैश्वीकरण की नीति लागू होती है एक बार फिर मुस्लिम सांसदों की संख्या लोकसभा में गिरती हुई दिखती है।
इसी दूसरे दौर में वैश्विक राजनीति में अमेरीकी साम्राज्यवाद मध्य एशिया में मुस्लिम बहुल देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करता है और इसे धार्मिक रंग देने में कोई कोताही नहीं बरतता है। खासकर, इसने इजरायल के माध्यम से यहूदी बनाम मुसलमान का रंग देकर इसने उसी तरह की मानसिकता का जन्म दिया जिस तरह से हिटलर ने यहूदी समुदाय के खिलाफ पूरे यूरोप में माहौल बना दिया और उनके कत्लेआम के लिए नीति बनाई और ऐसा करने के लिए उकसाने वाली राजनीति का प्रचार किया।
इसी दूसरे दौर में, मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन और उसकी रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सूचकांकों में कई जगह यह समुदाय दलित और आदिवासी समुदाय से भी पीछे चला गया है। इस रिपोर्ट पर बात हुई और इसके सुझावों को भुला दिया गया। यही वह दौर भी था जब भाजपा राम मंदिर निर्माण का अभियान चला रही थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा चुका था। भाजपा-आरएसएस के गठजोड़ और बजरंग दल और विहिप की आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति भारत के शहरों से लेकर कस्बों और गावों तक हिंदू-मुस्लिम दंगों और बाद में कई जगहों पर जनसंहारों में बदल रहा था। राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व का ध्रुवीकरण वस्तुगत तौर पर मुस्लिम समुदाय के बहिष्करण में बदल रहा था। यह कई स्तरों पर हुआ।
2022 में आक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के पहले तक मुस्लिम समुदाय की बेरोगारी की दर 17 प्रतिशत तक थी, जो बाद में 31.4 प्रतिशत तक चली गई। इसी तरह शहर में इस समुदाय की बेरोजगारी दर 15.6 प्रतिशत थी जो कोविड के दौरान और बाद में 23.3 प्रतिशत हो गई। श्रम बाजार में 2004-05 में भेदभाव की दर 59.3 प्रतिशत था जो 2019-20 में 68.3 प्रतिशत हो गया। नियमित आय के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि एक आम भारतीय के मुकाबले 49 प्रतिशत कम, 13,672 रुपये ही कमा रहा था। इसी तरह स्वरोजगार से होने वाली आय भी सामान्य भारतीय की आय से उसकी आय लगभग 4 हजार रुपये कम थी।
कोविड के दौरान मुस्लिम समुदाय पर एक योजनाबद्ध तरीके से मीडिया ने हमला किया जिसका सीधा असर समाज पर पड़ा। मुस्लिम समुदाय को ‘जिहाद’ की क्रोनोलॉजी बताई जाने लगी जिसकी अनुगूंज इस बार, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में सुनाई दी। वह एक भाषण में ‘वोट जिहाद’ करने वालों के खिलाफ सतर्क रहने के लिए कह रहे थे।
पीरीयोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक काम खोजने वाले श्रमिकों की संख्या में गिरावट आई है। यह पिछले साल की 55.2 प्रतिशत से बढ़कर 57.9 प्रतिशत हुआ है। यह पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाल के दिनों, जब मुस्लिम समुदाय के शिक्षित युवाओं ने आईएएस की परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं, तब उन्हें भी ‘नौकरी जिहाद’ कहकर प्रचारित किया गया। जबकि सच्चाई काफी भयावह है। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में मुस्लिम रोजगार का प्रतिशत पिछले दस साल से अधिक समय से 7 प्रतिशत से नीचे ही बना हुआ है। जबकि सरकारी नौकरियों में यह लगभग 5 प्रतिशत है। 2006-07 में यह लगभग 7 प्रतिशत था, 2011-12 में यह घटकर 6.24 प्रतिशत हो गया।
यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि शहरी समाज में दलित और आदिवासी के साथ आवास के संदर्भ में भेदभाव होता है। ‘घेटोटाइजेशन’ भारत के शहरी समाज का हिस्सा बनकर उभरा है। यह भेदभाव गांव में ‘दक्खिन टोला’ के रूप में था। वह चलते हुए शहर में भी आया। यही स्थिति मुस्लिम समुदाय के साथ भी है। दंगों ने इस विभाजन को और बढ़ाया। दंगों की राजनीति जब ‘राष्ट्रवाद’ की राजनीति का हिस्सा बनने लगी और सामाजिक ध्रुवीकरण से बढ़कर आर्थिक जगत में पैठ बना ली, तब सांस्कृतिक विभाजन भी साफ दिखने लगा। 1990 के बाद का ‘घेटोटाइजेशन’ बेहद भयावह तरीके से उभरा है। भारत की चुनाव व्यवस्था में वोट को जब बहुसंख्या की राजनीति का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया तब इसने कुछ और ही शक्ल अख्तियार कर ली। बहुत बेशर्मी के साथ इसे नफरती भाषणों का हिस्सा भी बना दिया गया।
सार्वजनिक जीवन में, खासकर श्रम में हिस्सेदारी, रोजगार, आवास और आय में घटती भागीदारी का सीधा अर्थ किसी समुदाय के सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति, संगठन और उसकी क्षमता, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को कम करता जाता है। यह स्थिति महिलाओं के लिए भी उतना ही सच है। यह सच्चाई भारत के श्रमिकों के लिए भी उतना ही सच् है। जो समुदाय जितना ही असंगठित क्षेत्र की ओर जाता है, श्रम के अवदान के अनुपात में जितना ही कम आय हासिल करता है, उतना ही राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिये की ओर बढ़ता जाता है। वह उतना ही कमजोर हालत में पहुंचता जाता है।
भारत के लोकसभा में मुस्लिम समुदाय से आने वाले सांसदों की कमी और यहां तक कि सरकार में नदारद प्रतिनिधित्व इसी राजनीतिक-अर्थशास्त्र की जमीन पर खड़ा है। यह एक दिन में नहीं बनता है। इसके बनने की एक पूरी प्रक्रिया है और इसे बनाने का एक पूरा ढांचा होता है। यह एक राजनीति है जो एक चली आ रही नीतियों के बीच से उभरती है और इस प्रक्रिया को ही एक विचारधारा में बदल देती है।
(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)